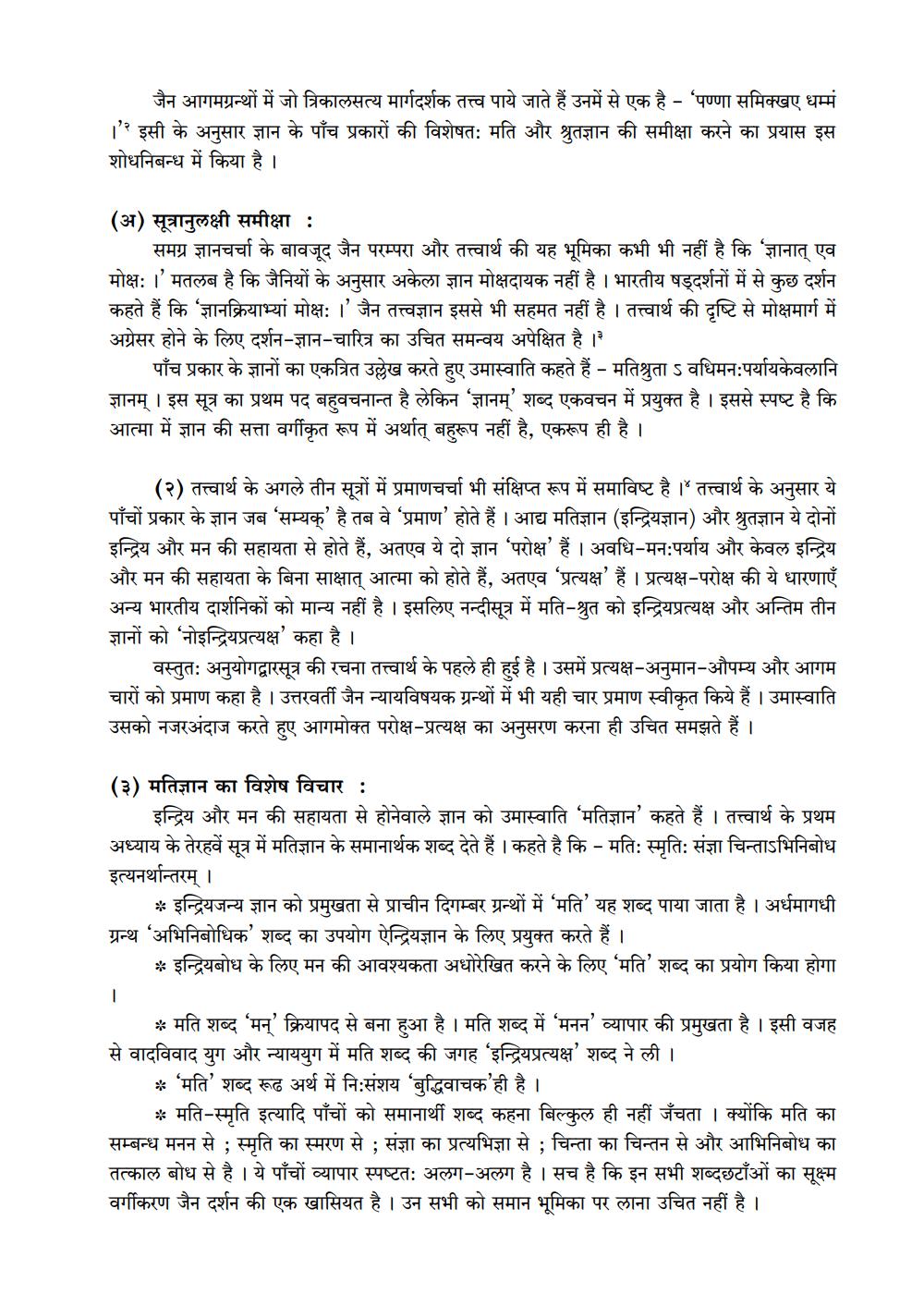Book Title: Tattvartha Sutra me Nihit Gyan Charcha Ek Nirikshan Author(s): Kaumudi Baldota Publisher: Kaumudi Baldota View full book textPage 3
________________ जैन आगमग्रन्थों में जो त्रिकालसत्य मार्गदर्शक तत्त्व पाये जाते हैं उनमें से एक है - ‘पण्णा समिक्खए धम्म ।' इसी के अनुसार ज्ञान के पाँच प्रकारों की विशेषत: मति और श्रुतज्ञान की समीक्षा करने का प्रयास इस शोधनिबन्ध में किया है। (अ) सूत्रानुलक्षी समीक्षा : समग्र ज्ञानचर्चा के बावजूद जैन परम्परा और तत्त्वार्थ की यह भूमिका कभी भी नहीं है कि 'ज्ञानात् एव मोक्षः ।' मतलब है कि जैनियों के अनुसार अकेला ज्ञान मोक्षदायक नहीं है । भारतीय षड्दर्शनों में से कुछ दर्शन कहते हैं कि 'ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः ।' जैन तत्त्वज्ञान इससे भी सहमत नहीं है । तत्त्वार्थ की दृष्टि से मोक्षमार्ग में अग्रेसर होने के लिए दर्शन-ज्ञान-चारित्र का उचित समन्वय अपेक्षित है । __ पाँच प्रकार के ज्ञानों का एकत्रित उल्लेख करते हुए उमास्वाति कहते हैं - मतिश्रुता ऽ वधिमन:पर्यायकेवलानि ज्ञानम् । इस सूत्र का प्रथम पद बहुवचनान्त है लेकिन 'ज्ञानम्' शब्द एकवचन में प्रयुक्त है । इससे स्पष्ट है कि आत्मा में ज्ञान की सत्ता वर्गीकृत रूप में अर्थात् बहुरूप नहीं है, एकरूप ही है । (२) तत्त्वार्थ के अगले तीन सूत्रों में प्रमाणचर्चा भी संक्षिप्त रूप में समाविष्ट है । तत्त्वार्थ के अनुसार ये पाँचों प्रकार के ज्ञान जब ‘सम्यक्' है तब वे ‘प्रमाण' होते हैं । आद्य मतिज्ञान (इन्द्रियज्ञान) और श्रुतज्ञान ये दोनों इन्द्रिय और मन की सहायता से होते हैं, अतएव ये दो ज्ञान ‘परोक्ष' हैं । अवधि-मन:पर्याय और केवल इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात् आत्मा को होते हैं, अतएव 'प्रत्यक्ष' हैं । प्रत्यक्ष-परोक्ष की ये धारणाएँ अन्य भारतीय दार्शनिकों को मान्य नहीं है । इसलिए नन्दीसूत्र में मति-श्रुत को इन्द्रियप्रत्यक्ष और अन्तिम तीन ज्ञानों को 'नोइन्द्रियप्रत्यक्ष' कहा है। ___वस्तुत: अनुयोगद्वारसूत्र की रचना तत्त्वार्थ के पहले ही हुई है । उसमें प्रत्यक्ष-अनुमान-औपम्य और आगम चारों को प्रमाण कहा है । उत्तरवर्ती जैन न्यायविषयक ग्रन्थों में भी यही चार प्रमाण स्वीकृत किये हैं । उमास्वाति उसको नजरअंदाज करते हुए आगमोक्त परोक्ष-प्रत्यक्ष का अनुसरण करना ही उचित समझते हैं । (३) मतिज्ञान का विशेष विचार : । इन्द्रिय और मन की सहायता से होनेवाले ज्ञान को उमास्वाति ‘मतिज्ञान' कहते हैं । तत्त्वार्थ के प्रथम अध्याय के तेरहवें सूत्र में मतिज्ञान के समानार्थक शब्द देते हैं । कहते है कि - मति: स्मृति: संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् । * इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रमुखता से प्राचीन दिगम्बर ग्रन्थों में ‘मति' यह शब्द पाया जाता है । अर्धमागधी ग्रन्थ 'अभिनिबोधिक' शब्द का उपयोग ऐन्द्रियज्ञान के लिए प्रयुक्त करते हैं। * इन्द्रियबोध के लिए मन की आवश्यकता अधोरेखित करने के लिए ‘मति' शब्द का प्रयोग किया होगा * मति शब्द ‘मन्' क्रियापद से बना हुआ है । मति शब्द में ‘मनन' व्यापार की प्रमुखता है । इसी वजह से वादविवाद युग और न्याययुग में मति शब्द की जगह ‘इन्द्रियप्रत्यक्ष' शब्द ने ली । * ‘मति' शब्द रूढ अर्थ में नि:संशय 'बुद्धिवाचक'ही है। * मति-स्मृति इत्यादि पाँचों को समानार्थी शब्द कहना बिल्कुल ही नहीं जंचता । क्योंकि मति का सम्बन्ध मनन से ; स्मृति का स्मरण से ; संज्ञा का प्रत्यभिज्ञा से ; चिन्ता का चिन्तन से और आभिनिबोध का तत्काल बोध से है । ये पाँचों व्यापार स्पष्टत: अलग-अलग है। सच है कि इन सभी शब्दछटाँओं का सूक्ष्म वर्गीकरण जैन दर्शन की एक खासियत है । उन सभी को समान भूमिका पर लाना उचित नहीं है।Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14