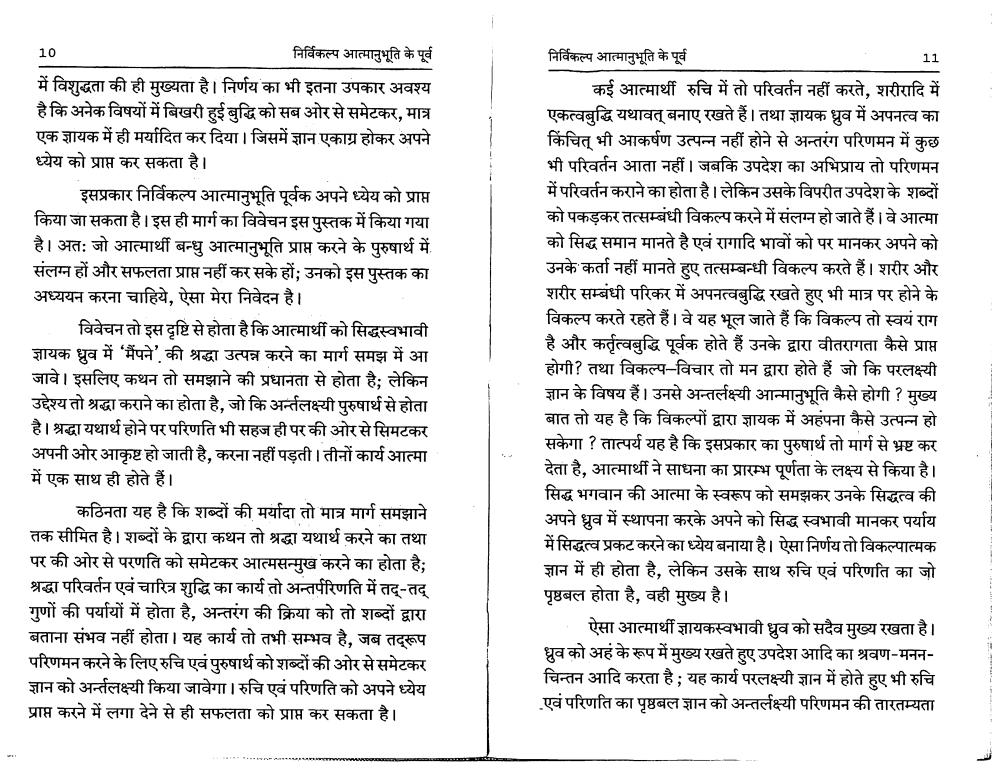Book Title: Nirvikalp Atmanubhuti ke Purv Author(s): Nemichand Patni Publisher: Todarmal Granthamala Jaipur View full book textPage 6
________________ निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व विशुद्धता की ही मुख्यता है। निर्णय का भी इतना उपकार अवश्य है कि अनेक विषयों में बिखरी हुई बुद्धि को सब ओर से समेटकर, मात्र एक ज्ञायक में ही मर्यादित कर दिया। जिसमें ज्ञान एकाग्र होकर अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। 10 इसप्रकार निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक अपने ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है। इस ही मार्ग का विवेचन इस पुस्तक में किया गया है। अतः जो आत्मार्थी बन्धु आत्मानुभूति प्राप्त करने के पुरुषार्थ में संलग्न हों और सफलता प्राप्त नहीं कर सके हों; उनको इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिये, ऐसा मेरा निवेदन है। विवेचन तो इस दृष्टि से होता है कि आत्मार्थी को सिद्धस्वभावी ज्ञायक ध्रुव में 'मैंने' की श्रद्धा उत्पन्न करने का मार्ग समझ में आ जावे। इसलिए कथन तो समझाने की प्रधानता से होता है; लेकिन उद्देश्य तो श्रद्धा कराने का होता है, जो कि अर्न्तलक्ष्यी पुरुषार्थ से होता है। श्रद्धा यथार्थ होने पर परिणति भी सहज ही पर की ओर से सिमटकर अपनी ओर आकृष्ट हो जाती है, करना नहीं पड़ती। तीनों कार्य आत्मा में एक साथ ही होते हैं। कठिनता यह है कि शब्दों की मर्यादा तो मात्र मार्ग समझाने तक सीमित है। शब्दों के द्वारा कथन तो श्रद्धा यथार्थ करने का तथा पर की ओर से परणति को समेटकर आत्मसन्मुख करने का होता है; श्रद्धा परिवर्तन एवं चारित्र शुद्धि का कार्य तो अन्तर्परिणति में तद्-तद् गुणों की पर्यायों में होता है, अन्तरंग की क्रिया को तो शब्दों द्वारा बताना संभव नहीं होता। यह कार्य तो तभी सम्भव है, जब तद्रूप परिणमन करने के लिए रुचि एवं पुरुषार्थ को शब्दों की ओर से समेटकर ज्ञान को अर्न्तलक्ष्यी किया जावेगा। रुचि एवं परिणति को अपने ध्येय प्राप्त करने में लगा देने से ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व 11 कई आत्मार्थी रुचि में तो परिवर्तन नहीं करते, शरीरादि में एकत्वबुद्धि यथावत् बनाए रखते हैं। तथा ज्ञायक ध्रुव में अपनत्व का किंचित् भी आकर्षण उत्पन्न नहीं होने से अन्तरंग परिणमन में कुछ भी परिवर्तन आता नहीं। जबकि उपदेश का अभिप्राय तो परिणमन में परिवर्तन कराने का होता है। लेकिन उसके विपरीत उपदेश के शब्दों को पकड़कर तत्सम्बंधी विकल्प करने में संलग्न हो जाते हैं। वे आत्मा को सिद्ध समान मानते है एवं रागादि भावों को पर मानकर अपने को उनके कर्ता नहीं मानते हुए तत्सम्बन्धी विकल्प करते हैं। शरीर और शरीर सम्बंधी परिकर में अपनत्वबुद्धि रखते हुए भी मात्र पर होने के विकल्प करते रहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि विकल्प तो स्वयं राग है और कर्तृत्वबुद्धि पूर्वक होते हैं उनके द्वारा वीतरागता कैसे प्राप्त होगी ? तथा विकल्प-विचार तो मन द्वारा होते हैं जो कि परलक्ष्यी ज्ञान के विषय हैं। उनसे अन्तर्लक्ष्यी आन्मानुभूति कैसे होगी ? मुख्य बात तो यह है कि विकल्पों द्वारा ज्ञायक में अहंपना कैसे उत्पन्न हो सकेगा ? तात्पर्य यह है कि इसप्रकार का पुरुषार्थ तो मार्ग से भ्रष्ट कर देता है, आत्मार्थी ने साधना का प्रारम्भ पूर्णता के लक्ष्य से किया है। सिद्ध भगवान की आत्मा के स्वरूप को समझकर उनके सिद्धत्व की अपने ध्रुव में स्थापना करके अपने को सिद्ध स्वभावी मानकर पर्याय में सिद्धत्व प्रकट करने का ध्येय बनाया है। ऐसा निर्णय तो विकल्पात्मक ज्ञान में ही होता है, लेकिन उसके साथ रुचि एवं परिणति का जो पृष्ठबल होता है, वही मुख्य है। ऐसा आत्मार्थी ज्ञायकस्वभावी ध्रुव को सदैव मुख्य रखता है। ध्रुव को अहं के रूप में मुख्य रखते हुए उपदेश आदि का श्रवण-मननचिन्तन आदि करता है; यह कार्य परलक्ष्यी ज्ञान में होते हुए भी रुचि . एवं परिणति का पृष्ठबल ज्ञान को अन्तर्लक्ष्यी परिणमन की तारतम्यताPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 80