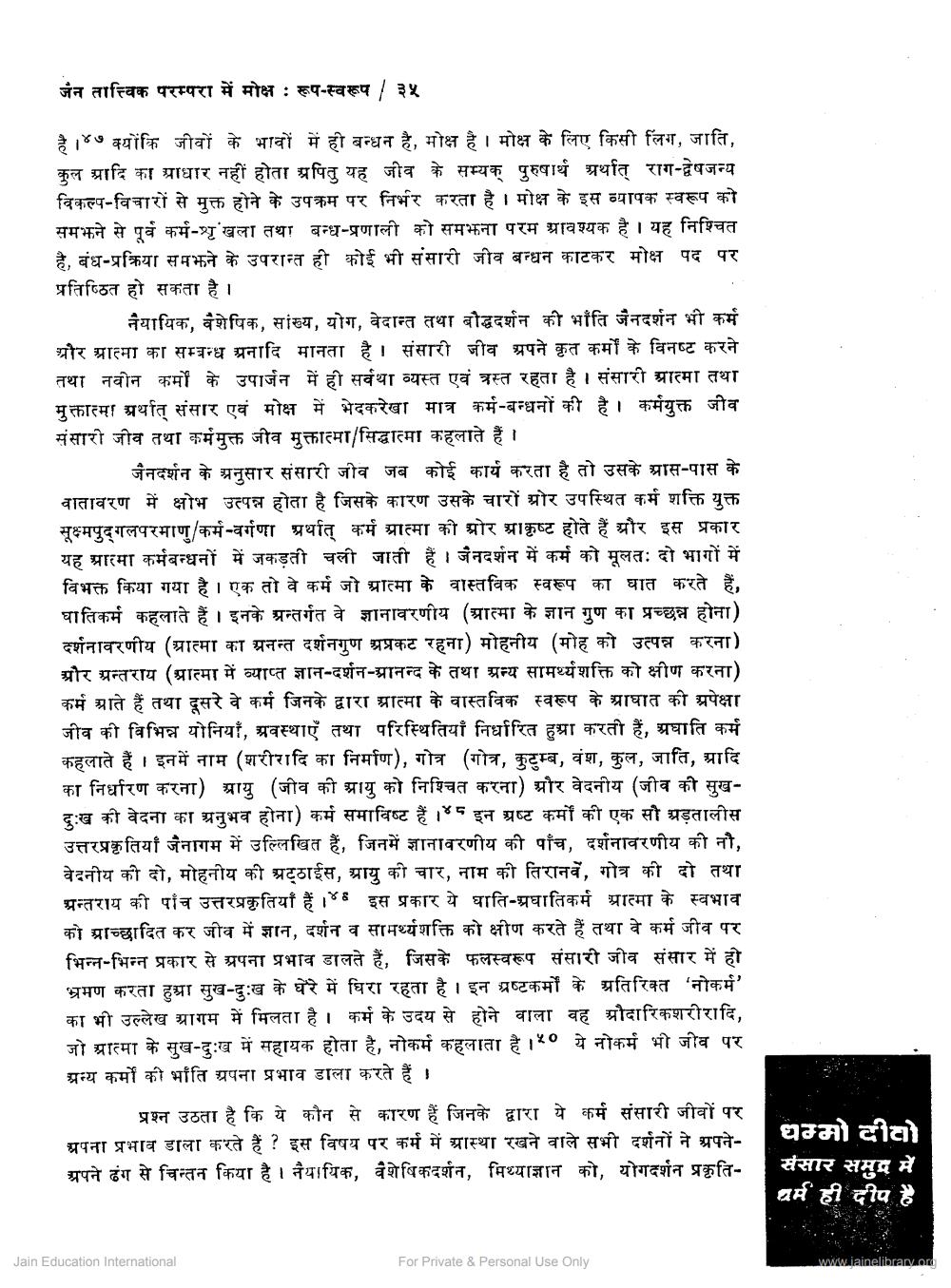Book Title: Jain Tattvika Paramparao me Swarup Moksharup Swarup Author(s): Rajiv Prachandiya Publisher: Z_Umravkunvarji_Diksha_Swarna_Jayanti_Smruti_Granth_012035.pdf View full book textPage 5
________________ जैन तात्त्विक परम्परा में मोक्ष : रूप-स्वरूप / ३५ है।४७ क्योंकि जीवों के भावों में ही बन्धन है, मोक्ष है। मोक्ष के लिए किसी लिंग, जाति, कुल आदि का प्राधार नहीं होता अपितु यह जीव के सम्यक् पुरुषार्थ अर्थात् राग-द्वेषजन्य विकल्प-विचारों से मुक्त होने के उपक्रम पर निर्भर करता है । मोक्ष के इस व्यापक स्वरूप को समझने से पूर्व कर्म-शृखला तथा बन्ध-प्रणाली को समझना परम आवश्यक है। यह निश्चित है, बंध-प्रक्रिया समझने के उपरान्त ही कोई भी संसारी जीव बन्धन काटकर मोक्ष पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त तथा बौद्धदर्शन की भाँति जैनदर्शन भी कर्म और आत्मा का सम्बन्ध अनादि मानता है। संसारी जीव अपने कृत कर्मों के विनष्ट करने तथा नवीन कर्मों के उपार्जन में ही सर्वथा व्यस्त एवं त्रस्त रहता है। संसारी आत्मा तथा मुक्तात्मा अर्थात् संसार एवं मोक्ष में भेदकरेखा मात्र कर्म-बन्धनों की है। कर्मयुक्त जीव संसारी जीव तथा कर्ममुक्त जीव मुक्तात्मा/सिद्धात्मा कहलाते हैं। जैनदर्शन के अनुसार संसारी जीव जब कोई कार्य करता है तो उसके आस-पास के वातावरण में क्षोभ उत्पन्न होता है जिसके कारण उसके चारों ओर उपस्थित कर्म शक्ति युक्त सूक्ष्मपुद्गलपरमाणु कर्म-वर्गणा अर्थात् कर्म आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं और इस प्रकार यह प्रारमा कर्मबन्धनों में जकड़ती चली जाती हैं। जैनदर्शन में कर्म को मूलतः दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो वे कर्म जो प्रात्मा के वास्तविक स्वरूप का घात करते हैं, घातिकर्म कहलाते हैं । इनके अन्तर्गत वे ज्ञानावरणीय (आत्मा के ज्ञान गुण का प्रच्छन्न होना) दर्शनावरणीय (प्रात्मा का अनन्त दर्शनगुण अप्रकट रहना) मोहनीय (मोह को उत्पन्न करना) और अन्तराय (प्रात्मा में व्याप्त ज्ञान-दर्शन-पानन्द के तथा अन्य सामर्थ्य शक्ति को क्षीण करना) कर्म पाते हैं तथा दूसरे वे कर्म जिनके द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप के प्राघात की अपेक्षा जीव की विभिन्न योनियाँ, अवस्थाएँ तथा परिस्थितियाँ निर्धारित हुआ करती हैं, अघाति कर्म कहलाते हैं । इनमें नाम (शरीरादि का निर्माण), गोत्र (गोत्र, कुटुम्ब, वंश, कुल, जाति, आदि का निर्धारण करना) आयु (जीव की आयु को निश्चित करना) और वेदनीय (जीव की सुखदुःख की वेदना का अनुभव होना) कर्म समाविष्ट हैं।४८ इन प्रष्ट कर्मों की एक सौ अड़तालीस उत्तरप्रकृतियाँ जैनागम में उल्लिखित हैं, जिनमें ज्ञानावरणीय की पाँच, दर्शनावरणीय की नौ, वेदनीय की दो, मोहनीय की अट्ठाईस, आयु की चार, नाम की तिरानवे, गोत्र की दो तथा अन्तराय की पाँच उत्तरप्रकृतियाँ हैं।४६ इस प्रकार ये घाति-प्रघातिकर्म प्रात्मा के स्वभाव को पाच्छादित कर जीव में ज्ञान, दर्शन व सामर्थ्यशक्ति को क्षीण करते हैं तथा वे कर्म जीव पर भिन्न-भिन्न प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके फलस्वरूप संसारी जीव संसार में हो भ्रमण करता हुआ सुख-दुःख के घेरे में घिरा रहता है । इन प्रष्टकर्मों के अतिरिक्त 'नोकर्म' का भी उल्लेख आगम में मिलता है। कर्म के उदय से होने वाला वह औदारिकशरीरादि, जो प्रात्मा के सुख-दुःख में सहायक होता है, नोकर्म कहलाता है।५० ये नोकर्म भी जीव पर अन्य कर्मों की भाँति अपना प्रभाव डाला करते हैं । प्रश्न उठता है कि ये कौन से कारण हैं जिनके द्वारा ये कर्म संसारी जीवों पर अपना प्रभाव डाला करते हैं ? इस विषय पर कर्म में आस्था रखने वाले सभी दर्शनों ने अपनेअपने ढंग से चिन्तन किया है। नैयायिक, वैशेषिकदर्शन, मिथ्याज्ञान को, योगदर्शन प्रकृति धम्मो दीटो संसार समुद्र में धर्म ही दीप है Jain Education International For Private & Personal Use OnlyPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16