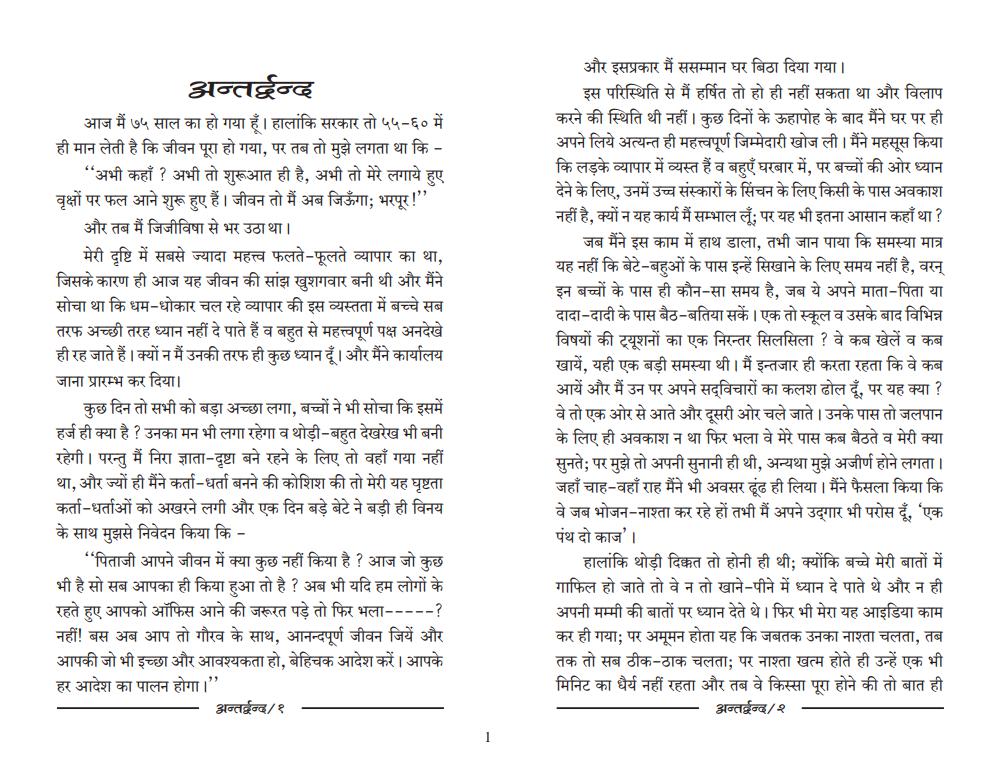Book Title: Antardvand Author(s): Parmatmaprakash Bharilla Publisher: Hukamchand Bharilla Charitable Trust Mumbai View full book textPage 4
________________ अन्तर्द्वन्द आज मैं ७५ साल का हो गया हैं। हालांकि सरकार तो ५५-६० में ही मान लेती है कि जीवन पूरा हो गया, पर तब तो मुझे लगता था कि - “अभी कहाँ ? अभी तो शुरूआत ही है, अभी तो मेरे लगाये हुए वृक्षों पर फल आने शुरू हुए हैं। जीवन तो मैं अब जिऊँगा; भरपूर!" और तब मैं जिजीविषा से भर उठा था। मेरी दृष्टि में सबसे ज्यादा महत्त्व फलते-फूलते व्यापार का था, जिसके कारण ही आज यह जीवन की सांझ खुशगवार बनी थी और मैंने सोचा था कि धम-धोकार चल रहे व्यापार की इस व्यस्तता में बच्चे सब तरफ अच्छी तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं व बहुत से महत्त्वपूर्ण पक्ष अनदेखे ही रह जाते हैं। क्यों न मैं उनकी तरफ ही कुछ ध्यान दूँ। और मैंने कार्यालय जाना प्रारम्भ कर दिया। ____ कुछ दिन तो सभी को बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने भी सोचा कि इसमें हर्ज ही क्या है ? उनका मन भी लगा रहेगा व थोड़ी-बहुत देखरेख भी बनी रहेगी। परन्तु मैं निरा ज्ञाता-दृष्टा बने रहने के लिए तो वहाँ गया नहीं था, और ज्यों ही मैंने कर्ता-धर्ता बनने की कोशिश की तो मेरी यह घृष्टता कर्ता-धर्ताओं को अखरने लगी और एक दिन बड़े बेटे ने बड़ी ही विनय के साथ मुझसे निवेदन किया कि - “पिताजी आपने जीवन में क्या कुछ नहीं किया है ? आज जो कुछ भी है सो सब आपका ही किया हुआ तो है ? अब भी यदि हम लोगों के रहते हुए आपको ऑफिस आने की जरूरत पड़े तो फिर भला-----? नहीं! बस अब आप तो गौरव के साथ, आनन्दपूर्ण जीवन जियें और आपकी जो भी इच्छा और आवश्यकता हो, बेहिचक आदेश करें। आपके हर आदेश का पालन होगा।" अन्तर्द्वन्द/१ और इसप्रकार मैं ससम्मान घर बिठा दिया गया। इस परिस्थिति से मैं हर्षित तो हो ही नहीं सकता था और विलाप करने की स्थिति थी नहीं। कुछ दिनों के ऊहापोह के बाद मैंने घर पर ही अपने लिये अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी खोज ली। मैंने महसूस किया कि लड़के व्यापार में व्यस्त हैं व बहुएँ घरबार में, पर बच्चों की ओर ध्यान देने के लिए, उनमें उच्च संस्कारों के सिंचन के लिए किसी के पास अवकाश नहीं है, क्यों न यह कार्य मैं सम्भाल लूँ; पर यह भी इतना आसान कहाँ था? जब मैंने इस काम में हाथ डाला, तभी जान पाया कि समस्या मात्र यह नहीं कि बेटे-बहुओं के पास इन्हें सिखाने के लिए समय नहीं है, वरन् इन बच्चों के पास ही कौन-सा समय है, जब ये अपने माता-पिता या दादा-दादी के पास बैठ-बतिया सकें । एक तो स्कूल व उसके बाद विभिन्न विषयों की ट्यूशनों का एक निरन्तर सिलसिला ? वे कब खेलें व कब खायें, यही एक बड़ी समस्या थी। मैं इन्तजार ही करता रहता कि वे कब आयें और मैं उन पर अपने सद्विचारों का कलश ढोल दूँ, पर यह क्या ? वे तो एक ओर से आते और दूसरी ओर चले जाते । उनके पास तो जलपान के लिए ही अवकाश न था फिर भला वे मेरे पास कब बैठते व मेरी क्या सुनते; पर मुझे तो अपनी सुनानी ही थी, अन्यथा मुझे अजीर्ण होने लगता। जहाँ चाह-वहाँ राह मैंने भी अवसर ढूंढ ही लिया। मैंने फैसला किया कि वे जब भोजन-नाश्ता कर रहे हों तभी मैं अपने उद्गार भी परोस दूँ, 'एक पंथ दो काज'। हालांकि थोड़ी दिक्कत तो होनी ही थी; क्योंकि बच्चे मेरी बातों में गाफिल हो जाते तो वे न तो खाने-पीने में ध्यान दे पाते थे और न ही अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान देते थे। फिर भी मेरा यह आइडिया काम कर ही गया; पर अमूमन होता यह कि जबतक उनका नाश्ता चलता, तब तक तो सब ठीक-ठाक चलता; पर नाश्ता खत्म होते ही उन्हें एक भी मिनिट का धैर्य नहीं रहता और तब वे किस्सा पूरा होने की तो बात ही - अन्तर्द्वन्द/२ -Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36