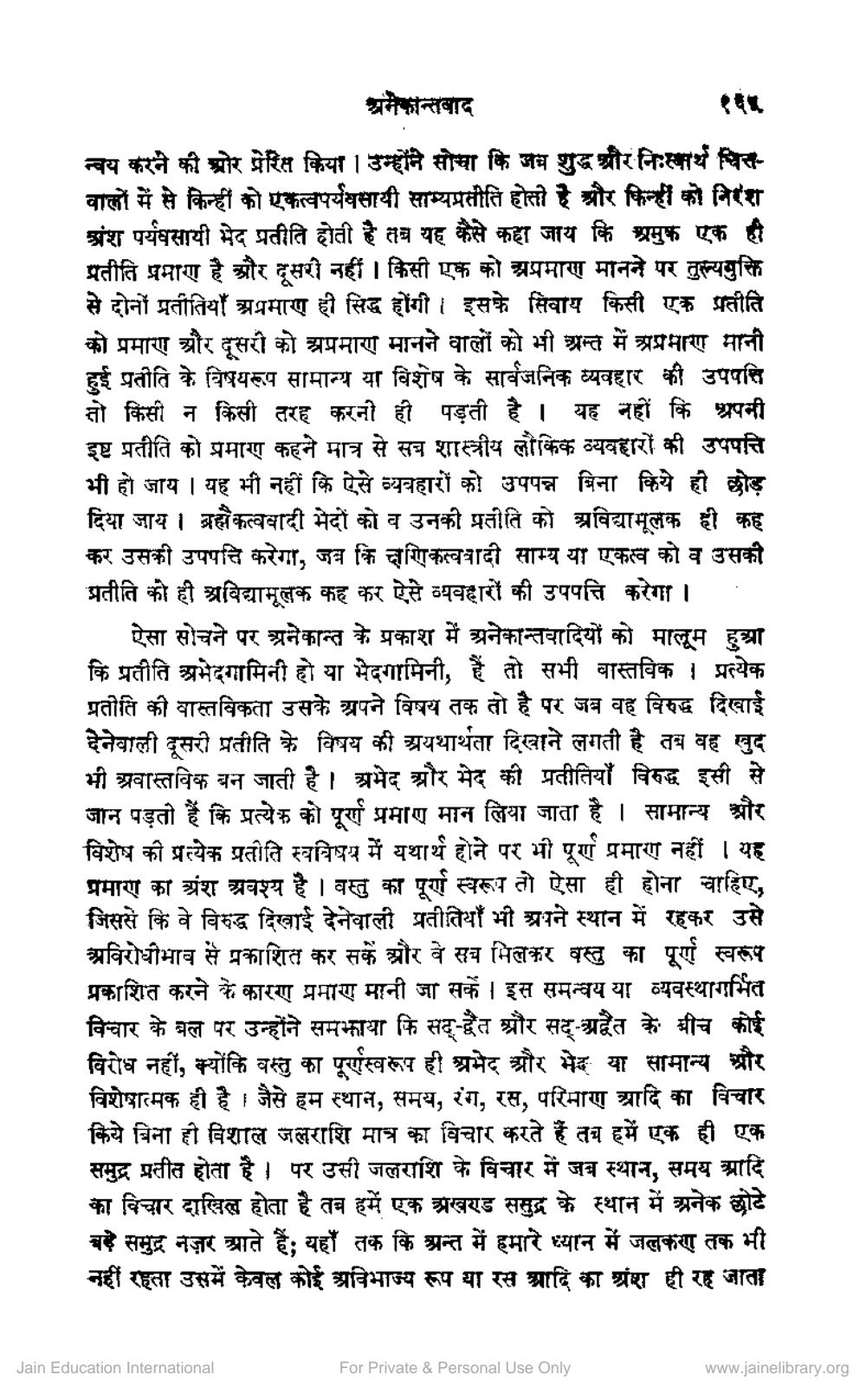Book Title: Anekantvada Author(s): Sukhlal Sanghavi Publisher: Z_Darshan_aur_Chintan_Part_1_2_002661.pdf View full book textPage 5
________________ श्रीकान्तवाद १५५ न्वय करने की ओर प्रेरित किया । उन्होंने सोचा कि अब शुद्ध और नि:स्वार्थ चिसवालों में से किन्हीं को एकत्वपर्यवसायी साभ्यप्रतीति होती है और किन्हीं को निरश अंश पर्यवसायी भेद प्रतीति होती है तब यह कैसे कहा जाय कि अमुक एक ही प्रतीति प्रमाण है और दूसरी नहीं। किसी एक को अप्रमाण मानने पर तुल्ययुक्ति से दोनों प्रतीतियाँ अप्रमाण ही सिद्ध होंगी। इसके सिवाय किसी एक प्रतीति को प्रमाण और दूसरी को अप्रमाण मानने वालों को भी अन्त में अप्रमाण मानी हुई प्रतीति के विषयरूप सामान्य या विशेष के सार्वजनिक व्यवहार की उपपत्ति तो किसी न किसी तरह करनी ही पड़ती है । यह नहीं कि अपनी इष्ट प्रतीति को प्रमाण कहने मात्र से सब शास्त्रीय लौकिक व्यवहारों की उपपत्ति भी हो जाय । यह भी नहीं कि ऐसे व्यवहारों को उपपन्न बिना किये ही छोड़ दिया जाय । ब्रह्मकत्ववादी भेदों को व उनकी प्रतीति को अविद्यामूलक ही कह कर उसकी उपपत्ति करेगा, जब कि क्षणिकत्ववादी साम्य या एकत्व को व उसकी प्रतीति को ही अविद्यामूलक कह कर ऐसे व्यवहारों की उपपत्ति करेगा। ऐसा सोचने पर अनेकान्त के प्रकाश में अनेकान्तवादियों को मालूम हुआ कि प्रतीति अभेदगामिनी हो या भेदगामिनी, हैं तो सभी वास्तविक । प्रत्येक प्रतीति की वास्तविकता उसके अपने विषय तक तो है पर जब वह विरुद्ध दिखाई देनेवाली दूसरी प्रतीति के विषय की अयथार्थता दिखाने लगती है तब वह खुद भी अवास्तविक बन जाती है। अभेद और भेद की प्रतीतियाँ विरुद्ध इसी से जान पड़ती हैं कि प्रत्येक को पूर्ण प्रमाण मान लिया जाता है । सामान्य और विशेष की प्रत्येक प्रतीति स्वविषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण नहीं । यह प्रमाण का अंश अवश्य है । वस्तु का पूर्ण स्वरूप तो ऐसा ही होना चाहिए, जिससे कि वे विरुद्ध दिखाई देनेवाली प्रतीतियाँ भी अपने स्थान में रहकर उसे अविरोधीभाव से प्रकाशित कर सके और वे सब मिलकर वस्तु का पूर्ण स्वरूप प्रकाशित करने के कारण प्रमाण मानी जा सकें । इस समन्वय या व्यवस्थागर्भित विचार के बल पर उन्होंने समझाया कि सद्-द्वैत और सद्-अद्वैत के बीच कोई विरोध नहीं, क्योंकि वस्तु का पूर्णस्वरूप ही अभेद और भेद या सामान्य और विशेषात्मक ही है । जैसे हम स्थान, समय, रंग, रस, परिमाण आदि का विचार किये बिना ही विशाल जलराशि मात्र का विचार करते हैं तब हमें एक ही एक समुद्र प्रतीत होता है। पर उसी जलराशि के विचार में जब स्थान, समय आदि का विचार दाखिल होता है तब हमें एक अखण्ड ससुद्र के स्थान में अनेक छोटे बड़े समुद्र नज़र आते हैं; यहाँ तक कि अन्त में हमारे ध्यान में जलकण तक भी नहीं रहता उसमें केवल कोई अविभाज्य रूप या रस आदि का अंश ही रह जाता Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13