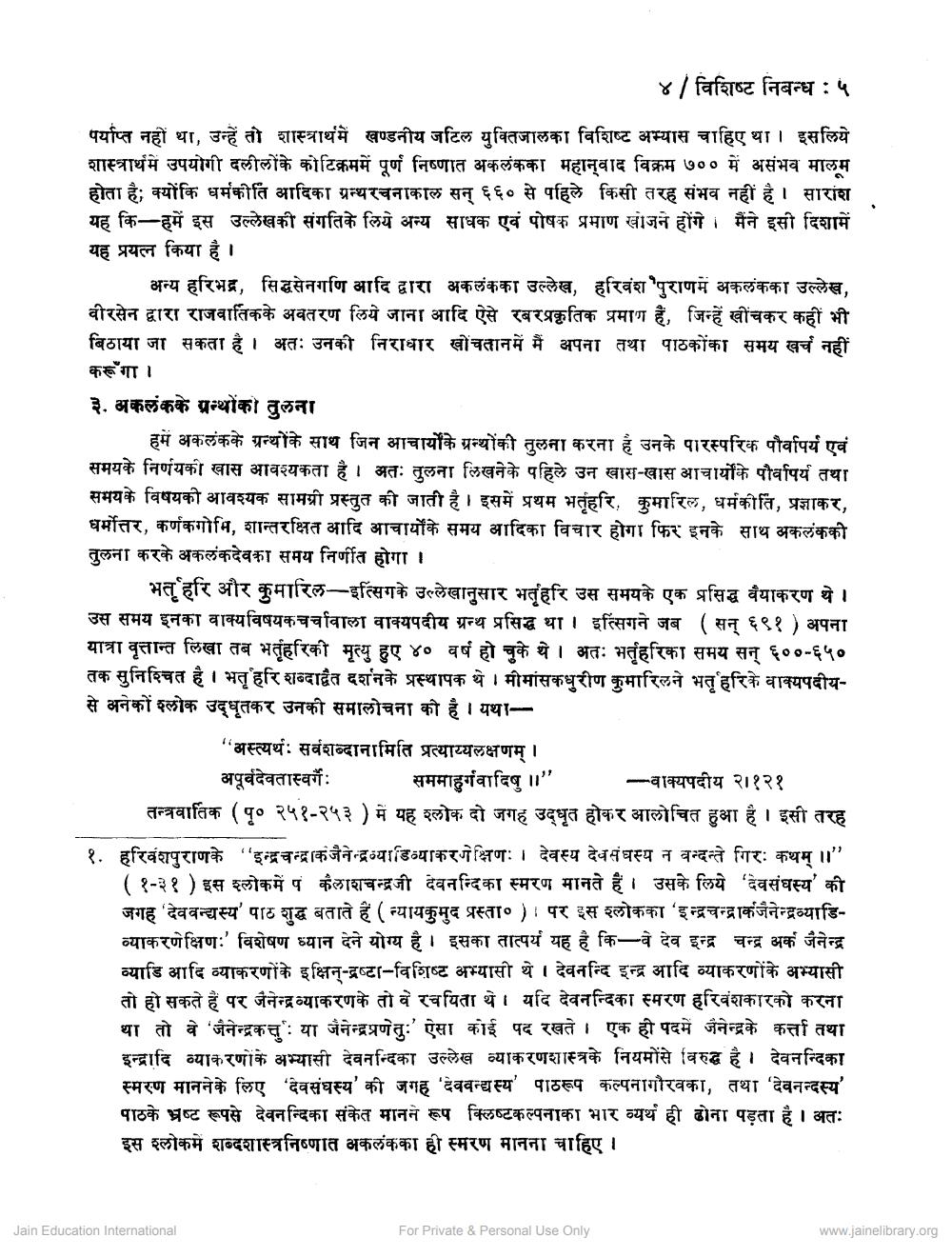Book Title: Akalank Granthtraya aur uske Karta Author(s): Akalankadev Publisher: Z_Mahendrakumar_Jain_Nyayacharya_Smruti_Granth_012005.pdf View full book textPage 5
________________ ४ / विशिष्ट निबन्ध : ५ पर्याप्त नहीं था, उन्हें तो शास्त्रार्थ में खण्डनीय जटिल युक्तिजालका विशिष्ट अभ्यास चाहिए था । इसलिये शास्त्रार्थ में उपयोगी दलीलोंके कोटिक्रम में पूर्ण निष्णात अकलंकका महान्वाद विक्रम ७०० में असंभव मालूम होता है; क्योंकि धर्मकीर्ति आदिका ग्रन्थरचनाकाल सन् ६६० से पहिले किसी तरह संभव नहीं है । सारांश यह कि हमें इस उल्लेखकी संगति के लिये अन्य साधक एवं पोषक प्रमाण खोजने होंगे। मैंने इसी दिशामें यह प्रयत्न किया है । अन्य हरिभद्र, सिद्धसेनगणि आदि द्वारा अकलंकका उल्लेख, हरिवंश पुराणम अकलंकका उल्लेख, वीरसेन द्वारा राजवार्तिक के अवतरण लिये जाना आदि ऐसे रबरप्रकृतिक प्रमाण हैं, जिन्हें खींचकर कहीं भी बिठाया जा सकता । अतः उनकी निराधार खींचतान में मैं अपना तथा पाठकोंका समय खर्च नहीं करूँगा । ३. अकलंकके ग्रन्थोंको तुलना हमें अकलंकके ग्रन्थों के साथ जिन आचार्योंके ग्रन्थोंकी तुलना करना है उनके पारस्परिक पौर्वापर्य एवं समय निर्णयकी खास आवश्यकता है । अतः तुलना लिखनेके पहिले उन खास खास आचार्यों के पौर्वापर्य तथा समय के विषयकी आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की जाती है। इसमें प्रथम भर्तृहरि कुमारिल, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, कर्णकगोमि, शान्तरक्षित आदि आचार्योंके समय आदिका विचार होगा फिर इनके साथ अकलंककी तुलना करके अकलंकदेवका समय निर्णीत होगा । भर्तृहरि और कुमारिल - इत्सिंग के उल्लेखानुसार भर्तृहरि उस समयके एक प्रसिद्ध वैयाकरण थे । उस समय इनका वाक्य विषयक चर्चावाला वाक्यपदीय ग्रन्थ प्रसिद्ध था । इत्सिंगने जब ( सन् ६९९ ) अपना यात्रा वृत्तान्त लिखा तब भर्तृहरिकी मृत्यु हुए ४० वर्षं हो चुके थे । अतः भर्तृहरिका समय सन् ६००-६५० तक सुनिश्चित है । भतृहरि शब्दाद्वैत दर्शन के प्रस्थापक थे । मीमांसकधुरीण कुमारिलने भर्तृहरिके वाक्यपदीयसे अनेकों श्लोक उद्धृतकर उनकी समालोचना की है । यथा "अस्त्यर्थः सर्वशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम् । अपूर्वदेवतास्वगै: सममाहुर्गवादिषु ।।" - वाक्यपदीय २।१२१ तन्त्रवार्तिक ( पृ० २५१ - २५३ ) में यह श्लोक दो जगह उद्धृत होकर आलोचित हुआ है । इसी तरह १. हरिवंशपुराणके "इन्द्रचन्द्राक जैनेन्द्रव्याडिव्याकरक्षिणः । देवस्य देवसंघस्य न वन्दन्ते गिरः कथम् ॥” ( १-३१ ) इस श्लोक में पं कैलाशचन्द्रजी देवनन्दिका स्मरण मानते हैं । उसके लिये 'देवसंघस्य' की जगह 'देववन्द्यस्य' पाठ शुद्ध बताते हैं (न्यायकुमुद प्रस्ता० ) । पर इस श्लोक का 'इन्द्रचन्द्रार्कजैनेन्द्रव्याडिव्याकरणेक्षिणः' विशेषण ध्यान देने योग्य है । इसका तात्पर्य यह है कि वे देव इन्द्र चन्द्र अर्क जैनेन्द्र व्याडि आदि व्याकरणोंके इक्षिन् द्रष्टा - विशिष्ट अभ्यासी थे । देवनन्दि इन्द्र आदि व्याकरणोंके अभ्यासी तो हो सकते हैं पर जैनेन्द्र व्याकरणके तो वे रचयिता थे। यदि देवनन्दिका स्मरण हरिवंशकारको करना था तो वे 'जैनेन्द्रकत्तुः या जैनेन्द्रप्रणेतुः' ऐसा कोई पद रखते । एक ही पदमें जैनेन्द्रके कर्त्ता तथा इन्द्रादि व्याकरणोंके अभ्यासी देवनन्दिका उल्लेख व्याकरणशास्त्र के नियमोंसे विरुद्ध है । देवनन्दिका स्मरण मानने के लिए 'देवसंघस्य' की जगह 'देववन्द्यस्य' पाठरूप कल्पनागौरवका, तथा 'देवनन्दस्य' पाठके भ्रष्ट रूपसे देवनन्दिका संकेत मानने रूप क्लिष्टकल्पनाका भार व्यर्थ ही ढोना पड़ता है । अतः इस श्लोक में शब्दशास्त्रनिष्णात अकलंकका ही स्मरण मानना चाहिए । Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 73