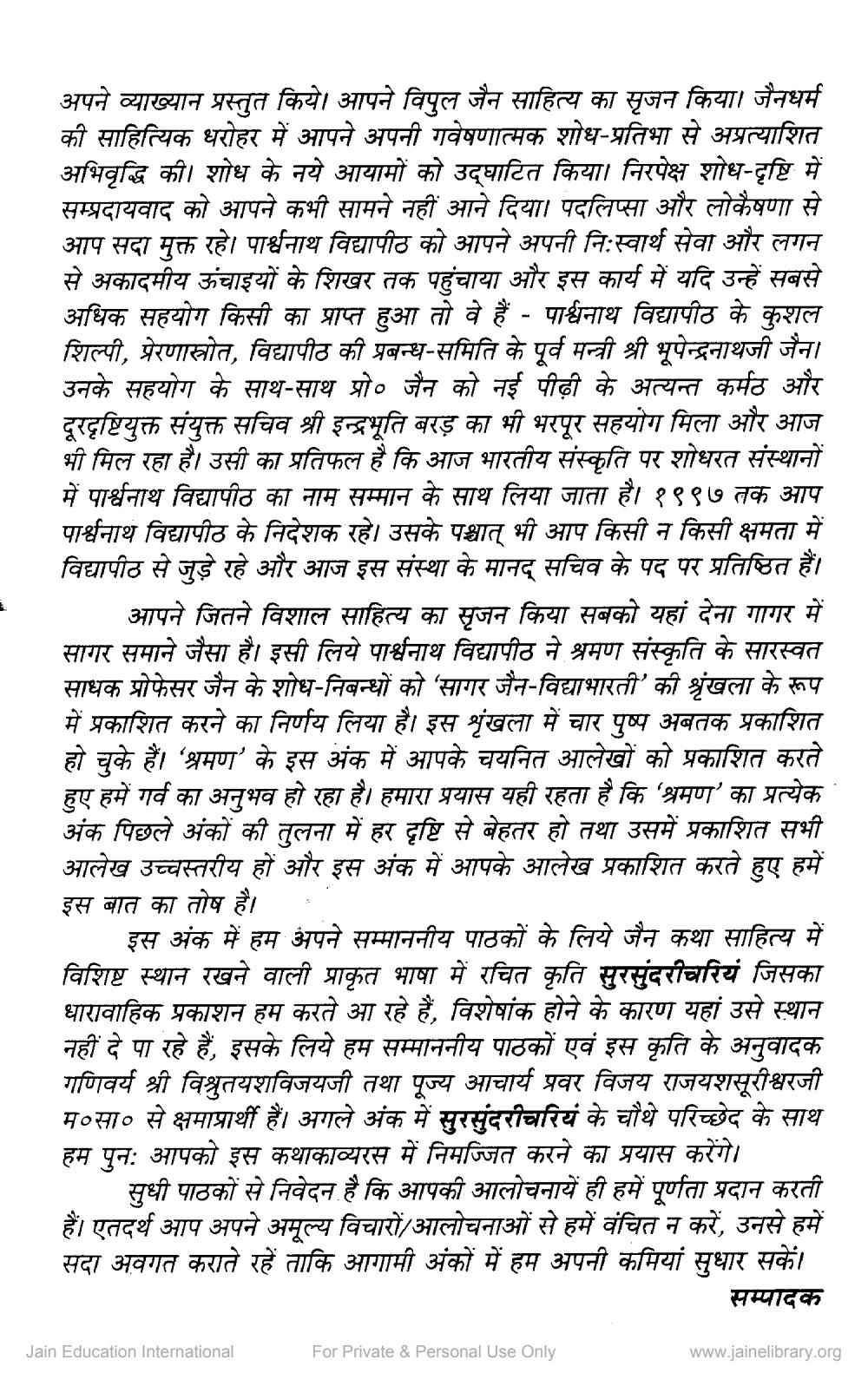Book Title: Sramana 2005 07 10 Author(s): Shreeprakash Pandey Publisher: Parshvanath Vidhyashram Varanasi View full book textPage 6
________________ अपने व्याख्यान प्रस्तुत किये। आपने विपुल जैन साहित्य का सृजन किया। जैनधर्म की साहित्यिक धरोहर में आपने अपनी गवेषणात्मक शोध-प्रतिभा से अप्रत्याशित अभिवृद्धि की। शोध के नये आयामों को उद्घाटित किया। निरपेक्ष शोध-दृष्टि में सम्प्रदायवाद को आपने कभी सामने नहीं आने दिया। पदलिप्सा और लोकैषणा से आप सदा मुक्त रहे। पार्श्वनाथ विद्यापीठ को आपने अपनी नि:स्वार्थ सेवा और लगन से अकादमीय ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाया और इस कार्य में यदि उन्हें सबसे अधिक सहयोग किसी का प्राप्त हुआ तो वे हैं - पार्श्वनाथ विद्यापीठ के कुशल शिल्पी, प्रेरणास्रोत, विद्यापीठ की प्रबन्ध-समिति के पूर्व मन्त्री श्री भूपेन्द्रनाथजी जैन। उनके सहयोग के साथ-साथ प्रो० जैन को नई पीढ़ी के अत्यन्त कर्मठ और दूरदृष्टियुक्त संयुक्त सचिव श्री इन्द्रभूति बरड़ का भी भरपूर सहयोग मिला और आज भी मिल रहा है। उसी का प्रतिफल है कि आज भारतीय संस्कृति पर शोधरत संस्थानों में पार्श्वनाथ विद्यापीठ का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। १९९७ तक आप पार्श्वनाथ विद्यापीठ के निदेशक रहे। उसके पश्चात् भी आप किसी न किसी क्षमता में विद्यापीठ से जुड़े रहे और आज इस संस्था के मानद् सचिव के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपने जितने विशाल साहित्य का सृजन किया सबको यहां देना गागर में सागर समाने जैसा है। इसी लिये पार्श्वनाथ विद्यापीठ ने श्रमण संस्कृति के सारस्वत साधक प्रोफेसर जैन के शोध-निबन्धों को 'सागर जैन-विद्याभारती' की श्रृंखला के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। इस श्रृंखला में चार पुष्प अबतक प्रकाशित हो चुके हैं। 'श्रमण' के इस अंक में आपके चयनित आलेखों को प्रकाशित करते हुए हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। हमारा प्रयास यही रहता है कि 'श्रमण' का प्रत्येक अंक पिछले अंकों की तुलना में हर दृष्टि से बेहतर हो तथा उसमें प्रकाशित सभी आलेख उच्चस्तरीय हों और इस अंक में आपके आलेख प्रकाशित करते हुए हमें इस बात का तोष है। . इस अंक में हम अपने सम्माननीय पाठकों के लिये जैन कथा साहित्य में विशिष्ट स्थान रखने वाली प्राकृत भाषा में रचित कृति सुरसुंदरीचरियं जिसका धारावाहिक प्रकाशन हम करते आ रहे हैं, विशेषांक होने के कारण यहां उसे स्थान नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिये हम सम्माननीय पाठकों एवं इस कृति के अनुवादक गणिवर्य श्री विश्रुतयशविजयजी तथा पूज्य आचार्य प्रवर विजय राजयशसूरीश्वरजी म०सा० से क्षमाप्रार्थी हैं। अगले अंक में सुरसुंदरीचरियं के चौथे परिच्छेद के साथ हम पुन: आपको इस कथाकाव्यरस में निमज्जित करने का प्रयास करेंगे। सुधी पाठकों से निवेदन है कि आपकी आलोचनायें ही हमें पूर्णता प्रदान करती हैं। एतदर्थ आप अपने अमूल्य विचारों/आलोचनाओं से हमें वंचित न करें, उनसे हमें सदा अवगत कराते रहें ताकि आगामी अंकों में हम अपनी कमियां सुधार सकें। सम्पादक Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 226