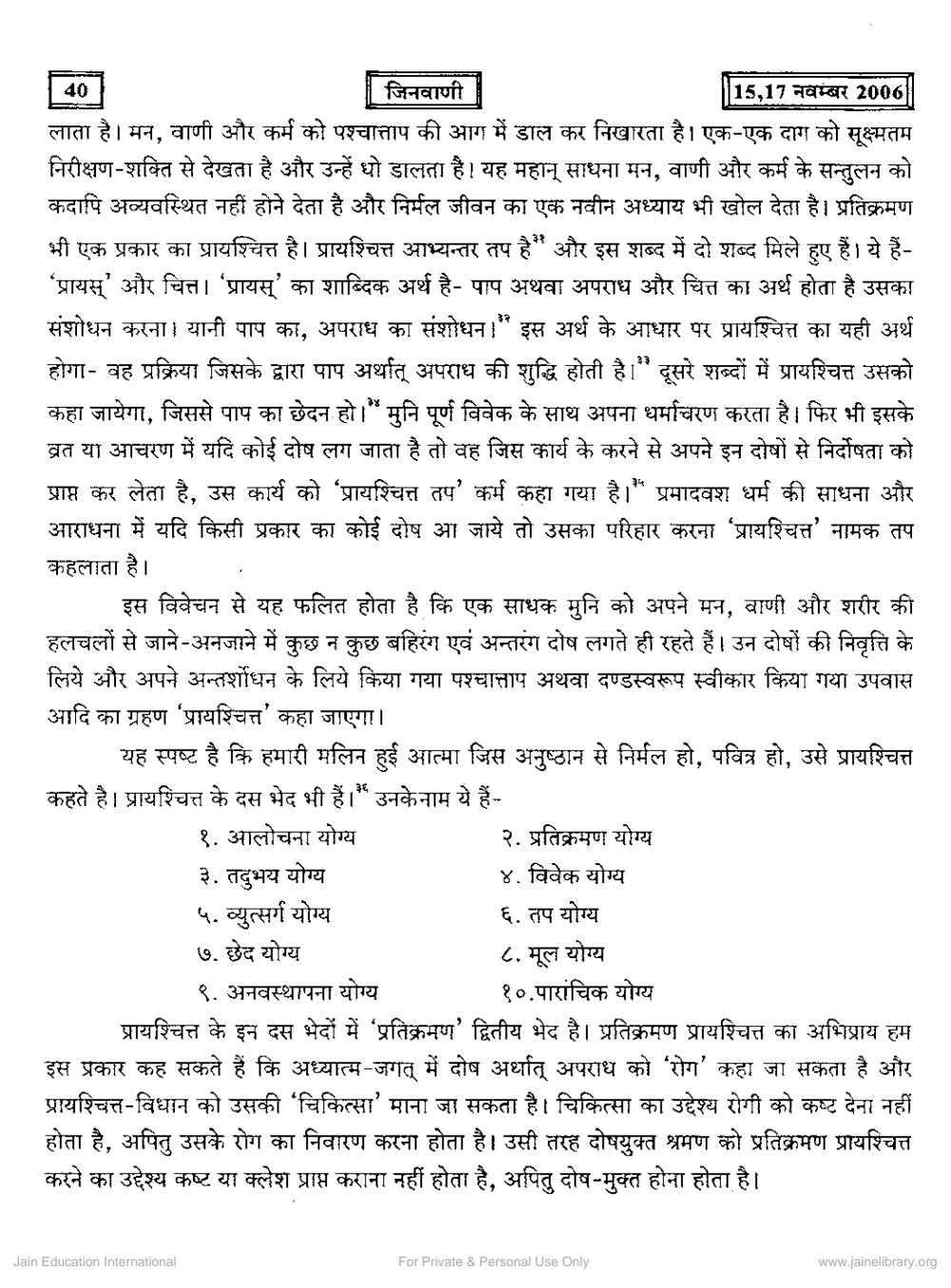Book Title: Pratikraman Avashyak Swarup aur Chintan Author(s): Rameshmuni Publisher: Z_Jinavani_002748.pdf View full book textPage 7
________________ 40 जिनवाणी ||15,17 नवम्बर 2006 लाता है। मन, वाणी और कर्म को पश्चात्ताप की आग में डाल कर निखारता है। एक-एक दाग को सूक्ष्मतम निरीक्षण-शक्ति से देखता है और उन्हें धो डालता है। यह महान् साधना मन, वाणी और कर्म के सन्तुलन को कदापि अव्यवस्थित नहीं होने देता है और निर्मल जीवन का एक नवीन अध्याय भी खोल देता है। प्रतिक्रमण भी एक प्रकार का प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त आभ्यन्तर तप है और इस शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं। ये हैं'प्रायस्' और चित्त। 'प्रायस् का शाब्दिक अर्थ है- पाप अथवा अपराध और चित्त का अर्थ होता है उसका संशोधन करना। यानी पाप का, अपराध का संशोधन।" इस अर्थ के आधार पर प्रायश्चित्त का यही अर्थ होगा- वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पाप अर्थात् अपराध की शुद्धि होती है। दूसरे शब्दों में प्रायश्चित्त उसको कहा जायेगा, जिससे पाप का छेदन हो। मुनि पूर्ण विवेक के साथ अपना धर्माचरण करता है। फिर भी इसके व्रत या आचरण में यदि कोई दोष लग जाता है तो वह जिस कार्य के करने से अपने इन दोषों से निर्दोषता को प्राप्त कर लेता है, उस कार्य को प्रायश्चित्त तप' कर्म कहा गया है।" प्रमादवश धर्म की साधना और आराधना में यदि किसी प्रकार का कोई दोष आ जाये तो उसका परिहार करना 'प्रायश्चित्त' नामक तप कहलाता है। ___ इस विवेचन से यह फलित होता है कि एक साधक मुनि को अपने मन, वाणी और शरीर की हलचलों से जाने-अनजाने में कुछ न कुछ बहिरंग एवं अन्तरंग दोष लगते ही रहते हैं। उन दोषों की निवृत्ति के लिये और अपने अन्तर्शोधन के लिये किया गया पश्चात्ताप अथवा दण्डस्वरूप स्वीकार किया गया उपवास आदि का ग्रहण ‘प्रायश्चित्त' कहा जाएगा। यह स्पष्ट है कि हमारी मलिन हुई आत्मा जिस अनुष्ठान से निर्मल हो, पवित्र हो, उसे प्रायश्चित्त कहते है। प्रायश्चित्त के दस भेद भी हैं। उनकेनाम ये हैं१. आलोचना योग्य २. प्रतिक्रमण योग्य ३. तदुभय योग्य ४. विवेक योग्य ५. व्युत्सर्ग योग्य ६. तप योग्य ७. छेद योग्य ८. मूल योग्य ९. अनवस्थापना योग्य १०.पारांचिक योग्य प्रायश्चित्त के इन दस भेदों में प्रतिक्रमण' द्वितीय भेद है। प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त का अभिप्राय हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अध्यात्म-जगत् में दोष अर्थात् अपराध को 'रोग' कहा जा सकता है और प्रायश्चित्त-विधान को उसकी 'चिकित्सा' माना जा सकता है। चिकित्सा का उद्देश्य रोगी को कष्ट देना नहीं होता है, अपितु उसके रोग का निवारण करना होता है। उसी तरह दोषयुक्त श्रमण को प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त करने का उद्देश्य कष्ट या क्लेश प्राप्त कराना नहीं होता है, अपितु दोष-मुक्त होना होता है। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13