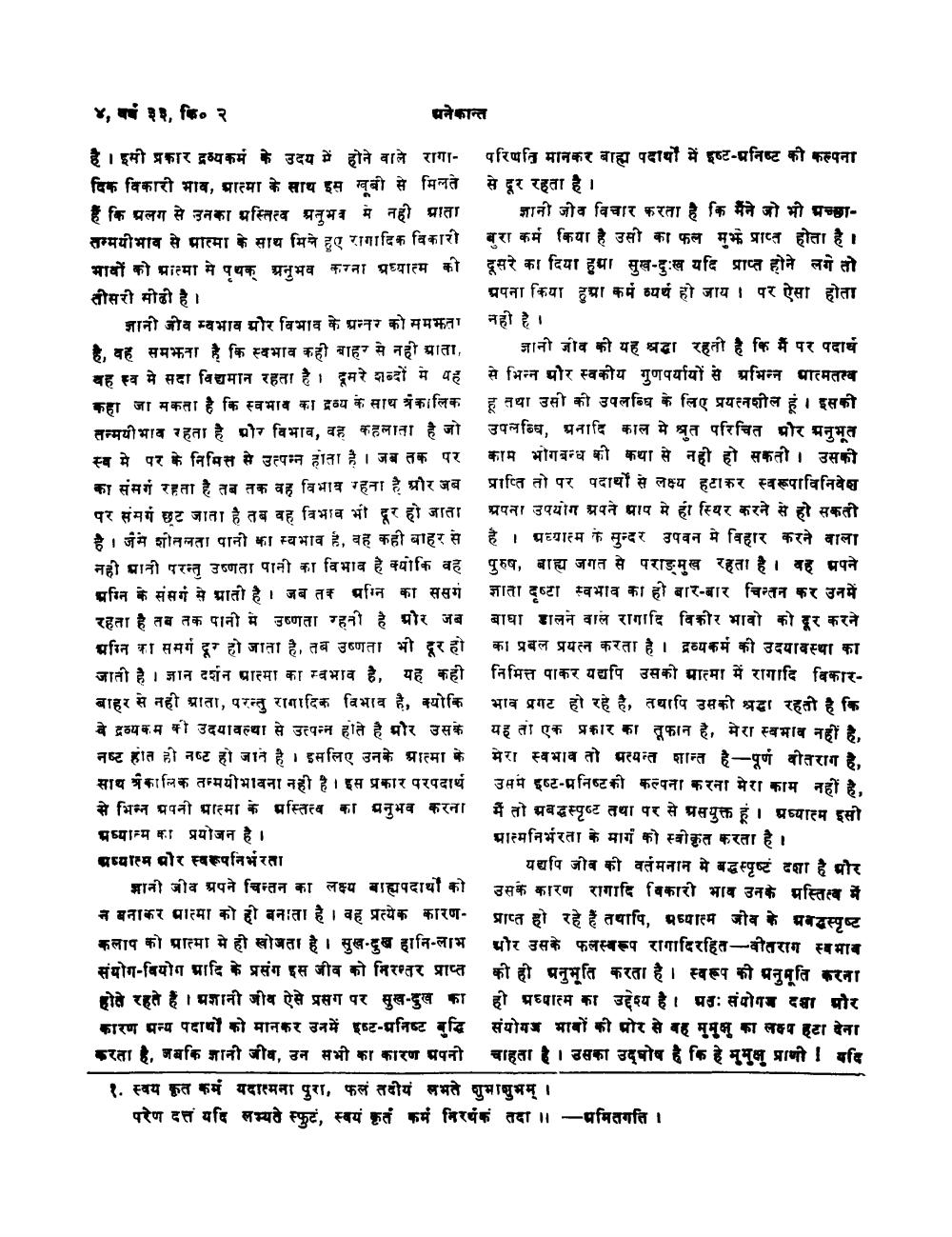Book Title: Anekant 1980 Book 33 Ank 01 to 04 Author(s): Gokulprasad Jain Publisher: Veer Seva Mandir Trust View full book textPage 7
________________ ४ वर्ष ३३, ०२ होने वाले रागा के खूबी से मिलते है । इसी प्रकार द्रव्यकर्म के दिक विकारी भाव, प्रात्मा हैं कि अलग से उनका अस्तित्व अनुभव मे नहीं घाता तन्मयीभाव से म्रात्मा के साथ मिले हुए रागादिक विकारी मावों को आत्मा मे पृथक अनुभव करना अध्यात्म की तीसरी मीठी है । उदय में साथ इस धनेकान्त ज्ञानी जीव स्वभाव और विभाव के अन्तर को समझता वह समझना है कि स्वभाव कही बाहर से नहीं आता, यह स्व मे सदा विद्यमान रहता है। दूसरे शब्दों में वह कहा जा सकता है कि स्वभाव का द्रव्य के साथ कालिक तन्मयीभाव रहता है और विभाव, वह कहलाता है जो स्व मे पर के निमित्त से उत्पन्न होता है। जब तक पर का संसर्ग रहता है तब तक वह विभाव रहना है और जब पर संगं छूट जाता है तब वह विभाव भी दूर हो जाता है । जैसे शीतलता पानी का स्वभाव है, वह कही बाहर से नही घानी परन्तु उष्णता पानी का विभाव है क्योंकि वह अग्नि के संसर्ग से भाती है। जब तक प्रग्नि का ससगं रहता है तब तक पानी में उष्णता रहती है और जब अग्नि का समर्ग दूर हो जाता है, तब उष्णता भी दूर हो जाती है। ज्ञान दर्शन प्रात्मा का स्वभाव है, यह कही बाहर से नही आता, परन्तु रागादिक विभाव है, क्योकि द्रव्यकम की उदयावल्या से उत्पन्न होते है मीर उसके नष्ट होत ही नष्ट हो जाते है । इसलिए उनके श्रात्मा के साथ कालिक तन्मयीभावना नहीं है। इस प्रकार परपदार्थ से भिन्न अपनी प्रात्मा के प्रस्तित्व का अनुभव करना अध्यात्म का प्रयोजन है । अध्यात्म बोर स्वरूप निर्भरता परियति मानकर बाह्य पदार्थों में इष्ट-प्रनिष्ट की कल्पना से दूर रहता है। बुरा ज्ञानी जीव विचार करता है कि मैंने जो भी अच्छाकर्म किया है उसी का फल मुझे प्राप्त होता है । दूसरे का दिया हुआ सुख-दुःख यदि प्राप्त होने लगे तो अपना किया हुआ कर्म व्यर्थ हो जाय । पर ऐसा होता नहीं है। जानो जीव की यह बद्धा रहती है कि मैं पर पदार्थ से भिन्न मोर स्वकीय गुणपर्यायों से अभिन्न धात्मतत्व हू तथा उसी की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील हूं। इसकी उपलब्धि धनादि काल मे श्रुत परिचित घोर अनुभूत काम भोगबन्ध की कथा से नहीं हो सकती उसकी प्राप्ति तो पर पदार्थों से लक्ष्य हटाकर स्वरूपाविनिवेश उपयोग अपने बाप में ही स्थिर करने से हो सकती है । अध्यात्म के सुन्दर उपवन मे विहार करने वाला पुरुष, बाह्य जगत से पराङ्मुख रहता है । वह पने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का हो बार-बार चिन्तन कर उनमें बाधा डालने वाले रागादि विकीर भावो को दूर करने का प्रबल प्रयत्न करता है । द्रव्यकर्म की उदयावस्था का निमित्त पाकर यद्यपि उसकी म्रात्मा में रागादि विकारभाव प्रगट हो रहे है, तथापि उसकी श्रद्धा रहती है कि यह तो एक प्रकार का तूफान है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो प्रत्यन्तान्त पूर्ण वीतराग है, उसमें इष्ट-प्रनिष्टकी कल्पना करना मेरा काम नहीं है, मैं तो अस्पृष्ट तथा पर से सयुक्त हूं। प्रप्यात्म इसी आत्मनिर्भरता के मार्ग को स्वीकृत करता है । यद्यपि जीव की वर्तमनान मे बद्धस्पृष्टं दशा है और उसके कारण रागादि विकारी भाव उनके प्रस्तित्व में प्राप्त हो रहे हैं तथापि, अध्यात्म जीव के स्पृष्ट और उसके फलस्वरूप रागादिरहित - वीतराग स्वभाव की ही अनुभूति करता है स्वरूप की धनुभूति करना ही अध्यात्म का उद्देश्य है । प्रतः संयोगज दक्षा घोर संयोगज भावों की घोर से वह मुमुक्षु का लक्ष्य हटा देना चाहता है। उसका उद्घोष है कि हे मुमुक्षु प्राणी ! यदि शुभाशुभम् । ज्ञानी जीव अपने चिन्तन का लक्ष्य बाह्यपदार्थों को न बनाकर मात्मा को ही बनाता है। वह प्रत्येक कारणकलाप को प्रात्मा मे ही खोजता है। सुख-दुख हानि-लाभ संयोग-वियोग प्रादि के प्रसंग इस जीव को निरन्तर प्राप्त होते रहते हैं। मशानी जीव ऐसे प्रसग पर सुख-दुख का कारण अन्य पदार्थों को मानकर उनमें इष्ट घनिष्ट बुद्धि करता है, जबकि ज्ञानी जीव उन सभी का कारण अपनी १. स्वयं कृत कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा । प्रमितगति ।Page Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 258