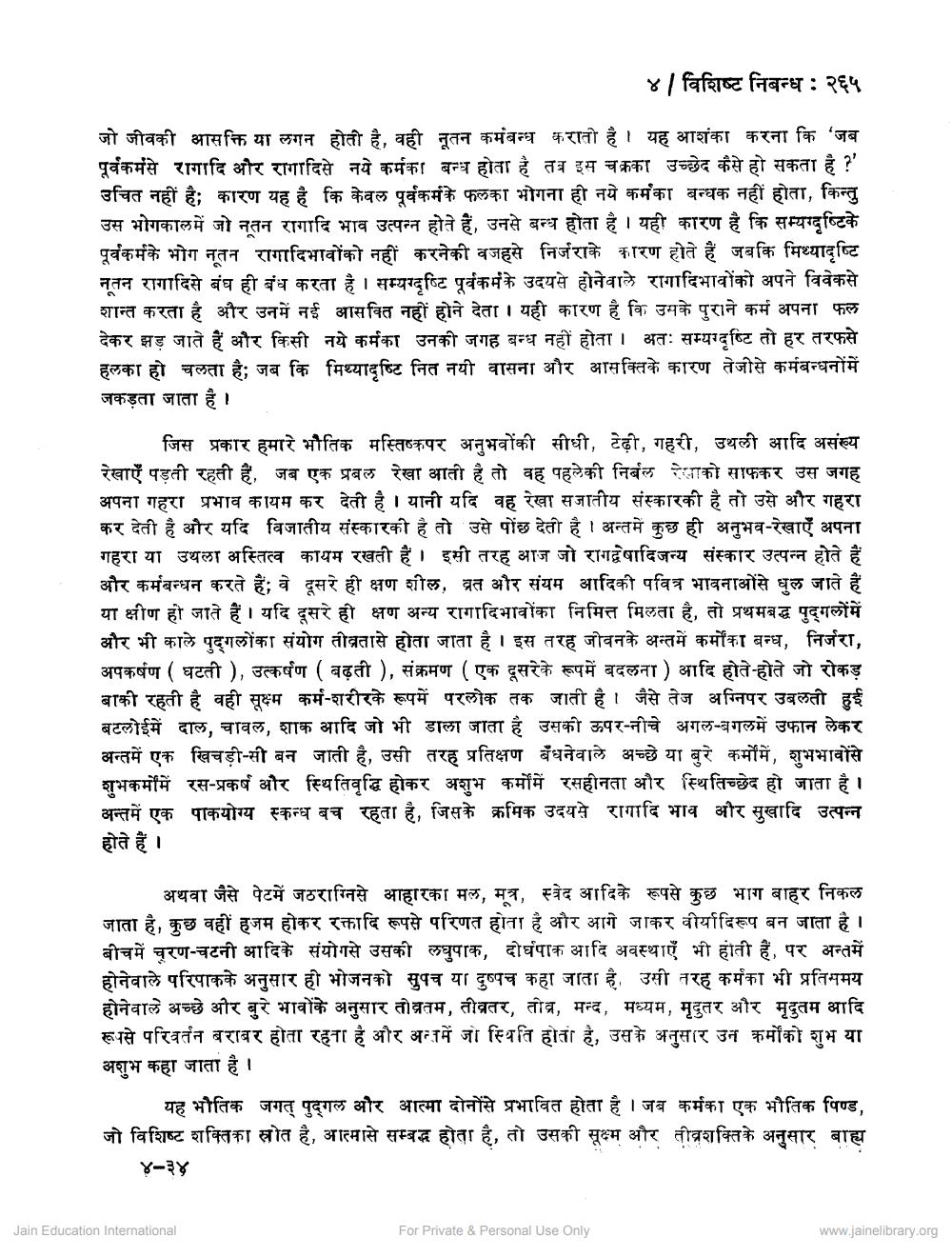Book Title: Tattva nirupana Author(s): Publisher: Z_Mahendrakumar_Jain_Nyayacharya_Smruti_Granth_012005.pdf View full book textPage 8
________________ ४/ विशिष्ट निबन्ध : २६५ जो जीवकी आसक्ति या लगन होती है, वही नूतन कर्मबन्ध कराती है। यह आशंका करना कि 'जब पूर्वकर्मसे रागादि और रागादिसे नये कर्मका बन्ध होता है तब इस चक्रका उच्छेद कैसे हो सकता है ?' उचित नहीं है; कारण यह है कि केवल पूर्वकर्मके फलका भोगना ही नये कर्मका बन्धक नहीं होता, किन्तु उस भोगकाल में जो नतन रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, उनसे बन्ध होता है । यही कारण है कि सम्यग्दृष्टिके पूर्वकर्मके भोग नतन रागादिभावोंको नहीं करनेकी वजहसे निर्जराके कारण होते हैं जबकि मिथ्यादृष्टि नूतन रागादिसे बंघ ही बंध करता है । सम्यग्दृष्टि पूर्वकर्मके उदयसे होनेवाले रागादिभावोंको अपने विवेकसे शान्त करता है और उनमें नई आसक्ति नहीं होने देता । यही कारण है कि उसके पुराने कर्म अपना फल देकर झड़ जाते हैं और किसी नये कर्मका उनकी जगह बन्ध नहीं होता। अतः सम्यग्दृष्टि तो हर तरफसे हलका हो चलता है; जब कि मिथ्यादृष्टि नित नयी वासना और आसक्तिके कारण तेजीसे कर्मबन्धनोंमें जकड़ता जाता है। जिस प्रकार हमारे भौतिक मस्तिष्कपर अनुभवोंकी सीधी, टेढ़ी, गहरी, उथली आदि असंख्य रेखाएँ पड़ती रहती है, जब एक प्रबल रेखा आती है तो वह पहलेकी निर्बल रेखाको साफकर उस जगह अपना गहरा प्रभाव कायम कर देती है। यानी यदि वह रेखा सजातीय संस्कारकी है तो उसे और गहरा कर देती है और यदि विजातीय संस्कारकी है तो उसे पोंछ देती है । अन्तमे कुछ ही अनुभव-रेखाएँ अपना गहरा या उथला अस्तित्व कायम रखती हैं। इसी तरह आज जो रागद्वेषादिजन्य संस्कार उत्पन्न होते हैं और कर्मबन्धन करते हैं; वे दूसरे ही क्षण शील, व्रत और संयम आदिकी पवित्र भावनाओंसे धुल जाते हैं या क्षीण हो जाते हैं। यदि दूसरे ही क्षण अन्य रागादिभावोंका निमित्त मिलता है, तो प्रथमबद्ध पुद्गलोंमें और भी काले पुद्गलोंका संयोग तीव्रतासे होता जाता है । इस तरह जीवनके अन्तमें कर्मोंका बन्ध, निर्जरा, अपकर्षण ( घटती), उत्कर्षण ( बढ़ती ), संक्रमण ( एक दूसरेके रूप में बदलना) आदि होते-होते जो रोकड़ बाकी रहती है वही सूक्ष्म कर्म-शरीरके रूपमें परलोक तक जाती है। जैसे तेज अग्निपर उबलती हुई बटलोईमें दाल, चावल, शाक आदि जो भी डाला जाता है उसकी ऊपर-नीचे अगल-बगलमें उफान लेकर अन्तमें एक खिचड़ी-सी बन जाती है, उसी तरह प्रतिक्षण बँधनेवाले अच्छे या बुरे कर्मोंमें, शुभभावोंसे शभकर्मोंमें रस-प्रकर्ष और स्थितिवृद्धि होकर अशभ कर्मों में रसहीनता और स्थितिच्छेद हो जाता है। अन्तमें एक पाकयोग्य स्कन्ध बच रहता है, जिसके क्रमिक उदयसे रागादि भाव और सूखादि उत्पन्न होते हैं। अथवा जैसे पेटमें जठराग्निसे आहारका मल, मत्र, स्वेद आदिके रूपसे कुछ भाग बाहर निकल जाता है, कुछ वहीं हजम होकर रक्तादि रूपसे परिणत होता है और आगे जाकर वीर्यादिरूप बन जाता है। बीचमें चरण-चटनी आदिके संयोगसे उसकी लघुपाक, दोघंपाक आदि अवस्थाएँ भी होती हैं, पर अन्तमें होनेवाले परिपाकके अनुसार ही भोजनको सुपच या दुष्पच कहा जाता है, उसी तरह कर्मका भी प्रतिसमय होनेवाले अच्छे और बुरे भावोंके अनुसार तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मध्यम, मृदुतर और मृदुतम आदि रूपसे परिवर्तन बराबर होता रहता है और अन्तमें जो स्थिति होता है, उसके अनुसार उन कर्मोंको शुभ या अशुभ कहा जाता है। यह भौतिक जगत् पुद्गल और आत्मा दोनोंसे प्रभावित होता है । जब कर्मका एक भौतिक पिण्ड, जो विशिष्ट शक्तिका स्रोत है, आत्मासे सम्बद्ध होता है, तो उसकी सूक्ष्म और तीव्रशक्तिके अनुसार बाह्य ४-३४ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25