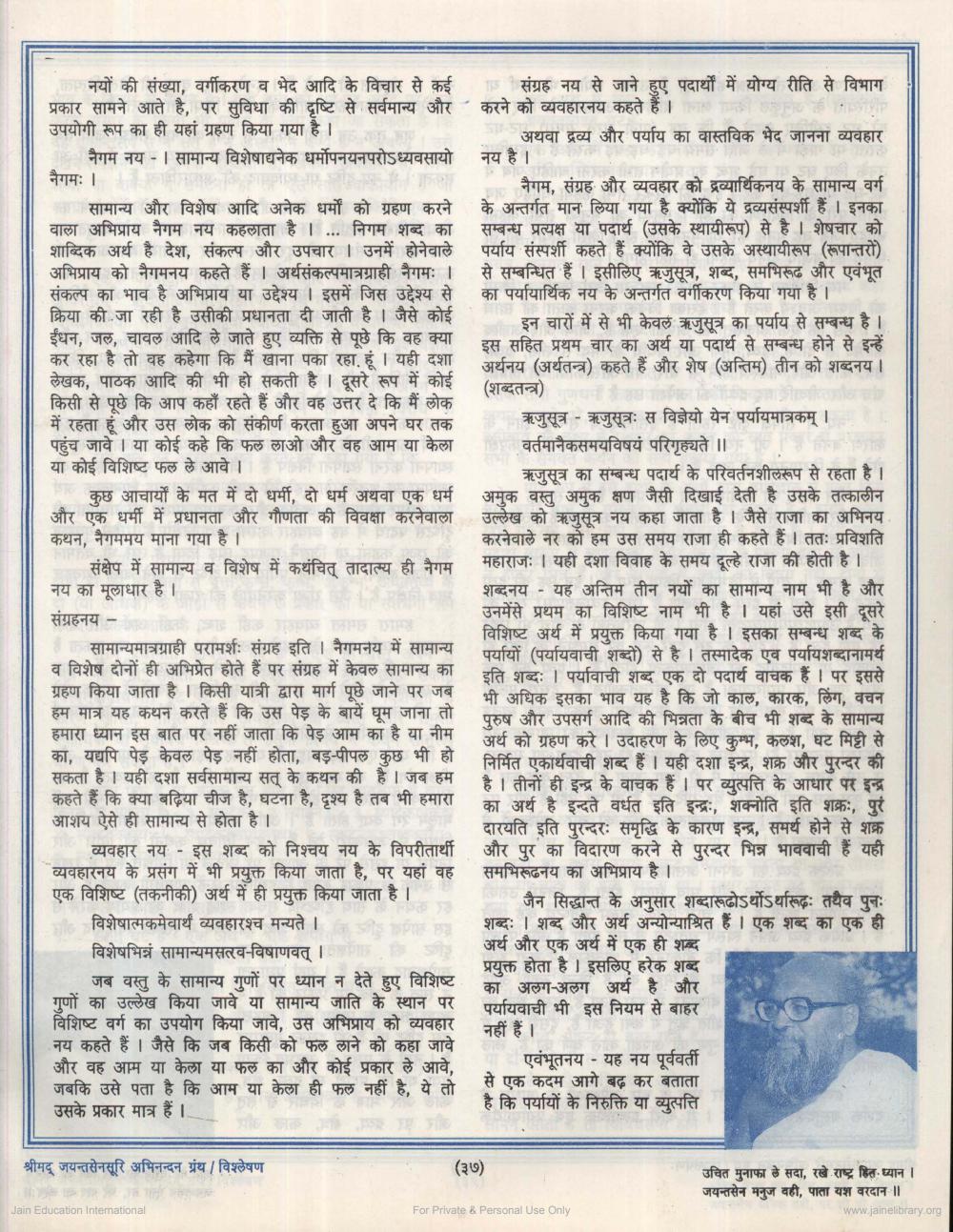Book Title: Syadvad Drushti Author(s): Shivnarayan Gaud Publisher: Z_Jayantsensuri_Abhinandan_Granth_012046.pdf View full book textPage 3
________________ नयों की संख्या, वर्गीकरण व भेद आदि के विचार से कई प्रकार सामने आते है, पर सुविधा की दृष्टि से सर्वमान्य और उपयोगी रूप का ही यहां ग्रहण किया गया है। नैगम नय । सामान्य विशेषाद्यनेक धर्मोपनयनपरोऽध्यवसायो नैगमः । सामान्य और विशेष आदि अनेक धर्मों को ग्रहण करने वाला अभिप्राय नैगम नय कहलाता है । निगम शब्द का शाब्दिक अर्थ है देश, संकल्प और उपचार । उनमें होनेवाले अभिप्राय को नैगमनय कहते हैं। अर्थसंकल्पमात्रग्राही नैगमः । संकल्प का भाव है अभिप्राय या उद्देश्य इसमें जिस उद्देश्य से क्रिया की जा रही है उसीकी प्रधानता दी जाती है। जैसे कोई ईंधन, जल, चावल आदि ले जाते हुए व्यक्ति से पूछे कि वह क्या कर रहा है तो वह कहेगा कि मैं खाना पका रहा हूं । यही दशा लेखक, पाठक आदि की भी हो सकती है। दूसरे रूप में कोई किसी से पूछे कि आप कहाँ रहते हैं और वह उत्तर दे कि मैं लोक में रहता हूं और उस लोक को संकीर्ण करता हुआ अपने घर तक पहुंच जावे । या कोई कहे कि फल लाओ और वह आम या केला या कोई विशिष्ट फल ले आवे । कुछ आचार्यों के मत में दो धर्मी, दो धर्म अथवा एक धर्म और एक धर्मी में प्रधानता और गौणता की विवक्षा करनेवाला कथन, नैगममय माना गया है। संक्षेप में सामान्य व विशेष में कथंचित् तादात्म्य ही नैगम नय का मूलाधार है। संग्रहनय Tapiss TOTIEN सामान्यमात्रग्राही परामर्शः संग्रह इति । नैगमनय में सामान्य व विशेष दोनों ही अभिप्रेत होते हैं पर संग्रह में केवल सामान्य का ग्रहण किया जाता है। किसी यात्री द्वारा मार्ग पूछे जाने पर जब हम मात्र यह कथन करते हैं कि उस पेड़ के बायें घूम जाना तो हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि पेड़ आम का है या नीम का, यद्यपि पेड़ केवल पेड़ नहीं होता, बड़-पीपल कुछ भी हो सकता है । यही दशा सर्वसामान्य सत् के कथन की है। जब हम कहते हैं कि क्या बढ़िया चीज है, घटना है, दृश्य है तब भी हमारा आशय ऐसे ही सामान्य से होता है। 316 व्यवहार नय इस शब्द को निश्चय नय के विपरीतार्थी व्यवहारनय के प्रसंग में भी प्रयुक्त किया जाता है, पर यहां यह एक विशिष्ट (तकनीकी) अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है । विशेषात्मकमेवार्थं व्यवहारश्च मन्यते । विशेषाभिनं सामान्यमसत्रय-विषाणवत् । P जब वस्तु के सामान्य गुणों पर ध्यान न देते हुए विशिष्ट गुणों का उल्लेख किया जावे या सामान्य जाति के स्थान पर विशिष्ट वर्ग का उपयोग किया जावे, उस अभिप्राय को व्यवहार नय कहते हैं । जैसे कि जब किसी को फल लाने को कहा जावे और वह आम या केला या फल का और कोई प्रकार ले आवे, जबकि उसे पता है कि आम या केला ही फल नहीं है, ये तो उसके प्रकार मात्र हैं । मी श्रीमद् जयन्तसेनसूरि अभिनन्दन ग्रंथ / विश्लेषण 83 Jain Education International संग्रह नय से जाने हुए पदार्थों में योग्य रीति से विभाग करने को व्यवहारनय कहते हैं। अथवा द्रव्य और पर्याय का वास्तविक भेद जानना व्यवहार नय है । नैगम, संग्रह और व्यवहार को द्रव्यार्थिकनय के सामान्य वर्ग के अन्तर्गत मान लिया गया है क्योंकि ये द्रव्यसंस्पर्शी हैं। इनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या पदार्थ (उसके स्थायीरूप) से है । शेषचार को पर्याय संस्पर्शी कहते हैं क्योंकि वे उसके अस्थायीरूप (रूपान्तरों) से सम्बन्धित हैं। इसीलिए ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत का पर्यायार्थिक नय के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया है । इन चारों में से भी केवल ऋजुसूत्र का पर्याय से सम्बन्ध है । इस सहित प्रथम चार का अर्थ या पदार्थ से सम्बन्ध होने से इन्हें अर्थनय (अर्थतन्त्र) कहते हैं और शेष (अन्तिम) तीन को शब्दनय । ( शब्दतन्त्र) ऋजुसूत्र ऋजुसूत्रः स विज्ञेयो येन पर्यायमात्रकम् । वर्तमानैकसमयविषयं परिगृह्यते ।। ऋजुसूत्र का सम्बन्ध पदार्थ के परिवर्तनशीलरूप से रहता है। अमुक वस्तु अमुक क्षण जैसी दिखाई देती है उसके तत्कालीन उल्लेख को ऋजुसूत्र नय कहा जाता है। जैसे राजा का अभिनय करनेवाले नर को हम उस समय राजा ही कहते हैं। ततः प्रविशति महाराजः । यही दशा विवाह के समय दूल्हे राजा की होती है। शब्दनय यह अन्तिम तीन नयों का सामान्य नाम भी है और उनमेंसे प्रथम का विशिष्ट नाम भी है। यहां उसे इसी दूसरे विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । इसका सम्बन्ध शब्द के पर्यायों (पर्यायवाची शब्दों) से है । तस्मादेक एव पर्यायशब्दानामर्थ इति शब्दः । पर्यावाची शब्द एक दो पदार्थ वाचक हैं। पर इससे भी अधिक इसका भाव यह है कि जो काल, कारक, लिंग, वचन पुरुष और उपसर्ग आदि की भिन्नता के बीच भी शब्द के सामान्य अर्थ को ग्रहण करे। उदाहरण के लिए कुम्भ, कलश, घट मिट्टी से निर्मित एकार्यवाची शब्द हैं। यही दशा इन्द्र, शक्र और पुरन्दर की है । तीनों ही इन्द्र के वाचक हैं। पर व्युत्पत्ति के आधार पर इन्द्र का अर्थ है इन्दते वर्धत इति इन्द्रः शक्नोति इति शक्रः पुर दारयति इति पुरन्दरः समृद्धि के कारण इन्द्र, समर्थ होने से शक और पुर का विदारण करने से पुरन्दर भिन्न भाववाची हैं यहीं समभिरूढनय का अभिप्राय है । जैन सिद्धान्त के अनुसार शब्दारूढोऽर्थोऽथरूदः तथैव पुनः शब्दः । शब्द और अर्थ अन्योन्याश्रित हैं । एक शब्द का एक ही अर्थ और एक अर्थ में एक ही शब्द प्रयुक्त होता है। इसलिए हरेक शब्द का अलग-अलग अर्थ है और पर्यायवाची भी इस नियम से बाहर नहीं हैं। एवंभूतनय यह नय पूर्ववर्ती से एक कदम आगे बढ़ कर बताता है कि पर्यायों के निरुक्ति या व्युत्पत्ति (३७) For Private & Personal Use Only 00 उचित मुनाफा के सदा, रखे राष्ट्र हित ध्यान । जयन्तसेन मनुज वही, पाता यश वरदान ॥ www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8