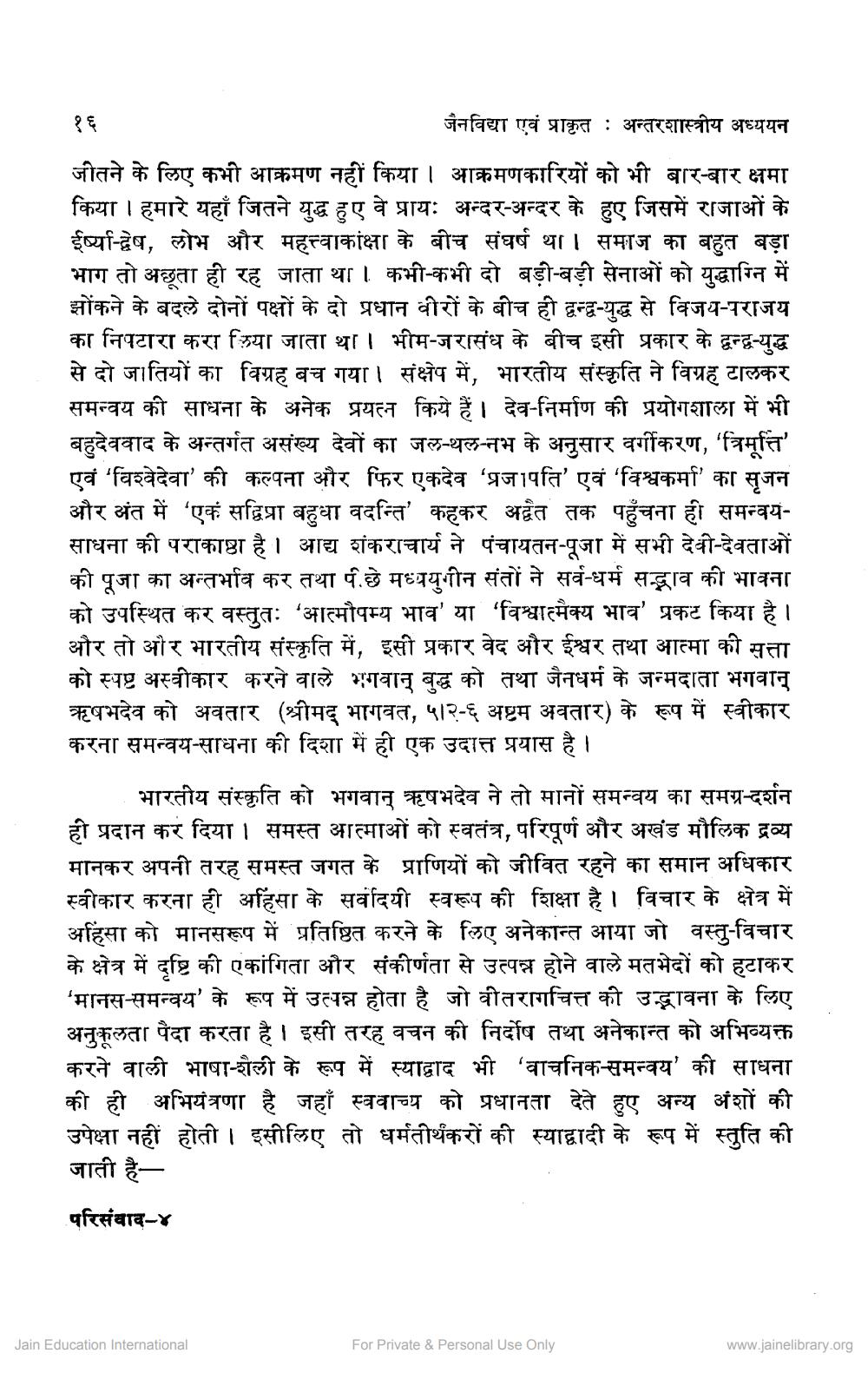Book Title: Samanvay Ki Sadhna Aur Jain Sanskriti Author(s): Ramji Sinh Publisher: Z_Jain_Vidya_evam_Prakrit_014026_HR.pdf View full book textPage 2
________________ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन जीतने के लिए कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमणकारियों को भी बार-बार क्षमा किया । हमारे यहाँ जितने युद्ध हुए वे प्रायः अन्दर-अन्दर के हुए जिसमें राजाओं के ईर्ष्या-द्वेष, लोभ और महत्त्वाकांक्षा के बीच संघर्ष था। समाज का बहुत बड़ा भाग तो अछूता ही रह जाता था। कभी-कभी दो बड़ी-बड़ी सेनाओं को युद्धाग्नि में झोंकने के बदले दोनों पक्षों के दो प्रधान वीरों के बीच ही द्वन्द्व-युद्ध से विजय-पराजय का निपटारा करा लिया जाता था। भीम-जरासंध के बीच इसी प्रकार के द्वन्द्व-युद्ध से दो जातियों का विग्रह बच गया। संक्षेप में, भारतीय संस्कृति ने विग्रह टालकर समन्वय की साधना के अनेक प्रयत्न किये हैं। देव-निर्माण की प्रयोगशाला में भी बहुदेववाद के अन्तर्गत असंख्य देवों का जल-थल-नभ के अनुसार वर्गीकरण, 'त्रिमूत्ति' एवं 'विश्वेदेवा' की कल्पना और फिर एकदेव 'प्रजापति' एवं 'विश्वकर्मा' का सृजन और अंत में 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' कहकर अद्वैत तक पहुँचना ही समन्वयसाधना की पराकाष्ठा है। आद्य शंकराचार्य ने पंचायतन-पूजा में सभी देवी-देवताओं की पूजा का अन्तर्भाव कर तथा प.छे मध्ययुगीन संतों ने सर्व-धर्म सद्भाव की भावना को उपस्थित कर वस्तुतः 'आत्मौपम्य भाव' या 'विश्वात्मैक्य भाव' प्रकट किया है। और तो और भारतीय संस्कृति में, इसी प्रकार वेद और ईश्वर तथा आत्मा की सत्ता को स्पष्ट अस्वीकार करने वाले भगवान् बुद्ध को तथा जैनधर्म के जन्मदाता भगवान् ऋषभदेव को अवतार (श्रीमद् भागवत, ५।२-६ अष्टम अवतार) के रूप में स्वीकार करना समन्वय-साधना की दिशा में ही एक उदात्त प्रयास है। . भारतीय संस्कृति को भगवान् ऋषभदेव ने तो मानों समन्वय का समग्र-दर्शन ही प्रदान कर दिया। समस्त आत्माओं को स्वतंत्र, परिपूर्ण और अखंड मौलिक द्रव्य मानकर अपनी तरह समस्त जगत के प्राणियों को जीवित रहने का समान अधिकार स्वीकार करना ही अहिंसा के सदियी स्वरूप की शिक्षा है। विचार के क्षेत्र में अहिंसा को मानसरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अनेकान्त आया जो वस्तु-विचार के क्षेत्र में दृष्टि की एकांगिता और संकीर्णता से उत्पन्न होने वाले मतभेदों को हटाकर 'मानस-समन्वय' के रूप में उत्पन्न होता है जो वीतरागचित्त की उद्भावना के लिए अनुकूलता पैदा करता है। इसी तरह वचन की निर्दोष तथा अनेकान्त को अभिव्यक्त करने वाली भाषा-शैली के रूप में स्याद्वाद भी 'वाचनिक-समन्वय' की साधना की ही अभियंत्रणा है जहाँ स्ववाच्य को प्रधानता देते हुए अन्य अंशों की उपेक्षा नहीं होती। इसीलिए तो धर्मतीर्थंकरों की स्याद्वादी के रूप में स्तुति की जाती है परिसंवाद-४ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9