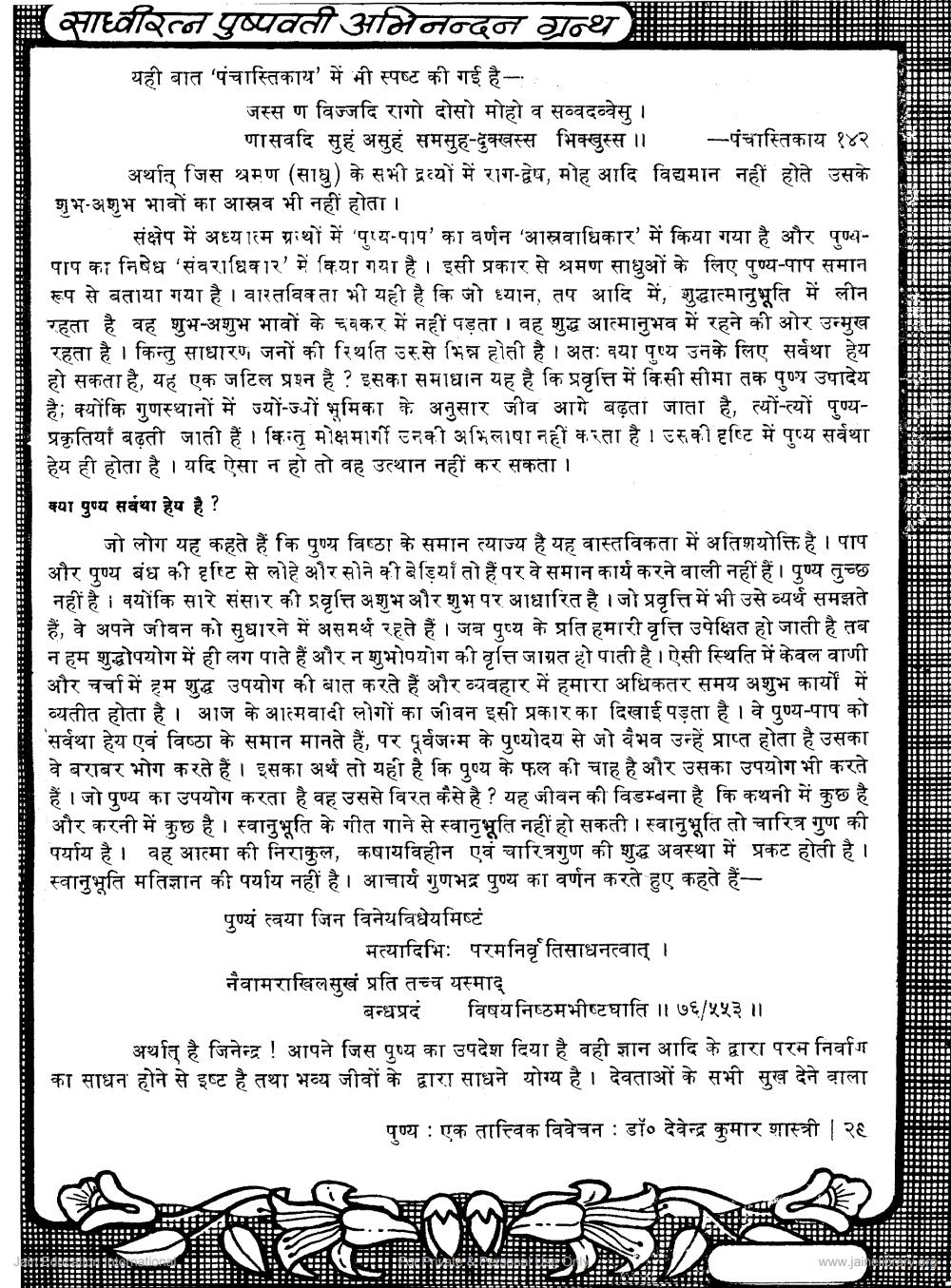Book Title: Punya Ek Tattvik Vivechan Author(s): Devendramuni Shastri Publisher: Z_Sadhviratna_Pushpvati_Abhinandan_Granth_012024.pdf View full book textPage 3
________________ iiiiiiiiiiii साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ) यही बात 'पंचास्तिकाय' में भी स्पष्ट की गई है जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सव्वदव्वेसु । णासवदि सुहं असुहं समसुह-दुक्खस्स भिक्खुस्स ॥ -पंचास्तिकाय १४२ अर्थात् जिस श्रमण (साधु) के सभी द्रव्यों में राग-द्वेष, मोह आदि विद्यमान नहीं होते उसके शुभ-अशुभ भावों का आस्रव भी नहीं होता। संक्षेप में अध्यात्म ग्रन्थों में 'पुण्य-पाप' का वर्णन 'आस्रवाधिकार' में किया गया है और पुण्यपाप का निषेध 'संबराधिकार' में किया गया है। इसी प्रकार से श्रमण साधुओं के लिए पण्य-पाप समान रूप से बताया गया है । वारतविक्ता भी यही है कि जो ध्यान, तप आदि में, शुद्धात्मानुभूति में लीन रहता है वह शुभ-अशुभ भावों के चक्कर में नहीं पड़ता। वह शुद्ध आत्मानुभव में रहने की ओर उन्मुख रहता है । किन्तु साधारण जनों की स्थिति उससे भिन्न होती है । अतः वया पुण्य उनके लिए सर्वथा हेय हो सकता है, यह एक जटिल प्रश्न है ? इसका समाधान यह है कि प्रवृत्ति में किसी सीमा तक पुण्य उपादेय है; क्योंकि गुणस्थानों में ज्यों-ज्यों भूमिका के अनुसार जीव आगे बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों पुण्यप्रकृतियाँ बढ़ती जाती हैं। किन्तु मोक्षमार्गी उनकी अभिलाषा नहीं करता है । उसकी दृष्टि में पुष्य सर्वथा हेय ही होता है । यदि ऐसा न हो तो वह उत्थान नहीं कर सकता। क्या पुण्य सर्वथा हेय है ? जो लोग यह कहते हैं कि पुण्य विष्ठा के समान त्याज्य है यह वास्तविकता में अतिशयोक्ति है । पाप और पूण्य बंध की दृष्टि से लोहे और सोने की बेड़ियाँ तो हैं पर वे समान कार्य करने वाली नहीं हैं। पुण्य तुच्छ नहीं है। क्योंकि सारे संसार की प्रवृत्ति अशुभ और शुभ पर आधारित है। जो प्रवृत्ति में भी उसे व्यर्थ समझते हैं, वे अपने जीवन को सुधारने में असमर्थ रहते हैं । जब पुण्य के प्रति हमारी वृत्ति उपेक्षित हो जाती है तब न हम शुद्धोपयोग में ही लग पाते हैं और न शुभोपयोग की वृत्ति जाग्रत हो पाती है। ऐसी स्थिति में केवल वाणी और चर्चा में हम शुद्ध उपयोग की बात करते हैं और व्यवहार में हमारा अधिकतर समय अशुभ कार्यों में व्यतीत होता है। आज के आत्मवादी लोगों का जीवन इसी प्रकार का दिखाई पड़ता है । वे पुण्य-पाप को सर्वथा हेय एवं विष्ठा के समान मानते हैं, पर पूर्वजन्म के पुण्योदय से जो वैभव उन्हें प्राप्त होता है उसका ते हैं। इसका अर्थ तो यही है कि पण्य के फल की चाह है और उसका उपयोग भी करते | हैं । जो पुण्य का उपयोग करता है वह उससे विरत कैसे है ? यह जीवन की विडम्बना है कि कथनी में कुछ है और करनी में कुछ है । स्वानुभूति के गीत गाने से स्वानुभूति नहीं हो सकती । स्वानुभूति तो चारित्र गुण की पर्याय है। वह आत्मा की निराकुल, कषायविहीन एवं चारित्रगुण की शुद्ध अवस्था में प्रकट होती है । स्वानुभूति मतिज्ञान की पर्याय नहीं है। आचार्य गुणभद्र पुण्य का वर्णन करते हुए कहते हैं पुण्यं त्वया जिन विनेयविधेयमिष्टं मत्यादिभिः परमनिर्वृतिसाधनत्वात् । नैवामराखिलसुखं प्रति तच्च यस्माद् बन्धप्रदं विषय निष्ठमभीष्टघाति ।। ७६/५५३ ॥ अर्थात् है जिनेन्द्र ! आपने जिस पुण्य का उपदेश दिया है वही ज्ञान आदि के द्वारा परम निर्वाण का साधन होने से इष्ट है तथा भव्य जीवों के द्वारा साधने योग्य है । देवताओं के सभी सुख देने वाला पुण्य : एक तात्त्विक विवेचन : डॉ० देवेन्द्र कुमार शास्त्री | २६ कम www.ialPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7