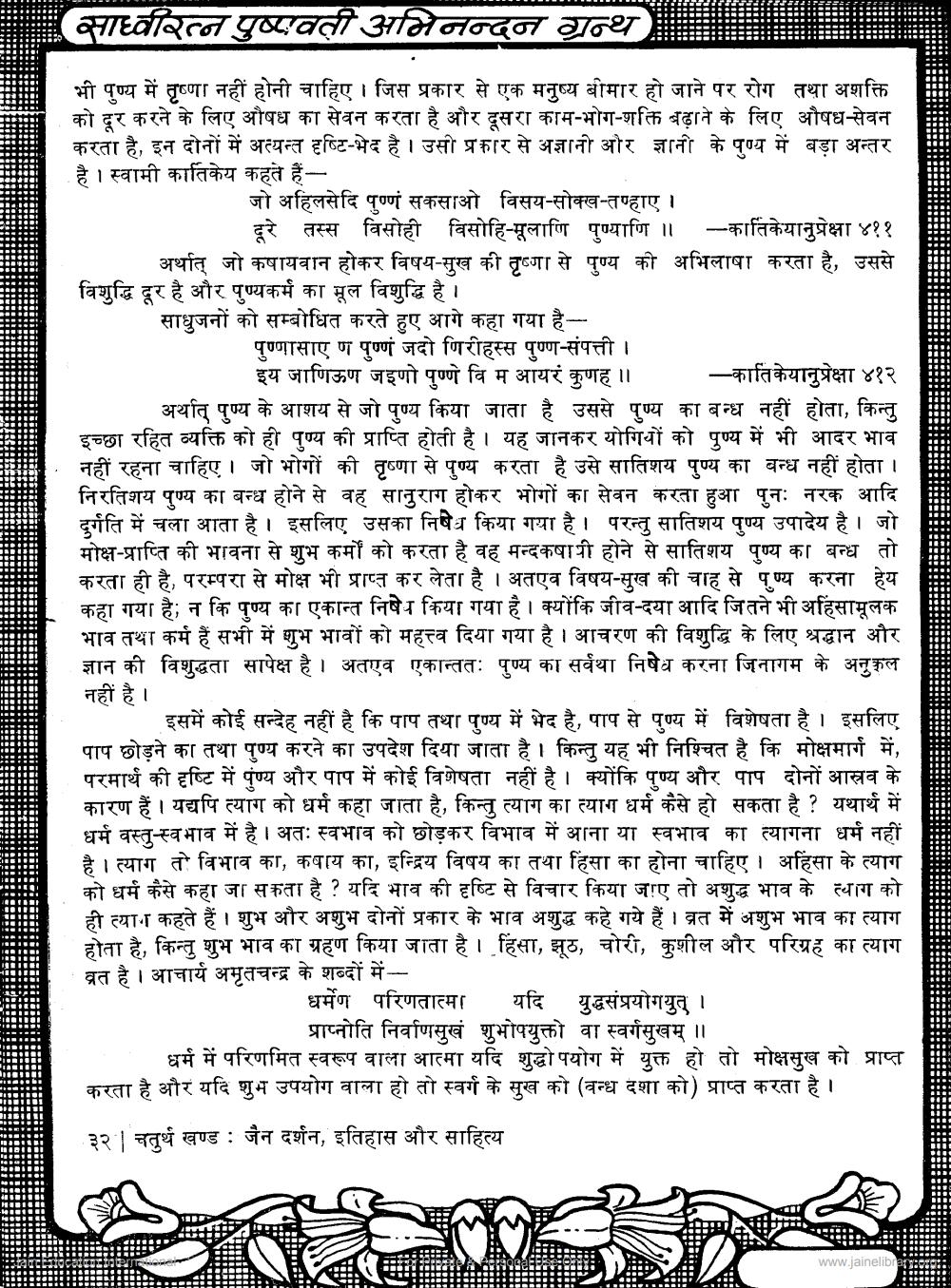Book Title: Punya Ek Tattvik Vivechan Author(s): Devendramuni Shastri Publisher: Z_Sadhviratna_Pushpvati_Abhinandan_Granth_012024.pdf View full book textPage 6
________________ साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ भी पुण्य में तृष्णा नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक मनुष्य बीमार हो जाने पर रोग तथा अशक्ति को दूर करने के लिए औषध का सेवन करता है और दूसरा काम भोग-शक्ति बढ़ाने के लिए औषध सेवन करता है, इन दोनों में अत्यन्त दृष्टि-भेद है । उसी प्रकार से अज्ञानी और ज्ञानी के पुण्य में बड़ा अन्तर है । स्वामी कार्तिकेय कहते हैं जो अहिलसेदि पुण्णं सकसाओ विसय- सोक्ख - तहाए । दूरे तस्स विसोही विसोहि मूलाणि पुण्याणि ॥ अर्थात् जो कषायवान होकर विषय-सुख की तृष्णा से पुण्य की विशुद्धि दूर है और पुण्यकर्म का मूल विशुद्धि है । साधुजनों को सम्बोधित करते हुए आगे कहा गया हैपुण्णासाए ण पुण्णं जदो गिरीहस्स पुण्ण-संपत्ती । इय जाणिऊण जइणो पुण्णे वि म आयरं कुणह ॥ - कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४११ अभिलाषा करता है, उससे - कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४१२ अर्थात् पुण्य के आशय से जो पुण्य किया जाता है उससे पुण्य का बन्ध नहीं होता, किन्तु इच्छा रहित व्यक्ति को ही पुण्य की प्राप्ति होती है । यह जानकर योगियों को पुण्य में भी आदर भाव नहीं रहना चाहिए । जो भोगों की तृष्णा से पुण्य करता है उसे सातिशय पुण्य का बन्ध नहीं होता । निरतिशय पुण्य का बन्ध होने से वह सानुराग होकर भोगों का सेवन करता हुआ पुनः नरक आदि दुर्गति में चला आता है । इसलिए उसका निषेध किया गया है । परन्तु सातिशय पुण्य उपादेय है । जो मोक्ष प्राप्ति की भावना से शुभ कर्मों को करता है वह मन्दकषायी होने से सातिशय पुण्य का बन्ध तो करता ही है, परम्परा 'मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है । अतएव विषय-सुख की चाह से पुण्य करना हेय कहा गया है, न कि पुण्य का एकान्त निषेध किया गया है। क्योंकि जीव दया आदि जितने भी अहिंसामूलक भाव तथा कर्म हैं सभी में शुभ भावों को महत्त्व दिया गया है । आचरण की विशुद्धि के लिए श्रद्धान और ज्ञान की विशुद्धता सापेक्ष है । अतएव एकान्ततः पुण्य का सर्वथा निषेध करना जिनागम के अनुकूल नहीं है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पाप तथा पुण्य में भेद है, पाप से पुण्य में विशेषता है । इसलिए पाप छोड़ने का तथा पुण्य करने का उपदेश दिया जाता है । किन्तु यह भी निश्चित है कि मोक्षमार्ग में, परमार्थ की दृष्टि में पुण्य और पाप में कोई विशेषता नहीं है । क्योंकि पुण्य और पाप दोनों आस्रव के कारण हैं । यद्यपि त्याग को धर्म कहा जाता है, किन्तु त्याग का त्याग धर्म कैसे हो सकता है ? यथार्थ में धर्म वस्तु स्वभाव में है । अतः स्वभाव को छोड़कर विभाव में आना या स्वभाव का त्यागना धर्म नहीं है । त्याग तो विभाव का, कषाय का, इन्द्रिय विषय का तथा हिंसा का होना चाहिए । अहिंसा के त्याग को धर्म कैसे कहा जा सकता है ? यदि भाव की दृष्टि से विचार किया जाए तो अशुद्ध भाव के त्याग को ही त्याग कहते हैं । शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव अशुद्ध कहे गये हैं । व्रत में अशुभ भाव का त्याग होता है, किन्तु शुभ भाव का ग्रहण किया जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग व्रत है । आचार्य अमृतचन्द्र के शब्दों में - धर्मेण परिणतात्मा यदि युद्धसंप्रयोगयुत् । प्राप्नोति निर्वाणसुखं शुभोपयुक्तो वा स्वर्गसुखम् ॥ धर्म में परिणमित स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्धोपयोग में युक्त हो तो मोक्षसुख को प्राप्त करता है और यदि शुभ उपयोग वाला हो तो स्वर्ग के सुख को (वन्ध दशा को ) प्राप्त करता है । ३२ | चतुर्थ खण्ड : जैन दर्शन, इतिहास और साहित्य www.jainelibnPage Navigation
1 ... 4 5 6 7