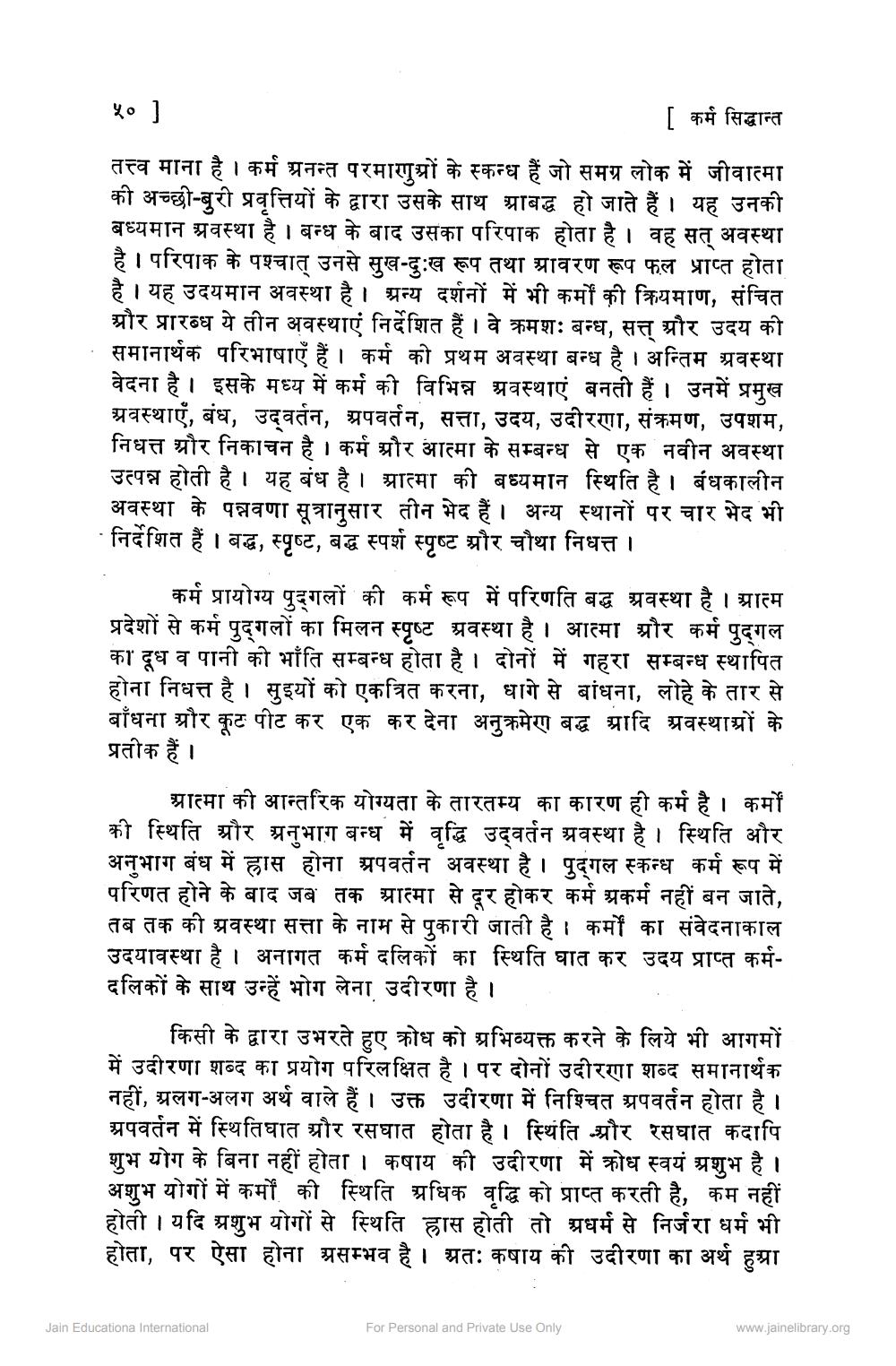Book Title: Karm Vimarsh Author(s): Bhagvati Muni Publisher: Z_Jinvani_Karmsiddhant_Visheshank_003842.pdf View full book textPage 2
________________ ५० ] [ कर्म सिद्धान्त तत्त्व माना है । कर्म अनन्त परमाणुओं के स्कन्ध हैं जो समग्र लोक में जीवात्मा की अच्छी-बुरी प्रवृत्तियों के द्वारा उसके साथ आबद्ध हो जाते हैं। यह उनकी बध्यमान अवस्था है । बन्ध के बाद उसका परिपाक होता है। वह सत् अवस्था है । परिपाक के पश्चात् उनसे सुख-दुःख रूप तथा आवरण रूप फल प्राप्त होता है । यह उदयमान अवस्था है। अन्य दर्शनों में भी कर्मों की क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध ये तीन अवस्थाएं निर्देशित हैं । वे क्रमशः बन्ध, सत्त् और उदय की समानार्थक परिभाषाएँ हैं। कर्म को प्रथम अवस्था बन्ध है । अन्तिम अवस्था वेदना है। इसके मध्य में कर्म की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। उनमें प्रमुख अवस्थाएँ, बंध, उद्वर्तन, अपवर्तन, सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमण, उपशम, निधत्त और निकाचन है । कर्म और आत्मा के सम्बन्ध से एक नवीन अवस्था उत्पन्न होती है। यह बंध है। आत्मा की बध्यमान स्थिति है। बंधकालीन अवस्था के पन्नवणा सूत्रानुसार तीन भेद हैं। अन्य स्थानों पर चार भेद भी निर्देशित हैं । बद्ध, स्पृष्ट, बद्ध स्पर्श स्पृष्ट और चौथा निधत्त । कर्म प्रायोग्य पुद्गलों की कर्म रूप में परिणति बद्ध अवस्था है । प्रात्म प्रदेशों से कर्म पुद्गलों का मिलन स्पृष्ट अवस्था है। आत्मा और कर्म पुद्गल का दूध व पानी को भाँति सम्बन्ध होता है। दोनों में गहरा सम्बन्ध स्थापित होना निधत्त है । सुइयों को एकत्रित करना, धागे से बांधना, लोहे के तार से बाँधना और कूट पीट कर एक कर देना अनुक्रमेण बद्ध आदि अवस्थाओं के प्रतीक हैं। आत्मा की आन्तरिक योग्यता के तारतम्य का कारण ही कर्म है। कर्मों की स्थिति और अनुभाग बन्ध में वृद्धि उद्वर्तन अवस्था है। स्थिति और अनुभाग बंध में ह्रास होना अपवर्तन अवस्था है। पुद्गल स्कन्ध कर्म रूप में परिणत होने के बाद जब तक आत्मा से दूर होकर कर्म अकर्म नहीं बन जाते, तब तक की अवस्था सत्ता के नाम से पुकारी जाती है। कर्मों का संवेदनाकाल उदयावस्था है। अनागत कर्म दलिकों का स्थिति घात कर उदय प्राप्त कर्मदलिकों के साथ उन्हें भोग लेना उदीरणा है । किसी के द्वारा उभरते हए क्रोध को अभिव्यक्त करने के लिये भी आगमों में उदीरणा शब्द का प्रयोग परिलक्षित है । पर दोनों उदीरणा शब्द समानार्थक नहीं, अलग-अलग अर्थ वाले हैं। उक्त उदीरणा में निश्चित अपवर्तन होता है। अपवर्तन में स्थितिघात और रसघात होता है। स्थिति और रसघात कदापि शुभ योग के बिना नहीं होता। कषाय की उदीरणा में क्रोध स्वयं अशुभ है। अशुभ योगों में कर्मों की स्थिति अधिक वृद्धि को प्राप्त करती है, कम नहीं होती । यदि अशुभ योगों से स्थिति ह्रास होती तो अधर्म से निर्जरा धर्म भी होता, पर ऐसा होना असम्भव है । अतः कषाय की उदीरणा का अर्थ हुआ Jain Educationa International For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12