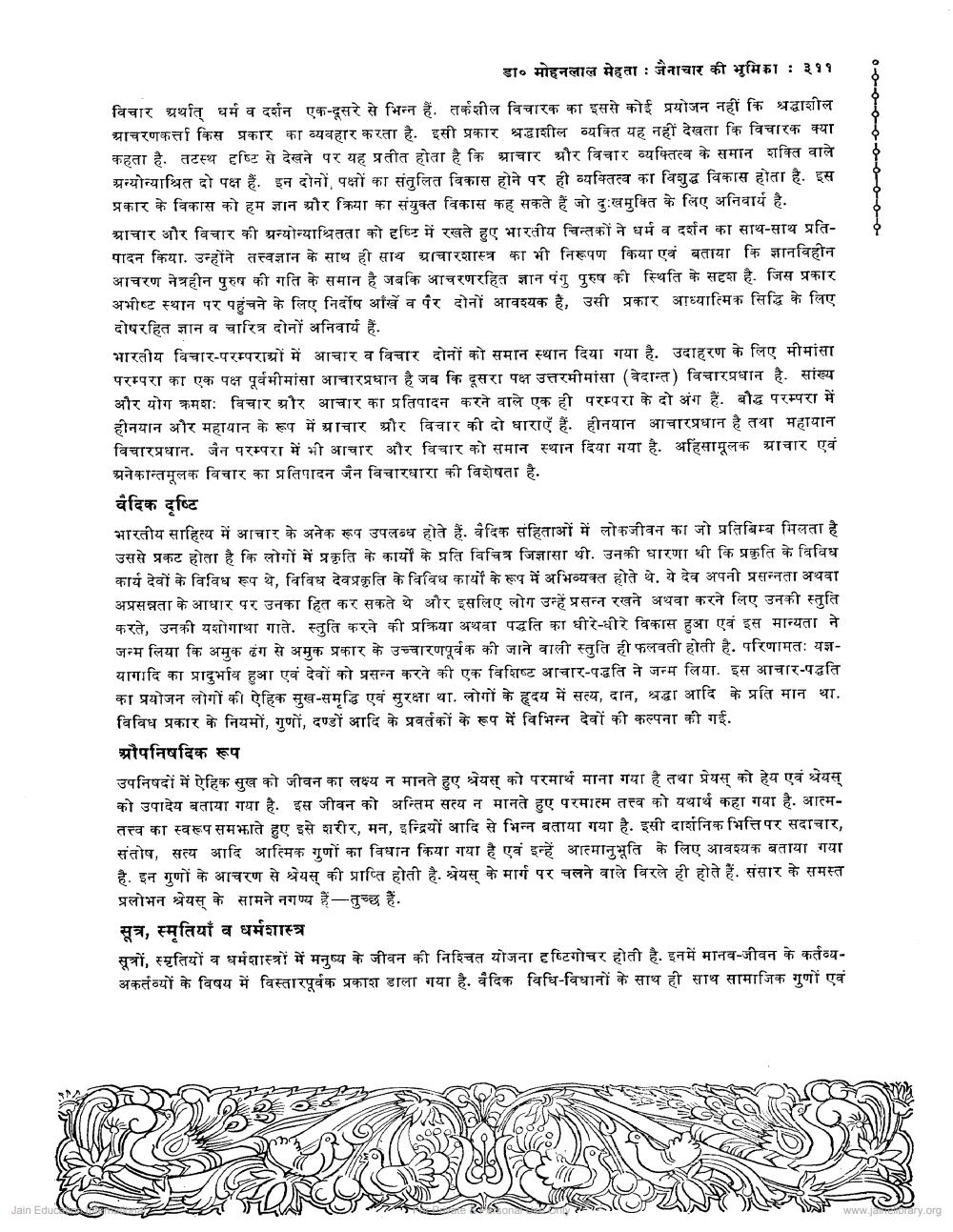Book Title: Jainachar ki Bhumika Author(s): Mohanlal Mehta Publisher: Z_Hajarimalmuni_Smruti_Granth_012040.pdf View full book textPage 2
________________ डा. मोहनलाल मेहता : जैनाचार की भूमिका : ३११ विचार अर्थात् धर्म व दर्शन एक-दूसरे से भिन्न हैं. तर्कशील विचारक का इससे कोई प्रयोजन नहीं कि श्रद्धाशील आचरणकर्ता किस प्रकार का व्यवहार करता है. इसी प्रकार श्रद्धाशील व्यक्ति यह नहीं देखता कि विचारक क्या कहता है. तटस्थ दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि आचार और विचार व्यक्तित्व के समान शक्ति वाले अन्योन्याश्रित दो पक्ष हैं. इन दोनों पक्षों का संतुलित विकास होने पर ही व्यक्तित्व का विशुद्ध विकास होता है. इस प्रकार के विकास को हम ज्ञान और क्रिया का संयुक्त विकास कह सकते हैं जो दुःखमुक्ति के लिए अनिवार्य है. आचार और विचार की अन्योन्याश्रितता को दृष्टि में रखते हुए भारतीय चिन्तकों ने धर्म व दर्शन का साथ-साथ प्रतिपादन किया. उन्होंने तत्त्वज्ञान के साथ ही साथ ग्राचारशास्त्र का भी निरूपण किया एवं बताया कि ज्ञानविहीन आचरण नेत्रहीन पुरुष की गति के समान है जबकि आचरणरहित ज्ञान पंग पुरुष की स्थिति के सदृश है. जिस प्रकार अभीष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए निर्दोष आँखें व पर दोनों आवश्यक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक सिद्धि के लिए दोषरहित ज्ञान व चारित्र दोनों अनिवार्य हैं. भारतीय विचार-परम्पराओं में आचार व विचार दोनों को समान स्थान दिया गया है. उदाहरण के लिए मीमांसा परम्परा का एक पक्ष पूर्वमीमांसा आचारप्रधान है जब कि दूसरा पक्ष उत्तरमीमांसा (वेदान्त) विचारप्रधान है. सांख्य और योग क्रमशः विचार और आचार का प्रतिपादन करने वाले एक ही परम्परा के दो अंग हैं. बौद्ध परम्परा में हीनयान और महायान के रूप में प्राचार और विचार की दो धाराएँ हैं. हीनयान आचारप्रधान है तथा महायान विचारप्रधान. जैन परम्परा में भी आचार और विचार को समान स्थान दिया गया है. अहिंसामूलक प्राचार एवं अनेकान्तमूलक विचार का प्रतिपादन जैन विचारधारा की विशेषता है. वैदिक दृष्टि भारतीय साहित्य में आचार के अनेक रूप उपलब्ध होते हैं. वैदिक संहिताओं में लोकजीवन का जो प्रतिबिम्ब मिलता है उससे प्रकट होता है कि लोगों में प्रकृति के कार्यों के प्रति विचित्र जिज्ञासा थी. उनकी धारणा थी कि प्रकृति के विविध कार्य देवों के विविध रूप थे, विविध देवप्रकृति के विविध कार्यों के रूप में अभिव्यक्त होते थे. ये देव अपनी प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता के आधार पर उनका हित कर सकते थे और इसलिए लोग उन्हें प्रसन्न रखने अथवा करने लिए उनकी स्तुति करते, उनकी यशोगाथा गाते. स्तुति करने की प्रक्रिया अथवा पद्धति का धीरे-धीरे विकास हुआ एवं इस मान्यता ने जन्म लिया कि अमुक ढंग से अमुक प्रकार के उच्चारणपूर्वक की जाने वाली स्तुति ही फलवती होती है. परिणामतः यज्ञयागादि का प्रादुर्भाव हुआ एवं देवों को प्रसन्न करने की एक विशिष्ट आचार-पद्धति ने जन्म लिया. इस आचार-पद्धति का प्रयोजन लोगों की ऐहिक सुख-समृद्धि एवं सुरक्षा था. लोगों के हृदय में सत्य, दान, श्रद्धा आदि के प्रति मान था. विविध प्रकार के नियमों, गुणों, दण्डों आदि के प्रवर्तकों के रूप में विभिन्न देवों की कल्पना की गई. औपनिषदिक रूप उपनिषदों में ऐहिक सुख को जीवन का लक्ष्य न मानते हुए श्रेयस् को परमार्थ माना गया है तथा प्रेयस् को हेय एवं श्रेयस् को उपादेय बताया गया है. इस जीवन को अन्तिम सत्य न मानते हुए परमात्म तत्त्व को यथार्थ कहा गया है. आत्मतत्त्व का स्वरूप समझाते हुए इसे शरीर, मन, इन्द्रियों आदि से भिन्न बताया गया है. इसी दार्शनिक भित्ति पर सदाचार, संतोष, सत्य आदि आत्मिक गुणों का विधान किया गया है एवं इन्हें आत्मानुभूति के लिए आवश्यक बताया गया है. इन गुणों के आचरण से श्रेयस् की प्राप्ति होती है. श्रेयस् के मार्ग पर चलने वाले विरले ही होते हैं. संसार के समस्त प्रलोभन श्रेयस् के सामने नगण्य हैं-तुच्छ हैं. सूत्र, स्मृतियाँ व धर्मशास्त्र सूत्रों, स्मृतियों व धर्मशास्त्रों में मनुष्य के जीवन की निश्चित योजना दृष्टिगोचर होती है. इनमें मानव-जीवन के कर्तव्यअकर्तव्यों के विषय में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है. वैदिक विधि-विधानों के साथ ही साथ सामाजिक गुणों एवं TI DIDEO NOR Jain Edu ww.jameriorary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8