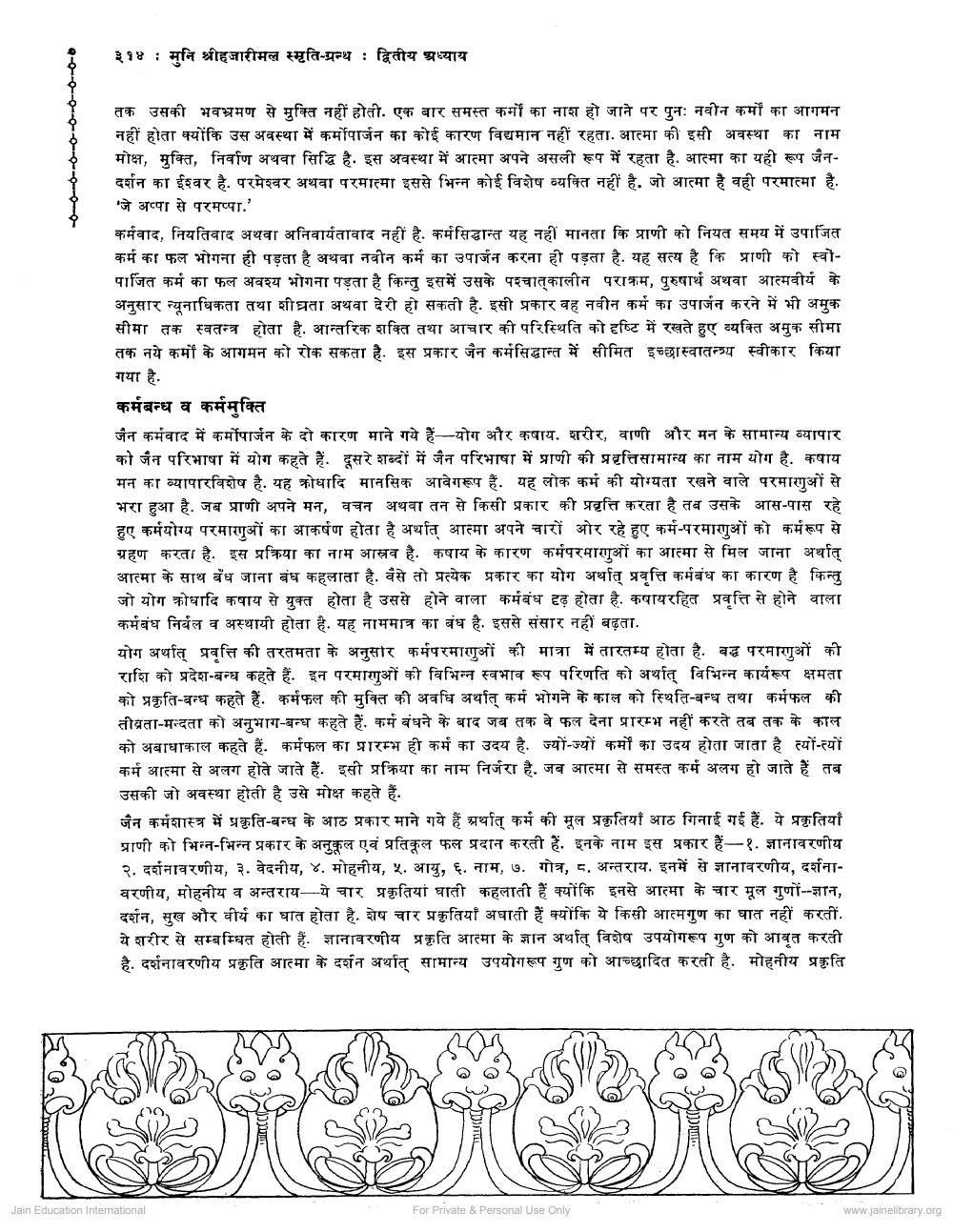Book Title: Jainachar ki Bhumika Author(s): Mohanlal Mehta Publisher: Z_Hajarimalmuni_Smruti_Granth_012040.pdf View full book textPage 5
________________ ३१४ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : द्वितीय अध्याय -0-0-0--0--0--0-0--01-0-0 तक उसकी भवभ्रमण से मुक्ति नहीं होती. एक बार समस्त कर्मों का नाश हो जाने पर पुनः नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता क्योंकि उस अवस्था में कर्मोपार्जन का कोई कारण विद्यमान नहीं रहता. आत्मा की इसी अवस्था का नाम मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण अथवा सिद्धि है. इस अवस्था में आत्मा अपने असली रूप में रहता है. आत्मा का यही रूप जैनदर्शन का ईश्वर है. परमेश्वर अथवा परमात्मा इससे भिन्न कोई विशेष व्यक्ति नहीं है. जो आत्मा है वही परमात्मा है. 'जे अप्पा से परमप्पा.' कर्मवाद, नियतिवाद अथवा अनिवार्यतावाद नहीं है. कर्मसिद्धान्त यह नहीं मानता कि प्राणी को नियत समय में उपाजित कर्म का फल भोगना ही पड़ता है अथवा नवीन कर्म का उपार्जन करना ही पड़ता है. यह सत्य है कि प्राणी को स्वोपार्जित कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है किन्तु इसमें उसके पश्चात्कालीन पराक्रम, पुरुषार्थ अथवा आत्मवीर्य के अनुसार न्यूनाधिकता तथा शीघ्रता अथवा देरी हो सकती है. इसी प्रकार वह नवीन कर्म का उपार्जन करने में भी अमुक सीमा तक स्वतन्त्र होता है. आन्तरिक शक्ति तथा आचार की परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए व्यक्ति अमुक सीमा तक नये कर्मों के आगमन को रोक सकता है. इस प्रकार जैन कर्मसिद्धान्त में सीमित इच्छास्वातन्त्र्य स्वीकार किया गया है. कर्मबन्ध व कर्ममुक्ति जैन कर्मवाद में कर्मोपार्जन के दो कारण माने गये हैं-योग और कषाय. शरीर, वाणी और मन के सामान्य व्यापार को जैन परिभाषा में योग कहते हैं. दूसरे शब्दों में जैन परिभाषा में प्राणी की प्रवृत्तिसामान्य का नाम योग है. कषाय मन का व्यापारविशेष है. यह क्रोधादि मानसिक आवेगरूप हैं. यह लोक कर्म की योग्यता रखने वाले परमाणुओं से भरा हुआ है. जब प्राणी अपने मन, वचन अथवा तन से किसी प्रकार की प्रवृत्ति करता है तब उसके आस-पास रहे हुए कर्मयोग्य परमाणुओं का आकर्षण होता है अर्थात् आत्मा अपने चारों ओर रहे हुए कर्म-परमाणुओं को कर्मरूप से ग्रहण करता है. इस प्रक्रिया का नाम आस्रव है. कषाय के कारण कर्मपरमाणुओं का आत्मा से मिल जाना अर्थात् आत्मा के साथ बंध जाना बंध कहलाता है. वैसे तो प्रत्येक प्रकार का योग अर्थात् प्रवृत्ति कर्मबंध का कारण है किन्तु जो योग क्रोधादि कषाय से युक्त होता है उससे होने वाला कर्मबंध दृढ़ होता है. कषायरहित प्रवृत्ति से होने वाला कर्मबंध निर्बल व अस्थायी होता है. यह नाममात्र का बंध है. इससे संसार नहीं बढ़ता. योग अर्थात् प्रवृत्ति की तरतमता के अनुसार कर्मपरमाणुओं की मात्रा में तारतम्य होता है. बद्ध परमाणुओं की राशि को प्रदेश-बन्ध कहते हैं. इन परमाणुओं की विभिन्न स्वभाव रूप परिणति को अर्थात् विभिन्न कार्यरूप क्षमता को प्रकृति-बन्ध कहते हैं. कर्मफल की मुक्ति की अवधि अर्थात् कर्म भोगने के काल को स्थिति-बन्ध तथा कर्मफल की तीव्रता-मन्दता को अनुभाग-बन्ध कहते हैं. कर्म बंधने के बाद जब तक वे फल देना प्रारम्भ नहीं करते तब तक के काल को अबाधाकाल कहते हैं. कर्मफल का प्रारम्भ ही कर्म का उदय है. ज्यों-ज्यों कर्मों का उदय होता जाता है त्यों-त्यों कर्म आत्मा से अलग होते जाते हैं. इसी प्रक्रिया का नाम निर्जरा है. जब आत्मा से समस्त कर्म अलग हो जाते हैं तब उसकी जो अवस्था होती है उसे मोक्ष कहते हैं. जैन कर्मशास्त्र में प्रकृति-बन्ध के आठ प्रकार माने गये हैं अर्थात् कर्म की मूल प्रकृतियाँ आठ गिनाई गई हैं. ये प्रकृतियाँ प्राणी को भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल फल प्रदान करती हैं. इनके नाम इस प्रकार हैं-१. ज्ञानावरणीय २. दर्शनावरणीय, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५. आयु, ६. नाम, ७. गोत्र, ८. अन्तराय. इनमें से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय व अन्तराय-ये चार प्रकृतियां घाती कहलाती हैं क्योंकि इनसे आत्मा के चार मूल गुणों--ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य का घात होता है. शेष चार प्रकृतियाँ अघाती हैं क्योंकि ये किसी आत्मगुण का घात नहीं करतीं. ये शरीर से सम्बन्धित होती हैं. ज्ञानावरणीय प्रकृति आत्मा के ज्ञान अर्थात् विशेष उपयोगरूप गुण को आवृत करती है. दर्शनावरणीय प्रकृति आत्मा के दर्शन अर्थात् सामान्य उपयोगरूप गुण को आच्छादित करती है. मोहनीय प्रकृति T10/ IDIO Jain Education Intemational For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8