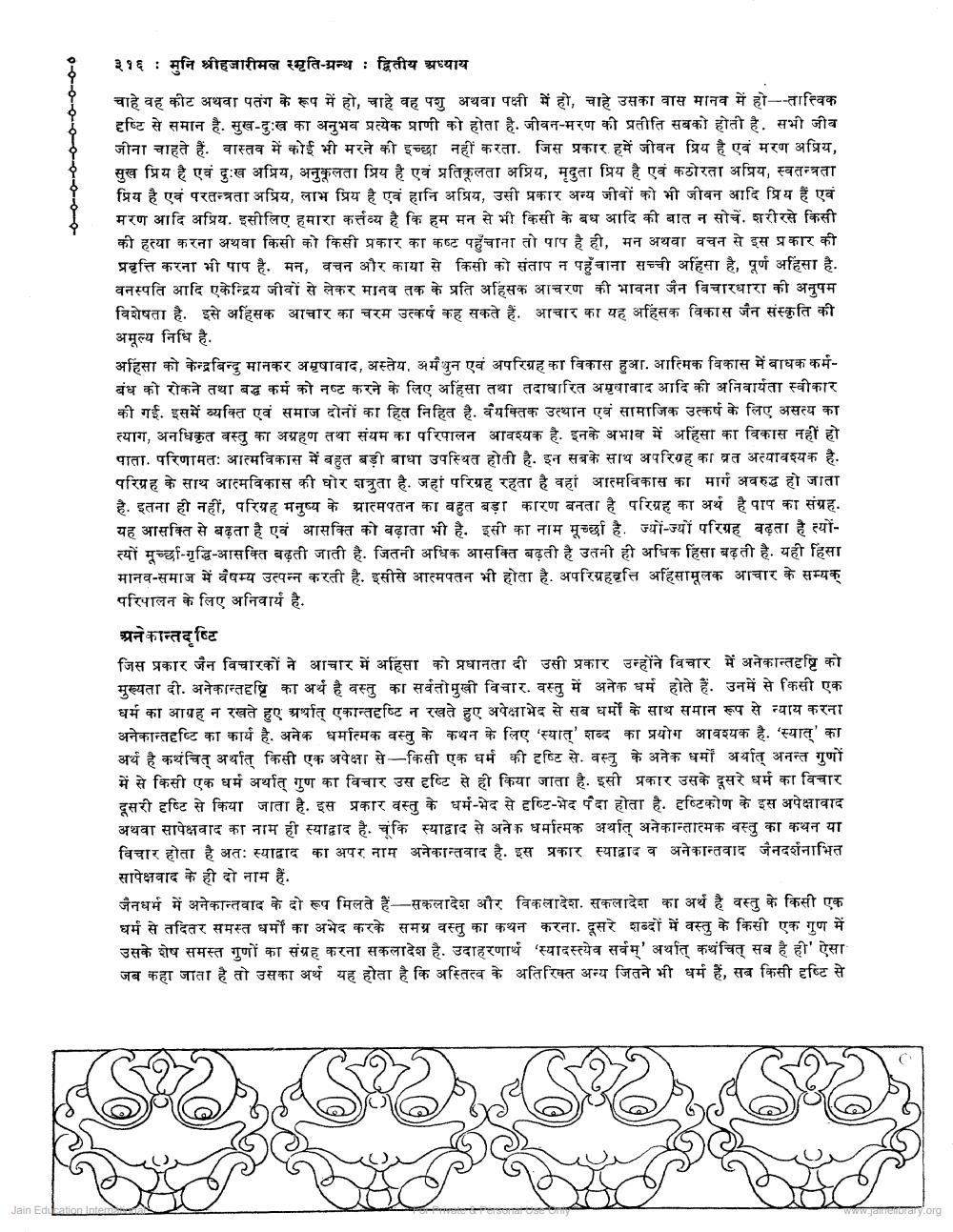Book Title: Jainachar ki Bhumika Author(s): Mohanlal Mehta Publisher: Z_Hajarimalmuni_Smruti_Granth_012040.pdf View full book textPage 7
________________ ३१६ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : द्वितीय अध्याय चाहे वह कीट अथवा पतंग के रूप में हो, चाहे वह पशु अथवा पक्षी में हो, चाहे उसका वास मानव में हो---तात्विक दृष्टि से समान है. सुख-दुःख का अनुभव प्रत्येक प्राणी को होता है. जीवन-मरण की प्रतीति सबको होती है. सभी जीव जीना चाहते हैं. वास्तव में कोई भी मरने की इच्छा नहीं करता. जिस प्रकार हमें जीवन प्रिय है एवं मरण अप्रिय, सुख प्रिय है एवं दुःख अप्रिय, अनुकूलता प्रिय है एवं प्रतिकूलता अप्रिय, मृदुता प्रिय है एवं कठोरता अप्रिय, स्वतन्त्रता प्रिय है एवं परतन्त्रता अप्रिय, लाभ प्रिय है एवं हानि अप्रिय, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी जीवन आदि प्रिय हैं एवं मरण आदि अप्रिय. इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम मन से भी किसी के बध आदि की बात न सोचें. शरीरसे किसी की हत्या करना अथवा किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाना तो पाप है ही, मन अथवा वचन से इस प्रकार की प्रवृत्ति करना भी पाप है. मन, वचन और काया से किसी को संताप न पहुँचाना सच्ची अहिंसा है, पूर्ण अहिंसा है. वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवों से लेकर मानव तक के प्रति अहिंसक आचरण की भावना जैन विचारधारा की अनुपम विशेषता है. इसे अहिंसक आचार का चरम उत्कर्ष कह सकते हैं. आचार का यह अहिंसक विकास जैन संस्कृति की अमूल्य निधि है. अहिंसा को केन्द्रबिन्दु मानकर अमृषावाद, अस्तेय, अमैथुन एवं अपरिग्रह का विकास हुआ. आत्मिक विकास में बाधक कर्मबंध को रोकने तथा बद्ध कर्म को नष्ट करने के लिए अहिंसा तथा तदाधारित अमृषावाद आदि की अनिवार्यता स्वीकार की गई. इसमें व्यक्ति एवं समाज दोनों का हित निहित है. वैयक्तिक उत्थान एवं सामाजिक उत्कर्ष के लिए असत्य का त्याग, अनधिकृत वस्तु का अग्रहण तथा संयम का परिपालन आवश्यक है. इनके अभाव में अहिंसा का विकास नहीं हो पाता. परिणामत: आत्मविकास में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित होती है. इन सबके साथ अपरिग्रह का व्रत अत्यावश्यक है. परिग्रह के साथ आत्मविकास की घोर शत्रुता है. जहां परिग्रह रहता है वहां आत्मविकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है. इतना ही नहीं, परिग्रह मनुष्य के आत्मपतन का बहुत बड़ा कारण बनता है परिग्रह का अर्थ है पाप का संग्रह. यह आसक्ति से बढ़ता है एवं आसक्ति को बढ़ाता भी है. इसी का नाम मूर्छा है. ज्यों-ज्यों परिग्रह बढ़ता है त्योंत्यों मूर्छा-गृद्धि-आसक्ति बढ़ती जाती है. जितनी अधिक आसक्ति बढ़ती है उतनी ही अधिक हिंसा बढ़ती है. यही हिंसा मानव-समाज में वैषम्य उत्पन्न करती है. इसीसे आत्मपतन भी होता है. अपरिग्रहवृत्ति अहिंसामूलक आचार के सम्यक् परिपालन के लिए अनिवार्य है. अनेकान्तदृष्टि जिस प्रकार जैन विचारकों ने आचार में अहिंसा को प्रधानता दी उसी प्रकार उन्होंने विचार में अनेकान्तदृष्टि को मुख्यता दी. अनेकान्तदृष्टि का अर्थ है वस्तु का सर्वतोमुखी विचार. वस्तु में अनेक धर्म होते हैं. उनमें से किसी एक धर्म का आग्रह न रखते हुए अर्थात् एकान्तदृष्टि न रखते हुए अपेक्षाभेद से सब धर्मों के साथ समान रूप से न्याय करना अनेकान्तदृष्टि का कार्य है. अनेक धर्मात्मक वस्तु के कथन के लिए 'स्यात्' शब्द का प्रयोग आवश्यक है. 'स्यात्' का अर्थ है कथंचित् अर्थात् किसी एक अपेक्षा से किसी एक धर्म की दृष्टि से. वस्तु के अनेक धर्मों अर्थात् अनन्त गुणों में से किसी एक धर्म अर्थात् गुण का विचार उस दृष्टि से ही किया जाता है. इसी प्रकार उसके दूसरे धर्म का विचार दूसरी दृष्टि से किया जाता है. इस प्रकार वस्तु के धर्म-भेद से दृष्टि-भेद पैदा होता है. दृष्टिकोण के इस अपेक्षावाद अथवा सापेक्षवाद का नाम ही स्याद्वाद है. चूंकि स्याद्वाद से अनेक धर्मात्मक अर्थात् अनेकान्तात्मक वस्तु का कथन या विचार होता है अतः स्याद्वाद का अपर नाम अनेकान्तवाद है. इस प्रकार स्याद्वाद व अनेकान्तवाद जैनदर्शनाभित सापेक्षवाद के ही दो नाम हैं. जैनधर्म में अनेकान्तवाद के दो रूप मिलते हैं—सकलादेश और विकलादेश. सकलादेश का अर्थ है वस्तु के किसी एक धर्म से तदितर समस्त धर्मों का अभेद करके समग्र वस्तु का कथन करना. दूसरे शब्दों में वस्तु के किसी एक गुण में उसके शेष समस्त गुणों का संग्रह करना सकलादेश है. उदाहरणार्थ 'स्यादस्त्येव सर्वम्' अर्थात् कथंचित् सब है ही' ऐसा जब कहा जाता है तो उसका अर्थ यह होता है कि अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य जितने भी धर्म हैं, सब किसी दृष्टि से Jain Edulation Intem Magarmendrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8