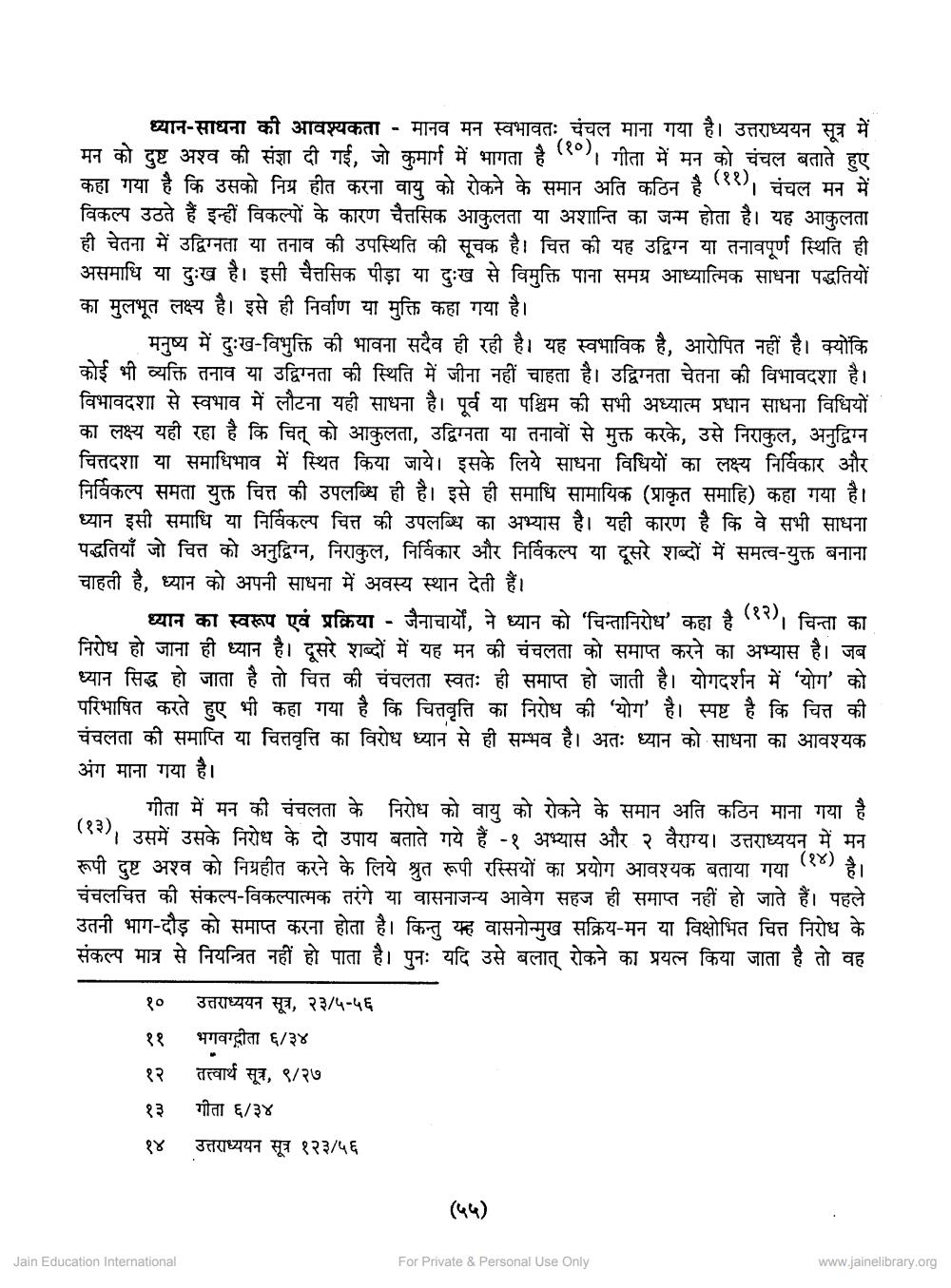Book Title: Jain Sadhna aur Dhyan Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Mahasati_Dway_Smruti_Granth_012025.pdf View full book textPage 3
________________ ध्यान-साधना की आवश्यकता - मानव मन स्वभावतः चंचल माना गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में मन को दुष्ट अश्व की संज्ञा दी गई, जो कुमार्ग में भागता है (१०)। गीता में मन को चंचल बताते हुए कहा गया है कि उसको निग्र हीत करना वायु को रोकने के समान अति कठिन है (११। चंचल मन में विकल्प उठते हैं इन्हीं विकल्पों के कारण चैत्तसिक आकुलता या अशान्ति का जन्म होता है। यह आकुलता ही चेतना में उद्विग्नता या तनाव की उपस्थिति की सूचक है। चित्त की यह उद्विग्न या तनावपूर्ण स्थिति ही असमाधि या दुःख है। इसी चैतसिक पीड़ा या दुःख से विमुक्ति पाना समग्र आध्यात्मिक साधना पद्धतियों का मुलभूत लक्ष्य है। इसे ही निर्वाण या मुक्ति कहा गया है। मनुष्य में दुःख-विभुक्ति की भावना सदैव ही रही है। यह स्वभाविक है, आरोपित नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तनाव या उद्विग्नता की स्थिति में जीना नहीं चाहता है। उद्विग्नता चेतना की विभावदशा है। विभावदशा से स्वभाव में लौटना यही साधना है। पूर्व या पश्चिम की सभी अध्यात्म प्रधान साधना विधियों का लक्ष्य यही रहा है कि चित को आकलता, उद्विग्नता या तनावों से मक्त करके. उसे निराकल. अनद्विग्न चित्तदशा या समाधिभाव में स्थित किया जाये। इसके लिये साधना विधियों का लक्ष्य निर्विकार और निर्विकल्प समता युक्त चित्त की उपलब्धि ही है। इसे ही समाधि सामायिक (प्राकृत समाहि) कहा गया है। ध्यान इसी समाधि या निर्विकल्प चित्त की उपलब्धि का अभ्यास है। यही कारण है कि वे सभी साधना पद्धतियाँ जो चित्त को अनुद्विग्न, निराकुल, निर्विकार और निर्विकल्प या दूसरे शब्दों में समत्व-युक्त बनाना चाहती है, ध्यान को अपनी साधना में अवस्य स्थान देती हैं। ध्यान का स्वरूप एवं प्रक्रिया - जैनाचार्यों, ने ध्यान को 'चिन्तानिरोध' कहा है (१२)। चिन्ता का निरोध हो जाना ही ध्यान है। दूसरे शब्दों में यह मन की चंचलता को समाप्त करने का अभ्यास है। जब ध्यान सिद्ध हो जाता है तो चित्त की चंचलता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। योगदर्शन में 'योग' को परिभाषित करते हुए भी कहा गया है कि चित्तवृत्ति का निरोध की 'योग' है। स्पष्ट है कि चित्त की चंचलता की समाप्ति या चित्तवृत्ति का विरोध ध्यान से ही सम्भव है। अतः ध्यान को साधना का आवश्यक अंग माना गया है। गीता में मन की चंचलता के निरोध को वायु को रोकने के समान अति कठिन माना गया है (१३)। उसमें उसके निरोध के दो उपाय बताते गये हैं -१ अभ्यास और २ वैराग्य। उत्तराध्ययन में मन रूपी दुष्ट अश्व को निग्रहीत करने के लिये श्रुत रूपी रस्सियों का प्रयोग आवश्यक बताया गया (१४) है। चंचलचित्त की संकल्प-विकल्पात्मक तरंगे या वासनाजन्य आवेग सहज ही समाप्त नहीं हो जाते हैं। पहले उतनी भाग-दौड़ को समाप्त करना होता है। किन्तु यह वासनोन्मुख सक्रिय-मन या विक्षोभित चित्त निरोध के संकल्प मात्र से नियन्त्रित नहीं हो पाता है। पुनः यदि उसे बलात् रोकने का प्रयत्न किया जाता है तो वह १० ११ १२ १३ उत्तराध्ययन सूत्र, २३/५-५६ भगवद्गीता ६/३४ तत्त्वार्थ सूत्र, ९/२७ गीता ६/३४ १४ उत्तराध्ययन सूत्र १२३/५६ (५५) Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29