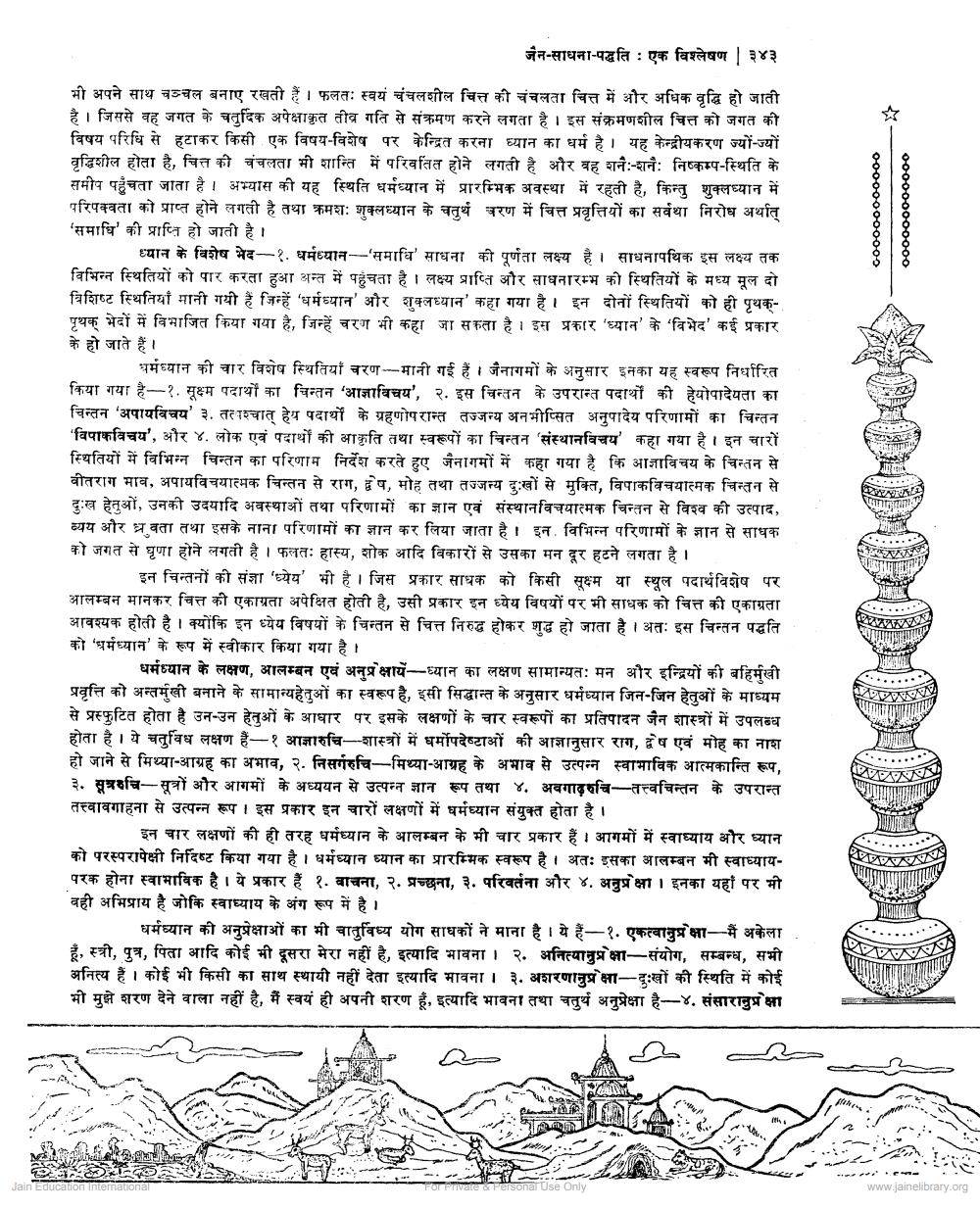Book Title: Jain Sadhna Paddhati Author(s): M P Patairiya Publisher: Z_Ambalalji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012038.pdf View full book textPage 5
________________ जैन-साधना-पद्धति : एक विश्लेषण | ३४३ ०००००००००००० ०००००००००००० भी अपने साथ चञ्चल बनाए रखती हैं । फलतः स्वयं चंचलशील चित्त की चंचलता चित्त में और अधिक वृद्धि हो जाती है। जिससे वह जगत के चतुर्दिक अपेक्षाकृत तीव्र गति से संक्रमण करने लगता है। इस संक्रमणशील चित्त को जगत की विषय परिधि से हटाकर किसी एक विषय-विशेष पर केन्द्रित करना ध्यान का धर्म है। यह केन्द्रीयकरण ज्यों-ज्यों वृद्धिशील होता है, चित्त की चंचलता भी शान्ति में परिवर्तित होने लगती है और वह शनैः-शनैः निष्कम्प-स्थिति के समीप पहुँचता जाता है। अभ्यास की यह स्थिति धर्मध्यान में प्रारम्भिक अवस्था में रहती है, किन्तु शुक्लध्यान में परिपक्वता को प्राप्त होने लगती है तथा क्रमशः शुक्लध्यान के चतुर्थ चरण में चित्त प्रवृत्तियों का सर्वथा निरोध अर्थात् 'समाधि' की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान के विशेष भेद-१. धर्मध्यान-'समाधि' साधना की पूर्णता लक्ष्य है। साधनापथिक इस लक्ष्य तक विभिन्न स्थितियों को पार करता हुआ अन्त में पहुंचता है। लक्ष्य प्राप्ति और साधनारम्भ की स्थितियों के मध्य मूल दो विशिष्ट स्थितियाँ मानी गयी हैं जिन्हें 'धर्मध्यान' और शुक्लध्यान' कहा गया है। इन दोनों स्थितियों को ही पृथक्पृथक् भेदों में विभाजित किया गया है, जिन्हें चरण भी कहा जा सकता है। इस प्रकार 'ध्यान' के 'विभेद' कई प्रकार के हो जाते हैं। धर्मध्यान की चार विशेष स्थितियाँ चरण-मानी गई हैं। जैनागमों के अनुसार इनका यह स्वरूप निर्धारित किया गया है-१. सूक्ष्म पदार्थों का चिन्तन 'आज्ञाविचय', २. इस चिन्तन के उपरान्त पदार्थों की हेयोपादेयता का चिन्तन 'अपायविचय' ३. तत्पश्चात् हेय पदार्थों के ग्रहणोपरान्त तज्जन्य अन भीप्सित अनुपादेय परिणामों का चिन्तन 'विपाकविचय', और ४. लोक एवं पदार्थों की आकृति तथा स्वरूपों का चिन्तन संस्थानविचय' कहा गया है। इन चारों स्थितियों में विभिन्न चिन्तन का परिणाम निर्देश करते हुए जैनागमों में कहा गया है कि आज्ञाविचय के चिन्तन से वीतराग माव, अपायविचयात्मक चिन्तन से राग, द्वेष, मोह तथा तज्जन्य दुःखों से मुक्ति, विपाकविचयात्मक चिन्तन से दुःख हेतुओं, उनकी उदयादि अवस्थाओं तथा परिणामों का ज्ञान एवं संस्थानविचयात्मक चिन्तन से विश्व की उत्पाद, व्यय और ध्र वता तथा इसके नाना परिणामों का ज्ञान कर लिया जाता है। इन विभिन्न परिणामों के ज्ञान से साधक को जगत से घृणा होने लगती है । फलतः हास्य, शोक आदि विकारों से उसका मन दूर हटने लगता है। इन चिन्तनों की संज्ञा 'ध्येय' भी है। जिस प्रकार साधक को किसी सूक्ष्म या स्थुल पदार्थ विशेष पर आलम्बन मानकर चित्त की एकाग्रता अपेक्षित होती है, उसी प्रकार इन ध्येय विषयों पर भी साधक को चित्त की एकाग्रता आवश्यक होती है। क्योंकि इन ध्येय विषयों के चिन्तन से चित्त निरुद्ध होकर शुद्ध हो जाता है । अतः इस चिन्तन पद्धति को 'धर्मध्यान' के रूप में स्वीकार किया गया है। धर्मध्यान के लक्षण, आलम्बन एवं अनुप्रंक्षायें-ध्यान का लक्षण सामान्यत: मन और इन्द्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अन्तर्मुखी बनाने के सामान्यहेतुओं का स्वरूप है, इसी सिद्धान्त के अनुसार धर्मध्यान जिन-जिन हेतुओं के माध्यम से प्रस्फुटित होता है उन-उन हेतुओं के आधार पर इसके लक्षणों के चार स्वरूपों का प्रतिपादन जैन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। ये चतुर्विध लक्षण हैं-१ आज्ञारुचि--शास्त्रों में धर्मोपदेष्टाओं की आज्ञानुसार राग, द्वेष एवं मोह का नाश हो जाने से मिथ्या-आग्रह का अभाव, २. निसर्गरुचि-मिथ्या-आग्रह के अभाव से उत्पन्न स्वाभाविक आत्मकान्ति रूप, ३. सूत्ररुचि-सूत्रों और आगमों के अध्ययन से उत्पन्न ज्ञान रूप तथा ४. अवगाढ़रुचि-तत्त्वचिन्तन के उपरान्त तत्त्वावगाहना से उत्पन्न रूप । इस प्रकार इन चारों लक्षणों में धर्मध्यान संयुक्त होता है। इन चार लक्षणों की ही तरह धर्मध्यान के आलम्बन के भी चार प्रकार हैं । आगमों में स्वाध्याय और ध्यान को परस्परापेक्षी निर्दिष्ट किया गया है। धर्मध्यान ध्यान का प्रारम्मिक स्वरूप है। अतः इसका आलम्बन मी स्वाध्यायपरक होना स्वाभाविक है। ये प्रकार हैं १. वाचना, २. प्रच्छना, ३. परिवर्तना और ४. अनुप्रेक्षा । इनका यहाँ पर भी वही अभिप्राय है जोकि स्वाध्याय के अंग रूप में है। धर्मध्यान की अनुप्रेक्षाओं का भी चातुर्विध्य योग साधकों ने माना है । ये हैं-१. एकत्वानुप्रेक्षा-मैं अकेला हूँ, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी दूसरा मेरा नहीं है, इत्यादि भावना। २. अनित्यानुप्रेक्षा-संयोग, सम्बन्ध, सभी अनित्य हैं । कोई भी किसी का साथ स्थायी नहीं देता इत्यादि भावना । ३. अशरणानुप्रक्षा-दुःखों की स्थिति में कोई भी मुझे शरण देने वाला नहीं है, मैं स्वयं ही अपनी शरण हूँ, इत्यादि भावना तथा चतुर्थ अनुप्रेक्षा है-४. संसारानुप्रेक्षा 5. TACardhai Torrnvare & Personar Use Only Jain Education International www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9