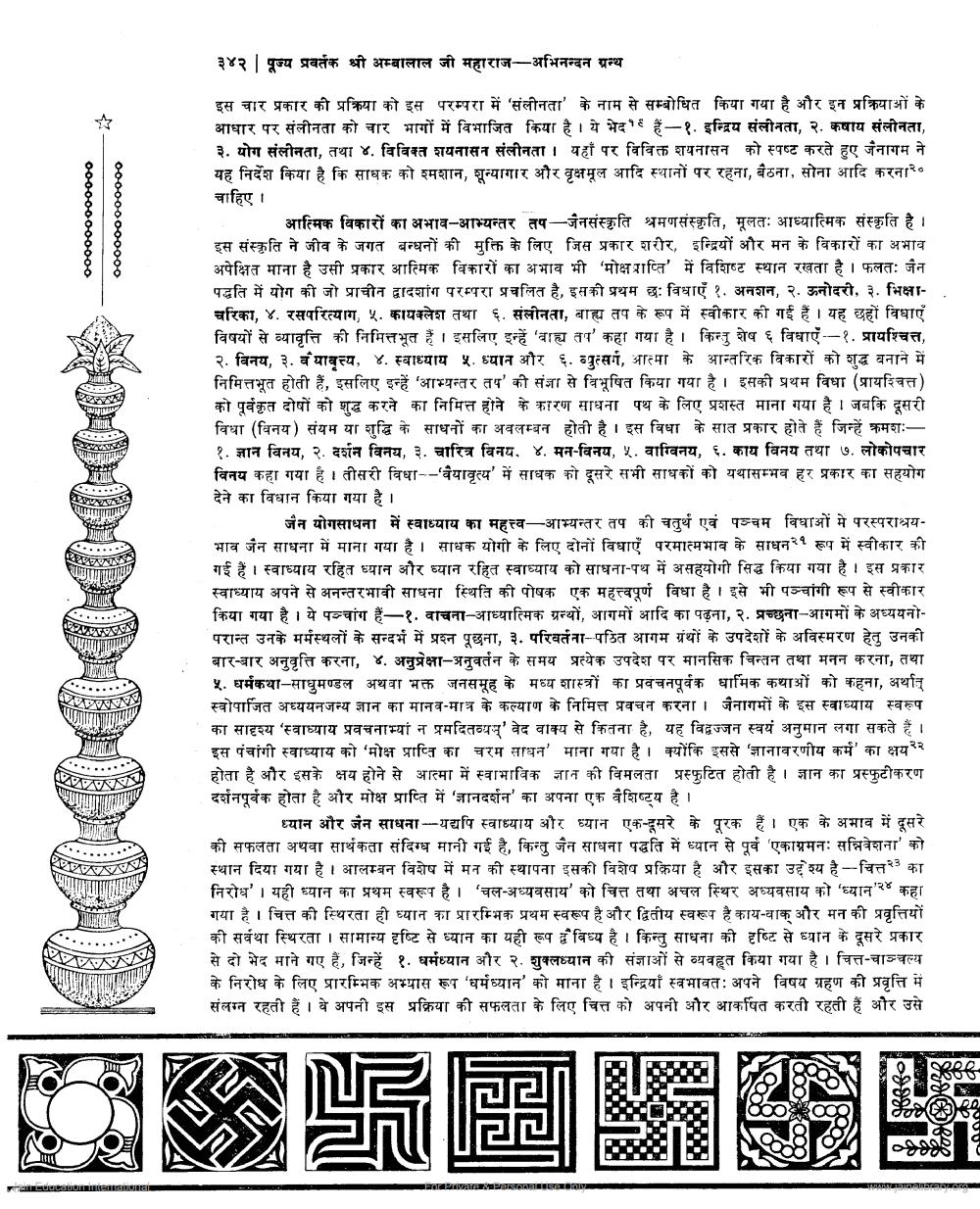Book Title: Jain Sadhna Paddhati Author(s): M P Patairiya Publisher: Z_Ambalalji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012038.pdf View full book textPage 4
________________ ३४२ | पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी महाराज-अभिनन्दन ग्रन्थ 1 000000000000 ०००००००००००० इस चार प्रकार की प्रक्रिया को इस परम्परा में 'संलीनता' के नाम से सम्बोधित किया गया है और इन प्रक्रियाओं के आधार पर संलीनता को चार भागों में विभाजित किया है । ये भेद६ हैं-१. इन्द्रिय संलीनता, २. कषाय संलीनता, ३. योग संलीनता, तथा ४. विविक्त शयनासन संलीनता। यहाँ पर विविक्त शयनासन को स्पष्ट करते हुए जैनागम ने यह निर्देश किया है कि साधक को श्मशान, शून्यागार और वृक्षमूल आदि स्थानों पर रहना, बैठना, सोना आदि करना२० चाहिए। आत्मिक विकारों का अभाव-आभ्यन्तर तप-जैनसंस्कृति श्रमणसंस्कृति, मूलतः आध्यात्मिक संस्कृति है। इस संस्कृति ने जीव के जगत बन्धनों की मुक्ति के लिए जिस प्रकार शरीर, इन्द्रियों और मन के विकारों का अभाव अपेक्षित माना है उसी प्रकार आत्मिक विकारों का अभाव भी 'मोक्ष प्राप्ति' में विशिष्ट स्थान रखता है । फलतः जैन पद्धति में योग की जो प्राचीन द्वादशांग परम्परा प्रचलित है, इसकी प्रथम छः विधाएँ १. अनशन, २. ऊनोदरी, ३. भिक्षाचरिका, ४. रसपरित्याग, ५. कायक्लेश तथा ६. संलीनता, बाह्य तप के रूप में स्वीकार की गई हैं। यह छहों विधाएँ विषयों से व्यावृत्ति की निमित्तभूत हैं । इसलिए इन्हें 'बाह्य तप' कहा गया है। किन्तु शेष ६ विधाएँ--१. प्रायश्चित्त, २. विनय, ३. व यावृत्त्य, ४. स्वाध्याय ५. ध्यान और ६. पुत्सर्ग, आत्मा के आन्तरिक विकारों को शुद्ध बनाने में निमित्तभूत होती हैं, इसलिए इन्हें 'आभ्यन्तर तय' की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इसकी प्रथम विधा (प्रायश्चित्त) को पूर्वकृत दोषों को शुद्ध करने का निमित्त होने के कारण साधना पथ के लिए प्रशस्त माना गया है । जबकि दूसरी विधा (विनय) संयम या शुद्धि के साधनों का अवलम्बन होती है । इस विधा के सात प्रकार होते हैं जिन्हें क्रमशः१. ज्ञान विनय, २. दर्शन विनय, ३. चारित्र विनय, ४. मन-विनय, ५. वाग्विनय, ६. काय विनय तथा ७. लोकोपचार विनय कहा गया है। तीसरी विधा--'वैयावृत्य' में साधक को दूसरे सभी साधकों को यथासम्भव हर प्रकार का सहयोग देने का विधान किया गया है। जैन योगसाधना में स्वाध्याय का महत्त्व-आभ्यन्तर तप की चतुर्थ एवं पञ्चम विधाओं में परस्पराश्रयभाव जैन साधना में माना गया है। साधक योगी के लिए दोनों विधाएँ परमात्मभाव के साधन२१ रूप में स्वीकार की गई हैं । स्वाध्याय रहित ध्यान और ध्यान रहित स्वाध्याय को साधना-पथ में असहयोगी सिद्ध किया गया है । इस प्रकार स्वाध्याय अपने से अनन्तरभावी साधना स्थिति की पोषक एक महत्त्वपूर्ण विधा है । इसे भी पञ्चांगी रूप से स्वीकार किया गया है । ये पञ्चांग हैं-१. वाचना-आध्यात्मिक ग्रन्थों, आगमों आदि का पढ़ना, २. प्रच्छना-आगमों के अध्ययनोपरान्त उनके मर्मस्थलों के सन्दर्भ में प्रश्न पूछना, ३. परिवर्तना-पठित आगम ग्रंथों के उपदेशों के अविस्मरण हेतु उनकी बार-बार अनुवृत्ति करना, ४. अनुप्रेक्षा-अनुवर्तन के समय प्रत्येक उपदेश पर मानसिक चिन्तन तथा मनन करना, तथा ५. धर्मकथा-साधुमण्डल अथवा भक्त जनसमूह के मध्य शास्त्रों का प्रवचनपूर्वक धार्मिक कथाओं को कहना, अर्थात् स्वोपाजित अध्ययनजन्य ज्ञान का मानव-मात्र के कल्याण के निमित्त प्रवचन करना । जैनागमों के इस स्वाध्याय स्वरूप का सादृश्य 'स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्' वेद वाक्य से कितना है, यह विद्वज्जन स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इस पंचांगी स्वाध्याय को 'मोक्ष प्राप्ति का चरम साधन' माना गया है। क्योंकि इससे 'ज्ञानावरणीय कर्म' का क्षय२२ होता है और इसके क्षय होने से आत्मा में स्वाभाविक ज्ञान की विमलता प्रस्फुटित होती है। ज्ञान का प्रस्फुटीकरण दर्शनपूर्वक होता है और मोक्ष प्राप्ति में 'ज्ञानदर्शन' का अपना एक वैशिष्ट्य है। ध्यान और जैन साधना-यद्यपि स्वाध्याय और ध्यान एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे की सफलता अथवा सार्थकता संदिग्ध मानी गई है, किन्तु जैन साधना पद्धति में ध्यान से पूर्व 'एकानमनः सन्निवेशना' को स्थान दिया गया है। आलम्बन विशेष में मन की स्थापना इसकी विशेष प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य है -चित्तका निरोध' । यही ध्यान का प्रथम स्वरूप है। 'चल-अध्यवसाय' को चित्त तथा अचल स्थिर अध्यवसाय को 'ध्यान'२४ कहा गया है । चित्त की स्थिरता ही ध्यान का प्रारम्भिक प्रथम स्वरूप है और द्वितीय स्वरूप है काय-वाक् और मन की प्रवृत्तियों की सर्वथा स्थिरता । सामान्य दृष्टि से ध्यान का यही रूप द्वविध्य है । किन्तु साधना की दृष्टि से ध्यान के दूसरे प्रकार से दो भेद माने गए हैं, जिन्हें १. धर्मध्यान और २. शुक्लध्यान की संज्ञाओं से व्यवहृत किया गया है । चित्त-चाञ्चल्य के निरोध के लिए प्रारम्भिक अभ्यास रूप 'धर्मध्यान' को माना है । इन्द्रियाँ स्वभावत: अपने विषय ग्रहण की प्रवृत्ति में संलग्न रहती हैं । वे अपनी इस प्रक्रिया की सफलता के लिए चित्त को अपनी और आकर्षित करती रहती हैं और उसे 原圖圖圖圖圖圖 ESP 0000 FOR P ATIESEPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9