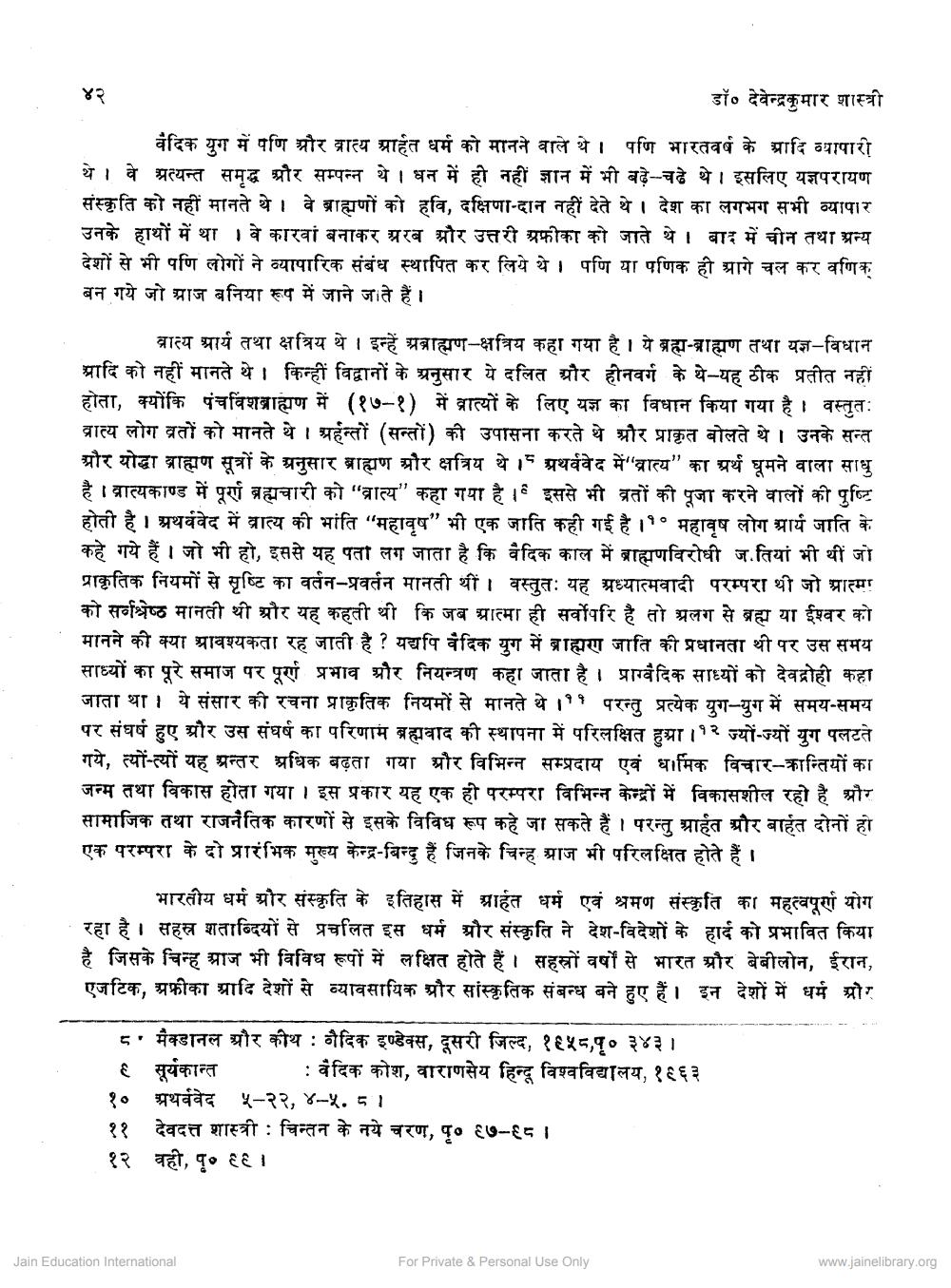Book Title: Jain Dharm aur uske Siddhant Author(s): Devendramuni Shastri Publisher: Z_Jinvijay_Muni_Abhinandan_Granth_012033.pdf View full book textPage 3
________________ डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री वैदिक युग में पणि और व्रात्य आहत धर्म को मानने वाले थे। पणि भारतवर्ष के आदि व्यापारी थे। वे अत्यन्त समृद्ध और सम्पन्न थे । धन में ही नहीं ज्ञान में भी बढ़े-चढे थे। इसलिए यज्ञपरायण संस्कृति को नहीं मानते थे। वे ब्राह्मणों को हवि, दक्षिणा-दान नहीं देते थे। देश का लगभग सभी व्यापार उनके हाथों में था । वे कारवां बनाकर अरब और उत्तरी अफ्रीका को जाते थे। बाद में चीन तथा अन्य देशों से भी पणि लोगों ने व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिये थे। पणि या पणिक ही आगे चल कर वणिक बन गये जो पाज बनिया रूप में जाने जाते हैं। व्रात्य आर्य तथा क्षत्रिय थे । इन्हें अब्राह्मण-क्षत्रिय कहा गया है। ये ब्रह्म-ब्राह्मण तथा यज्ञ-विधान आदि को नहीं मानते थे। किन्हीं विद्वानों के अनुसार ये दलित और हीनवर्ग के थे-यह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पंचविंशब्राह्मण में (१७-१) में व्रात्यों के लिए यज्ञ का विधान किया गया है। वस्तुतः व्रात्य लोग व्रतों को मानते थे। अर्हन्तों (सन्तों) की उपासना करते थे और प्राकृत बोलते थे। उनके सन्त और योद्धा ब्राह्मण सूत्रों के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। अथर्ववेद में"व्रात्य" का अर्थ घूमने वाला साधु है । व्रात्यकाण्ड में पूर्ण ब्रह्मचारी को "व्रात्य" कहा गया है। इससे भी व्रतों की पूजा करने वालों की पुष्टि होती है । अथर्ववेद में व्रात्य की भांति “महावृष" भी एक जाति कही गई है ।'' महावृष लोग आर्य जाति के कहे गये हैं । जो भी हो, इससे यह पता लग जाता है कि वैदिक काल में ब्राह्मणविरोधी ज.तियां भी थीं जो प्राकृतिक नियमों से सृष्टि का वर्तन-प्रवर्तन मानती थीं। वस्तुतः यह अध्यात्मवादी परम्परा थी जो प्रात्मा को सर्वश्रेष्ठ मानती थी और यह कहती थी कि जब आत्मा ही सर्वोपरि है तो अलग से ब्रह्म या ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता रह जाती है ? यद्यपि वैदिक युग में ब्राह्मण जाति की प्रधानता थी पर उस समय साध्यों का पूरे समाज पर पूर्ण प्रभाव और नियन्त्रण कहा जाता है। प्राग्वैदिक साध्यों को देवद्रोही कहा जाता था। ये संसार की रचना प्राकृतिक नियमों से मानते थे। परन्तु प्रत्येक युग-युग में समय-समय पर संघर्ष हुए और उस संघर्ष का परिणाम ब्रह्मवाद की स्थापना में परिलक्षित हुआ।१२ ज्यों-ज्यों युग पलटते गये, त्यों-त्यों यह अन्तर अधिक बढ़ता गया और विभिन्न सम्प्रदाय एवं धार्मिक विचार-क्रान्तियों का जन्म तथा विकास होता गया। इस प्रकार यह एक ही परम्परा विभिन्न केन्द्रों में विकासशील रहो है और सामाजिक तथा राजनैतिक कारणों से इसके विविध रूप कहे जा सकते हैं । परन्तु पाहत और बार्हत दोनों हो एक परम्परा के दो प्रारंभिक मुख्य केन्द्र-बिन्दु हैं जिनके चिन्ह आज भी परिलक्षित होते हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति के इतिहास में प्रार्हत धर्म एवं श्रमण संस्कृति का महत्वपूर्ण योग · रहा है। सहस्र शताब्दियों से प्रचलित इस धर्म और संस्कृति ने देश-विदेशों के हार्द को प्रभावित किया है जिसके चिन्ह आज भी विविध रूपों में लक्षित होते हैं। सहस्रों वर्षों से भारत और बेबीलोन, ईरान, एजटिक, अफ्रीका आदि देशों से व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबन्ध बने हुए हैं। इन देशों में धर्म और ८' मैक्डानल और कीथ : गैदिक इण्डेक्स, दूसरी जिल्द, १६५८,पृ० ३४३ । ६ सूर्यकान्त : वैदिक कोश, वाराणसेय हिन्दू विश्वविद्यालय, १६६३ १० अथर्ववेद ५-२२, ४-५.८ । ११ देवदत्त शास्त्री : चिन्तन के नये चरण, १०६७-६८ । १२ वही, पृ० ६६। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10