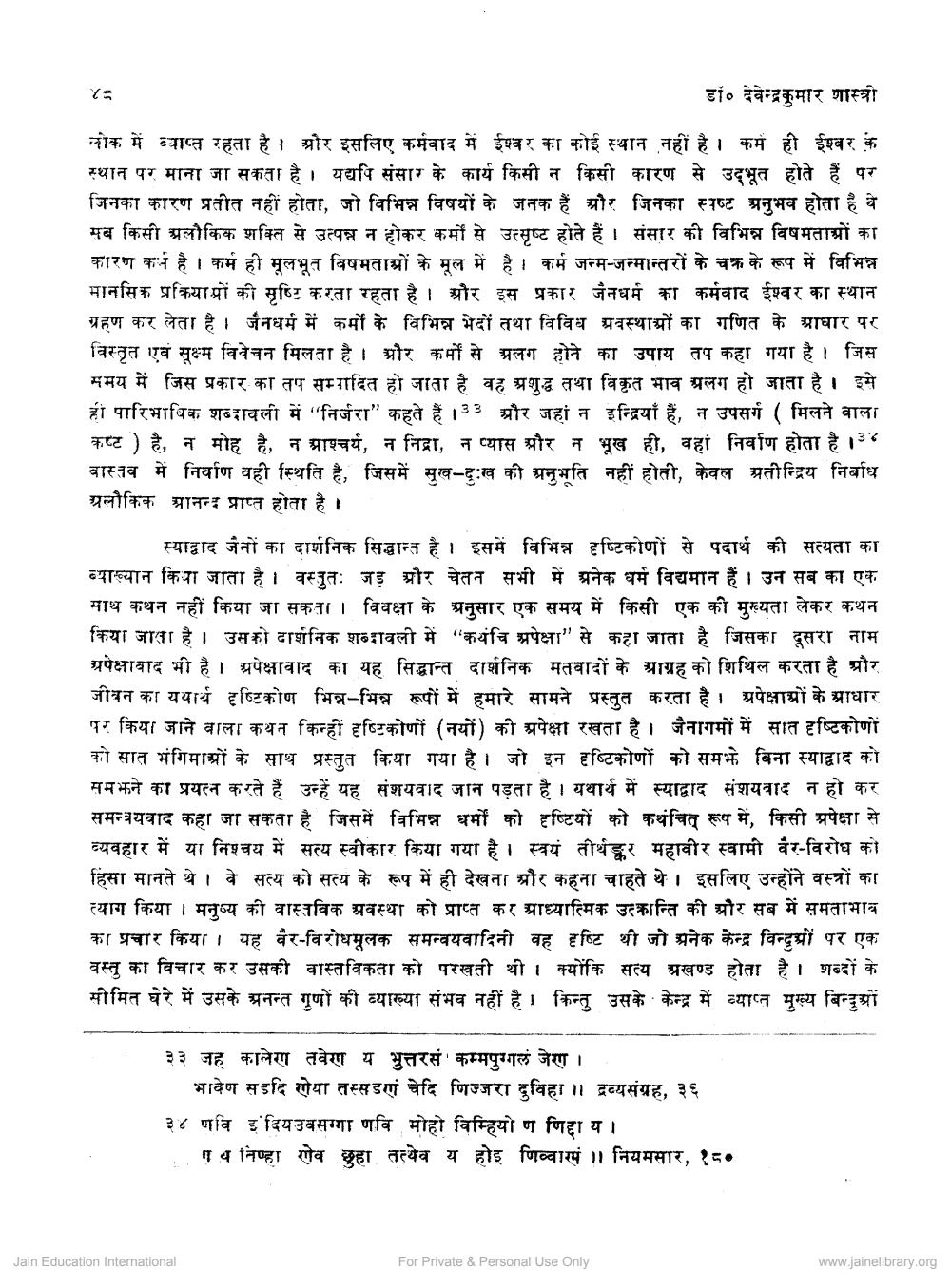Book Title: Jain Dharm aur uske Siddhant Author(s): Devendramuni Shastri Publisher: Z_Jinvijay_Muni_Abhinandan_Granth_012033.pdf View full book textPage 9
________________ डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री लोक में व्याप्त रहता है। और इसलिए कर्मवाद में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। कम ही ईश्वर के स्थान पर माना जा सकता है। यद्यपि संसार के कार्य किसी न किसी कारण से उद्भूत होते हैं पर जिनका कारण प्रतीत नहीं होता, जो विभिन्न विषयों के जनक हैं और जिनका स्पष्ट अनुभव होता है वे सब किसी अलौकिक शक्ति से उत्पन्न न होकर कर्मों से उत्सष्ट होते हैं। संसार की विभिन्न विषमताओं का कारण कर्न है। कर्म ही मुलभूत विषमताओं के मूल में है। कर्म जन्म-जन्मान्तरों के चक्र के रूप में विभिन्न मानसिक प्रकियामों की सृष्टि करता रहता है। और इस प्रकार जैनधर्म का कर्मवाद ईश्वर का स्थान ग्रहण कर लेता है। जैनधर्म में कर्मों के विभिन्न भेदों तथा विविध अवस्थाओं का गणित के आधार पर विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचन मिलता है। और कर्मों से अलग होने का उपाय तप कहा गया है। जिस ममय में जिस प्रकार का तप सम्पादित हो जाता है वह अशुद्ध तथा विकृत भाव अलग हो जाता है। इसे ही पारिभाषिक शब्दावली में "निर्जरा" कहते हैं। 33 और जहां न इन्द्रियाँ हैं, न उपसर्ग ( मिलने वाला कष्ट ) है, न मोह है, न आश्चर्य, न निद्रा, न प्यास और न भूख ही, वहां निर्वाण होता है । वास्तव में निर्वाण वही स्थिति है, जिसमें सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती, केवल अतीन्द्रिय निर्बाध अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है। स्याद्वाद जैनों का दार्शनिक सिद्धान्त है। इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों से पदार्थ की सत्यता का व्याख्यान किया जाता है। वस्तुतः जड़ और चेतन सभी में अनेक धर्म विद्यमान हैं। उन सब का एक माथ कथन नहीं किया जा सकता। विवक्षा के अनुसार एक समय में किसी एक की मुख्यता लेकर कथन किया जाता है। उसको दार्शनिक शब्दावली में "कयंचि अपेक्षा" से कहा जाता है जिसका दूसरा नाम अपेक्षावाद भी है। अपेक्षावाद का यह सिद्धान्त दार्शनिक मतवादों के प्राग्रह को शिथिल करता है और जीवन का यथार्थ दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अपेक्षाओं के आधार पर किया जाने वाला कथन किन्हीं दृष्टिकोणों (नयों) की अपेक्षा रखता है। जैनागमों में सात दृष्टिकोणों को सात भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। जो इन दृष्टिकोणों को समझे बिना स्याद्वाद को समझने का प्रयत्न करते हैं उन्हें यह संशयवाद जान पड़ता है। यथार्थ में स्याद्वाद संशयवाद न हो कर समन्वयवाद कहा जा सकता है जिसमें विभिन्न धर्मों को दृष्टियों को कथंचित् रूप में, किसी अपेक्षा से व्यवहार में या निश्चय में सत्य स्वीकार किया गया है। स्वयं तीर्थङ्कर महावीर स्वामी वैर-विरोध को हिसा मानते थे। वे सत्य को सत्य के रूप में ही देखना और कहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया। मनुष्य की वास्तविक अवस्था को प्राप्त कर आध्यात्मिक उत्क्रान्ति की और सब में समताभाव का प्रचार किया। यह वैर-विरोधमूलक समन्वयवादिनी वह दृष्टि थी जो अनेक केन्द्र विन्दुनों पर एक वस्तु का विचार कर उसकी वास्तविकता को परखती थी। क्योंकि सत्य अखण्ड होता है। शब्दों के सीमित घेरे में उसके अनन्त गुणों की व्याख्या संभव नहीं है। किन्तु उसके केन्द्र में व्याप्त मुख्य बिन्दुओं ३३ जह कालेण तवेण य भुत्तरसं ' कम्मपुग्गलं जेरण । ___ भावेण सडदि रणेया तस्सडणं चेदि णिज्जरा दुविहा ॥ द्रव्यसंग्रह, ३६ ३४ णवि इदिय उवसग्गा णवि मोहो विम्हियो ण णिद्दा य । 14 निहा रणेव छुहा तत्येव य होइ णिव्वारमं । नियमसार, १८. Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10