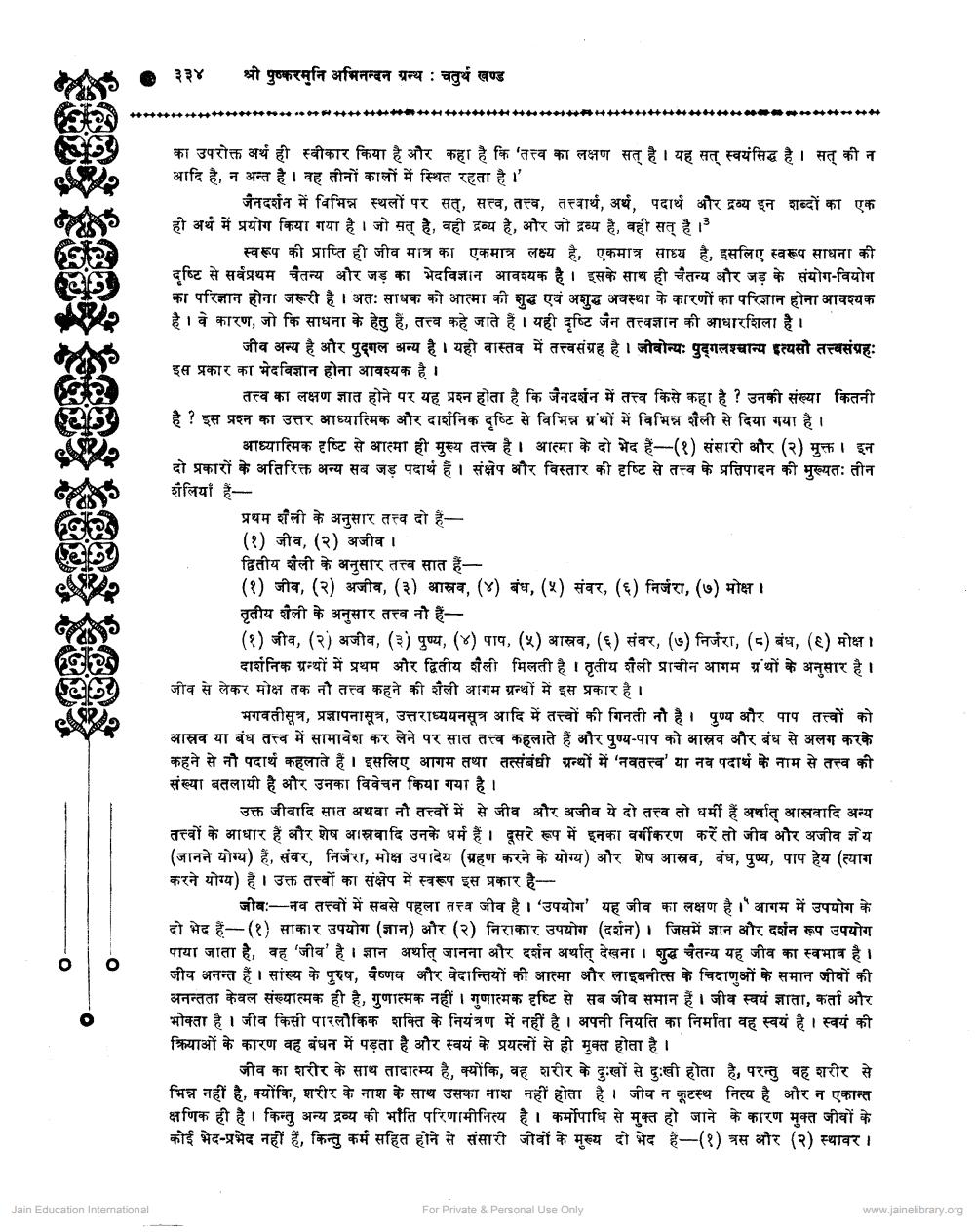Book Title: Jain Darshan me Tattva chintan Author(s): Dharmasheeliashreeji Publisher: Z_Pushkarmuni_Abhinandan_Granth_012012.pdf View full book textPage 2
________________ ० Jain Education International ३३४ श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : चतुर्थ खण्ड का उपरोक्त अर्थ ही स्वीकार किया है और कहा है कि 'तत्व का लक्षण सत् है । यह सत् स्वयंसिद्ध है । सत् की न आदि है, न अन्त है। वह तीनों कालों में स्थित रहता है ।' जैनदर्शन में विभिन्न स्थलों पर सत्, सत्त्व, तत्त्व, तस्वार्थ, अर्थ, पदार्थ और द्रव्य इन शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। जो सत् है, वही द्रव्य है, और जो द्रव्य है, वही सत् है । 3 स्वरूप की प्राप्ति ही जीव मात्र का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र साध्य है, इसलिए स्वरूप साधना की दृष्टि से सर्वप्रथम चैतन्य और जड़ का भेदविज्ञान आवश्यक है। इसके साथ ही चैतन्य और जड़ के संयोग-वियोग का परिज्ञान होना जरूरी है । अतः साधक को आत्मा की शुद्ध एवं अशुद्ध अवस्था के कारणों का परिज्ञान होना आवश्यक है । वे कारण, जो कि साधना के हेतु हैं, तत्त्व कहे जाते हैं । यही दृष्टि जैन तत्त्वज्ञान की आधारशिला है । जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है । यहो वास्तव में तत्त्वसंग्रह है । जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः इस प्रकार का भेदविज्ञान होना आवश्यक है । तत्त्व का लक्षण ज्ञात होने पर यह प्रश्न होता है कि जैनदर्शन में तत्त्व किसे कहा है ? उनकी संख्या कितनी है ? इस प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न शैली से दिया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा ही मुख्य तत्त्व है । आत्मा के दो भेद हैं- (१) संसारी और (२) मुक्त । इन दो प्रकारों के अतिरिक्त अन्य सब जड़ पदार्थ हैं। संक्षेप और विस्तार की दृष्टि से तत्त्व के प्रतिपादन की मुख्यतः तीन हनियाँ - प्रथम शैली के अनुसार तत्त्व दो हैं(१) जीव, (२) अजीव । द्वितीय शैली के अनुसार तत्त्व सात हैं (१) जीव, (२) अजीव, (३) आस्रव, (४) बंध, (५) संवर, (६) निर्जरा, (७) मोक्ष | तृतीय शैली के अनुसार तत्त्व नी है— (१) जीव, (२) अजीव, (३) पुण्य, (४) पाप, (५) आस्रव, (६) संवर, (७) निर्जरा, (८) बंध, (६) मोक्ष | दार्शनिक ग्रन्थों में प्रथम और द्वितीय शैली मिलती है । तृतीय शैली प्राचीन आगम ग्रंथों के अनुसार है । जीव से लेकर मोक्ष तक नौ तत्त्व कहने की शैली आगम ग्रन्थों में इस प्रकार है । भगवतीसूत्र, प्रज्ञापनासूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र आदि में तत्त्वों की गिनती नौ है । पुण्य और पाप तत्त्वों को आसव या बंध तत्त्व में सामावेश कर लेने पर सात तत्त्व कहलाते हैं और पुण्य पाप को आस्रव और बंध से अलग करके कहने से नौ पदार्थ कहलाते हैं । इसलिए आगम तथा तत्संबंधी ग्रन्थों में 'नवतत्त्व' या नव पदार्थ के नाम से तत्त्व की संख्या बतलायी है और उनका विवेचन किया गया है। उक्त जीवादि सात अथवा नौ तत्त्वों में से जीव और अजीव ये दो तत्त्व तो धर्मी हैं अर्थात् आस्रवादि अन्य तत्त्वों के आधार हैं और शेष आस्रवादि उनके धर्म हैं। दूसरे रूप में इनका वर्गीकरण करें तो जीव और अजीव ज्ञ ेय (जानने योग्य) हैं, संवर, निर्जरा, मोक्ष उपादेय ( ग्रहण करने के योग्य) और शेष आस्रव, बंध, पुण्य, पाप हेय ( त्याग करने योग्य) हैं । उक्त तत्त्वों का संक्षेप में स्वरूप इस प्रकार है जीब:-नव तत्त्वों में सबसे पहला तत्त्व जीव है । 'उपयोग' यह जीव का लक्षण है ।' आगम में उपयोग के दो भेद हैं- ( १ ) साकार उपयोग (ज्ञान) और (२) निराकार उपयोग (दर्शन)। जिसमें ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग पाया जाता है, वह 'जीव' है। ज्ञान अर्थात् जानना और दर्शन अर्थात् देखना । शुद्ध चैतन्य यह जीव का स्वभाव है । जीव अनन्त हैं । सांख्य के पुरुष, वैष्णव और वेदान्तियों की आत्मा और लाइबनीत्स के चिदाणुओं के समान जीवों की अनन्तता केवल संख्यात्मक ही है, गुणात्मक नहीं । गुणात्मक दृष्टि से भोक्ता है । जीव किसी पारलौकिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। क्रियाओं के कारण वह बंधन में पड़ता है और स्वयं के प्रयत्नों से ही सब जीव समान हैं। जीव स्वयं ज्ञाता, कर्ता और अपनी नियति का निर्माता वह स्वयं है। स्वयं की मुक्त होता है । जीव का शरीर के साथ तादात्म्य है, क्योंकि, वह शरीर के दुःखों से दुःखी होता है, परन्तु वह शरीर से भिन्न नहीं है, क्योंकि, शरीर के नाश के साथ उसका नाश नहीं होता है। जीव न कूटस्थ क्षणिक ही है । किन्तु अन्य द्रव्य की भाँति परिणामीनित्य है । कर्मोपाधि से मुक्त हो जाने कोई भेद-प्रभेद नहीं है, किन्तु कर्म सहित होने से संसारी जीवों के मुख्य दो भेद हैं- ( १ ) नित्य है और न एकान्त के कारण मुक्त जीवों के स और (२) स्थावर । For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10