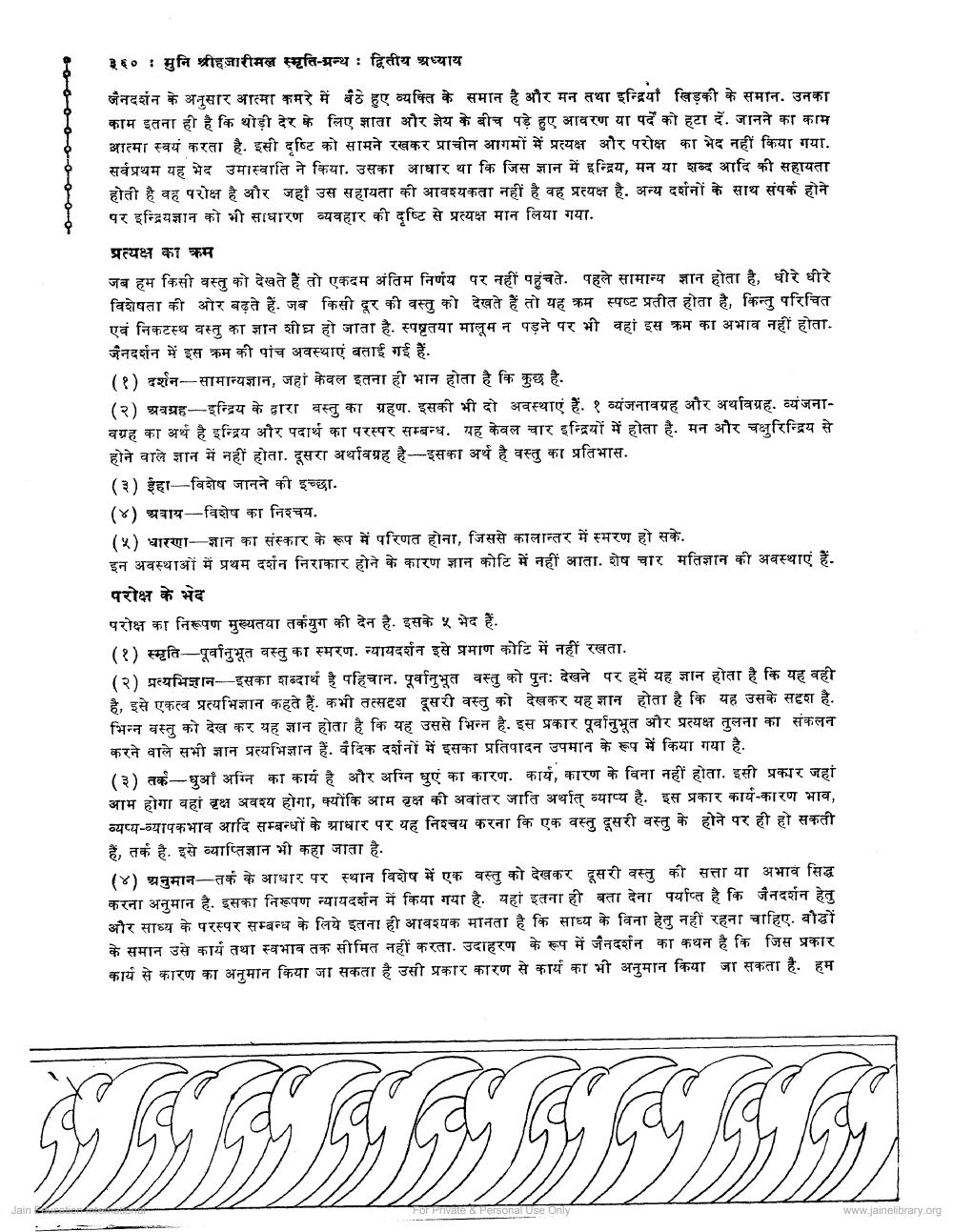Book Title: Jain Darshan aur Vigyan Author(s): Indra Chandra Shastri Publisher: Z_Hajarimalmuni_Smruti_Granth_012040.pdf View full book textPage 4
________________ ३६० : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-प्रन्थ : द्वितीय अध्याय जैनदर्शन के अनुसार आत्मा कमरे में बैठे हुए व्यक्ति के समान है और मन तथा इन्द्रियाँ खिड़की के समान. उनका काम इतना ही है कि थोड़ी देर के लिए ज्ञाता और ज्ञेय के बीच पड़े हुए आवरण या पर्दै को हटा दें. जानने का काम आत्मा स्वयं करता है. इसी दृष्टि को सामने रखकर प्राचीन आगमों में प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद नहीं किया गया. सर्वप्रथम यह भेद उमास्वाति ने किया. उसका आधार था कि जिस ज्ञान में इन्द्रिय, मन या शब्द आदि की सहायता होती है वह परोक्ष है और जहाँ उस सहायता की आवश्यकता नहीं है वह प्रत्यक्ष है. अन्य दर्शनों के साथ संपर्क होने पर इन्द्रियज्ञान को भी साधारण व्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक्ष मान लिया गया. प्रत्यक्ष का क्रम जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो एकदम अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचते. पहले सामान्य ज्ञान होता है, धीरे धीरे विशेषता की ओर बढ़ते हैं. जब किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो यह क्रम स्पष्ट प्रतीत होता है, किन्तु परिचित एवं निकटस्थ वस्तु का ज्ञान शीघ्र हो जाता है. स्पर्धतया मालूम न पड़ने पर भी बहां इस क्रम का अभाव नहीं होता. जैनदर्शन में इस क्रम की पांच अवस्थाएं बताई गई हैं. (१) दर्शन-सामान्यज्ञान, जहां केवल इतना ही भान होता है कि कुछ है. (२) अवग्रह-इन्द्रिय के द्वारा वस्तु का ग्रहण. इसकी भी दो अवस्थाएं हैं. १ व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह. व्यंजनावग्रह का अर्थ है इन्द्रिय और पदार्थ का परस्पर सम्बन्ध. यह केवल चार इन्द्रियों में होता है. मन और चक्षुरिन्द्रिय से होने वाले ज्ञान में नहीं होता. दूसरा अर्थावग्रह है-इसका अर्थ है वस्तु का प्रतिभास. (३) ईहा—विशेष जानने की इच्छा . (४) अवाय-विशेष का निश्चय. (५) धारणा–ज्ञान का संस्कार के रूप में परिणत होना, जिससे कालान्तर में स्मरण हो सके. इन अवस्थाओं में प्रथम दर्शन निराकार होने के कारण ज्ञान कोटि में नहीं आता. शेष चार मतिज्ञान की अवस्थाएं हैं. परोक्ष के भेद परोक्ष का निरूपण मुख्यतया तर्कयुग की देन है. इसके ५ भेद हैं. (१) स्मृति–पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण. न्यायदर्शन इसे प्रमाण कोटि में नहीं रखता. (२) प्रत्यभिज्ञान-इसका शब्दार्थ है पहिचान. पूर्वानुभूत वस्तु को पुनः देखने पर हमें यह ज्ञान होता है कि यह वही है, इसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहते हैं. कभी तत्सदृश दूसरी वस्तु को देखकर यह ज्ञान होता है कि यह उसके सदृश है. भिन्न वस्तु को देख कर यह ज्ञान होता है कि यह उससे भिन्न है. इस प्रकार पूर्वानुभूत और प्रत्यक्ष तुलना का संकलन करने वाले सभी ज्ञान प्रत्यभिज्ञान हैं. वैदिक दर्शनों में इसका प्रतिपादन उपमान के रूप में किया गया है. (३) तर्क-धुओं अग्नि का कार्य है और अग्नि धुएं का कारण. कार्य, कारण के विना नहीं होता. इसी प्रकार जहां आम होगा वहां वृक्ष अवश्य होगा, क्योंकि आम वृक्ष की अवांतर जाति अर्थात् व्याप्य है. इस प्रकार कार्य-कारण भाव, व्यप्य-व्यापकभाव आदि सम्बन्धों के आधार पर यह निश्चय करना कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के होने पर ही हो सकती हैं, तर्क है. इसे व्याप्तिज्ञान भी कहा जाता है. (४) अनुमान-तर्क के आधार पर स्थान विशेष में एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु की सत्ता या अभाव सिद्ध करना अनुमान है. इसका निरूपण न्यायदर्शन में किया गया है. यहां इतना ही बता देना पर्याप्त है कि जैनदर्शन हेतु और साध्य के परस्पर सम्बन्ध के लिये इतना ही आवश्यक मानता है कि साध्य के विना हेतु नहीं रहना चाहिए. बौद्धों के समान उसे कार्य तथा स्वभाव तक सीमित नहीं करता. उदाहरण के रूप में जनदर्शन का कथन है कि जिस प्रकार कार्य से कारण का अनुमान किया जा सकता है उसी प्रकार कारण से कार्य का भी अनुमान किया जा सकता है. हम RECE Jain Canolianimoon ne & Personal use only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11