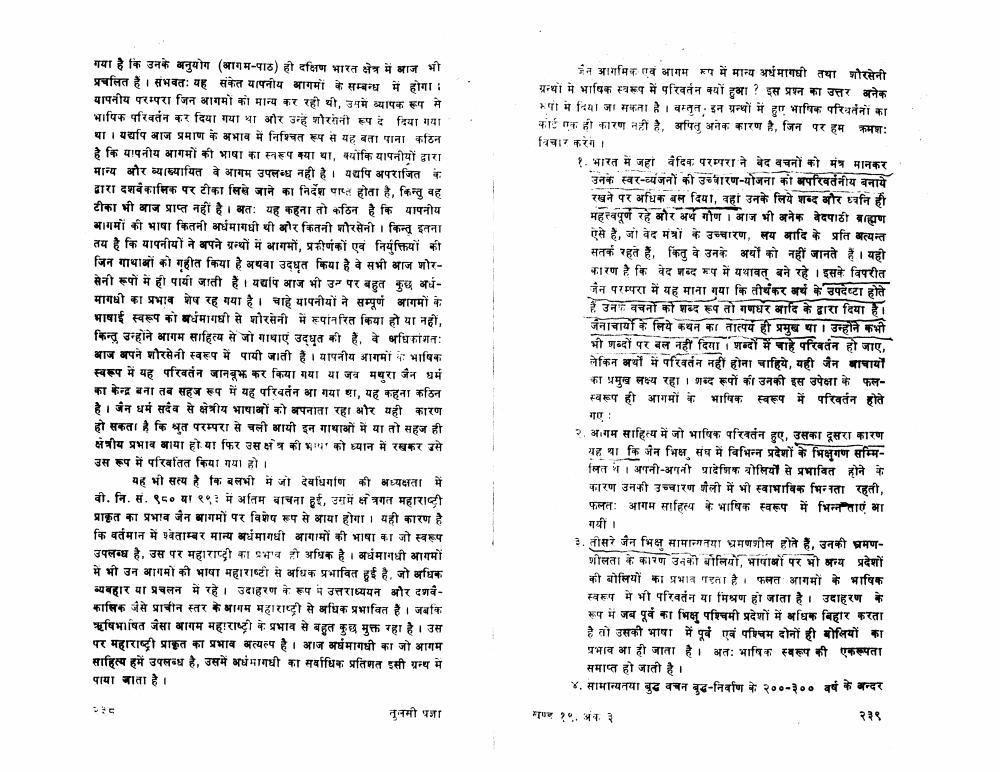Book Title: Jain Agamo Me Hua Bhashik Swarup Parivartan Ek Vimarsh Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Sagarmal Jain View full book textPage 4
________________ गया है कि उनके अनुयोग (आगम-पाठ) ही दक्षिण भारत क्षेत्र में आज भी प्रचलित हैं। संभवतः यह संकेत यापनीय आगमों के सम्बन्ध में होगा यापनीय परम्परा जिन आगमों को मान्य कर रही थी, उसमें व्यापक रूप मे भाषिक परिवर्तन कर दिया गया था और उन्हें शौरसेनी रूप दे दिया गया था। यद्यपि आज प्रमाण के अभाव में निश्चित रूप से यह बता पाना कठिन है कि पापनीय आगमों की भाषा का स्वरूप क्या था, क्योंकि यापनीयों द्वारा मान्य और व्याख्यायित वे आगम उपलब्ध नही है। यद्यपि अपराजित के द्वारा दशकालिक पर टीका लिखे जाने का निर्देश पाप्त होता है, किन्तु वह टीका भी आज प्राप्त नहीं है। अतः यह कहना तो कठिन है कि यापनीय आगमों की भाषा कितनी अर्धमागधी थी ओर कितनी शौरसेनी किन्तु इतना तय है कि यापनीयों ने अपने ग्रन्थों में आगमों, प्रकीर्णकों एवं नियुक्तियों की जिन गाथाओं को गृहीत किया है अथवा उधृत किया है वे सभी आज शोरसेनी रूपों में ही पायी जाती हैं। यद्यपि आज भी उन पर बहुत कुछ अर्धमागधी का प्रभाव शेष रह गया है। चाहे यापनीयों ने सम्पूर्ण आगमों के भाषाई स्वरूप को अर्धमागधी से शौरसेनी में रूपांतरित किया हो या नहीं, किन्तु उन्होंने आगम साहित्य से जो गाथाएं उद्धृत की है, वे अधिकांशतः आज अपने शौरसेनी स्वरूप में पायी जाती है। यापनीय आगमों के भाषिक स्वरूप में यह परिवर्तन जानबूझ कर किया गया या जब मथुरा जैन धर्म का केन्द्र बना तब सहज रूप में यह परिवर्तन आ गया था, यह कहना कठिन है। जैन धर्म सदैव से क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाता रहा और यही कारण हो सकता है कि धुत परम्परा से चली आयी इन गाथाओं में या तो सहज ही क्षेत्रीय प्रभाव माया हो या फिर उस क्षेत्र की भयको ध्यान में रखकर उसे उस रूप में परिवर्तित किया गया हो । यह भी सत्य है कि बलभी में जो देवधिगांण की अध्यक्षता में बी. नि. सं. ९८० या २९३ में अतिम बाचना हुई, उसमें क्षेत्रगत महाराष्ट्री प्राकृत का प्रभाव जैन आगमों पर विशेष रूप से आया होगा। यही कारण है कि वर्तमान में श्वेताम्बर मान्य अर्धमागधी आगामों की भाषा का जो स्वरूप उपलब्ध है, उस पर महाराष्ट्री का प्रभाव ही अधिक है। अर्धमागधी आगमों में भी उन आगमों की भाषा महाराष्ट्री से अधिक प्रभावित हुई है, जो अधिक व्यवहार या प्रचलन में रहे। उदाहरण के रूप में उत्तराध्ययन और दशवेकालिक जैसे प्राचीन स्तर के आगम महाराष्ट्री से अधिक प्रभावित हैं। जबकि ऋषिभाषित जैसा आगम महाराष्ट्री के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त रहा है। उस पर महाराष्ट्री प्राकृत का प्रभाव अत्यल्प है। आज अर्धमागधी का जो आगम साहित्य हमें उपलब्ध है, उसमें अर्धमागधी का सर्वाधिक प्रतिशत इसी ग्रन्थ में पाया जाता है। 225 तुलसी पज्ञा जैन आगमिक एवं आगम रूप में मान्य अर्धमागधी तथा शौरसेनी ग्रन्थों में भाषिक स्वरूप में परिवर्तन क्यों हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर अनेक रूप में दिया जा सकता है। वस्तुत इन ग्रन्थों में हुए भाषिक परिवर्तनों का कोई एक ही कारण नहीं है, अपितु अनेक कारण है, जिन पर हम क्रमश: विचार करेंगे। १. भारत में जहां वैदिक परम्परा ने वेद वचनों को मंत्र मानकर उनके स्वर व्यंजनों की उच्चारण-योजना को अपरिवर्तनीय बनाये रखने पर अधिक बल दिया, वहां उनके लिये शब्द और ध्वनि ही महत्वपूर्ण रहे और अर्थ गौण । आज भी अनेक वेदपाठी ब्राह्मण ऐसे हैं, जो वेद मंत्रों के उच्चारण, लय आदि के प्रति अत्यन्त सतर्क रहते हैं, किंतु वे उनके अर्थों को नहीं जानते हैं। यही कारण है कि वेद शब्द रूप में यथावत् बने रहे। इसके विपरीत जैन परम्परा में यह माना गया कि तीर्थंकर अर्थ के उपदेष्टा होते है उनके वचनों को शब्द रूप तो गणधर आदि के द्वारा दिया है। जैनाचार्यो के लिये कथन का तात्पर्य ही प्रमुख था। उन्होंने कभी भी शब्दों पर बल नहीं दिया। शब्दों में चाहे परिवर्तन हो जाए, लेकिन अर्थों में परिवर्तन नहीं होना चाहिये, यही जैन बाचायों का प्रमुख लक्ष्य रहा । शब्द रूपों की उनकी इस उपेक्षा के फलस्वरूप ही आगमों के भाषिक स्वरूप में परिवर्तन होते गए २. आगम साहित्य में जो भाषिक परिवर्तन हुए, उसका दूसरा कारण यह था कि जैन भिक्षु संघ में विभिन्न प्रदेशों के भिक्षुगण सम्मि लित थे। अपनी-अपनी प्रादेशिक बोलियों से प्रभावित होने के कारण उनकी उच्चारण शैली में भी स्वाभाविक भिन्नता रहती फलतः आगम साहित्य के भाषिक स्वरूप में भिन्नताएं भा गयीं । ३. तीसरे जैन भिक्षु सामान्यतया भ्रमणशील होते हैं, उनकी भ्रमणशीलता के कारण उनको बोलियों, भाषाओं पर भी अन्य प्रदेशों की बोलियों का प्रभाव गरता है फलत: आगमों के भाषिक स्वरूप में भी परिवर्तन या मिश्रण हो जाता है। उदाहरण के रूप में जब पूर्व का भिक्षु पश्चिमी प्रदेशों में अधिक बिहार करता है तो उसकी भाषा में पूर्व एवं पश्चिम दोनों ही बोलियों का प्रभाव आ ही जाता है। अतः भाषिक स्वरूप की एकरूपता समाप्त हो जाती है। ४. सामान्यतया बुद्ध वचन बुद्ध-निर्वाण के २००-३०० वर्ष के अन्दर १०२ २३९Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10