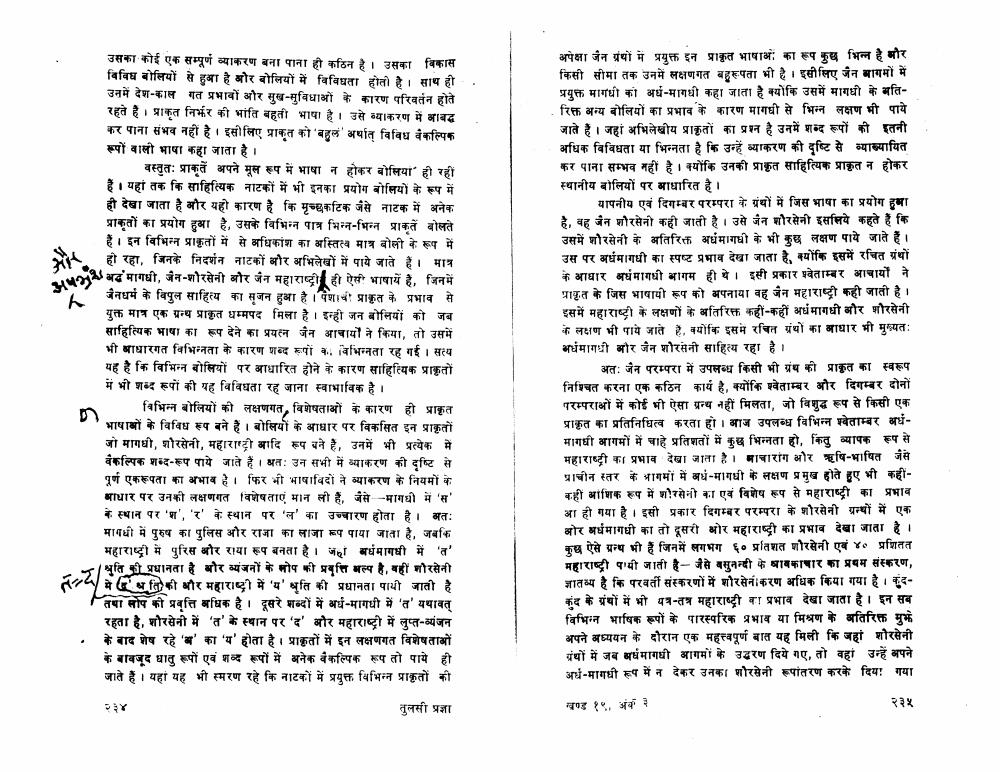Book Title: Jain Agamo Me Hua Bhashik Swarup Parivartan Ek Vimarsh Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Sagarmal Jain View full book textPage 2
________________ और अHNA उसका कोई एक सम्पूर्ण व्याकरण बना पाना ही कठिन है। उसका विकास विविध बोलियों से हुआ है और बोलियों में विविधता होती है। साथ ही . उनमें देश-काल गत प्रभावों और मुख-मुविधाओं के कारण परिवर्तन होते रहते है। प्राकृत निर्भर की भांति बहती भाषा है। उसे व्याकरण में आबद्ध कर पाना संभव नहीं है । इसीलिए प्राकृत को बहुल' अर्थात् विविध वैकल्पिक रूपों वाली भाषा कहा जाता है। वस्तुतः प्राकृतें अपने मूल रूप में भाषा न होकर बोलिया' ही रहीं है। यहां तक कि साहित्यिक नाटकों में भी इनका प्रयोग बोलियों के रूप में ही देखा जाता है और यही कारण है कि मृच्छकटिक जैसे नाटक में अनेक प्राकृतों का प्रयोग हुआ है, उसके विभिन्न पात्र भिन्न-भिन्न प्राकृत बोलते है। इन विभिन्न प्राकृतों में से अधिकांश का अस्तित्व मात्र बोली के रूप में ही रहा, जिनके निदर्शन नाटकों और अभिलेखों में पाये जाते है। मात्र अद्धमागधी, जैन-शौरसेनी और जैन महाराष्ट्रीही ऐसी भाषायें है, जिनमें जैनधर्म के विपुल साहित्य का सृजन हुआ है । पेशाची प्राकृत के प्रभाव से युक्त मात्र एक ग्रन्थ प्राकृत धम्मपद मिला है। इन्ही जन बोलियों को जब साहित्यिक भाषा का रूप देने का प्रयत्न जैन आचार्यों ने किया, तो उसमें भी बाधारगत विभिन्नता के कारण शब्द रूपों .. विभिन्नता रह गई। सत्य यह है कि विभिन्न बोलियों पर आधारित होने के कारण साहित्यिक प्राकृतों में भी शब्द रूपों की यह विविधता रह जाना स्वाभाविक है। विभिन्न बोलियों की लक्षणगत, विशेषताओं के कारण ही प्राकृत भाषामों के विविध रूप बने हैं । बोलियों के आधार पर विकसित इन प्राकृतों जो मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री आदि रूप बने हैं, उनमें भी प्रत्येक में वैकल्पिक शब्द-रूप पाये जाते हैं । अत: उन सभी में व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण एकरूपता का अभाव है। फिर भी भाषाविदों ने व्याकरण के नियमों के माधार पर उनकी लक्षणगत विशेषताएं मान ली हैं, जैसे -मागधी में 'स' के स्थान पर 'श', 'र' के स्थान पर 'ल' का उच्चारण होता है। अतः मागधी में पुरुष का पुलिस और राजा का लाजा रूप पाया जाता है, जबकि महाराष्ट्री में पुरिस और राया रूप बनता है। अर्धमागधी में 'त' श्रुति की प्रधानता है और व्यंजनों के मोप की प्रवृत्ति मल्प है, वहीं गौरसेनी 14/ मे तिकी और महाराष्ट्री में 'य' श्रुति की प्रधानता पायी जाती है तथा गोप की प्रवृत्ति अधिक है। दूसरे शब्दों में अर्धमागधी में 'त' यथावत् रहता है, शौरसेनी में 'त' के स्थान पर 'द' और महाराष्ट्री में लुप्त-व्यंजन के बाद शेष रहे 'ब' का 'य' होता है। प्राकृतों में इन लक्षणगत विशेषताओं के बावजूद धातु रूपों एवं शब्द रूपों में अनेक वैकल्पिक रूप तो पाये ही जाते हैं । यहा यह भी स्मरण रहे कि नाटकों में प्रयुक्त विभिन्न प्राकृतों की तुलसी प्रज्ञा अपेक्षा जैन ग्रंथों में प्रयुक्त इन प्राकृत भाषा का रूप कुछ भिन्न है और किसी सीमा तक उनमें लक्षणगत बहुरूपता भी है। इसीलिए जैन भागमों में प्रयुक्त मागधी को अर्ध-मागधी कहा जाता है क्योकि उसमें मागधी के भतिरिक्त अन्य बोलियों का प्रभाव के कारण मागधी से भिन्न लक्षण भी पाये जाते है । जहाँ अभिलेखीय प्राकृतों का प्रश्न है उनमें शब्द रूपों की इतनी अधिक विविधता या भिन्नता है कि उन्हें व्याकरण की दृष्टि से म्याख्यायित कर पाना सम्भव नहीं है। क्योंकि उनकी प्राकृत साहित्यिक प्राकृत न होकर स्थानीय बोलियों पर आधारित है। यापनीय एवं दिगम्बर परम्परा के ग्रंथों में जिस भाषा का प्रयोग हुमा है, वह जैन शौरसेनी कही जाती है । उसे जैन शौरसेनी इसलिये कहते है कि उसमें शौरसेनी के अतिरिक्त अर्धमागधी के भी कुछ लक्षण पाये जाते हैं। उस पर अर्धमागधी का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि इसमें रचित ग्रंथों के आधार अर्धमागधी भागम ही थे। इसी प्रकार श्वेताम्बर आचार्यों ने प्राकृत के जिस भाषायी रूप को अपनाया वह जैन महाराष्ट्री कही जाती है। इसमें महाराष्ट्री के लक्षणों के अतिरिक्त कहीं-कहीं अर्धमागधी और शौरसेनी के लक्षण भी पाये जाते हैं, क्योंकि इसमे रचित ग्रंथों का बाधार भी मुग्यतः भर्धमागधी और जैन शौरसेनी साहित्य रहा है। अतः जैन परम्परा में उपलब्ध किसी भी ग्रंथ की प्राकृत का स्वरूप निश्चित करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं मिलता, जो विशुद्ध रूप से किसी एक प्राकृत का प्रतिनिधित्व करता हो। आज उपलब्ध विभिन्न श्वेताम्बर अर्धमागधी आगमों में चाहे प्रतिशतों में कुछ भिन्नता हो, किंतु व्यापक रूप से महाराष्ट्री का प्रभाव देखा जाता है। माचारांग और ऋषि-भाषित जैसे प्राचीन स्तर के आगमों में अधं-मागधी के लक्षण प्रमुख होते हुए भी कहींकहीं आशिक रूप में शौरसेनी का एवं विशेष रूप से महाराष्ट्री का प्रभाव आ ही गया है। इसी प्रकार दिगम्बर परम्परा के शौरसेनी ग्रन्थों में एक ओर अर्धमागधी का तो दूसरी ओर महाराष्ट्री का प्रभाव देखा जाता है। कुछ ऐसे अन्य भी हैं जिनमें लगभग ६० प्रतिशत शौरसेनी एवं ४० प्रशितत महाराष्ट्री पायी जाती है-जैसे वसुनन्दी के बावकाचार का प्रथम संस्करण, ज्ञातव्य है कि परवर्ती संस्करणों में शौरसेनीकरण अधिक किया गया है। कुंदकुंद के ग्रंथों में भी यत्र-तत्र महाराष्ट्री वा प्रभाव देखा जाता है। इन सब विभिन्न भाषिक रूपों के पारस्परिक प्रभाव या मिश्रण के अतिरिक्त मुझे अपने अध्ययन के दौरान एक महत्त्वपूर्ण बात यह मिली कि जहां शौरसेनी ग्रंथों में जब अर्धमागधी आगमों के उद्धरण दिये गए, तो वहां उन्हें अपने अर्ध-मागधी रूप में न देकर उनका शौरसेनी रूपांतरण करके दिया गया खण्ड ११, अंक ३ २३५Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10