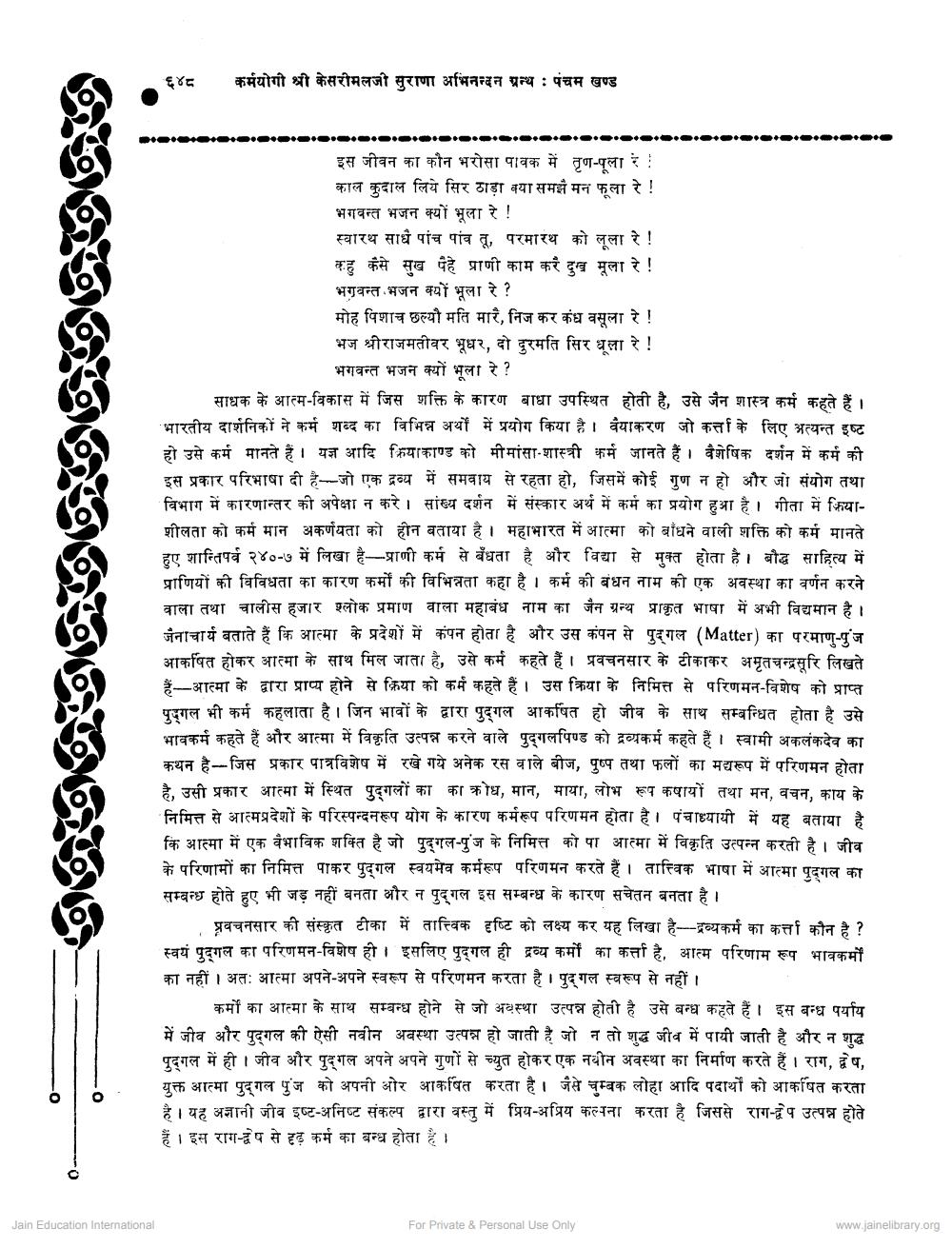Book Title: Hindi Jain Gitikavya me Karm Siddhant Author(s): Shreechand Jain Publisher: Z_Kesarimalji_Surana_Abhinandan_Granth_012044.pdf View full book textPage 2
________________ ६४८ कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : पंचम खण्ड .-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-. -. -.-. इस जीवन का कौन भरोसा पावक में तृण-पूला रे काल कुदाल लिये सिर ठाड़ा क्या समझै मन फूला रे ! भगवन्त भजन क्यों भूला रे ! स्वारथ साधै पांच पांव तू, परमारथ को लूला रे ! कहु कैसे सुख पैहे प्राणी काम करै दुख मूला रे ! भगवन्त भजन क्यों भूला रे? । मोह पिशाच छल्यौ मति मारै, निज कर कंध वसूला रे ! भज श्रीराजमतीवर भूधर, दो दुरमति सिर धूला रे ! भगवन्त भजन क्यों भूला रे ? साधक के आत्म-विकास में जिस शक्ति के कारण बाधा उपस्थित होती है, उसे जैन शास्त्र कर्म कहते हैं। भारतीय दार्शनिकों ने कर्म शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। वैयाकरण जो कर्ता के लिए अत्यन्त इष्ट हो उसे कर्म मानते हैं । यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड को मीमांसा-शास्त्री कर्म जानते । वैशेषिक दर्शन में कर्म की इस प्रकार परिभाषा दी है जो एक द्रव्य में समवाय से रहता हो, जिसमें कोई गुण न हो और जो संयोग तथा विभाग में कारणान्तर की अपेक्षा न करे। सांख्य दर्शन में संस्कार अर्थ में कर्म का प्रयोग हुआ है। गीता में कियाशीलता को कर्म मान अकर्णयता को हीन बताया है। महाभारत में आत्मा को बाँधने वाली शक्ति को कर्म मानते हए शान्तिपर्व २४०-७ में लिखा है-प्राणी कर्म से बँधता है और विद्या से मुक्त होता है। बौद्ध साहित्य में प्राणियों की विविधता का कारण कर्मों की विभिन्नता कहा है । कर्म की बंधन नाम की एक अवस्था का वर्णन करने वाला तथा चालीस हजार श्लोक प्रमाण वाला महाबंध नाम का जैन ग्रन्थ प्राकृत भाषा में अभी विद्यमान है। जैनाचार्य बताते हैं कि आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है और उस कंपन से पुद्गल (Matter) का परमाणु-पुंज आकर्षित होकर आत्मा के साथ मिल जाता है, उसे कर्म कहते हैं। प्रवचनसार के टीकाकर अमृतचन्द्रसूरि लिखते हैं-आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से क्रिया को कर्म कहते हैं। उस क्रिया के निमित्त से परिणमन-विशेष को प्राप्त पुदगल भी कर्म कहलाता है। जिन भावों के द्वारा पुद्गल आकर्षित हो जीव के साथ सम्बन्धित होता है उसे भावकर्म कहते हैं और आत्मा में विकृति उत्पन्न करने वाले पुद्गलपिण्ड को द्रव्यकर्म कहते हैं। स्वामी अकलंकदेव का कथन है-जिस प्रकार पात्रविशेष में रखे गये अनेक रस वाले बीज, पुष्प तथा फलों का मद्यरूप में परिणमन होता है, उसी प्रकार आत्मा में स्थित पुद्गलों का का क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषायों तथा मन, वचन, काय के निमित्त से आत्मप्रदेशों के परिस्पन्दनरूप योग के कारण कर्मरूप परिणमन होता है। पंचाध्यायी में यह बताया है कि आत्मा में एक वैभाविक शक्ति है जो पुद्गल-पुंज के निमित्त को पा आत्मा में विकृति उत्पन्न करती है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल स्वयमेव कर्मरूप परिणमन करते हैं। तात्त्विक भाषा में आत्मा पुदगल का सम्बन्ध होते हुए भी जड़ नहीं बनता और न पुद्गल इस सम्बन्ध के कारण सचेतन बनता है। . प्रवचनसार की संस्कृत टीका में तात्त्विक दृष्टि को लक्ष्य कर यह लिखा है-द्रव्यकर्म का कर्ता कौन है ? स्वयं पुद्गल का परिणमन-विशेष ही। इसलिए पुद्गल ही द्रव्य कर्मों का कर्ता है, आत्म परिणाम रूप भावकों का नहीं। अत: आत्मा अपने-अपने स्वरूप से परिणमन करता है। पुद्गल स्वरूप से नहीं। कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होने से जो अबस्था उत्पन्न होती है उसे बन्ध कहते हैं। इस बन्ध पर्याय में जीव और पुद्गल की ऐसी नवीन अवस्था उत्पन्न हो जाती है जो न तो शुद्ध जीव में पायी जाती है और न शुद्ध पुद्गल में ही । जीव और पुद्गल अपने अपने गुणों से च्युत होकर एक नवीन अवस्था का निर्माण करते हैं। राग, द्वेष, युक्त आत्मा पुद्गल पुंज को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे चुम्बक लोहा आदि पदार्थों को आकर्षित करता है। यह अज्ञानी जीव इष्ट-अनिष्ट संकल्प द्वारा वस्तु में प्रिय-अप्रिय कल्पना करता है जिससे राग-द्वप उत्पन्न होते हैं । इस राग-द्वेष से दृढ़ कर्म का बन्ध होता है। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10