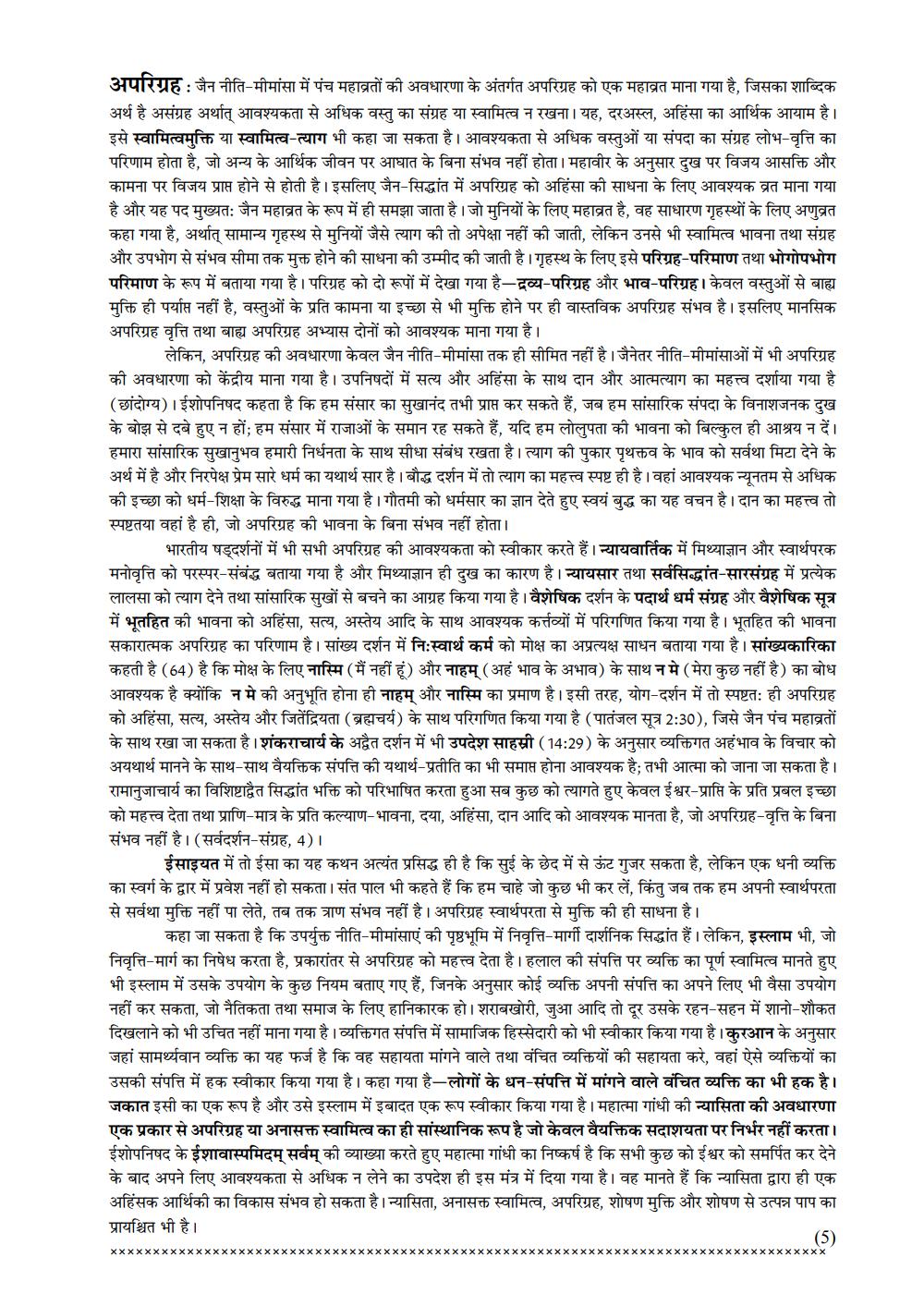Book Title: Aparigraha Author(s): D R Mehta Publisher: D R Mehta View full book textPage 5
________________ अपरिग्रह : जैन नीति-मीमांसा में पंच महाव्रतों की अवधारणा के अंतर्गत अपरिग्रह को एक महाव्रत माना गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है असंग्रह अर्थात् आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह या स्वामित्व न रखना। यह, दरअस्ल, अहिंसा का आर्थिक आयाम है। इसे स्वामित्वमुक्ति या स्वामित्व-त्याग भी कहा जा सकता है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं या संपदा का संग्रह लोभ-वृत्ति का परिणाम होता है, जो अन्य के आर्थिक जीवन पर आघात के बिना संभव नहीं होता। महावीर के अनुसार दुख पर विजय आसक्ति और कामना पर विजय प्राप्त होने से होती है। इसलिए जैन-सिद्धांत में अपरिग्रह को अहिंसा की साधना के लिए आवश्यक व्रत माना गया है और यह पद मुख्यत: जैन महाव्रत के रूप में ही समझा जाता है। जो मुनियों के लिए महाव्रत है, वह साधारण गृहस्थों के लिए अणुव्रत कहा गया है, अर्थात् सामान्य गृहस्थ से मुनियों जैसे त्याग की तो अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन उनसे भी स्वामित्व भावना तथा संग्रह और उपभोग से संभव सीमा तक मुक्त होने की साधना की उम्मीद की जाती है। गृहस्थ के लिए इसे परिग्रह-परिमाण तथा भोगोपभोग परिमाण के रूप में बताया गया है। परिग्रह को दो रूपों में देखा गया है-द्रव्य-परिग्रह और भाव-परिग्रह। केवल वस्तुओं से बाह्य मुक्ति ही पर्याप्त नहीं है, वस्तुओं के प्रति कामना या इच्छा से भी मुक्ति होने पर ही वास्तविक अपरिग्रह संभव है। इसलिए मानसिक अपरिग्रह वृत्ति तथा बाह्य अपरिग्रह अभ्यास दोनों को आवश्यक माना गया है। लेकिन, अपरिग्रह की अवधारणा केवल जैन नीति-मीमांसा तक ही सीमित नहीं है। जैनेतर नीति-मीमांसाओं में भी अपरिग्रह की अवधारणा को केंद्रीय माना गया है। उपनिषदों में सत्य और अहिंसा के साथ दान और आत्मत्याग का महत्त्व दर्शाया गया है (छांदोग्य)। ईशोपनिषद कहता है कि हम संसार का सुखानंद तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब हम सांसारिक संपदा के विनाशजनक दुख के बोझ से दबे हुए न हों; हम संसार में राजाओं के समान रह सकते हैं, यदि हम लोलुपता की भावना को बिल्कुल ही आश्रय न दें। हमारा सांसारिक सुखानुभव हमारी निर्धनता के साथ सीधा संबंध रखता है। त्याग की पुकार पृथक्तव के भाव को सर्वथा मिटा देने के अर्थ में है और निरपेक्ष प्रेम सारे धर्म का यथार्थ सार है। बौद्ध दर्शन में तो त्याग का महत्त्व स्पष्ट ही है। वहां आवश्यक न्यूनतम से अधिक की इच्छा को धर्म-शिक्षा के विरुद्ध माना गया है। गौतमी को धर्मसार का ज्ञान देते हुए स्वयं बुद्ध का यह वचन है। दान का महत्त्व तो स्पष्टतया वहां है ही, जो अपरिग्रह की भावना के बिना संभव नहीं होता। भारतीय षड्दर्शनों में भी सभी अपरिग्रह की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। न्यायवार्तिक में मिथ्याज्ञान और स्वार्थपरक मनोवृत्ति को परस्पर-संबंद्ध बताया गया है और मिथ्याज्ञान ही दुख का कारण है। न्यायसार तथा सर्वसिद्धांत-सारसंग्रह में प्रत्येक लालसा को त्याग देने तथा सांसारिक सुखों से बचने का आग्रह किया गया है। वैशेषिक दर्शन के पदार्थ धर्म संग्रह और वैशेषिक सूत्र में भूतहित की भावना को अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि के साथ आवश्यक कर्तव्यों में परिगणित किया गया है। भूतहित की भावना सकारात्मक अपरिग्रह का परिणाम है। सांख्य दर्शन में निःस्वार्थ कर्म को मोक्ष का अप्रत्यक्ष साधन बताया गया है। सांख्यकारिका कहती है (64) है कि मोक्ष के लिए नास्मि (मैं नहीं हूं) और नाहम् (अहं भाव के अभाव) के साथ न मे (मेरा कुछ नहीं है) का बोध आवश्यक है क्योंकि न मे की अनुभूति होना ही नाहम् और नास्मि का प्रमाण है। इसी तरह, योग-दर्शन में तो स्पष्टतः ही अपरिग्रह को अहिंसा, सत्य, अस्तेय और जितेंद्रियता (ब्रह्मचर्य) के साथ परिगणित किया गया है (पातंजल सूत्र 2:30), जिसे जैन पंच महाव्रतों के साथ रखा जा सकता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में भी उपदेश साहस्री (14:29) के अनुसार व्यक्तिगत अहंभाव के विचार को अयथार्थ मानने के साथ-साथ वैयक्तिक संपत्ति की यथार्थ-प्रतीति का भी समाप्त होना आवश्यक है; तभी आत्मा को जाना जा सकता है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत भक्ति को परिभाषित करता हुआ सब कुछ को त्यागते हुए केवल ईश्वर-प्राप्ति के प्रति प्रबल इच्छा को महत्त्व देता तथा प्राणि-मात्र के प्रति कल्याण-भावना, दया, अहिंसा, दान आदि को आवश्यक मानता है, जो अपरिग्रह-वृत्ति के बिना संभव नहीं है। (सर्वदर्शन-संग्रह, 4)। ईसाइयत में तो ईसा का यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध ही है कि सुई के छेद में से ऊंट गुजर सकता है, लेकिन एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग के द्वार में प्रवेश नहीं हो सकता। संत पाल भी कहते हैं कि हम चाहे जो कुछ भी कर लें, किंतु जब तक हम अपनी स्वार्थपरता से सर्वथा मुक्ति नहीं पा लेते, तब तक त्राण संभव नहीं है। अपरिग्रह स्वार्थपरता से मुक्ति की ही साधना है। कहा जा सकता है कि उपर्युक्त नीति-मीमांसाएं की पृष्ठभूमि में निवृत्ति-मार्गी दार्शनिक सिद्धांत हैं। लेकिन, इस्लाम भी, जो निवृत्ति-मार्ग का निषेध करता है, प्रकारांतर से अपरिग्रह को महत्त्व देता है। हलाल की संपत्ति पर व्यक्ति का पूर्ण स्वामित्व मानते हुए भी इस्लाम में उसके उपयोग के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनके अनुसार कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अपने लिए भी वैसा उपयोग नहीं कर सकता, जो नैतिकता तथा समाज के लिए हानिकारक हो। शराबखोरी, जुआ आदि तो दूर उसके रहन-सहन में शानो-शौकत दिखलाने को भी उचित नहीं माना गया है। व्यक्तिगत संपत्ति में सामाजिक हिस्सेदारी को भी स्वीकार किया गया है। कुरआन के अनुसार जहां सामर्थ्यवान व्यक्ति का यह फर्ज है कि वह सहायता मांगने वाले तथा वंचित व्यक्तियों की सहायता करे, वहां ऐसे व्यक्तियों का उसकी संपत्ति में हक स्वीकार किया गया है। कहा गया है लोगों के धन-संपत्ति में मांगने वाले वंचित व्यक्ति का भी हक है। जकात इसी का एक रूप है और उसे इस्लाम में इबादत एक रूप स्वीकार किया गया है। महात्मा गांधी की न्यासिता की अवधारणा एक प्रकार से अपरिग्रह या अनासक्त स्वामित्व का ही सांस्थानिक रूप है जो केवल वैयक्तिक सदाशयता पर निर्भर नहीं करता। ईशोपनिषद के ईशावास्पमिदम् सर्वम् की व्याख्या करते हुए महात्मा गांधी का निष्कर्ष है कि सभी कुछ को ईश्वर को समर्पित कर देने के बाद अपने लिए आवश्यकता से अधिक न लेने का उपदेश ही इस मंत्र में दिया गया है। वह मानते हैं कि न्यासिता द्वारा ही एक अहिंसक आर्थिकी का विकास संभव हो सकता है। न्यासिता, अनासक्त स्वामित्व, अपरिग्रह, शोषण मुक्ति और शोषण से उत्पन्न पाप का प्रायश्चित भी है। (5) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16