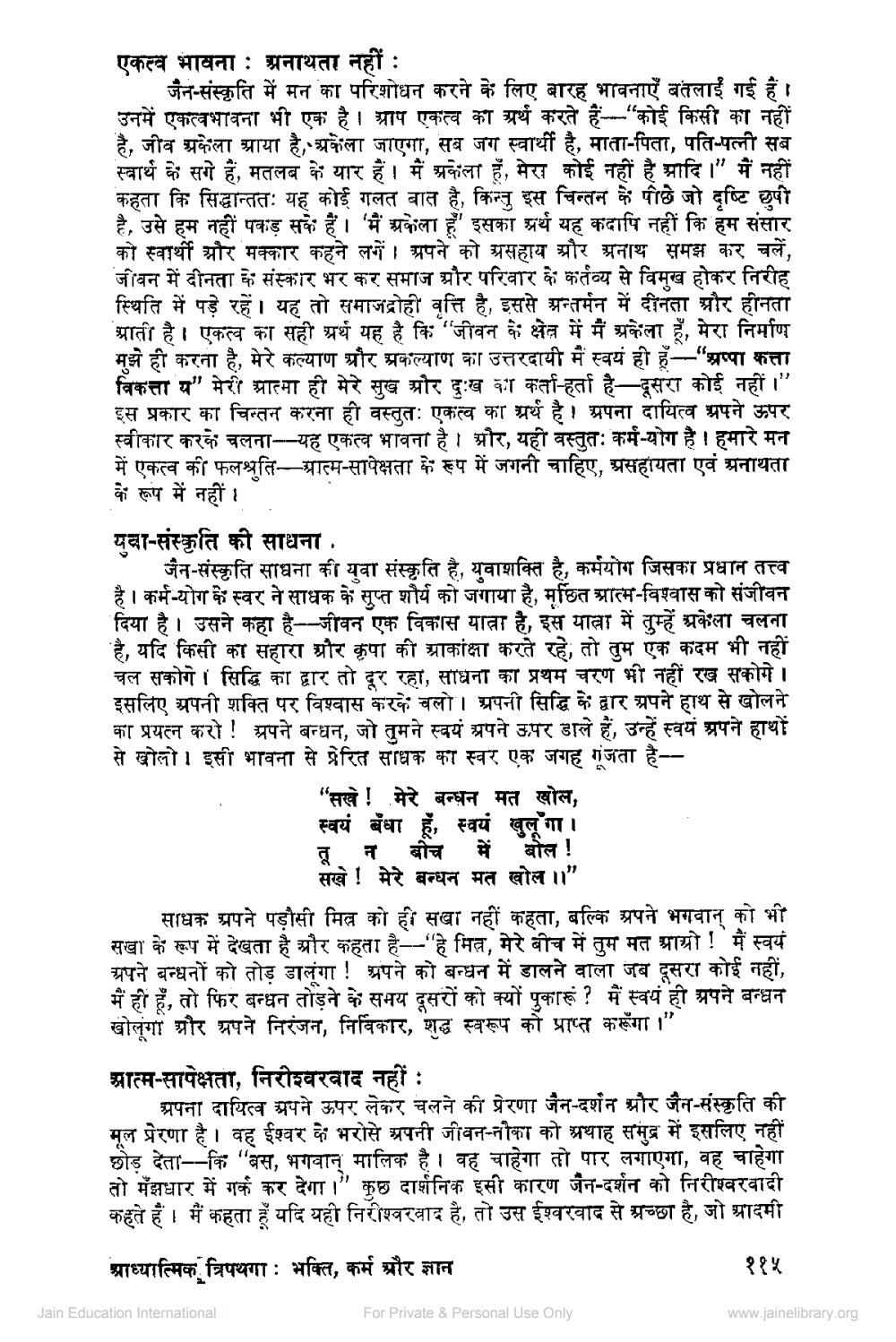Book Title: Adhyatmik Tripthaga Bhakti Karm Aur Gyan Author(s): Amarmuni Publisher: Z_Panna_Sammikkhaye_Dhammam_Part_01_003408_HR.pdf View full book textPage 3
________________ एकत्व भावना : अनाथता नहीं : जैन-संस्कृति में मन का परिशोधन करने के लिए बारह भावनाएँ बतलाई गई हैं। उनमें एकत्वभावना भी एक है। आप एकत्व का अर्थ करते हैं---“कोई किसी का नहीं है, जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा, सब जग स्वार्थी है, माता-पिता, पति-पत्नी सब स्वार्थ के सगे हैं, मतलब के यार हैं। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है आदि ।" मैं नहीं कहता कि सिद्धान्ततः यह कोई गलत बात है, किन्तु इस चिन्तन के पीछे जो दृष्टि छुपी है, उसे हम नहीं पकड़ सके हैं। 'मैं अकेला हूँ' इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम संसार को स्वाथी और मक्कार कहने लग। अपने को असहाय और अनाथ समझ कर चल, जीवन में दीनता के संस्कार भर कर समाज और परिवार के कर्तव्य से विमुख होकर निरीह स्थिति में पड़े रहें। यह तो समाजद्रोही वत्ति है, इससे अन्तर्मन में दीनता और हीनता आती है। एकत्व का सही अर्थ यह है कि "जीवन के क्षेत्र में मैं अकेला हूँ, मेरा निर्माण मुझे ही करना है, मेरे कल्याण और अकल्याण का उत्तरदायी मैं स्वयं ही हूँ--"अप्पा कत्ता विकत्ता य" मेरी आत्मा ही मेरे सुख और दुःख का कर्ता-हर्ता है-दूसरा कोई नहीं।" इस प्रकार का चिन्तन करना ही वस्तुतः एकत्व का अर्थ है। अपना दायित्व अपने ऊपर स्वीकार करके चलना-यह एकत्व भावना है। और, यही वस्तुतः कर्म-योग है। हमारे मन में एकत्व की फलश्रुति-प्रात्म-सापेक्षता के रूप में जगनी चाहिए, असहायता एवं अनाथता के रूप में नहीं। युवा-संस्कृति की साधना . जैन-संस्कृति साधना की युवा संस्कृति है, युवाशक्ति है, कर्मयोग जिसका प्रधान तत्त्व है। कर्म-योग के स्वर ने साधक के सुप्त शौर्य को जगाया है, मछित आत्म-विश्वास को संजीवन दिया है। उसने कहा है--जीवन एक विकास यात्रा है, इस यात्रा में तुम्हें अकेला चलना है, यदि किसी का सहारा और कृपा की आकांक्षा करते रहे, तो तुम एक कदम भी नहीं चल सकोगे। सिद्धि का द्वार तो दूर रहा, साधना का प्रथम चरण भी नहीं रख सकोगे। इसलिए अपनी शक्ति पर विश्वास करके चलो। अपनी सिद्धि के द्वार अपने हाथ से खोलने का प्रयत्न करो! अपने बन्धन, जो तुमने स्वयं अपने ऊपर डाले हैं, उन्हें स्वयं अपने हाथों से खोलो। इसी भावना से प्रेरित साधक का स्वर एक जगह गंजता है "सखे ! मेरे बन्धन मत खोल, स्वयं बंधा हूँ, स्वयं खुलूगा। तू न बीच में बोल! सखे ! मेरे बन्धन मत खोल ॥" साधक अपने पड़ौसी मित्र को ही सखा नहीं कहता, बल्कि अपने भगवान् को भी सखा के रूप में देखता है और कहता है--"हे मित्र, मेरे बीच में तुम मत पायो ! मैं स्वयं अपने बन्धनों को तोड़ डालूंगा ! अपने को बन्धन में डालने वाला जब दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूँ, तो फिर बन्धन तोड़ने के समय दूसरों को क्यों पुकारूं? मैं स्वयं ही अपने बन्धन खोलूंगा और अपने निरंजन, निर्विकार, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करूँगा।" आत्म-सापेक्षता, निरीश्वरवाद नहीं । अपना दायित्व अपने ऊपर लेकर चलने की प्रेरणा जैन-दर्शन और जैन-संस्कृति की मूल प्रेरणा है। वह ईश्वर के भरोसे अपनी जीवन-नौका को अथाह समुद्र में इसलिए नहीं छोड़ देता--कि "बस, भगवान् मालिक है । वह चाहेगा तो पार लगाएगा, वह चाहेगा तो मँझधार में गर्क कर देगा।" कुछ दार्शनिक इसी कारण जैन-दर्शन को निरीश्वरवादी कहते हैं। मैं कहता हूँ यदि यही निरीश्वरवाद है, तो उस ईश्वरवाद से अच्छा है, जो आदमी आध्यात्मिक त्रिपथगा : भक्ति, कर्म और ज्ञान ११५ Jain Education Intemational For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8