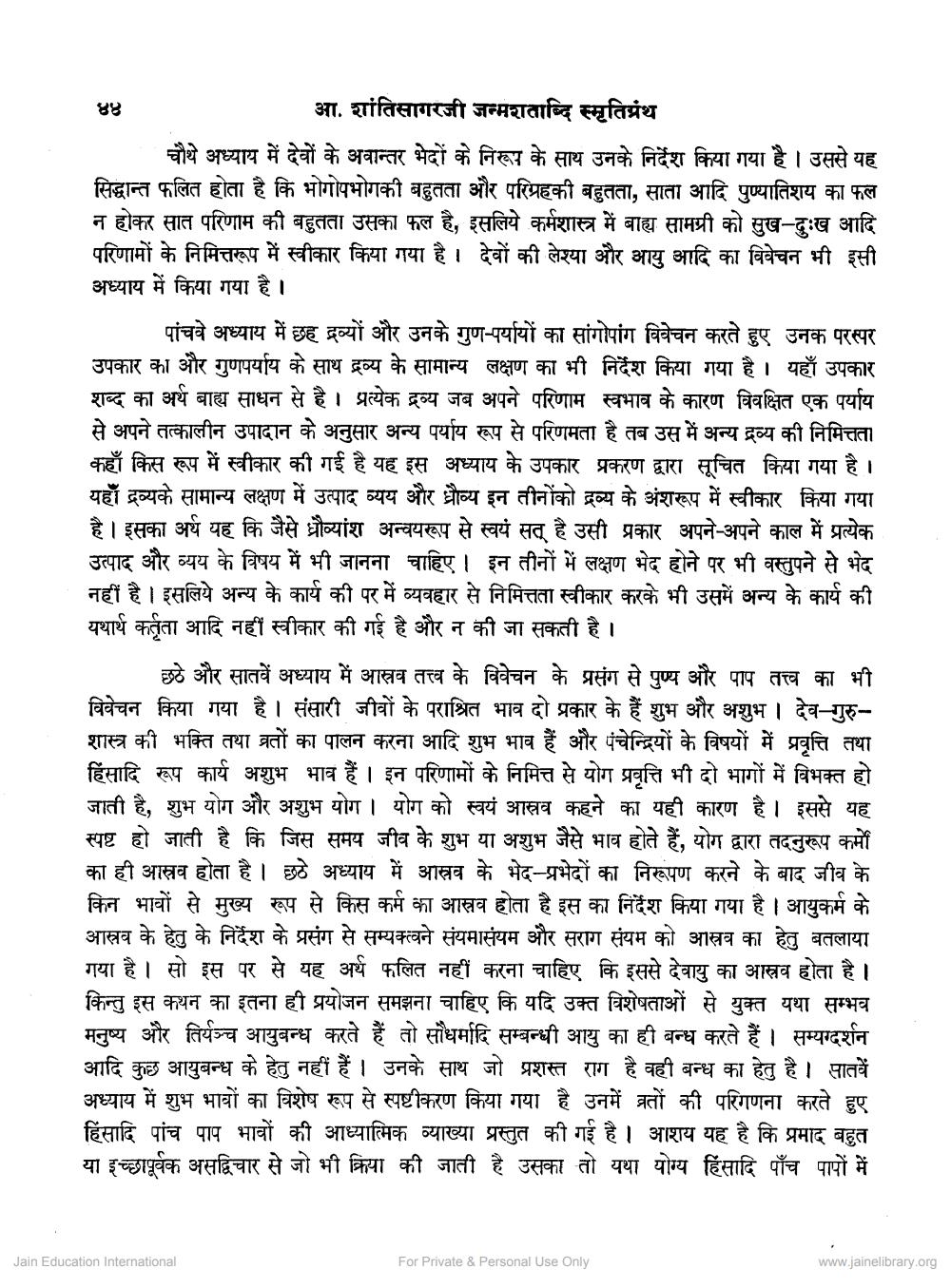Book Title: Tattvartha Sutra aur Uski Tikaye Author(s): Fulchandra Jain Shatri Publisher: Z_Acharya_Shantisagar_Janma_Shatabdi_Mahotsav_Smruti_Granth_012022.pdf View full book textPage 8
________________ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रंथ चौथे अध्याय में देवों के अवान्तर भेदों के निरूप के साथ उनके निर्देश किया गया है । उससे यह सिद्धान्त फलित होता है कि भोगोपभोगकी बहुतता और परिग्रहकी बहुतता, साता आदि पुण्यातिशय का फल न होकर सात परिणाम की बहुतता उसका फल है, इसलिये कर्मशास्त्र में बाह्य सामग्री को सुख-दुःख आदि परिणामों के निमित्तरूप में स्वीकार किया गया है। देवों की लेश्या और आयु आदि का विवेचन भी इसी अध्याय में किया गया है। पांचवे अध्याय में छह द्रव्यों और उनके गुण-पर्यायों का सांगोपांग विवेचन करते हुए उनक परस्पर उपकार का और गुणपर्याय के साथ द्रव्य के सामान्य लक्षण का भी निर्देश किया गया है। यहाँ उपकार शब्द का अर्थ बाह्य साधन से है। प्रत्येक द्रव्य जब अपने परिणाम स्वभाव के कारण विवक्षित एक पर्याय से अपने तत्कालीन उपादान के अनुसार अन्य पर्याय रूप से परिणमता है तब उस में अन्य द्रव्य की निमित्तता कहाँ किस रूप में स्वीकार की गई है यह इस अध्याय के उपकार प्रकरण द्वारा सूचित किया गया है । यहाँ द्रव्यके सामान्य लक्षण में उत्पाद व्यय और ध्रौव्य इन तीनोंको द्रव्य के अंशरूप में स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ यह कि जैसे ध्रौव्यांश अन्वयरूप से स्वयं सत् है उसी प्रकार अपने-अपने काल में प्रत्येक उत्पाद और व्यय के विषय में भी जानना चाहिए। इन तीनों में लक्षण भेद होने पर भी वस्तुपने से भेद नहीं है । इसलिये अन्य के कार्य की पर में व्यवहार से निमित्तता स्वीकार करके भी उसमें अन्य के कार्य की यथार्थ कर्तृता आदि नहीं स्वीकार की गई है और न की जा सकती है। छठे और सातवें अध्याय में आस्रव तत्त्व के विवेचन के प्रसंग से पुण्य और पाप तत्त्व का भी विवेचन किया गया है। संसारी जीवों के पराश्रित भाव दो प्रकार के हैं शुभ और अशुभ । देव-गुरुशास्त्र की भक्ति तथा व्रतों का पालन करना आदि शुभ भाव हैं और पंचेन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्ति तथा हिंसादि रूप कार्य अशुभ भाव हैं । इन परिणामों के निमित्त से योग प्रवृत्ति भी दो भागों में विभक्त हो जाती है, शुभ योग और अशुभ योग । योग को स्वयं आस्रव कहने का यही कारण है। इससे यह स्पष्ट हो जाती है कि जिस समय जीव के शुभ या अशुभ जैसे भाव होते हैं, योग द्वारा तदनुरूप कर्मों का ही आस्रव होता है। छठे अध्याय में आस्रव के भेद-प्रभेदों का निरूपण करने के बाद जीव के किन भावों से मुख्य रूप से किस कर्म का आस्रव होता है इस का निर्देश किया गया है । आयुकर्म के आस्रव के हेतु के निर्देश के प्रसंग से सम्यक्त्वने संयमासंयम और सराग संयम को आस्रव का हेतु बतलाया गया है। सो इस पर से यह अर्थ फलित नहीं करना चाहिए कि इससे देवायु का आस्रव होता है । किन्तु इस कथन का इतना ही प्रयोजन समझना चाहिए कि यदि उक्त विशेषताओं से युक्त यथा सम्भव मनुष्य और तिर्यञ्च आयुबन्ध करते हैं तो सौधर्मादि सम्बन्धी आयु का ही बन्ध करते हैं। सम्यग्दर्शन आदि कुछ आयुबन्ध के हेतु नहीं हैं। उनके साथ जो प्रशस्त राग है वही बन्ध का हेतु है। सातवें अध्याय में शुभ भावों का विशेष रूप से स्पष्टीकरण किया गया है उनमें व्रतों की परिगणना करते हुए हिंसादि पांच पाप भावों की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। आशय यह है कि प्रमाद बहुत या इच्छापूर्वक असद्विचार से जो भी क्रिया की जाती है उसका तो यथा योग्य हिंसादि पाँच पापों में Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20