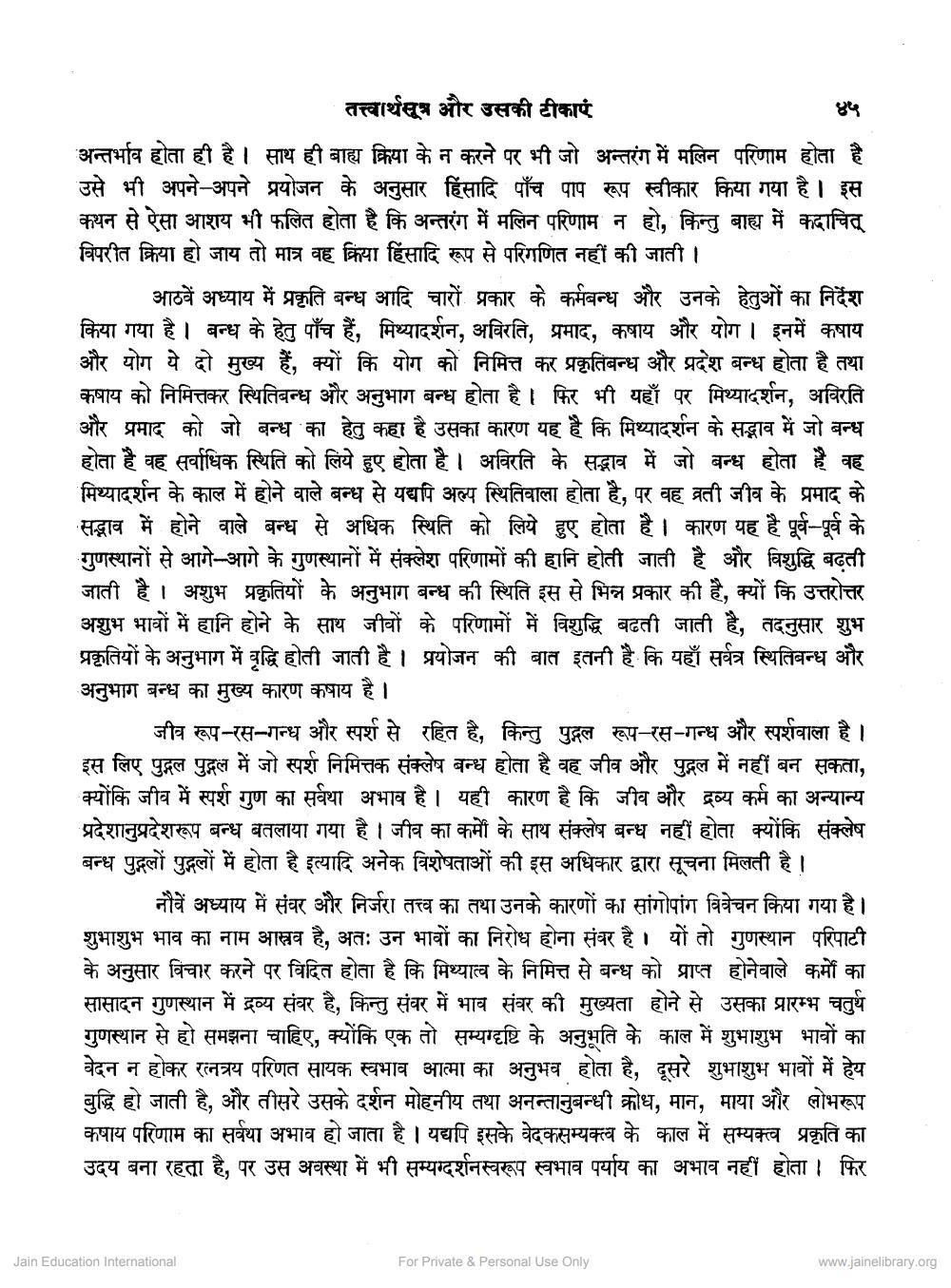Book Title: Tattvartha Sutra aur Uski Tikaye Author(s): Fulchandra Jain Shatri Publisher: Z_Acharya_Shantisagar_Janma_Shatabdi_Mahotsav_Smruti_Granth_012022.pdf View full book textPage 9
________________ तत्त्वार्थसूत्र और उसकी टीकाएं अन्तर्भाव होता ही है । साथ ही बाह्य क्रिया के न करने पर भी जो अन्तरंग में मलिन परिणाम होता है। उसे भी अपने-अपने प्रयोजन के अनुसार हिंसादि पाँच पाप रूप स्वीकार किया गया है । इस कथन से ऐसा आशय भी फलित होता है कि अन्तरंग में मलिन परिणाम न हो, किन्तु बाह्य में कदाचित् विपरीत क्रिया हो जाय तो मात्र वह क्रिया हिंसादि रूप से परिगणित नहीं की जाती । आठवें अध्याय में प्रकृति बन्ध आदि चारों प्रकार के कर्मबन्ध और उनके हेतुओं का निर्देश किया गया है । बन्ध के हेतु पाँच हैं, मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग । इनमें कषाय और योग ये दो मुख्य हैं, क्यों कि योग को निमित्त कर प्रकृतिबन्ध और प्रदेश बन्ध होता है तथा कषाय को निमित्तकर स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्ध होता है । फिर भी यहाँ पर मिथ्यादर्शन, अविरति और प्रमाद को जो बन्ध का हेतु कहा है उसका कारण यह है कि मिथ्यादर्शन के सद्भाव में जो बन्ध होता है वह सर्वाधिक स्थिति को लिये हुए होता है । अविरति के सद्भाव में जो बन्ध होता है वह मिथ्यादर्शन के काल में होने वाले बन्ध से यद्यपि अल्प स्थितिवाला होता है, पर वह व्रती जीव के प्रमाद के सद्भाव में होने वाले बन्ध से अधिक स्थिति को लिये हुए होता है । कारण यह है पूर्व-पूर्व के गुणस्थानों से आगे-आगे के गुणस्थानों में संक्लेश परिणामों की हानि होती जाती है और विशुद्धि बढ़ती जाती है । अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग बन्ध की स्थिति इस से भिन्न प्रकार की है, क्यों कि उत्तरोत्तर अशुभ भावों में हानि होने के साथ जीवों के परिणामों में विशुद्धि बढती जाती है, तदनुसार शुभ प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि होती जाती है प्रयोजन की बात इतनी है कि यहाँ सर्वत्र स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्ध का मुख्य कारण कषाय है । 1 । जीव रूप-रस- गन्ध और स्पर्श से रहित है, किन्तु पुद्गल रूप-रस- गन्ध और स्पर्शवाला है । इस लिए पुद्गल पुद्गल में जो स्पर्श निमित्तक संक्लेष बन्ध होता है वह जीव और पुद्गल में नहीं बन सकता, क्योंकि जीव में स्पर्श गुण का सर्वथा अभाव है । यही कारण है कि जीव और द्रव्य कर्म का अन्यान्य प्रदेशानुप्रदेशरूप बन्ध बतलाया गया है । जीव का कर्मों के साथ संक्लेष बन्ध नहीं होता क्योंकि संक्लेष बन्ध पुद्गलों पुद्गलों में होता है इत्यादि अनेक विशेषताओं की इस अधिकार द्वारा सूचना मिलती है । ४५ नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्त्व का तथा उनके कारणों का सांगोपांग विवेचन किया गया है। शुभाशुभ भाव का नाम आस्त्रव है, अतः उन भावों का निरोध होना संवर है । यों तो गुणस्थान परिपाटी के अनुसार विचार करने पर विदित होता है कि मिथ्यात्व के निमित्त से बन्ध को प्राप्त होनेवाले कर्मों का सासादन गुणस्थान में द्रव्य संवर है, किन्तु संवर में भाव संवर की मुख्यता होने से उसका प्रारम्भ चतुर्थ गुणस्थान से हो समझना चाहिए, क्योंकि एक तो सम्यग्दृष्टि के अनुभूति के शुभाशुभ भावों का वेदन न होकर रत्नत्रय परिणत सायक स्वभाव आत्मा का अनुभव होता है, दूसरे शुभाशुभ भावों में हेय बुद्धि हो जाती है, और तीसरे उसके दर्शन मोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभरूप कषाय परिणाम का सर्वथा अभाव हो जाता है । यद्यपि इसके वेदकसम्यक्त्व के काल में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय बना रहता है, पर उस अवस्था में भी सम्यग्दर्शनस्वरूप स्वभाव पर्याय का अभाव नहीं होता । फिर काल Jain Education International For Private & Personal Use Only में www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20