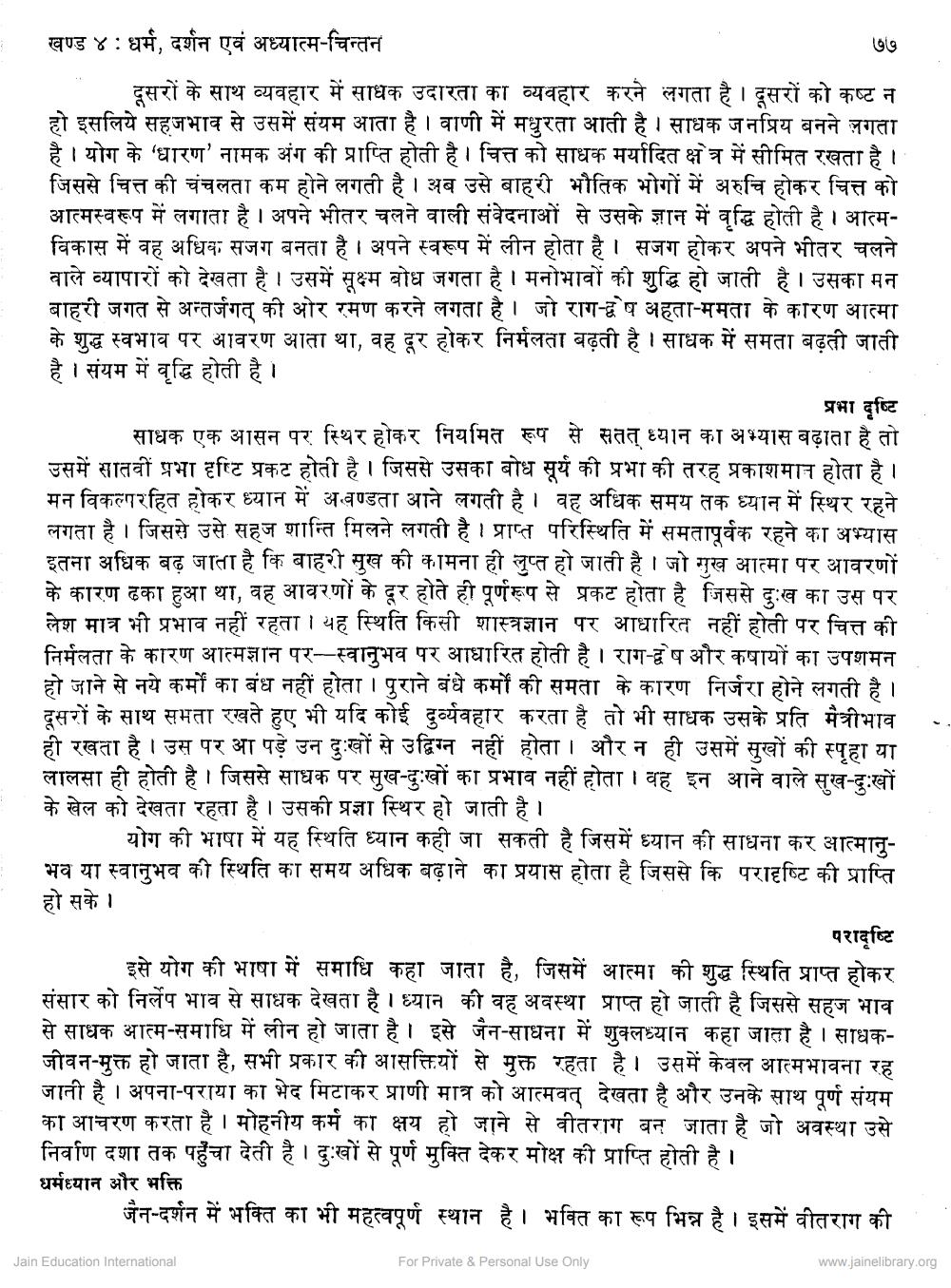Book Title: Swarup Sadhna ka Marg Yoga evam Bhakti Author(s): Sushil Kumar Publisher: Z_Sajjanshreeji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012028.pdf View full book textPage 5
________________ ওও खण्ड ४ : धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म-चिन्तन दूसरों के साथ व्यवहार में साधक उदारता का व्यवहार करने लगता है । दूसरों को कष्ट न हो इसलिये सहजभाव से उसमें संयम आता है । वाणी में मधुरता आती है। साधक जनप्रिय बनने लगता है। योग के 'धारण' नामक अंग की प्राप्ति होती है। चित्त को साधक मर्यादित क्षेत्र में सीमित रखता है। जिससे चित्त की चंचलता कम होने लगती है । अब उसे बाहरी भौतिक भोगों में अरुचि होकर चित्त को आत्मस्वरूप में लगाता है । अपने भीतर चलने वाली संवेदनाओं से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है । आत्मविकास में वह अधिक सजग बनता है । अपने स्वरूप में लीन होता है। सजग होकर अपने भीतर चलने वाले व्यापारों को देखता है। उसमें सूक्ष्म बोध जगता है । मनोभावों की शुद्धि हो जाती है। उसका मन बाहरी जगत से अन्तर्जगत् की ओर रमण करने लगता है। जो राग-द्वेष अहता-ममता के कारण आत्मा के शुद्ध स्वभाव पर आवरण आता था, वह दूर होकर निर्मलता बढ़ती है । साधक में समता बढ़ती जाती है। संयम में वृद्धि होती है। प्रभा दृष्टि साधक एक आसन पर स्थिर होकर नियमित रूप से सतत् ध्यान का अभ्यास बढ़ाता है तो उसमें सातवीं प्रभा दृष्टि प्रकट होती है । जिससे उसका बोध सूर्य की प्रभा की तरह प्रकाशमान होता है । मन विकल्परहित होकर ध्यान में अखण्डता आने लगती है। वह अधिक समय तक ध्यान में स्थिर रहने लगता है। जिससे उसे सहज शान्ति मिलने लगती है। प्राप्त परिस्थिति में समतापूर्वक रहने का अभ्यास इतना अधिक बढ़ जाता है कि बाहरी सुख की कामना ही लुप्त हो जाती है । जो मुख आत्मा पर आवरणों के कारण ढका हुआ था, वह आवरणों के दूर होते ही पूर्णरूप से प्रकट होता है जिससे दुःख का उस पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं रहता । यह स्थिति किसी शास्त्रज्ञान पर आधारित नहीं होती पर चित्त की निर्मलता के कारण आत्मज्ञान पर-स्वानुभव पर आधारित होती है। राग-द्वेष और कषायों का उपशमन हो जाने से नये कर्मों का बंध नहीं होता । पुराने बंधे कर्मों की समता के कारण निर्जरा होने लगती है। दूसरों के साथ समता रखते हुए भी यदि कोई दुर्व्यवहार करता है तो भी साधक उसके प्रति मैत्रीभाव ही रखता है । उस पर आ पड़े उन दुःखों से उद्विग्न नहीं होता। और न ही उसमें सुखों की स्पृहा या लालसा ही होती है। जिससे साधक पर सुख-दुःखों का प्रभाव नहीं होता । वह इन आने वाले सुख-दुःखों के खेल को देखता रहता है। उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। योग की भाषा में यह स्थिति ध्यान कही जा सकती है जिसमें ध्यान की साधना कर आत्मानुभव या स्वानुभव की स्थिति का समय अधिक बढ़ाने का प्रयास होता है जिससे कि परादृष्टि की प्राप्ति हो सके। परादृष्टि इसे योग की भाषा में समाधि कहा जाता है, जिसमें आत्मा की शुद्ध स्थिति प्राप्त होकर संसार को निर्लेप भाव से साधक देखता है । ध्यान की वह अवस्था प्राप्त हो जाती है जिससे सहज भाव से साधक आत्म-समाधि में लीन हो जाता है। इसे जैन-साधना में शुक्लध्यान कहा जाता है । साधकजीवन-मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रहता है। उसमें केवल आत्मभावना रह जाती है । अपना-पराया का भेद मिटाकर प्राणी मात्र को आत्मवत् देखता है और उनके साथ पूर्ण संयम का आचरण करता है । मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने से वीतराग बन जाता है जो अवस्था उसे निर्वाण दशा तक पहुँचा देती है । दुःखों से पूर्ण मुक्ति देकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मध्यान और भक्ति जैन-दर्शन में भक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति का रूप भिन्न है। इसमें वीतराग की Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6