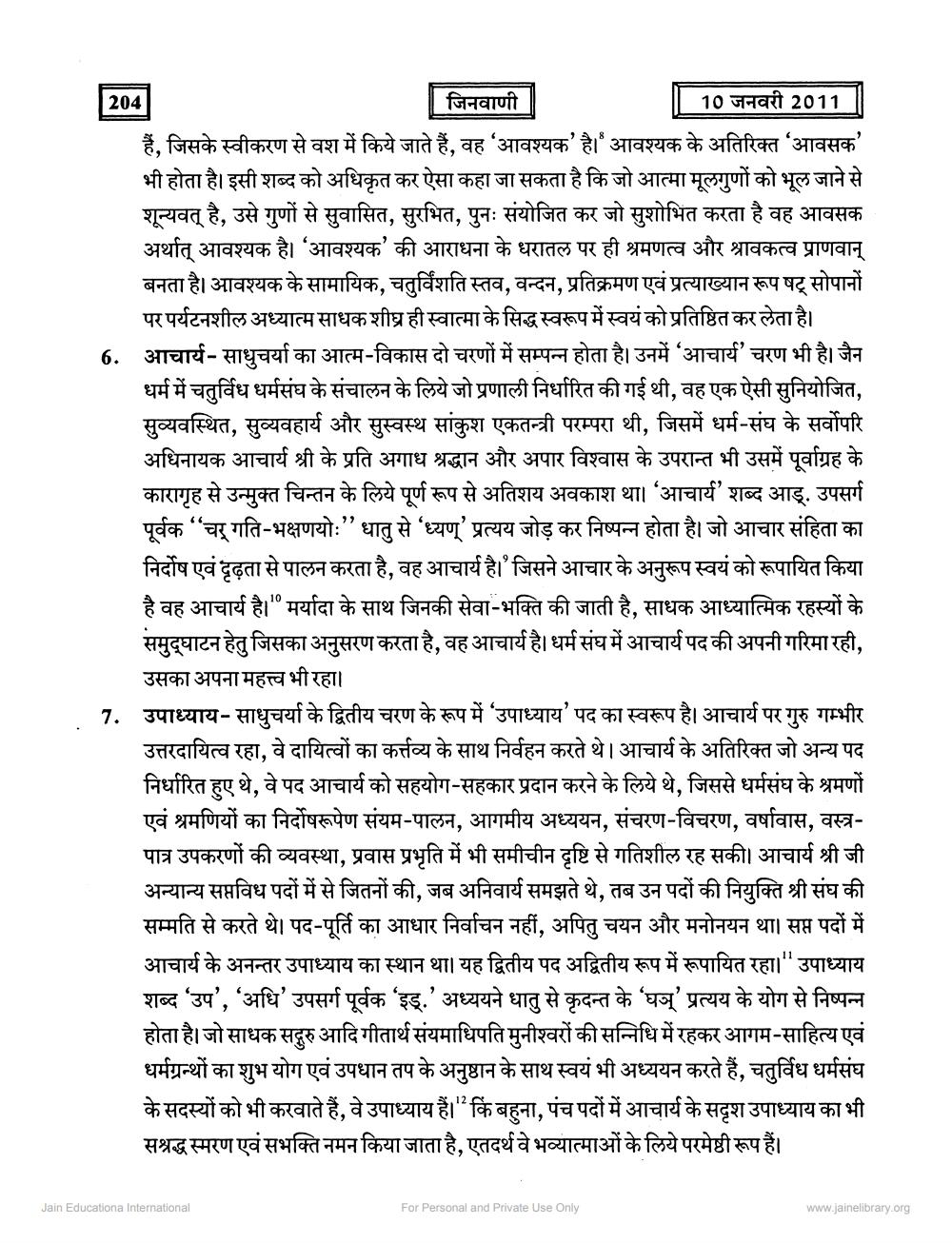Book Title: Shramanachar Parichayak Katipay Paribhashik Shabda Author(s): Rameshmuni Publisher: Z_Jinvani_Guru_Garima_evam_Shraman_Jivan_Visheshank_003844.pdf View full book textPage 3
________________ 204 जिनवाणी 10 जनवरी 2011 हैं, जिसके स्वीकरण से वश में किये जाते हैं, वह 'आवश्यक' है।' आवश्यक के अतिरिक्त 'आवसक' भी होता है। इसी शब्द को अधिकृत कर ऐसा कहा जा सकता है कि जो आत्मा मूलगुणों को भूल जाने से शून्यवत् है, उसे गुणों से सुवासित, सुरभित, पुनः संयोजित कर जो सुशोभित करता है वह आवसक अर्थात् आवश्यक है। ‘आवश्यक' की आराधना के धरातल पर ही श्रमणत्व और श्रावकत्व प्राणवान् बनता है। आवश्यक के सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वन्दन, प्रतिक्रमण एवं प्रत्याख्यान रूप षट् सोपानों पर पर्यटनशील अध्यात्म साधक शीघ्र ही स्वात्मा के सिद्ध स्वरूप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर लेता है। 6. आचार्य - साधुचर्या का आत्म-विकास दो चरणों में सम्पन्न होता है। उनमें 'आचार्य' चरण भी है। जैन धर्म में चतुर्विध धर्मसंघ के संचालन के लिये जो प्रणाली निर्धारित की गई थी, वह एक ऐसी सुनियोजित, सुव्यवस्थित, सुव्यवहार्य और सुस्वस्थ सांकुश एकतन्त्री परम्परा थी, जिसमें धर्म-संघ के सर्वोपरि अधिनायक आचार्य श्री के प्रति अगाध श्रद्धान और अपार विश्वास के उपरान्त भी उसमें पूर्वाग्रह के गृह से उन्मुक्त चिन्तन के लिये पूर्ण रूप से अतिशय अवकाश था। 'आचार्य' शब्द आड्. उपसर्ग पूर्वक “चर् गति-भक्षणयोः " धातु से 'ध्यण्' प्रत्यय जोड़ कर निष्पन्न होता है। जो आचार संहिता का निर्दोष एवं दृढ़ता से पालन करता है, वह आचार्य है।' जिसने आचार के अनुरूप स्वयं को रूपायित किया है वह आचार्य है।" मर्यादा के साथ जिनकी सेवा - भक्ति की जाती है, साधक आध्यात्मिक रहस्यों के समुद्घाटन हेतु जिसका अनुसरण करता है, वह आचार्य है। धर्म संघ में आचार्य पद की अपनी गरिमा रही, उसका अपना महत्त्व भी रहा। 7. उपाध्याय- साधुचर्या के द्वितीय चरण के रूप में 'उपाध्याय' पद का स्वरूप है। आचार्य पर गुरु गम्भीर उत्तरदायित्व रहा, वे दायित्वों का कर्त्तव्य के साथ निर्वहन करते थे । आचार्य के अतिरिक्त जो अन्य पद निर्धारित हुए थे, वे पद आचार्य को सहयोग - सहकार प्रदान करने के लिये थे, जिससे धर्मसंघ के श्रमणों एवं श्रमणियों का निर्दोषरूपेण संयम- पालन, आगमीय अध्ययन, संचरण - विचरण, वर्षावास, वस्त्रपात्र उपकरणों की व्यवस्था, प्रवास प्रभृति में भी समीचीन दृष्टि से गतिशील रह सकी। आचार्य श्री जी अन्यान्य सप्तविध पदों में से जितनों की, जब अनिवार्य समझते थे, तब उन पदों की नियुक्ति श्री संघ की सम्मति से करते थे। पद-पूर्ति का आधार निर्वाचन नहीं, अपितु चयन और मनोनयन था। सप्त पदों में आचार्य के अनन्तर उपाध्याय का स्थान था। यह द्वितीय पद अद्वितीय रूप में रूपायित रहा।" उपाध्याय शब्द ‘उप’, ‘अधि’ उपसर्ग पूर्वक 'इड्. ' अध्ययने धातु से कृदन्त के 'घञ्' प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। जो साधक सद्गुरु आदि गीतार्थ संयमाधिपति मुनीश्वरों की सन्निधि में रहकर आगम-साहित्य एवं धर्मग्रन्थों का शुभ योग एवं उपधान तप के अनुष्ठान के साथ स्वयं भी अध्ययन करते हैं, चतुर्विध धर्मसंघ के सदस्यों को भी करवाते हैं, वे उपाध्याय हैं।" किं बहुना, पंच पदों में आचार्य के सदृश उपाध्याय का भी सश्रद्ध स्मरण एवं सभक्ति नमन किया जाता है, एतदर्थ वे भव्यात्माओं के लिये परमेष्ठी रूप हैं। Jain Educationa International For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7