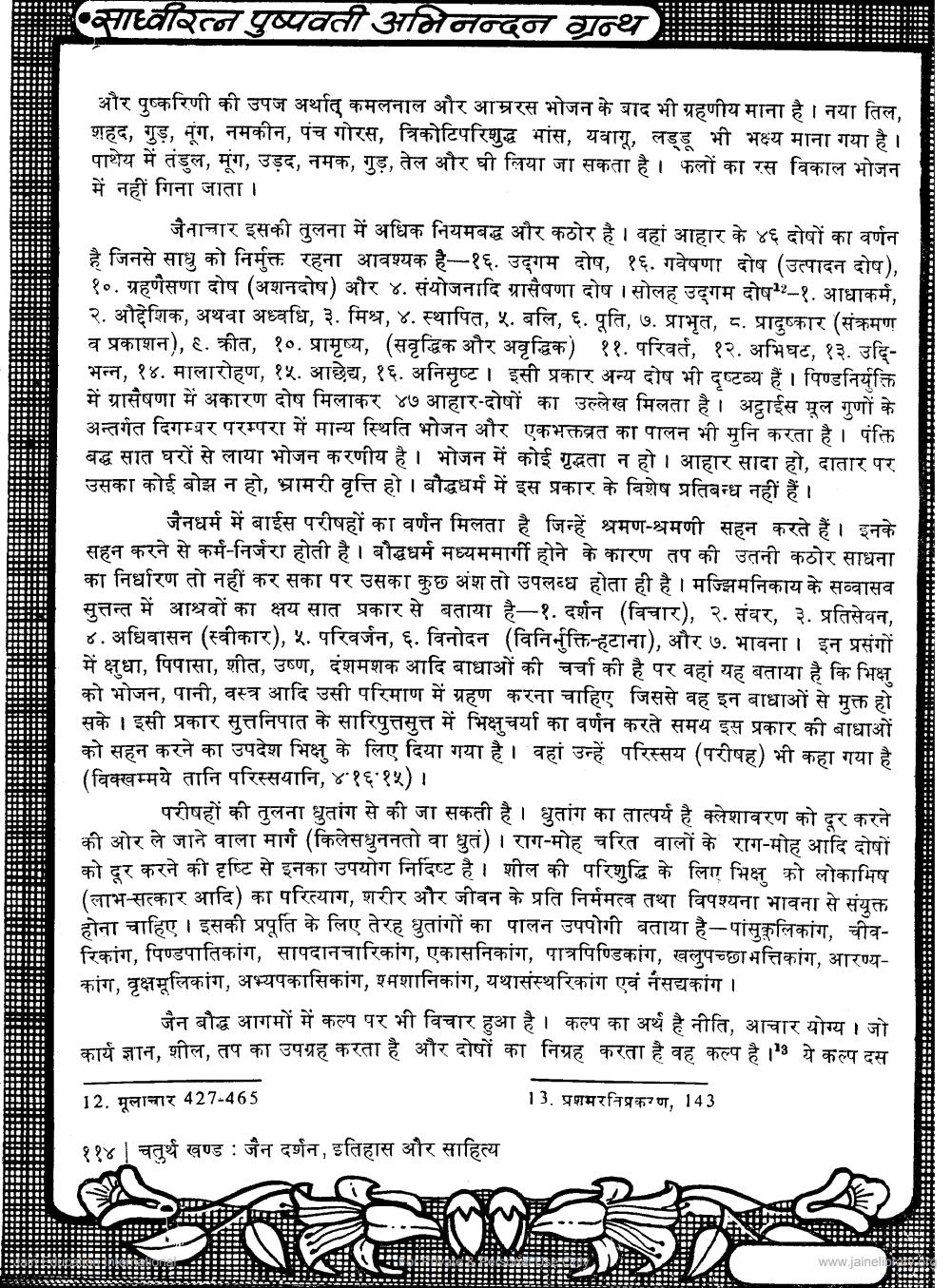Book Title: Shraman Achar Miamnsa Author(s): Bhagchandra Jain Publisher: Z_Sadhviratna_Pushpvati_Abhinandan_Granth_012024.pdf View full book textPage 5
________________ ● साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ और पुष्करिणी की उपज अर्थात् कमलनाल और आम्ररस भोजन के बाद भी ग्रहणीय माना है । नया तिल, शहद, गुड़, मूंग, नमकीन, पंच गोरस, त्रिकोटिपरिशुद्ध मांस, यवागू, लड्डू भी भक्ष्य माना गया है । पाथेय में तंडुल, मूंग, उड़द, नमक, गुड़, तेल और घी लिया जा सकता है। फलों का रस विकाल भोजन में नहीं गिना जाता । जैनाचार इसकी तुलना में अधिक नियमबद्ध और कठोर है । वहां आहार के ४६ दोषों का वर्णन है जिनसे साधु को निर्मुक्त रहना आवश्यक है - १६. उद्गम दोष, १६. गवेषणा दोष ( उत्पादन दोष ), १०. ग्रहणैसणा दोष ( अशनदोष) और ४. संयोजनादि ग्रासैषणा दोष । सोलह उद्गम दोष - १. आधाकर्म, २. औद्देशिक, अथवा अध्वधि, ३. मिश्र, ४. स्थापित, ५. बलि, ६. पूति, ७. प्राभृत, ८ प्रादुष्कार (संक्रमण व प्रकाशन ), ६. क्रीत, १०. प्रामृष्य, (सवृद्धिक और अवृद्धिक) ११. परिवर्त, १२. अभिघट, १३. उदिभन्न, १४. मालारोहण, १५. आछेद्य, १६. अनिसृष्ट । इसी प्रकार अन्य दोष भी दृष्टव्य हैं । पिण्डनिर्युक्ति में ग्रासैषणा में अकारण दोष मिलाकर ४७ आहार- दोषों का उल्लेख मिलता है। अट्ठाईस मूल गुणों के अन्तर्गत दिगम्बर परम्परा में मान्य स्थिति भोजन और एकभक्तव्रत का पालन भी मुनि करता है । पंक्ति बद्ध सात घरों से लाया भोजन करणीय है । भोजन में कोई गृद्धता न हो। आहार सादा हो, दातार पर उसका कोई बोझ न हो, भ्रामरी वृत्ति हो । बौद्धधर्म में इस प्रकार के विशेष प्रतिबन्ध नहीं हैं । 1 जैनधर्म में बाईस परीषहों का वर्णन मिलता है जिन्हें श्रमण श्रमणी सहन करते हैं । इनके सहन करने से कर्म - निर्जरा होती है । बौद्धधर्म मध्यममार्गी होने के कारण तप की उतनी कठोर साधना का निर्धारण तो नहीं कर सका पर उसका कुछ अंश तो उपलब्ध होता ही है । मज्झिमनिकाय के सव्वासव सुत्तन्त में आश्रवों का क्षय सात प्रकार से बताया है - १. दर्शन (विचार), २. संवर, ३. प्रतिसेवन, ४. अधिवासन ( स्वीकार), ५. परिवर्जन, ६. विनोदन (विनिर्मुक्ति- हटाना ), और ७. भावना । इन प्रसंगों में क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक आदि बाधाओं की चर्चा की है पर वहां यह बताया है कि भिक्षु को भोजन, पानी, वस्त्र आदि उसी परिमाण में ग्रहण करना चाहिए जिससे वह इन बाधाओं से मुक्त हो सके । इसी प्रकार सुत्तनिपात के सारिपुत्तसुत्त में भिक्षुचर्या का वर्णन करते समय इस प्रकार की बाधाओं को सहन करने का उपदेश भिक्षु के लिए दिया गया है। वहां उन्हें परिस्सय ( परीषह ) भी कहा गया है। ( विक्खम्ये तानि परिस्सयानि, ४ १६-१५) । 1 परीषों की तुलना धुतांग से की जा सकती है । धुतांग का तात्पर्य है क्लेशावरण को दूर करने की ओर ले जाने वाला मार्ग (किलेसधुननतो वा धुतं) । राग- मोह चरित वालों के राग- मोह आदि दोषों को दूर करने की दृष्टि से इनका उपयोग निर्दिष्ट है । शील की परिशुद्धि के लिए भिक्षु को लोकाभिष ( लाभ - सत्कार आदि) का परित्याग, शरीर और जीवन के प्रति निर्ममत्व तथा विपश्यना भावना से संयुक्त होना चाहिए । इसकी प्रपूर्ति के लिए तेरह धुतांगों का पालन उपपोगी बताया है- पांसुकुलिकांग, चीवरिकांग, पिण्डपातिकांग, सापदानचारिकांग, एकासनिकांग, पात्रपिण्डिकांग, खलुपच्छा भत्तिकांग, आरण्यकांग, वृक्षमूलिकांग, अभ्यपकासिकांग, श्मशानिकांग, यथासंस्थरिकांग एवं सद्यांग । जैन बौद्ध आगमों में कल्प पर भी विचार हुआ है । कल्प का अर्थ है नीति, आचार योग्य । जो कार्य ज्ञान, शील, तप का उपग्रह करता है और दोषों का निग्रह करता है वह कल्प है । ये कल्प द 12. मूलाचार 427-465 13. प्रशमरतिप्रकरण, 143 ११४ | चतुर्थ खण्ड : जैन दर्शन, इतिहास और साहित्य www.jainellowPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10