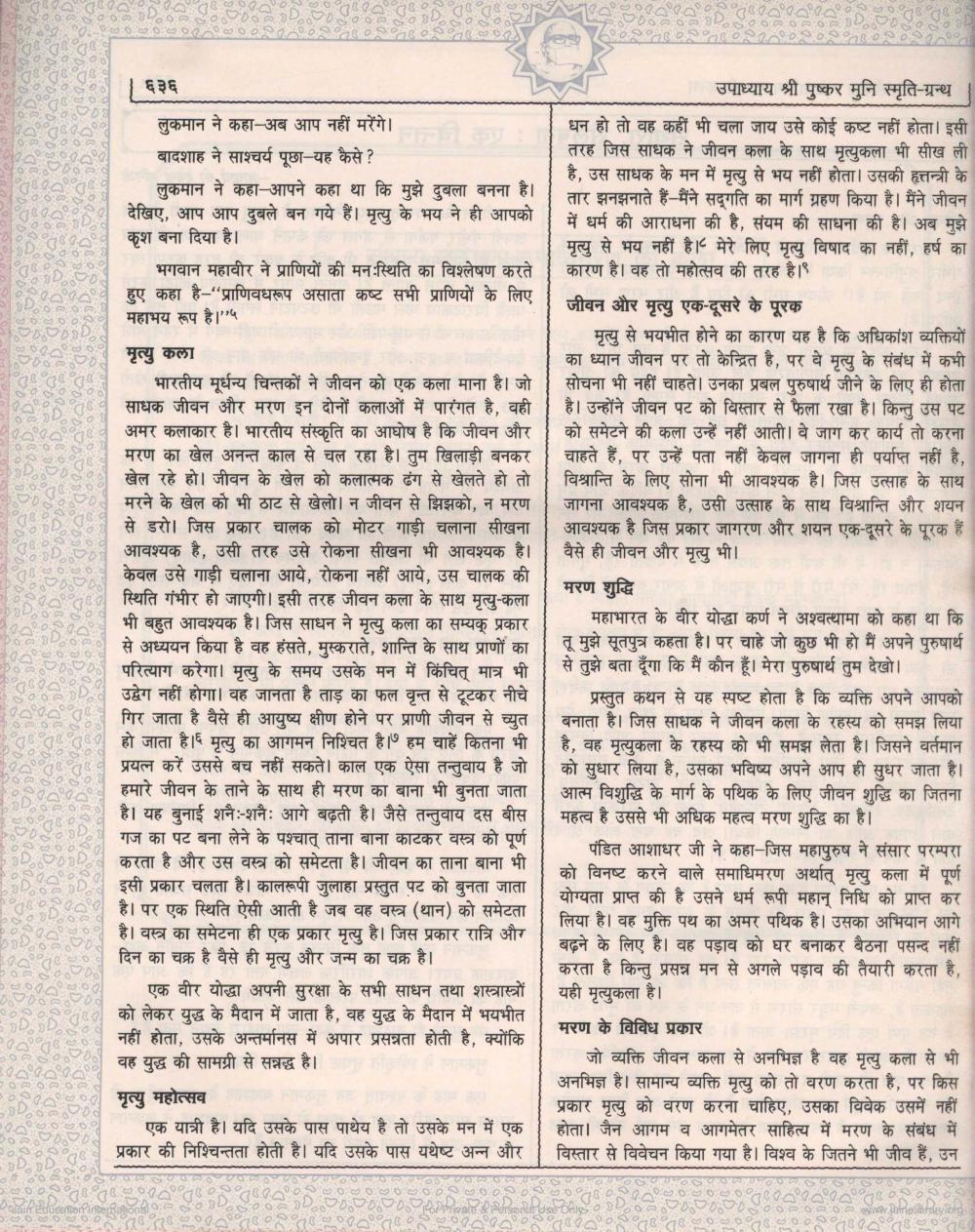Book Title: Santhara Sanleshna Ek Chintan Author(s): Devendramuni Shastri Publisher: Z_Nahta_Bandhu_Abhinandan_Granth_012007.pdf View full book textPage 2
________________ ६३६ लुकमान ने कहा- अब आप नहीं मरेंगे। बादशाह ने साश्चर्य पूछा- यह कैसे ? लुकमान ने कहा- आपने कहा था कि मुझे दुबला बनना है। देखिए, आप आप दुबले बन गये हैं। मृत्यु के भय ने ही आपको कृश बना दिया है। भगवान महावीर ने प्राणियों की मनःस्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है- "प्राणिवधरूप असाता कष्ट सभी प्राणियों के लिए महाभय रूप है। "५ मृत्यु कला भारतीय मूर्धन्य चिन्तकों ने जीवन को एक कला माना है। जो साधक जीवन और मरण इन दोनों कलाओं में पारंगत है, वही अमर कलाकार है। भारतीय संस्कृति का आघोष है कि जीवन और मरण का खेल अनन्त काल से चल रहा है। तुम खिलाड़ी बनकर खेल रहे हो। जीवन के खेल को कलात्मक ढंग से खेलते हो तो मरने के खेल को भी ठाट से खेलो। न जीवन से झिझको, न मरण से डरो जिस प्रकार चालक को मोटर गाड़ी चलाना सीखना आवश्यक है, उसी तरह उसे रोकना सीखना भी आवश्यक है। केवल उसे गाड़ी चलाना आये, रोकना नहीं आये, उस चालक की स्थिति गंभीर हो जाएगी। इसी तरह जीवन कला के साथ मृत्यु-कला भी बहुत आवश्यक है। जिस साधन ने मृत्यु कला का सम्यक् प्रकार से अध्ययन किया है वह हंसते, मुस्कराते, शान्ति के साथ प्राणों का परित्याग करेगा। मृत्यु के समय उसके मन में किंचित् मात्र भी उद्वेग नहीं होगा। वह जानता है ताड़ का फल वृन्त से टूटकर नीचे गिर जाता है वैसे ही आयुष्य क्षीण होने पर प्राणी जीवन से च्युत हो जाता है । ६ मृत्यु का आगमन निश्चित है। हम चाहें कितना भी प्रयत्न करें उससे बच नहीं सकते काल एक ऐसा तन्तुवाय है जो हमारे जीवन के ताने के साथ ही मरण का बाना भी बुनता जाता है । यह बुनाई शनैः-शनैः आगे बढ़ती है। जैसे तन्तुवाय दस बीस गज का पट बना लेने के पश्चात् ताना बाना काटकर वस्त्र को पूर्ण करता है और उस वस्त्र को समेटता है जीवन का ताना बाना भी इसी प्रकार चलता है। कालरूपी जुलाहा प्रस्तुत पट को बुनता जाता है पर एक स्थिति ऐसी आती है जब यह वस्त्र (धान) को समेटता है। वस्त्र का समेटना ही एक प्रकार मृत्यु है जिस प्रकार रात्रि और दिन का चक्र है वैसे ही मृत्यु और जन्म का चक्र है। एक वीर योद्धा अपनी सुरक्षा के सभी साधन तथा शस्त्रास्त्रों को लेकर युद्ध के मैदान में जाता है, वह युद्ध के मैदान में भयभीत नहीं होता, उसके अन्तर्मानस में अपार प्रसन्नता होती है, क्योंकि वह युद्ध की सामग्री से सन्नद्ध है। मृत्यु महोत्सव एक यात्री है। यदि उसके पास पाथेय है तो उसके मन में एक प्रकार की निश्चिन्तता होती है। यदि उसके पास यथेष्ट अन्न और उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि स्मृति ग्रन्थ धन हो तो वह कहीं भी चला जाय उसे कोई कष्ट नहीं होता। इसी तरह जिस साधक ने जीवन कला के साथ मृत्युकला भी सीख ली है, उस साधक के मन में मृत्यु से भय नहीं होता। उसकी हत्तन्त्री के तार झनझनाते हैं-मैंने सद्गति का मार्ग ग्रहण किया है। मैंने जीवन में धर्म की आराधना की है, संयम की साधना की है। अब मुझे मृत्यु से भय नहीं है।" मेरे लिए मृत्यु विषाद का नहीं, हर्ष का कारण है। वह तो महोत्सव की तरह है । ९ जीवन और मृत्यु एक-दूसरे के पूरक मृत्यु से भयभीत होने का कारण यह है कि अधिकांश व्यक्तियों का ध्यान जीवन पर तो केन्द्रित है, पर वे मृत्यु के संबंध में कभी सोचना भी नहीं चाहते। उनका प्रबल पुरुषार्थ जीने के लिए ही होता है। उन्होंने जीवन पट को विस्तार से फैला रखा है। किन्तु उस पट को समेटने की कला उन्हें नहीं आती। वे जाग कर कार्य तो करना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं केवल जागना ही पर्याप्त नहीं है, विश्रान्ति के लिए सोना भी आवश्यक है। जिस उत्साह के साथ जागना आवश्यक है, उसी उत्साह के साथ विश्रान्ति और शयन आवश्यक है जिस प्रकार जागरण और शयन एक-दूसरे के पूरक वैसे ही जीवन और मृत्यु भी। मरण शुद्धि महाभारत के वीर योद्धा कर्ण ने अश्वत्थामा को कहा था कि तू मुझे सूतपुत्र कहता है। पर चाहे जो कुछ भी हो मैं अपने पुरुषार्थ से तुझे बता दूँगा कि मैं कौन हूँ। मेरा पुरुषार्थ तुम देखो। प्रस्तुत कथन से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अपने आपको बनाता है। जिस साधक ने जीवन कला के रहस्य को समझ लिया है, वह मृत्युकला के रहस्य को भी समझ लेता है। जिसने वर्तमान को सुधार लिया है, उसका भविष्य अपने आप ही सुधर जाता है। आत्म विशुद्धि के मार्ग के पथिक के लिए जीवन शुद्धि का जितना महत्व है उससे भी अधिक महत्व मरण शुद्धि का है। पंडित आशाधर जी ने कहा- जिस महापुरुष ने संसार परम्परा को विनष्ट करने वाले समाधिमरण अर्थात् मृत्यु कला में पूर्ण योग्यता प्राप्त की है उसने धर्म रूपी महान् निधि को प्राप्त कर लिया है। वह मुक्ति पथ का अमर पथिक है। उसका अभियान आगे बढ़ने के लिए है। वह पड़ाव को घर बनाकर बैठना पसन्द नहीं करता है किन्तु प्रसन्न मन से अगले पड़ाव की तैयारी करता है, यही मृत्युकला है। मरण के विविध प्रकार जो व्यक्ति जीवन कला से अनभिज्ञ है वह मृत्यु कला से भी अनभिज्ञ है। सामान्य व्यक्ति मृत्यु को तो वरण करता है, पर किस प्रकार मृत्यु को वरण करना चाहिए, उसका विवेक उसमें नहीं होता। जैन आगम व आगमेतर साहित्य में मरण के संबंध में विस्तार से विवेचन किया गया है। विश्व के जितने भी जीव है, उन www.parelifey brgsPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21