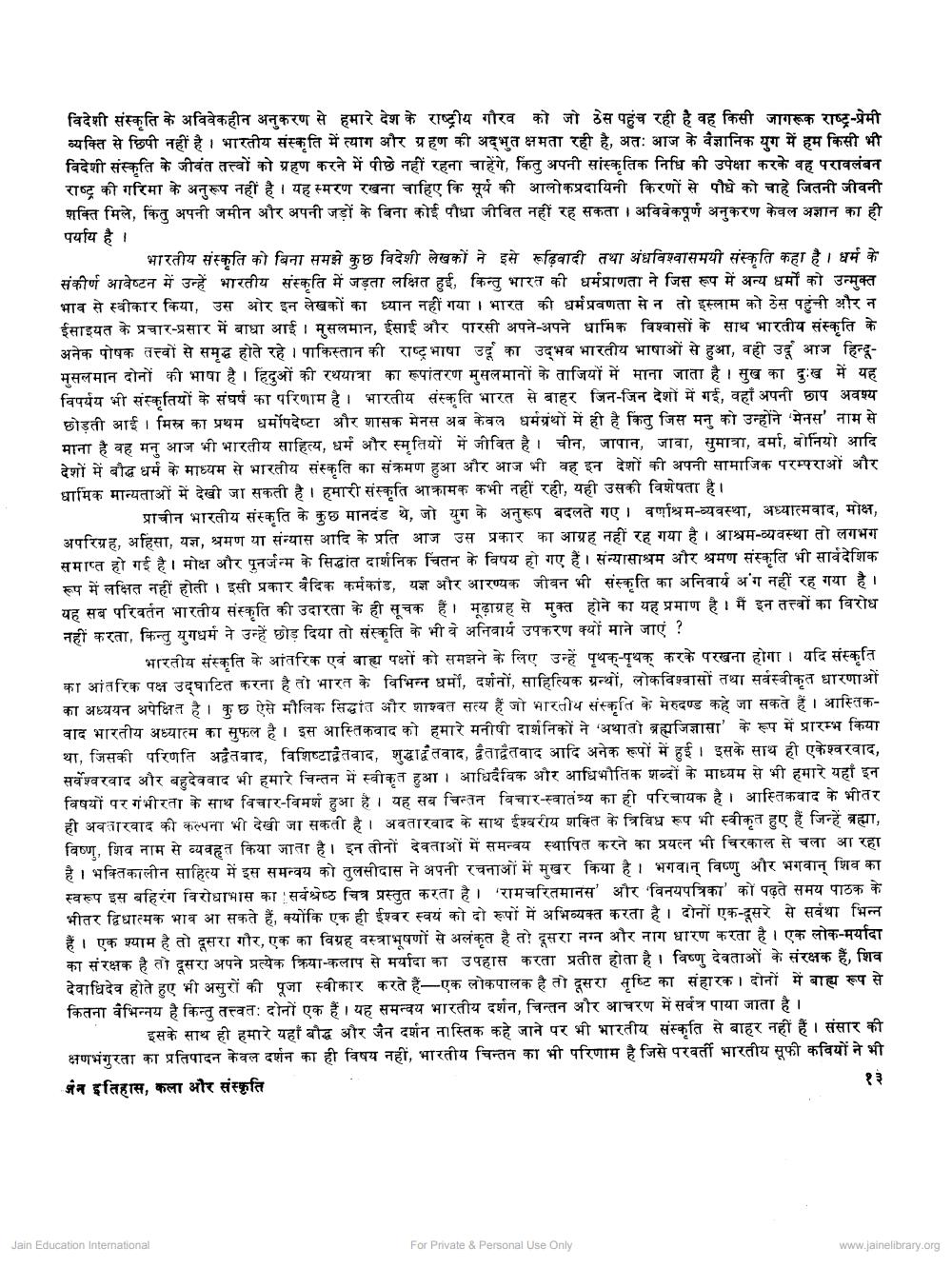Book Title: Sanskruti ka Swarup Bharatiya Sanskrut aur Jain Sanskruti Author(s): Vijayendra Snataka Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 5
________________ विदेशी संस्कृति के अविवेकहीन अनुकरण से हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंच रही है वह किसी जागरूक राष्ट्र-प्रेमी व्यक्ति से छिपी नहीं है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है, अतः आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्त्वों को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहेंगे, किंतु अपनी सांस्कृतिक निधि की उपेक्षा करके वह परावलंबन राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है । यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य की आलोकप्रदायिनी किरणों से पौधे को चाहे जितनी जीवनी शक्ति मिले, किंतु अपनी जमीन और अपनी जड़ों के बिना कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता । अविवेकपूर्ण अनुकरण केवल अज्ञान का ही पर्याय है। भारतीय संस्कृति को बिना समझे कुछ विदेशी लेखकों ने इसे रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासमयी संस्कृति कहा है। धर्म के संकीर्ण आवेष्टन में उन्हें भारतीय संस्कृति में जड़ता लक्षित हुई, किन्तु भारत की धर्मप्राणता ने जिस रूप में अन्य धर्मों को उन्मुक्त भाव से स्वीकार किया, उस ओर इन लेखकों का ध्यान नहीं गया। भारत की धर्मप्रवणता से न तो इस्लाम को ठेस पहुंची और न ईसाइयत के प्रचार-प्रसार में बाधा आई । मुसलमान, ईसाई और पारसी अपने-अपने धार्मिक विश्वासों के साथ भारतीय संस्कृति के अनेक पोषक तत्त्वों से समृद्ध होते रहे । पाकिस्तान की राष्ट्र भाषा उर्दू का उद्भव भारतीय भाषाओं से हुआ, वही उर्दू आज हिन्दूमुसलमान दोनों की भाषा है। हिंदुओं की रथयात्रा का रूपांतरण मुसलमानों के ताजियों में माना जाता है। सुख का दुःख में यह विपर्यय भी संस्कृतियों के संघर्ष का परिणाम है। भारतीय संस्कृति भारत से बाहर जिन-जिन देशों में गई, वहाँ अपनी छाप अवश्य छोड़ती आई । मिस्र का प्रथम धर्मोपदेष्टा और शासक मेनस अब केवल धर्मग्रंथों में ही है किंतु जिस मनु को उन्होंने 'मेनस' नाम से माना है वह मनु आज भी भारतीय साहित्य, धर्म और स्मृतियों में जीवित है। चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, बर्मा, बोनियो आदि देशों में बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संक्रमण हुआ और आज भी वह इन देशों की अपनी सामाजिक परम्पराओं और धार्मिक मान्यताओं में देखी जा सकती है। हमारी संस्कृति आक्रामक कभी नहीं रही, यही उसकी विशेषता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के कुछ मानदंड थे, जो युग के अनुरूप बदलते गए। वर्णाश्रम-व्यवस्था, अध्यात्मवाद, मोक्ष, अपरिग्रह, अहिंसा, यज्ञ, श्रमण या संन्यास आदि के प्रति आज उस प्रकार का आग्रह नहीं रह गया है। आश्रम-व्यवस्था तो लगभग समाप्त हो गई है। मोक्ष और पुनर्जन्म के सिद्धांत दार्शनिक चिंतन के विषय हो गए हैं। संन्यासाश्रम और श्रमण संस्कृति भी सार्वदेशिक रूप में लक्षित नहीं होती। इसी प्रकार वैदिक कर्मकांड, यज्ञ और आरण्यक जीवन भी संस्कृति का अनिवार्य अंग नहीं रह गया है। यह सब परिवर्तन भारतीय संस्कृति की उदारता के ही सूचक हैं। मूढ़ाग्रह से मुक्त होने का यह प्रमाण है। मैं इन तत्त्वों का विरोध नहीं करता, किन्तु युगधर्म ने उन्हें छोड़ दिया तो संस्कृति के भी वे अनिवार्य उपकरण क्यों माने जाएं ? ___ भारतीय संस्कृति के आंतरिक एवं बाह्य पक्षों को समझने के लिए उन्हें पृथक्-पृथक् करके परखना होगा। यदि संस्कृति का आंतरिक पक्ष उद्घाटित करना है तो भारत के विभिन्न धर्मों, दर्शनों, साहित्यिक ग्रन्थों, लोकविश्वासों तथा सर्वस्वीकृत धारणाओं का अध्ययन अपेक्षित है। कुछ ऐसे मौलिक सिद्धांत और शाश्वत सत्य हैं जो भारतीय संस्कृति के मेरुदण्ड कहे जा सकते हैं। आस्तिकवाद भारतीय अध्यात्म का सुफल है। इस आस्तिकवाद को हमारे मनीषी दार्शनिकों ने 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' के रूप में प्रारम्भ किया था, जिसकी परिणति अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद आदि अनेक रूपों में हुई। इसके साथ ही एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद और बहुदेववाद भी हमारे चिन्तन में स्वीकृत हुआ। आधिदैविक और आधिभौतिक शब्दों के माध्यम से भी हमारे यहाँ इन विषयों पर गंभीरता के साथ विचार-विमर्श हुआ है। यह सब चिन्तन विचार-स्वातंत्र्य का ही परिचायक है। आस्तिकवाद के भीतर ही अवतारवाद की कल्पना भी देखी जा सकती है। अवतारवाद के साथ ईश्वरीय शक्ति के त्रिविध रूप भी स्वीकृत हुए हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शिव नाम से व्यवहृत किया जाता है। इन तीनों देवताओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न भी चिरकाल से चला आ रहा है। भक्तिकालीन साहित्य में इस समन्वय को तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में मुखर किया है। भगवान् विष्णु और भगवान् शिव का स्वरूप इस बहिरंग विरोधाभास का सर्वश्रेष्ठ चित्र प्रस्तुत करता है। 'रामचरितमानस' और 'विनयपत्रिका' को पढ़ते समय पाठक के भीतर द्विधात्मक भाव आ सकते हैं, क्योंकि एक ही ईश्वर स्वयं को दो रूपों में अभिव्यक्त करता है। दोनों एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। एक श्याम है तो दूसरा गौर, एक का विग्रह वस्त्राभूषणों से अलंकृत है तो दूसरा नग्न और नाग धारण करता है। एक लोक-मर्यादा का संरक्षक है तो दूसरा अपने प्रत्येक क्रिया-कलाप से मर्यादा का उपहास करता प्रतीत होता है। विष्णु देवताओं के संरक्षक हैं, शिव देवाधिदेव होते हुए भी असुरों की पूजा स्वीकार करते हैं—एक लोकपालक है तो दूसरा सृष्टि का संहारक। दोनों में बाह्य रूप से कितना वैभिन्नय है किन्तु तत्त्वत: दोनों एक हैं। यह समन्वय भारतीय दर्शन, चिन्तन और आचरण में सर्वत्र पाया जाता है। इसके साथ ही हमारे यहाँ बौद्ध और जैन दर्शन नास्तिक कहे जाने पर भी भारतीय संस्कृति से बाहर नहीं हैं। संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन केवल दर्शन का ही विषय नहीं, भारतीय चिन्तन का भी परिणाम है जिसे परवर्ती भारतीय सूफी कवियों ने भी जैन इतिहास, कला और संस्कृति १३ " जाता है। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8