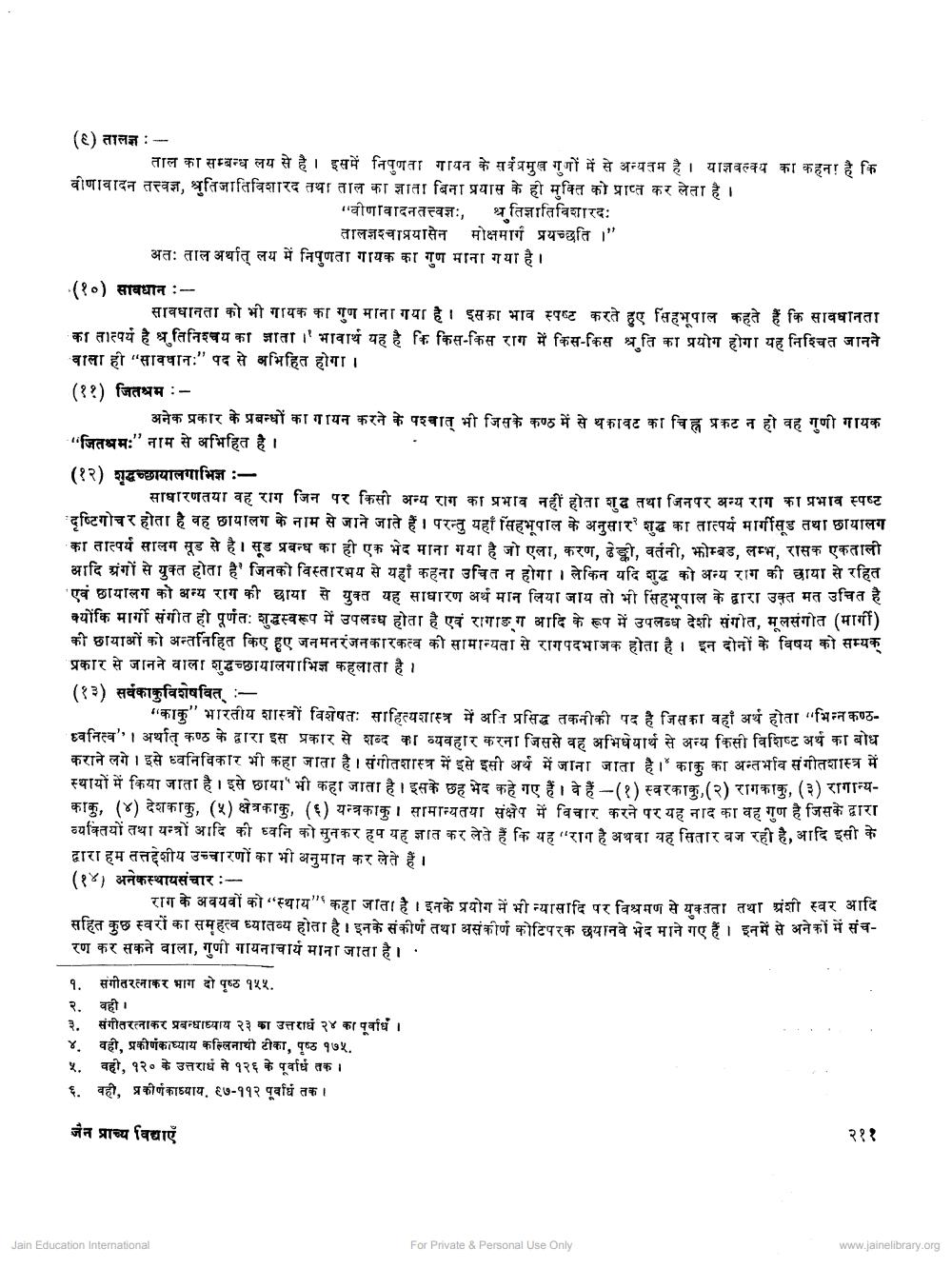Book Title: Sangit Samaysar ke Sandarbh me Gayak Gan Dosh Vivechan Author(s): Vachaspati Moudgalya Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 7
________________ अनक (६) तालज्ञ : ताल का सम्बन्ध लय से है। इसमें निपुणता गायन के सर्वप्रमुख गुगों में से अन्यतम है। याज्ञवल्क्य का कहना है कि वीणावादन तत्त्वज्ञ, श्रुतिजातिविशारद तथा ताल का ज्ञाता बिना प्रयास के ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । "वीणावादनतत्त्वज्ञः, श्रतिज्ञातिविशारदः तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग प्रयच्छति ।" अतः ताल अर्थात् लय में निपुणता गायक का गुण माना गया है। (१०) सावधान : सावधानता को भी गायक का गुण माना गया है। इसका भाव स्पष्ट करते हुए सिंहभूपाल कहते हैं कि सावधानता का तात्पर्य है श्रुतिनिश्चय का ज्ञाता। भावार्थ यह है कि किस-किस राग में किस-किस श्रुति का प्रयोग होगा यह निश्चित जानने वाला ही "सावधानः" पद से अभिहित होगा। (११) जितश्रम : अनेक प्रकार के प्रबन्धों का गायन करने के पश्चात् भी जिसके कण्ठ में से थकावट का चिह्न प्रकट न हो वह गुणी गायक "जितश्रमः" नाम से अभिहित है। (१२) शुद्धच्छायालगाभिज्ञ : साधारणतया वह राग जिन पर किसी अन्य राग का प्रभाव नहीं होता शुद्ध तथा जिनपर अन्य राग का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है वह छायालग के नाम से जाने जाते हैं। परन्तु यहाँ सिहभपाल के अनुसार शुद्ध का तात्पर्य मार्गीसूड तथा छायालग का तात्पर्य सालग सूड से है। सूड प्रबन्ध का ही एक भेद माना गया है जो एला, करण, ढेकी, वर्तनी, झोम्बड, लम्भ, रासक एकताली आदि अंगों से युक्त होता है जिनको विस्तारभय से यहाँ कहना उचित न होगा। लेकिन यदि शुद्ध को अन्य राग की छाया से रहित 'एवं छायालग को अन्य राग की छाया से युक्त यह साधारण अर्थ मान लिया जाय तो भी सिंहभपाल के द्वारा उक्त मत उचित है क्योंकि मार्गी संगीत ही पूर्णत: शुद्धस्वरूप में उपलब्ध होता है एवं रागाङग आदि के रूप में उपलब्ध देशी संगीत, मूलसंगोत (मागी) की छायाओं को अन्तनिहित किए हुए जनमनरंजनकारकत्व की सामान्यता से राग पदभाजक होता है। इन दोनों के विषय को सम्यक प्रकार से जानने वाला शुद्धच्छायालगाभिज्ञ कहलाता है। (१३) सर्वकाकुविशेषवित् : "काकु" भारतीय शास्त्रों विशेषतः साहित्यशास्त्र में अति प्रसिद्ध तकनीकी पद है जिसका वहाँ अर्थ होता "भिन्न कण्ठध्वनित्व'' । अर्थात् कण्ठ के द्वारा इस प्रकार से शब्द का व्यवहार करना जिससे वह अभिधेयार्थ से अन्य किसी विशिष्ट अर्थ का बाध कराने लगे। इसे ध्वनिविकार भी कहा जाता है। संगीतशास्त्र में इसे इसी अर्थ में जाना जाता है। काकु का अन्तर्भाव संगीतशास्त्र म स्थायों में किया जाता है। इसे छाया' भी कहा जाता है। इसके छह भेद कहे गए हैं। वे हैं-(१)स्वरकाकु,(२) रागकाकु, (३) रागान्यकाकू, (४) देशकाकु, (५) क्षेत्रकाकु, (६) यन्त्रकाकु। सामान्यतया संक्षेप में विचार करने पर यह नाद का वह गुण है जिसके द्वारा व्यक्तियों तथा यन्त्रों आदि की ध्वनि को सुनकर हप यह ज्ञात कर लेते हैं कि यह 'राग है अथवा यह सितार बज रही है, आदि इसी के द्वारा हम तत्तद्देशीय उच्चारणों का भी अनुमान कर लेते हैं। (१४) अनेकस्थायसंचार : राग के अवयवों को “स्थाय" कहा जाता है । इनके प्रयोग में भी न्यासादि पर विश्रमण से युक्तता तथा अंशी स्वर आदि सहित कुछ स्वरों का समूहत्व ध्यातव्य होता है। इनके संकीर्ण तथा असंकीर्ण कोटिपरक छयानवे भेद माने गए हैं। इनमें से अनेकों में संचरण कर सकने वाला, गुणी गायनाचार्य माना जाता है।। १. संगीतरत्नाकर भाग दो पृष्ठ १५५. २. वही। ३. संगीतरत्नाकर प्रबन्धाध्याय २३ का उत्तराधं २४ का पूर्वार्ध । ४. वही, प्रकोणकाध्याय कल्लिनाथी टीका, पृष्ठ १७५. ५. वही, १२० के उत्तराधं से १२६ के पूर्वार्ध तक । ६. वही, प्रकीर्णकाध्याय, ६७-११२ पूर्वार्ध तक । जैन प्राच्य विद्याएँ २११ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16