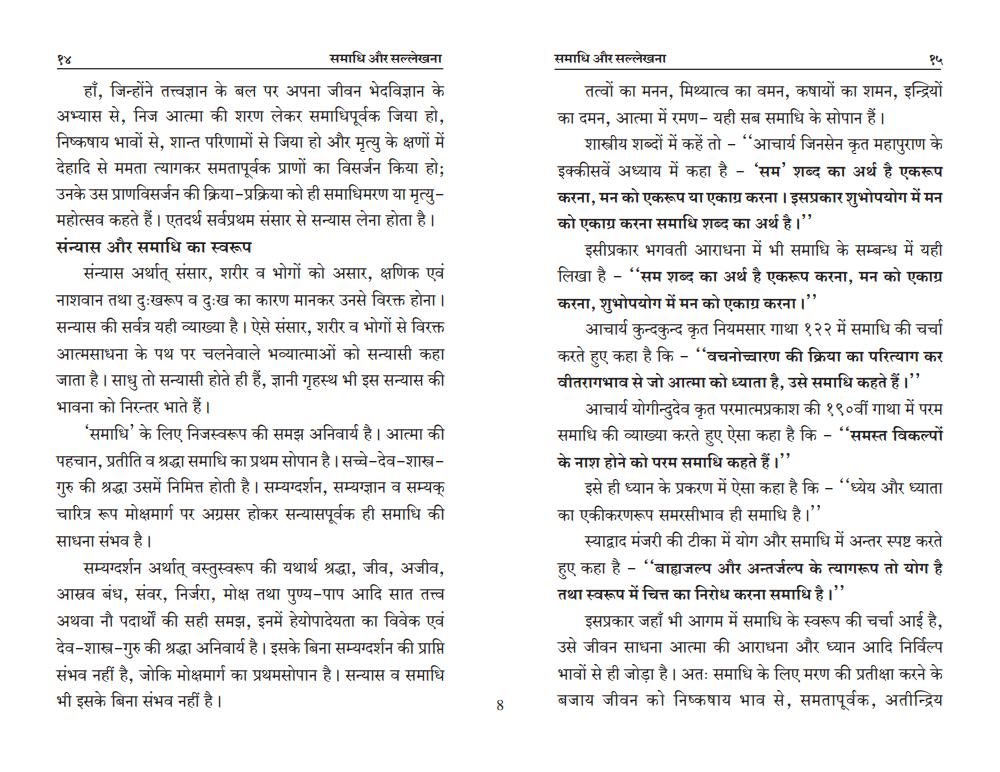Book Title: Samadhi aur Sallekhana Author(s): Ratanchand Bharilla Publisher: Digambar Jain Vidwatparishad Trust View full book textPage 8
________________ समाधि और सल्लेखना हाँ, जिन्होंने तत्त्वज्ञान के बल पर अपना जीवन भेदविज्ञान के अभ्यास से, निज आत्मा की शरण लेकर समाधिपूर्वक जिया हो, निष्कषाय भावों से, शान्त परिणामों से जिया हो और मृत्यु के क्षणों में देहादि से ममता त्यागकर समतापूर्वक प्राणों का विसर्जन किया हो; उनके उस प्राणविसर्जन की क्रिया-प्रक्रिया को ही समाधिमरण या मृत्युमहोत्सव कहते हैं। एतदर्थ सर्वप्रथम संसार से सन्यास लेना होता है। संन्यास और समाधि का स्वरूप संन्यास अर्थात् संसार, शरीर व भोगों को असार, क्षणिक एवं नाशवान तथा दुःखरूप व दुःख का कारण मानकर उनसे विरक्त होना । सन्यास की सर्वत्र यही व्याख्या है। ऐसे संसार, शरीर व भोगों से विरक्त आत्मसाधना के पथ पर चलनेवाले भव्यात्माओं को सन्यासी कहा ता है। साधु तो सन्यासी होते ही हैं, ज्ञानी गृहस्थ भी इस सन्यास की भावना को निरन्तर भाते हैं। १४ 'समाधि' के लिए निजस्वरूप की समझ अनिवार्य है। आत्मा की पहचान, प्रतीति व श्रद्धा समाधि का प्रथम सोपान है। सच्चे-देव-शास्त्रगुरु की श्रद्धा उसमें निमित्त होती है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र रूप मोक्षमार्ग पर अग्रसर होकर सन्यासपूर्वक ही समाधि की साधना संभव है। सम्यग्दर्शन अर्थात् वस्तुस्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, जीव, अजीव, आस्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष तथा पुण्य-पाप आदि सात तत्त्व अथवा नौ पदार्थों की सही समझ, इनमें हेयोपादेयता का विवेक एवं देव - शास्त्र - गुरु की श्रद्धा अनिवार्य है। इसके बिना सम्यग्दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है, जोकि मोक्षमार्ग का प्रथमसोपान है। सन्यास व समाधि भी इसके बिना संभव नहीं है। 8 समाधि और सल्लेखना तत्वों का मनन, मिथ्यात्व का वमन, कषायों का शमन, इन्द्रियों का दमन, आत्मा में रमण- यही सब समाधि के सोपान हैं। शास्त्रीय शब्दों में कहें तो “आचार्य जिनसेन कृत महापुराण के इक्कीसवें अध्याय में कहा है- 'सम' शब्द का अर्थ है एकरूप करना, मन को एकरूप या एकाग्र करना। इसप्रकार शुभोपयोग में मन को एकाग्र करना समाधि शब्द का अर्थ है।" इसीप्रकार भगवती आराधना में भी समाधि के सम्बन्ध में यही लिखा है - "सम शब्द का अर्थ है एकरूप करना, मन को एकाग्र करना, शुभोपयोग में मन को एकाग्र करना । " आचार्य कुन्दकुन्द कृत नियमसार गाथा १२२ में समाधि की चर्चा करते हुए कहा है कि - “वचनोच्चारण की क्रिया का परित्याग कर वीतरागभाव से जो आत्मा को ध्याता है, उसे समाधि कहते हैं।" आचार्य योगीन्दुदेव कृत परमात्मप्रकाश की १९० वीं गाथा में परम समाधि की व्याख्या करते हुए ऐसा कहा है कि - "समस्त विकल्पों के नाश होने को परम समाधि कहते हैं।" इसे ही ध्यान के प्रकरण में ऐसा कहा है कि - " ध्येय और ध्याता का एकीकरणरूप समरसीभाव ही समाधि है ।" स्याद्वाद मंजरी की टीका में योग और समाधि में अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है – “बाह्यजल्प और अन्तर्जल्प के त्यागरूप तो योग है तथा स्वरूप में चित्त का निरोध करना समाधि है।" इसप्रकार जहाँ भी आगम में समाधि के स्वरूप की चर्चा आई है, उसे जीवन साधना आत्मा की आराधना और ध्यान आदि निर्विल्प भावों से ही जोड़ा है। अतः समाधि के लिए मरण की प्रतीक्षा करने के बजाय जीवन को निष्कषाय भाव से, समतापूर्वक, अतीन्द्रियPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23