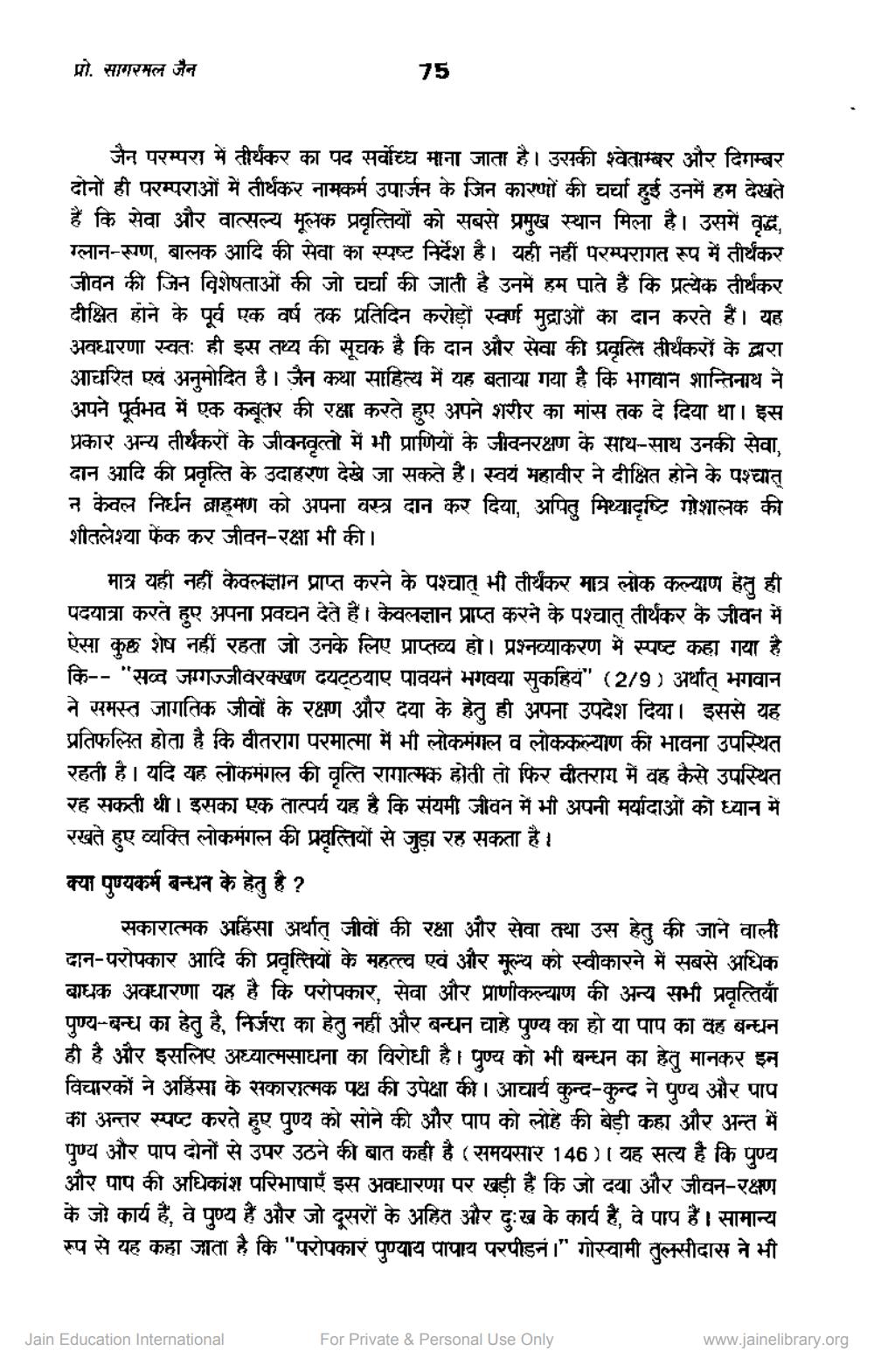Book Title: Sakaratmak Ahinsa ki Bhumika Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Sagar_Jain_Vidya_Bharti_Part_2_001685.pdf View full book textPage 7
________________ प्रो. सागरमल जैन 75 जैन परम्परा में तीर्थंकर का पद सर्वोच्य माना जाता है। उसकी श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में तीर्थंकर नामकर्म उपार्जन के जिन कारणों की चर्चा हुई उनमें हम देखते हैं कि सेवा और वात्सल्य मूलक प्रवृत्तियों को सबसे प्रमुख स्थान मिला है। उसमें वृद्ध, ग्लान-रूपण, बालक आदि की सेवा का स्पष्ट निर्देश है। यही नहीं परम्परागत रूप में तीर्थंकर जीवन की जिन विशेषताओं की जो चर्चा की जाती है उनमें हम पाते हैं कि प्रत्येक तीर्थंकर दीक्षित होने के पूर्व एक वर्ष तक प्रतिदिन करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हैं। यह अवधारणा स्वतः ही इस तथ्य की सूचक है कि दान और सेवा की प्रवृत्ति तीर्थंकरों के द्वारा आचरित एवं अनुमोदित है। जैन कथा साहित्य में यह बताया गया है कि भगवान शान्तिनाथ ने अपने पूर्वभव में एक कबूतर की रक्षा करते हुए अपने शरीर का मांस तक दे दिया था। इस प्रकार अन्य तीर्थंकरों के जीवनवृत्तो में भी प्राणियों के जीवनरक्षण के साथ-साथ उनकी सेवा, दान आदि की प्रवृत्ति के उदाहरण देखे जा सकते है। स्वयं महावीर ने दीक्षित होने के पश्चात् न केवल निर्धन ब्राह्मण को अपना वस्त्र दान कर दिया, अपितु मिथ्यादृष्टि गोशालक की शीतलेश्या फेंक कर जीवन-रक्षा भी की। मात्र यही नहीं केवलज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् भी तीर्थंकर मात्र लोक कल्याण हेतु ही पदयात्रा करते हुए अपना प्रवचन देते हैं। केवलज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् तीर्थंकर के जीवन में ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जो उनके लिए प्राप्तव्य हो। प्रश्नव्याकरण में स्पष्ट कहा गया है कि-- "सव्व जग्गज्जीवरक्खण दयट्ठयाए पावयन भगवया सुकहिय" (2/9 ) अर्थात् भगवान ने समस्त जागतिक जीवों के रक्षण और दया के हेतु ही अपना उपदेश दिया। इससे यह प्रतिफलित होता है कि वीतराग परमात्मा में भी लोकमंगल व लोककल्याण की भावना उपस्थित रहती है। यदि यह लोकमंगल की वृत्ति रागात्मक होती तो फिर वीतराग में वह कैसे उपस्थित रह सकती थी। इसका एक तात्पर्य यह है कि संयमी जीवन में भी अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति लोकमंगल की प्रवृत्तियों से जुड़ा रह सकता है। क्या पुण्यकर्म बन्धन के हेतु है ? सकारात्मक अहिंसा अर्थात् जीवों की रक्षा और सेवा तथा उस हेतु की जाने वाली दान-परोपकार आदि की प्रवृत्तियों के महत्त्व एवं और मूल्य को स्वीकारने में सबसे अधिक बाधक अवधारणा यह है कि परोपकार, सेवा और प्राणीकल्याण की अन्य सभी प्रवृत्तियाँ पुण्य-बन्ध का हेतु है, निर्जरा का हेतु नहीं और बन्धन चाहे पुण्य का हो या पाप का वह बन्धन ही है और इसलिए अध्यात्मसाधना का विरोधी है। पुण्य को भी बन्धन का हेतु मानकर इन विचारकों ने अहिंसा के सकारात्मक पक्ष की उपेक्षा की। आचार्य कुन्द-कुन्द ने पुण्य और पाप का अन्तर स्पष्ट करते हुए पुण्य को सोने की और पाप को लोहे की बेड़ी कहा और अन्त में पुण्य और पाप दोनों से उपर उठने की बात कही है (समयसार 146 ) । यह सत्य है कि पुण्य और पाप की अधिकांश परिभाषाएँ इस अवधारणा पर खड़ी है कि जो दया और जीवन-रक्षण के जो कार्य है, वे पुण्य हैं और जो दूसरों के अहित और दुःख के कार्य है, वे पाप है। सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि "परोपकारं पुण्याय पापाय परपीड़नं।" गोस्वामी तुलसीदास ने भी Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18