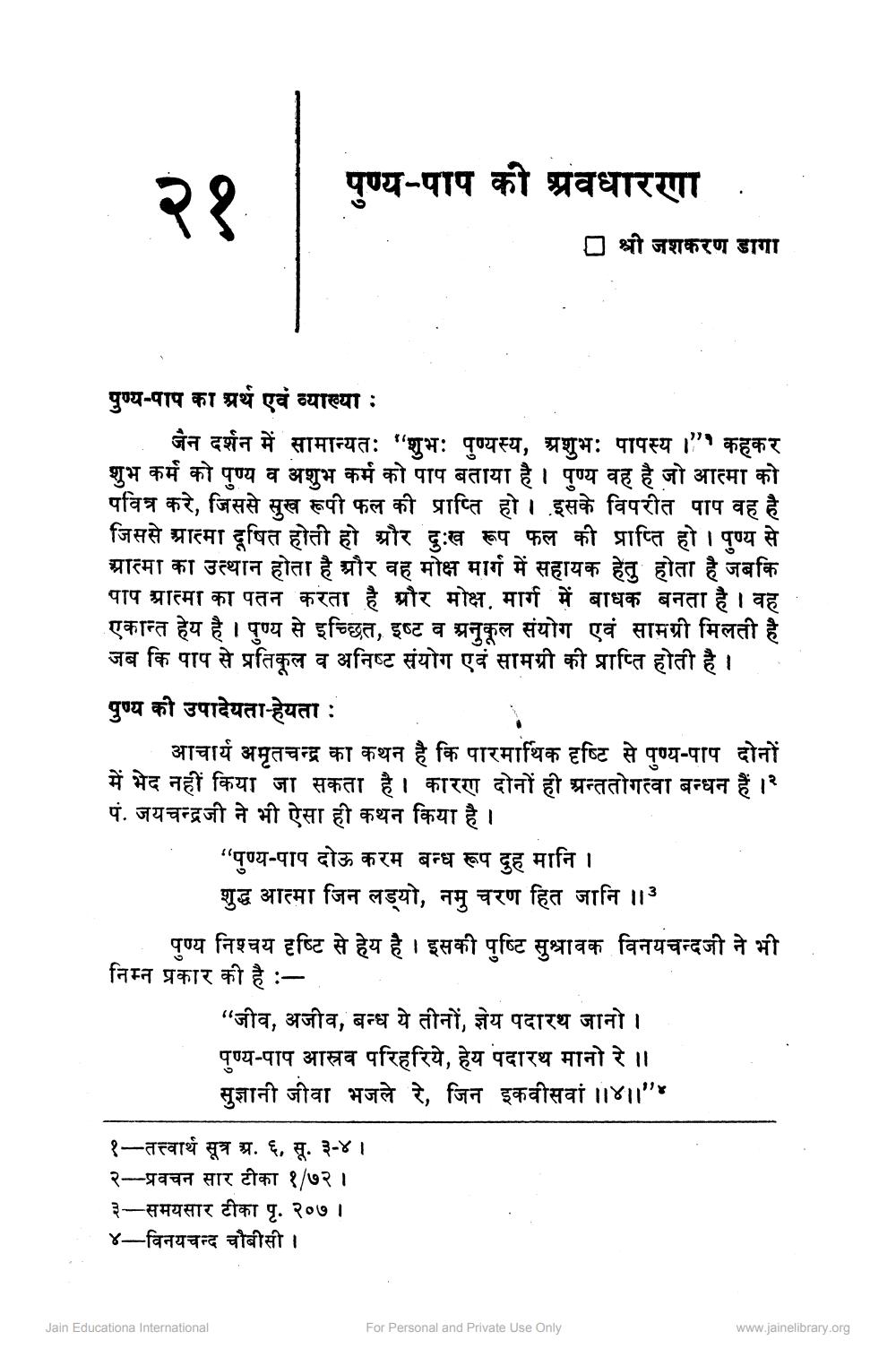Book Title: Punya Paap ki Avdharna Author(s): Jashkaran Daga Publisher: Z_Jinvani_Karmsiddhant_Visheshank_003842.pdf View full book textPage 1
________________ २१ पुण्य-पाप की अवधारणा . 0 श्री जशकरण डागा पुण्य-पाप का अर्थ एवं व्याख्या : . जैन दर्शन में सामान्यतः "शुभः पुण्यस्य, अशुभः पापस्य ।" कहकर शुभ कर्म को पुण्य व अशुभ कर्म को पाप बताया है। पुण्य वह है जो आत्मा को पवित्र करे, जिससे सुख रूपी फल की प्राप्ति हो। इसके विपरीत पाप वह है जिससे आत्मा दूषित होती हो और दुःख रूप फल की प्राप्ति हो । पुण्य से आत्मा का उत्थान होता है और वह मोक्ष मार्ग में सहायक हेतु होता है जबकि पाप आत्मा का पतन करता है और मोक्ष. मार्ग में बाधक बनता है । वह एकान्त हेय है । पुण्य से इच्छित, इष्ट व अनुकूल संयोग एवं सामग्री मिलती है जब कि पाप से प्रतिकूल व अनिष्ट संयोग एवं सामग्री की प्राप्ति होती है। पुण्य की उपादेयता हेयता: आचार्य अमृतचन्द्र का कथन है कि पारमार्थिक दृष्टि से पुण्य-पाप दोनों में भेद नहीं किया जा सकता है। कारण दोनों ही अन्ततोगत्वा बन्धन हैं । पं. जयचन्द्रजी ने भी ऐसा ही कथन किया है । "पुण्य-पाप दोऊ करम बन्ध रूप दुह मानि । शुद्ध आत्मा जिन लड्यो, नमु चरण हित जानि ॥3 पुण्य निश्चय दृष्टि से हेय है । इसकी पुष्टि सुश्रावक विनयचन्दजी ने भी . निम्न प्रकार की है : "जीव, अजीव, बन्ध ये तीनों, ज्ञेय पदारथ जानो। पुण्य-पाप आस्रव परिहरिये, हेय पदारथ मानो रे ॥ सुज्ञानी जीवा भजले रे, जिन इकवीसवां ॥४॥"" १-तत्त्वार्थ सूत्र अ. ६, सू. ३-४ । २-प्रवचन सार टीका १/७२ । ३-समयसार टीका पृ. २०७ । ४-विनयचन्द चौबीसी। Jain Educationa International For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11