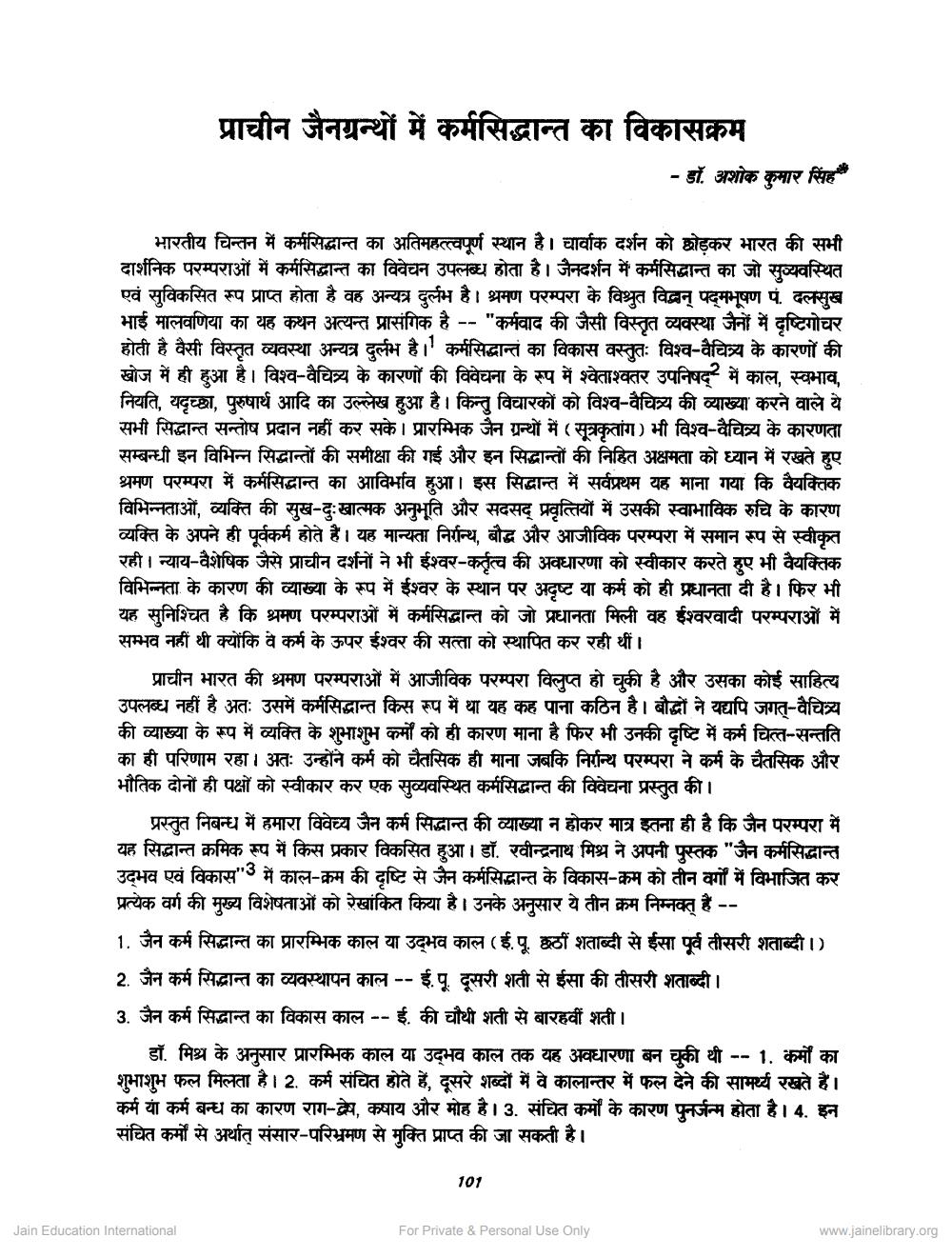Book Title: Prachin Jain Grantho me Karmsiddhant ka Vikaskram Author(s): Ashok Kumar Singh Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 1
________________ प्राचीन जैनग्रन्थों में कर्मसिद्धान्त का विकासक्रम - डॉ. अशोक कुमार सिंह भारतीय चिन्तन में कर्मसिद्धान्त का अतिमहत्त्वपूर्ण स्थान है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर भारत की सभी दार्शनिक परम्पराओं में कर्मसिद्धान्त का विवेचन उपलब्ध होता है। जैनदर्शन में कर्मसिद्धान्त का जो सुव्यवस्थित एवं सुविकसित रूप प्राप्त होता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। श्रमण परम्परा के विश्रुत विद्वान् पद्मभूषण पं. दलसुख भाई मालवणिया का यह कथन अत्यन्त प्रासंगिक है -- "कर्मवाद की जैसी विस्तृत व्यवस्था जैनों में दृष्टिगोचर होती है वैसी विस्तृत व्यवस्था अन्यत्र दुर्लभ है। कर्मसिद्धान्त का विकास वस्तुतः विश्व-वैचित्र्य के कारणों की खोज में ही हुआ है। विश्व-वैचित्र्य के कारणों की विवेचना के रूप में श्वेताश्वतर उपनिषद में काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, पुरुषार्थ आदि का उल्लेख हुआ है। किन्तु विचारकों को विश्व-वैचित्र्य की व्याख्या करने वाले ये सभी सिद्धान्त सन्तोष प्रदान नहीं कर सके। प्रारम्भिक जैन ग्रन्थों में (सूत्रकृतांग) भी विश्व-वैचित्र्य के कारणता सम्बन्धी इन विभिन्न सिद्धान्तों की समीक्षा की गई और इन सिद्धान्तों की निहित अक्षमता को ध्यान में रखते हुए श्रमण परम्परा में कर्मसिद्धान्त का आविर्भाव हुआ। इस सिद्धान्त में सर्वप्रथम यह माना गया कि वैयक्तिक विभिन्नताओं, व्यक्ति की सुख-दुःखात्मक अनुभति और सदसद प्रवत्तियों में उसकी स्वाभाविक रुचि के कारण व्यक्ति के अपने ही पूर्वकर्म होते है। यह मान्यता निर्गन्थ, बौद्ध और आजीविक परम्परा में समान रूप से स्वीकृत रही। न्याय-वैशेषिक जैसे प्राचीन दर्शनों ने भी ईश्वर-कर्तत्व की अवधारणा को स्वीकार करते हुए भी वैयक्तिक विभिन्नता के कारण की व्याख्या के रूप में ईश्वर के स्थान पर अदृष्ट या कर्म को ही प्रधानता दी है। फिर भी यह सुनिश्चित है कि श्रमण परम्पराओं में कर्मसिद्धान्त को जो प्रधानता मिली वह ईश्वरवादी परम्पराओं में सम्भव नहीं थी क्योंकि वे कर्म के ऊपर ईश्वर की सत्ता को स्थापित कर रही थीं।। प्राचीन भारत की श्रमण परम्पराओं में आजीविक परम्परा विलुप्त हो चुकी है और उसका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है अतः उसमें कर्मसिद्धान्त किस रूप में था यह कह पाना कठिन है। बौद्धों ने यद्यपि जगत-वैचित्र्य की व्याख्या के रूप में व्यक्ति के शुभाशुभ कर्मों को ही कारण माना है फिर भी उनकी दृष्टि में कर्म चित्त-सन्तति का ही परिणाम रहा। अतः उन्होंने कर्म को चैतसिक ही माना जबकि निर्गन्थ परम्परा ने कर्म के चैतसिक और भौतिक दोनों ही पक्षों को स्वीकार कर एक सुव्यवस्थित कर्मसिद्धान्त की विवेचना प्रस्तुत की। प्रस्तुत निबन्ध में हमारा विवेच्य जैन कर्म सिद्धान्त की व्याख्या न होकर मात्र इतना ही है कि जैन परम्परा में यह सिद्धान्त क्रमिक रूप में किस प्रकार विकसित हुआ। डॉ. रवीन्द्रनाथ मिश्र ने अपनी पुस्तक "जैन कर्मसिद्धान्त उद्भव एवं विकास"3 में काल-क्रम की दृष्टि से जैन कर्मसिद्धान्त के विकास-क्रम को तीन वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया है। उनके अनुसार ये तीन क्रम निम्नवत् है -- 1. जैन कर्म सिद्धान्त का प्रारम्भिक काल या उद्भव काल (ई.पू. छठी शताब्दी से ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी।) 2. जैन कर्म सिद्धान्त का व्यवस्थापन काल -- ई.पू. दूसरी शती से ईसा की तीसरी शताब्दी। 3. जैन कर्म सिद्धान्त का विकास काल -- ई. की चौथी शती से बारहवीं शती। डॉ. मिश्र के अनुसार प्रारम्भिक काल या उद्भव काल तक यह अवधारणा बन चुकी थी -- 1. कर्मों का शुभाशुभ फल मिलता है। 2. कर्म संचित होते हैं, दूसरे शब्दों में वे कालान्तर में फल देने की सामर्थ्य रखते हैं। कर्म या कर्म बन्ध का कारण राग-द्वेष, कषाय और मोह है। 3. संचित कर्मों के कारण पुनर्जन्म होता है। 4. इन संचित कर्मों से अर्थात संसार-परिभ्रमण से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 101 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13