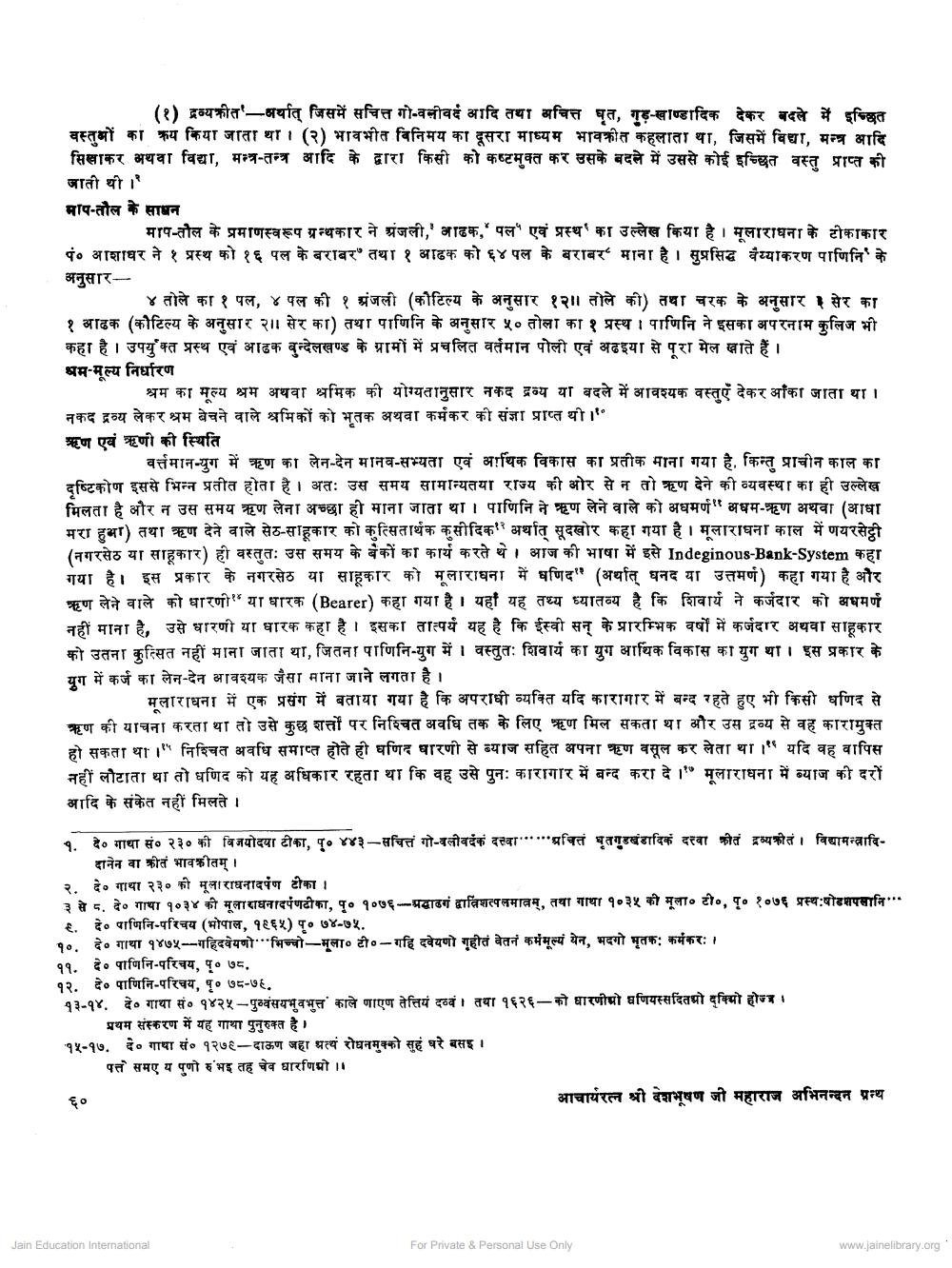Book Title: Mularadhna Aetihasik Sanskrutik evam Sahityik Mulyankan Author(s): Rajaram Jain Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 4
________________ (१) द्रव्यकीत अर्थात् जिसमें सचित्त गो-वनीय आदि तथा बचत त गुड़-खाण्डादिक देकर बदले में वस्तुओं का क्रय किया जाता था । (२) भावभीत विनिमय का दूसरा माध्यम भावक्रीत कहलाता था, जिसमें विद्या, मन्त्र आदि सिखाकर अथवा विद्या, मन्त्र-तन्त्र आदि के द्वारा किसी को कष्टमुक्त कर उसके बदले में उससे कोई इच्छित वस्तु प्राप्त की जाती थी।" माप-तौल के साधन माप-तौल के प्रमाणस्वरूप ग्रन्थकार ने अंजली, ' आढक, पल' एवं प्रस्थ का उल्लेख किया है। मूलाराधना के टीकाकार पं० आशाधर ने १ प्रस्थ को १६ पल के बराबर तथा १ आढक को ६४ पल के बराबर' माना है । सुप्रसिद्ध वैय्याकरण पाणिनि' के अनुसार ४ तोले का १ पल, ४ पल की १ अंजली (कौटिल्य के अनुसार १२|| तोले की ) तथा चरक के अनुसार ३ सेर का १ आढक (कौटिल्य के अनुसार २|| सेर का ) तथा पाणिनि के अनुसार ५० तोला का १ प्रस्थ । पाणिनि ने इसका अपरनाम कुलिज भी कहा है । उपर्युक्त प्रस्थ एवं आढक बुन्देलखण्ड के ग्रामों में प्रचलित वर्तमान पोली एवं अढइया से पूरा मेल खाते हैं । श्रम-मूल्य निर्धारण श्रम का मूल्य श्रम अथवा श्रमिक की योग्यतानुसार नकद द्रव्य या बदले में आवश्यक वस्तुएँ देकर आँका जाता था । नकद द्रव्य लेकर श्रम बेचने वाले श्रमिकों को भूतक अथवा कर्मकर की संज्ञा प्राप्त थी । " ऋण एवं ऋणी की स्थिति वर्त्तमान युग में ऋण का लेन-देन मानव सभ्यता एवं आर्थिक विकास का प्रतीक माना गया है, किन्तु प्राचीन काल का दृष्टिकोण इससे भिन्न प्रतीत होता है । अतः उस समय सामान्यतया राज्य की ओर से न तो ऋण देने की व्यवस्था का ही उल्लेख मिलता है और न उस समय ऋण लेना अच्छा ही माना जाता था । पाणिनि ने ऋण लेने वाले को अधमर्ण" अधम ऋण अथवा ( आधा मरा हुआ) तथा ऋण देने वाले सेठ साहूकार को कुत्सितार्थक कुसीदिक" अर्थात् सूदखोर कहा गया है । मूलाराधना काल में जयरसेट्ठी (नगरसेठ या साहूकार) ही वस्तुतः उस समय के बैंकों का कार्य करते थे। आज की भाषा में इसे Indeginous Bank-System कहा गया है। इस प्रकार के नगरसेठ या साहूकार को मूलाराधना में पणिद" ( अर्थात् पनद या उत्तमर्ण) कहा गया है और ऋण लेने वाले को धारणी" या धारक (Bearer ) कहा गया है । यहाँ यह तथ्य ध्यातव्य है कि शिवार्य ने कर्जदार को अधमर्ण नहीं माना है, उसे धारणी या धारक कहा है । इसका तात्पर्य यह है कि ईस्वी सन् के प्रारम्भिक वर्षों में कर्जदार अथवा साहूकार को उतना कुत्सित नहीं माना जाता था, जितना पाणिनि-युग में । वस्तुतः शिवार्य का युग आर्थिक विकास का युग था । इस प्रकार के युग में कर्ज का लेन-देन आवश्यक जैसा माना जाने लगता है । मूलाराधना में एक प्रसंग में बताया गया है कि अपराधी व्यक्ति यदि कारागार में बन्द रहते हुए भी किसी घणिद से ऋण की याचना करता था तो उसे कुछ शर्तों पर निश्चित अवधि तक के लिए ऋण मिल सकता था और उस द्रव्य से वह कारामुक्त हो सकता था । " निश्चित अवधि समाप्त होते ही घणिद धारणी से ब्याज सहित अपना ऋण वसूल कर लेता था।" यदि वह वापिस नहीं लौटाता था तो घणिद को यह अधिकार रहता था कि वह उसे पुनः कारागार में बन्द करा दे ।" मूलाराधना में ब्याज की दरों आदि के संकेत नहीं मिलते। १. दे० गाथा सं० २३० की विजयोदया टीका, पु० ४४३ – सचित्तं गो-वलीवर्दकं दत्वा प्रचितं घृतगुडखंडादिकं दत्वा क्रीतं द्रव्यक्रीतं । विद्यामन्त्रादिदानेन वा क्रीतं भावकीतम् । २. दे० गाथा २३० की मूलाराधनादर्पण टीका । · ३ से ८. दे० गाथा १०३४ की मूलाराधनादर्पणटीका, पृ० १०७६ - अद्धाढगं द्वात्रिंशत्यलमात्रम्, तथा गाथा १०३५ की मूला० टी० पू० १०७६ प्रस्थः षोडशपलानि ... ९. दे० पाणिनि-परिचय (भोपाल, १९६५) पृ० ७४-७५. १०. दे० गाथा १४७५ -- गहिदवेयणो भिच्चो मूला० टी० - गहि दवेयणो गृहीतं वेतनं कर्ममूल्यं येन, भदगो मृतकः कर्मकरः । ११. दे० पाणिनि-परिचय, पू० ७८. १२. दे० पाणिनि-परिचय, पृ० ७८ ७६. १३-१४. दे० गाथा सं० १४२५ – पुग्वंसयभुवभुत्त काले गाएण तेत्तियं दव्वं । तथा १६२६ - को धारणीम्रो धणियस्सदितो द्विमो हो । प्रथम संस्करण में १५-१७. दे० गाथा सं० पत्त समए य पुणो ६० - Jain Education International यह गाथा पुनरुक्त है। १२७६ - दाऊण जहा धत्यं रोधनमुक्को सुहं घरे बस । भइ तह चैव धारणिम्रो ।। आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16