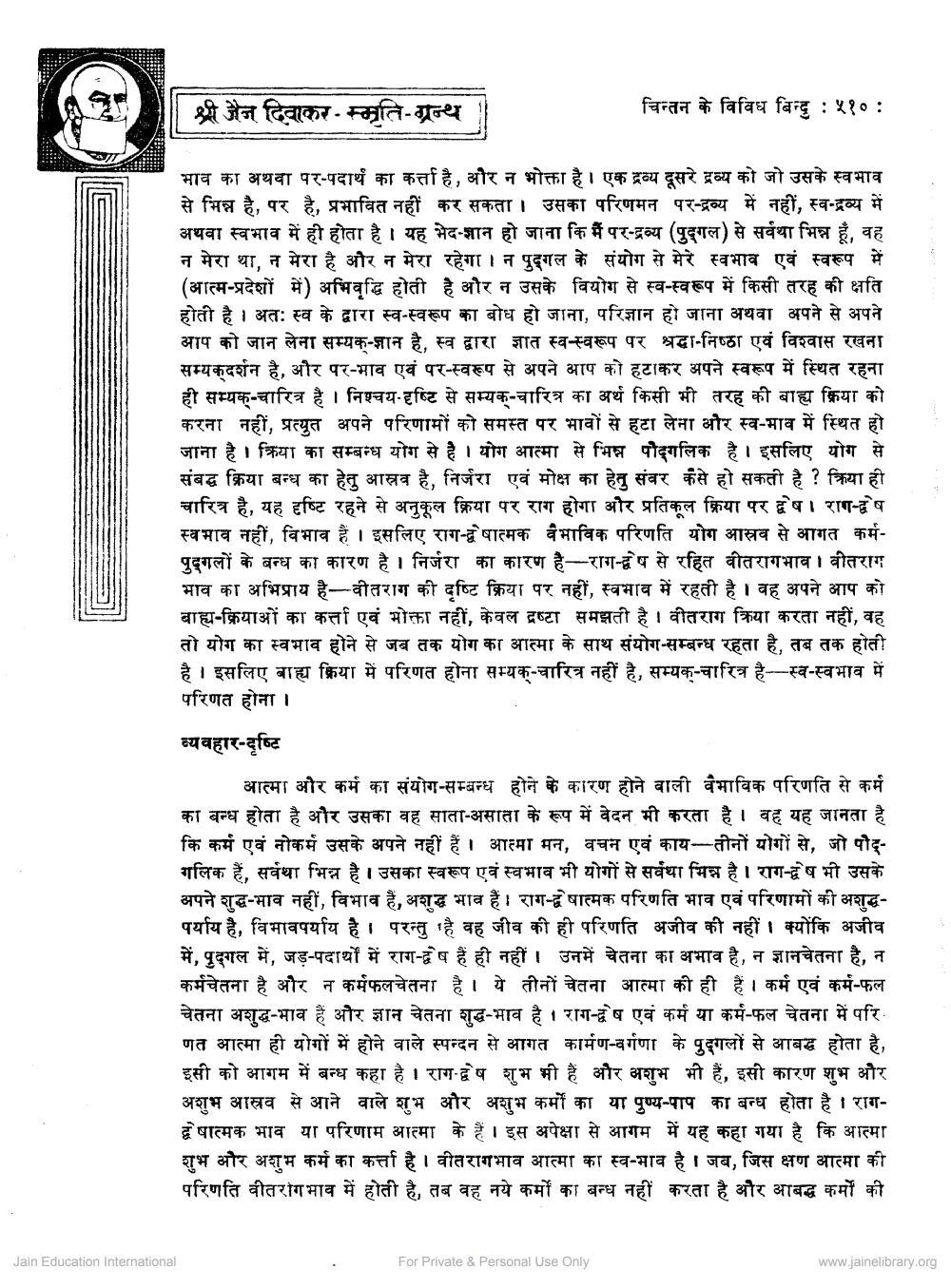Book Title: Karm Bandhan evam Mukti ki Prakriya Author(s): Samdarshimuni Publisher: Z_Jain_Divakar_Smruti_Granth_012021.pdf View full book textPage 4
________________ श्री जैन दिवाकर स्मृति-ग्रन्थ ।। चिन्तन के विविध बिन्दु : ५१० : भाव का अथवा पर-पदार्थ का कर्ता है, और न भोक्ता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जो उसके स्वभाव से भिन्न है, पर है, प्रभावित नहीं कर सकता। उसका परिणमन पर-द्रव्य में नहीं, स्व-द्रव्य में अथवा स्वभाव में ही होता है। यह भेद-शान हो जाना कि मैं पर-द्रव्य (पुद्गल) से सर्वथा भिन्न हूँ, वह न मेरा था, न मेरा है और न मेरा रहेगा। न पुद्गल के संयोग से मेरे स्वभाव एवं स्वरूप में (आत्म-प्रदेशों में) अभिवृद्धि होती है और न उसके वियोग से स्व-स्वरूप में किसी तरह की क्षति होती है। अत: स्व के द्वारा स्व-स्वरूप का बोध हो जाना, परिज्ञान हो जाना अथवा अपने से अपने आप को जान लेना सम्यक्-ज्ञान है, स्व द्वारा ज्ञात स्व-स्वरूप पर श्रद्धा-निष्ठा एवं विश्वास रखना सम्यकदर्शन है, और पर-भाव एवं पर-स्वरूप से अपने आप को हटाकर अपने स्वरूप में स्थित रहना ही सम्यक्-चारित्र है । निश्चय-दृष्टि से सम्यक-चारित्र का अर्थ किसी भी तरह की बाह्य क्रिया को करना नहीं, प्रत्युत अपने परिणामों को समस्त पर भावों से हटा लेना और स्व-भाव में स्थित हो जाना है। क्रिया का सम्बन्ध योग से है । योग आत्मा से भिन्न पौद्गलिक है। इसलिए योग से संबद्ध क्रिया बन्ध का हेतु आस्रव है, निर्जरा एवं मोक्ष का हेतु संवर कैसे हो सकती है ? क्रिया ही चारित्र है, यह दृष्टि रहने से अनुकूल क्रिया पर राग होगा और प्रतिकूल क्रिया पर द्वेष । राग-द्वेष स्वभाव नहीं, विभाव हैं। इसलिए राग-द्वेषात्मक वैभाविक परिणति योग आस्रव से आगत कर्मपुद्गलों के बन्ध का कारण है। निर्जरा का कारण है-राग-द्वेष से रहित वीतरागभाव । वीतराम भाव का अभिप्राय है-वीतराग की दृष्टि क्रिया पर नहीं, स्वभाव में रहती है। वह अपने आप को बाह्य-क्रियाओं का कर्ता एवं भोक्ता नहीं, केवल द्रष्टा समझती है । वीतराग क्रिया करता नहीं, वह तो योग का स्वभाव होने से जब तक योग का आत्मा के साथ संयोग-सम्बन्ध रहता है, तब तक होती है। इसलिए बाह्य क्रिया में परिणत होना सम्यक-चारित्र नहीं है, सम्यक-चारित्र है-स्व-स्वभाव में परिणत होना। व्यवहार-दृष्टि आत्मा और कर्म का संयोग-सम्बन्ध होने के कारण होने वाली वैभाविक परिणति से कर्म का बन्ध होता है और उसका वह साता-असाता के रूप में वेदन भी करता है। वह यह जानता है कि कर्म एवं नोकर्म उसके अपने नहीं हैं। आत्मा मन, वचन एवं काय-तीनों योगों से, जो पौद्गलिक हैं, सर्वथा भिन्न है। उसका स्वरूप एवं स्वभाव भी योगों से सर्वथा भिन्न है। राग-द्वेष भी उसके अपने शुद्ध-भाव नहीं, विभाव हैं, अशुद्ध भाव हैं। राग-द्वेषात्मक परिणति भाव एवं परिणामों की अशुद्धपर्याय है, विभावपर्याय है। परन्तु है वह जीव की ही परिणति अजीव की नहीं। क्योंकि अजीव में, पुद्गल में, जड़-पदार्थों में राग-द्वेष हैं ही नहीं। उनमें चेतना का अभाव है, न ज्ञानचेतना है, न कर्मचेतना है और न कर्मफलचेतना है। ये तीनों चेतना आत्मा की ही हैं। कर्म एवं कर्म-फल चेतना अशुद्ध-भाव हैं और ज्ञान चेतना शुद्ध-भाव है। राग-द्वेष एवं कर्म या कर्म-फल चेतना में परि णत आत्मा ही योगों में होने वाले स्पन्दन से आगत कार्मण-वर्गणा के पुद्गलों से आबद्ध होता है, इसी को आगम में बन्ध कहा है। राग-द्वेष शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं, इसी कारण शुभ और अशुभ आस्रव से आने वाले शुभ और अशुभ कर्मों का या पुण्य-पाप का बन्ध होता है। रागद्वेषात्मक भाव या परिणाम आत्मा के हैं। इस अपेक्षा से आगम में यह कहा गया है कि आत्मा शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता है। वीतरागभाव आत्मा का स्व-भाव है । जब, जिस क्षण आत्मा की परिणति वीतरोगभाव में होती है, तब वह नये कर्मों का बन्ध नहीं करता है और आबद्ध कर्मों की Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12