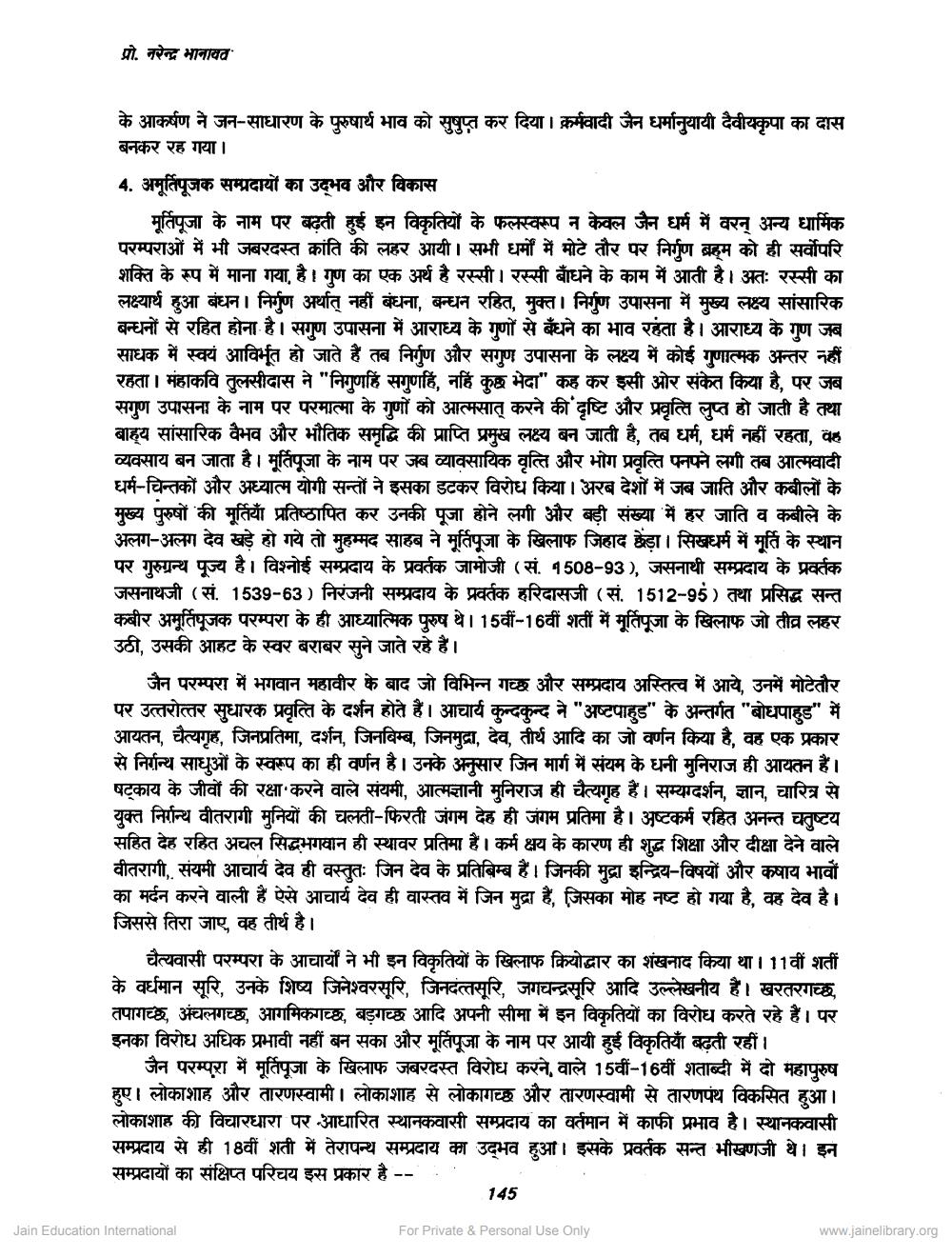Book Title: Jain Dharm me Amurtipujak Sampradayo ka Udbhav evam Itihas Author(s): Narendra Bhanavat Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 5
________________ प्रो. नरेन्द्र भानावत के आकर्षण ने जन-साधारण के पुरुषार्थ भाव को सुषुप्त कर दिया । क्रर्मवादी जैन धर्मानुयायी दैवीयकृपा का दास बनकर रह गया। 4. अमूर्तिपूजक सम्प्रदायों का उद्भव और विकास पर जब मूर्तिपूजा के नाम पर बढ़ती हुई इन विकृतियों के फलस्वरूप न केवल जैन धर्म में वरन् अन्य धार्मिक परम्पराओं में भी जबरदस्त क्रांति की लहर आयी । सभी धर्मों में मोटे तौर पर निर्गुण ब्रह्म को ही सर्वोपरि शक्ति के रूप में माना गया है। गुण का एक अर्थ है रस्सी । रस्सी बाँधने के काम में आती है। अतः रस्सी का लक्ष्यार्थ हुआ बंधन | निर्गुण अर्थात् नहीं बंधना, बन्धन रहित, मुक्त। निर्गुण उपासना में मुख्य लक्ष्य सांसारिक बन्धनों से रहित होना है। सगुण उपासना में आराध्य के गुणों से बँधने का भाव रहता है। आराध्य के गुण जब साधक में स्वयं आविर्भूत हो जाते हैं तब निर्गुण और सगुण उपासना के लक्ष्य में कोई गुणात्मक अन्तर नहीं रहता । महाकवि तुलसीदास ने "निगुणहिं सगुणहिं नहिं कुछ भेदा" कह कर इसी ओर संकेत किया सगुण उपासना के नाम पर परमात्मा के गुणों को आत्मसात् करने की दृष्टि और प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है तथा बाह्य सांसारिक वैभव और भौतिक समृद्धि की प्राप्ति प्रमुख लक्ष्य बन जाती है, तब धर्म, धर्म नहीं रहता, वह व्यवसाय बन जाता है। मूर्तिपूजा के नाम पर जब व्यावसायिक वृत्ति और भोग प्रवृत्ति पनपने लगी तब आत्मवादी धर्म-चिन्तकों और अध्यात्म योगी सन्तों ने इसका डटकर विरोध किया। अरब देशों में जब जाति और कबीलों के मुख्य पुरुषों की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित कर उनकी पूजा होने लगी और बड़ी संख्या में हर जाति व कबीले के अलग-अलग देव खड़े हो गये तो मुहम्मद साहब ने मूर्तिपूजा के खिलाफ जिहाद छेड़ा। सिखधर्म में मूर्ति के स्थान पर गुरुग्रन्थ पूज्य है । विश्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक जामोजी (सं. 1508-93), जसनाथी सम्प्रदाय के प्रवर्तक जसनाथजी (सं. 1539-63) निरंजनी सम्प्रदाय के प्रवर्तक हरिदासजी (सं. 1512-95 ) तथा प्रसिद्ध सन्त कबीर अमूर्तिपूजक परम्परा के ही आध्यात्मिक पुरुष थे। 15वीं - 16वीं शतीं में मूर्तिपूजा के खिलाफ जो तीव्र लहर उठी, उसकी आहट के स्वर बराबर सुने जाते रहे हैं। जैन परम्परा में भगवान महावीर के बाद जो विभिन्न गच्छ और सम्प्रदाय अस्तित्व में आये, उनमें मोटेतौर पर उत्तरोत्तर सुधारक प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने " अष्टपाहुड" के अन्तर्गत "बोधपाहुड" में आयतन, चैत्यगृह, जिनप्रतिमा, दर्शन, जिनबिम्ब, जिनमुद्रा, देव, तीर्थ आदि का जो वर्णन किया है, वह एक प्रकार से निर्ग्रन्थ साधुओं के स्वरूप का ही वर्णन है। उनके अनुसार जिन मार्ग में संयम के धनी मुनिराज ही आयतन हैं। षट्काय के जीवों की रक्षा करने वाले संयमी, आत्मज्ञानी मुनिराज ही चैत्यगृह हैं। सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र से युक्त निर्मन्थ वीतरागी मुनियों की चलती-फिरती जंगम देह ही जंगम प्रतिमा है। अष्टकर्म रहित अनन्त चतुष्टय सहित देह रहित अचल सिद्धभगवान ही स्थावर प्रतिमा हैं। कर्म क्षय के कारण ही शुद्ध शिक्षा और दीक्षा देने वाले वीतरागी, संयमी आचार्य देव ही वस्तुतः जिन देव के प्रतिबिम्ब हैं। जिनकी मुद्रा इन्द्रिय-विषयों और कषाय भावों का मर्दन करने वाली हैं ऐसे आचार्य देव ही वास्तव में जिन मुद्रा हैं, जिसका मोह नष्ट हो गया है, वह देव है । जिससे तिरा जाए, वह तीर्थ है। चैत्यवासी परम्परा के आचार्यों ने भी इन विकृतियों के खिलाफ क्रियोद्धार का शंखनाद किया था । 11वीं शतीं के वर्धमान सूरि, उनके शिष्य जिनेश्वरसूरि, जिनदत्तसूरि, जगचन्द्रसूरि आदि उल्लेखनीय है । खरतरगच्छ, तपागच्छ, अंचलगच्छ, आगमिकगच्छ, बड़गच्छ आदि अपनी सीमा में इन विकृतियों का विरोध करते रहे हैं। पर इनका विरोध अधिक प्रभावी नहीं बन सका और मूर्तिपूजा के नाम पर आयी हुई विकृतियाँ बढ़ती रहीं । जैन परम्परा में मूर्तिपूजा के खिलाफ जबरदस्त विरोध करने वाले 15वीं - 16वीं शताब्दी में दो महापुरुष हुए। लोकाशाह और तारणस्वामी। लोकाशाह से लोकागच्छ और तारणस्वामी से तारणपंथ विकसित हुआ । लोकाशाह की विचारधारा पर आधारित स्थानकवासी सम्प्रदाय का वर्तमान में काफी प्रभाव है। स्थानकवासी सम्प्रदाय से ही 18वीं शती में तेरापन्थ सम्प्रदाय का उद्भव हुआ। इसके प्रवर्तक सन्त भीखणजी थे। इन सम्प्रदायों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है -- Jain Education International 145 For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10