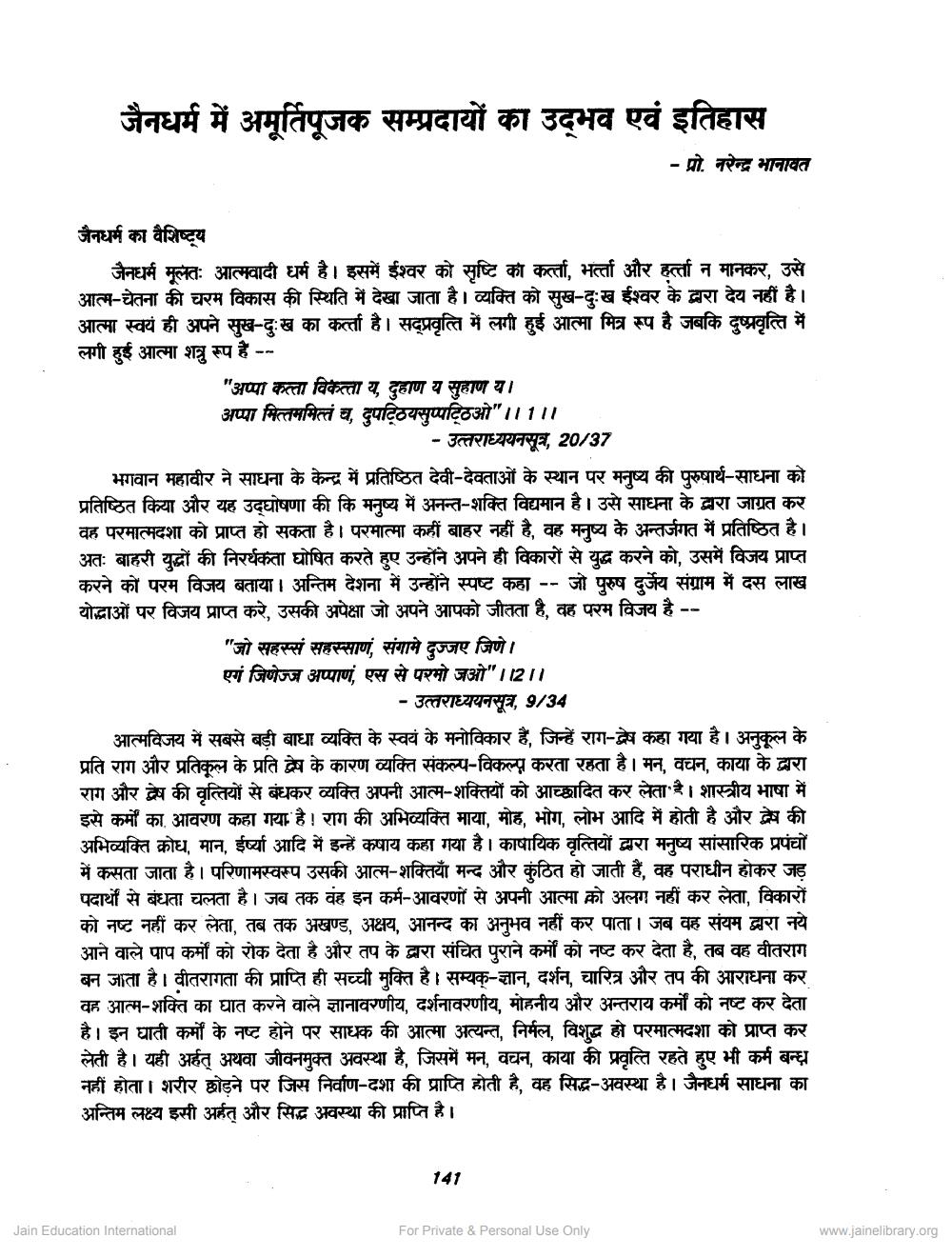Book Title: Jain Dharm me Amurtipujak Sampradayo ka Udbhav evam Itihas Author(s): Narendra Bhanavat Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 1
________________ जैनधर्म में अमूर्तिपूजक सम्प्रदायों का उद्भव एवं इतिहास -प्रो. नरेन्द्र भानावत जैनधर्म का वैशिष्ट्य जैनधर्म मूलतः आत्मवादी धर्म है। इसमें ईश्वर को सृष्टि का कर्ता, भर्ता और हर्ता न मानकर, उसे आत्म-चेतना की चरम विकास की स्थिति में देखा जाता है। व्यक्ति को सुख-दुःख ईश्वर के द्वारा देय नहीं है। आत्मा स्वयं ही अपने सुख-दुःख का कर्ता है। सद्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा मित्र रूप है जबकि दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा शत्रु रूप है --- "अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य। अप्पा मित्तममित्तं च, दुपट्ठियसुप्पट्ठिओ" ।।1।। - उत्तराध्ययनसूत्र, 20/37 भगवान महावीर ने साधना के केन्द्र में प्रतिष्ठित देवी-देवताओं के स्थान पर मनुष्य की पुरुषार्थ-साधना को प्रतिष्ठित किया और यह उद्घोषणा की कि मनुष्य में अनन्त-शक्ति विद्यमान है। उसे साधना के बरा जाग्रत कर वह परमात्मदशा को प्राप्त हो सकता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह मनुष्य के अन्तर्जगत में प्रतिष्ठित है। अतः बाहरी युद्धों की निरर्थकता घोषित करते हुए उन्होंने अपने ही विकारों से युद्ध करने को, उसमें विजय प्राप्त करने को परम विजय बताया। अन्तिम देशना में उन्होंने स्पष्ट कहा -- जो पुरुष दुर्जेय संग्राम में दस लाख योद्धाओं पर विजय प्राप्त करे, उसकी अपेक्षा जो अपने आपको जीतता है. वह परम विजय है-- "जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे। एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ"11211 - उत्तराध्ययनसूत्र, 9/34 आत्मविजय में सबसे बड़ी बाधा व्यक्ति के स्वयं के मनोविकार है, जिन्हें राग-द्वेष कहा गया है। अनुकूल के प्रति राग और प्रतिकूल के प्रति देष के कारण व्यक्ति संकल्प-विकल्प करता रहता है। मन, वचन, काया के द्वारा राग और देष की वृत्तियों से बंधकर व्यक्ति अपनी आत्म-शक्तियों को आच्छादित कर लेता है। शास्त्रीय भाषा में इसे कर्मों का आवरण कहा गया है। राग की अभिव्यक्ति माया, मोह, भोग, लोभ आदि में होती है और द्वेष की अभिव्यक्ति क्रोध, मान, ईर्ष्या आदि में इन्हें कषाय कहा गया है। काषायिक वृत्तियों द्वारा मनुष्य सांसारिक प्रपंचों में कसता जाता है। परिणामस्वरूप उसकी आत्म-शक्तियाँ मन्द और कुंठित हो जाती हैं, वह पराधीन होकर जड़ पदार्थों से बंधता चलता है। जब तक वह इन कर्म-आवरणों से अपनी आत्मा को अलग नहीं कर लेता, विकारों को नष्ट नहीं कर लेता, तब तक अखण्ड, अक्षय, आनन्द का अनुभव नहीं कर पाता। जब वह संयम द्वारा नये आने वाले पाप कर्मों को रोक देता है और तप के द्वारा संचित पुराने कर्मों को नष्ट कर देता है, तब वह वीतराग बन जाता है। वीतरागता की प्राप्ति ही सच्ची मुक्ति है। सम्यक्-ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना कर वह आत्म-शक्ति का घात करने वाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मों को नष्ट कर देता है। इन घाती कर्मों के नष्ट होने पर साधक की आत्मा अत्यन्त, निर्मल, विशुद्ध हो परमात्मदशा को प्राप्त कर लेती है। यही अर्हत् अथवा जीवनमुक्त अवस्था है, जिसमें मन, वचन, काया की प्रवृत्ति रहते हुए भी कर्म बन्न नहीं होता। शरीर छोड़ने पर जिस निर्वाण-दशा की प्राप्ति होती है, वह सिद्ध-अवस्था है। जैनधर्म साधना का अन्तिम लक्ष्य इसी अर्हत् और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है। 141 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10