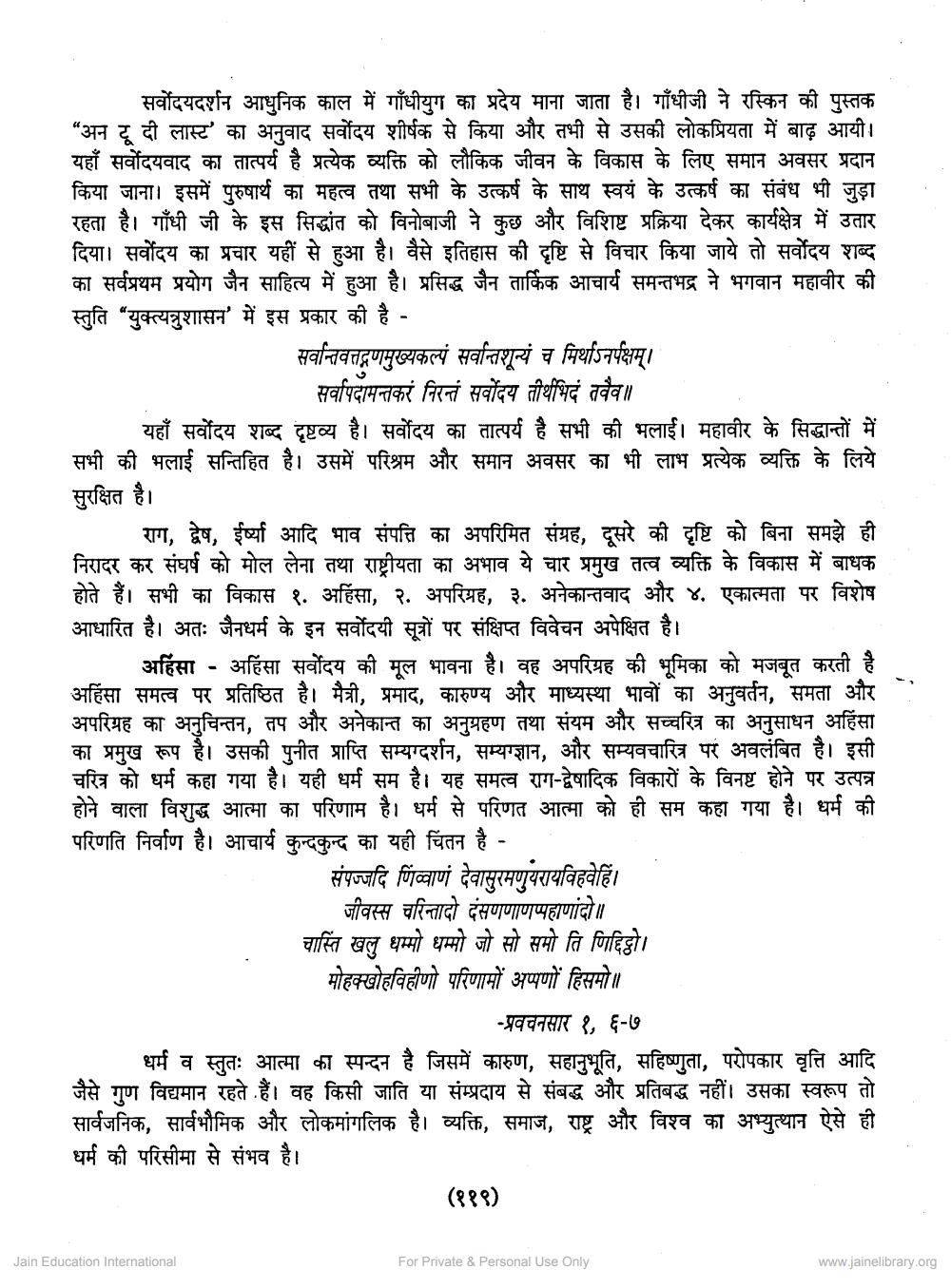Book Title: Jain Dharm Sarvodaya tirth Hai Author(s): Bhagchandra Jain Publisher: Z_Mahasati_Dway_Smruti_Granth_012025.pdf View full book textPage 3
________________ सर्वोदयदर्शन आधुनिक काल में गाँधीयुग का प्रदेय माना जाता है। गाँधीजी ने रस्किन की पुस्तक “अन टू दी लास्ट' का अनुवाद सर्वोदय शीर्षक से किया और तभी से उसकी लोकप्रियता में बाढ़ आयी। यहाँ सर्वोदयवाद का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को लौकिक जीवन के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना। इसमें पुरुषार्थ का महत्व तथा सभी के उत्कर्ष के साथ स्वयं के उत्कर्ष का संबंध भी जुड़ा रहता है। गाँधी जी के इस सिद्धांत को विनोबाजी ने कुछ और विशिष्ट प्रक्रिया देकर कार्यक्षेत्र में उतार दिया। सर्वोदय का प्रचार यहीं से हुआ है। वैसे इतिहास की दृष्टि से विचार किया जाये तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। प्रसिद्ध जैन तार्किक आचार्य समन्तभद्र ने भगवान महावीर की स्तुति “युक्त्यनुशासन' में इस प्रकार की है - सर्वान्तवत्तद्गणमुख्यकल्पं सर्वान्तशून्यं च मिर्थाऽनर्पक्षम्। सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदय तीर्थभिदं तवैव॥ यहाँ सर्वोदय शब्द दृष्टव्य है। सर्वोदय का तात्पर्य है सभी की भलाई। महावीर के सिद्धान्तों में सभी की भलाई सन्तिहित है। उसमें परिश्रम और समान अवसर का भी लाभ प्रत्येक व्यक्ति के लिये सुरक्षित है। राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि भाव संपत्ति का अपरिमित संग्रह, दूसरे की दृष्टि को बिना समझे ही निरादर कर संघर्ष को मोल लेना तथा राष्ट्रीयता का अभाव ये चार प्रमुख तत्व व्यक्ति के विकास में बाधक होते हैं। सभी का विकास १. अहिंसा, २. अपरिग्रह, ३. अनेकान्तवाद और ४. एकात्मता पर विशेष आधारित है। अतः जैनधर्म के इन सर्वोदयी सूत्रों पर संक्षिप्त विवेचन अपेक्षित है। अहिंसा - अहिंसा सर्वोदय की मूल भावना है। वह अपरिग्रह की भूमिका को मजबूत करती है अहिंसा समत्व पर प्रतिष्ठित है। मैत्री, प्रमाद, कारुण्य और माध्यस्था भावों का अनुवर्तन, समता और अपरिग्रह का अनुचिन्तन, तप और अनेकान्त का अनुग्रहण तथा संयम और सच्चरित्र का अनुसाधन अहिंसा का प्रमुख रूप है। उसकी पुनीत प्राप्ति सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यवचारित्र पर अवलंबित है। इसी चरित्र को धर्म कहा गया है। यही धर्म सम है। यह समत्व राग-द्वेषादिक विकारों के विनष्ट होने पर उत्पन्न होने वाला विशुद्ध आत्मा का परिणाम है। धर्म से परिणत आत्मा को ही सम कहा गया है। धर्म की परिणति निर्वाण है। आचार्य कुन्दकुन्द का यही चिंतन है - संपज्जदि णिब्वाणं देवासुरमणुयरायविहवेहि। जीवस्स चरिन्तादो दंसणणाणप्पहाणांदो। चास्ति खलु धम्मो धम्मो जो सो समो ति णिद्दिट्ठो। मोहक्खोहविहीणो परिणामों अप्पणों हिसमो॥ __ -प्रवचनसार १, ६-७ ___ धर्म व स्तुतः आत्मा का स्पन्दन है जिसमें कारुण, सहानुभूति, सहिष्णुता, परोपकार वृत्ति आदि जैसे गुण विद्यमान रहते हैं। वह किसी जाति या संम्प्रदाय से संबद्ध और प्रतिबद्ध नहीं। उसका स्वरूप तो सार्वजनिक, सार्वभौमिक और लोकमांगलिक है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का अभ्युत्थान ऐसे ही धर्म की परिसीमा से संभव है। (११९) Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10