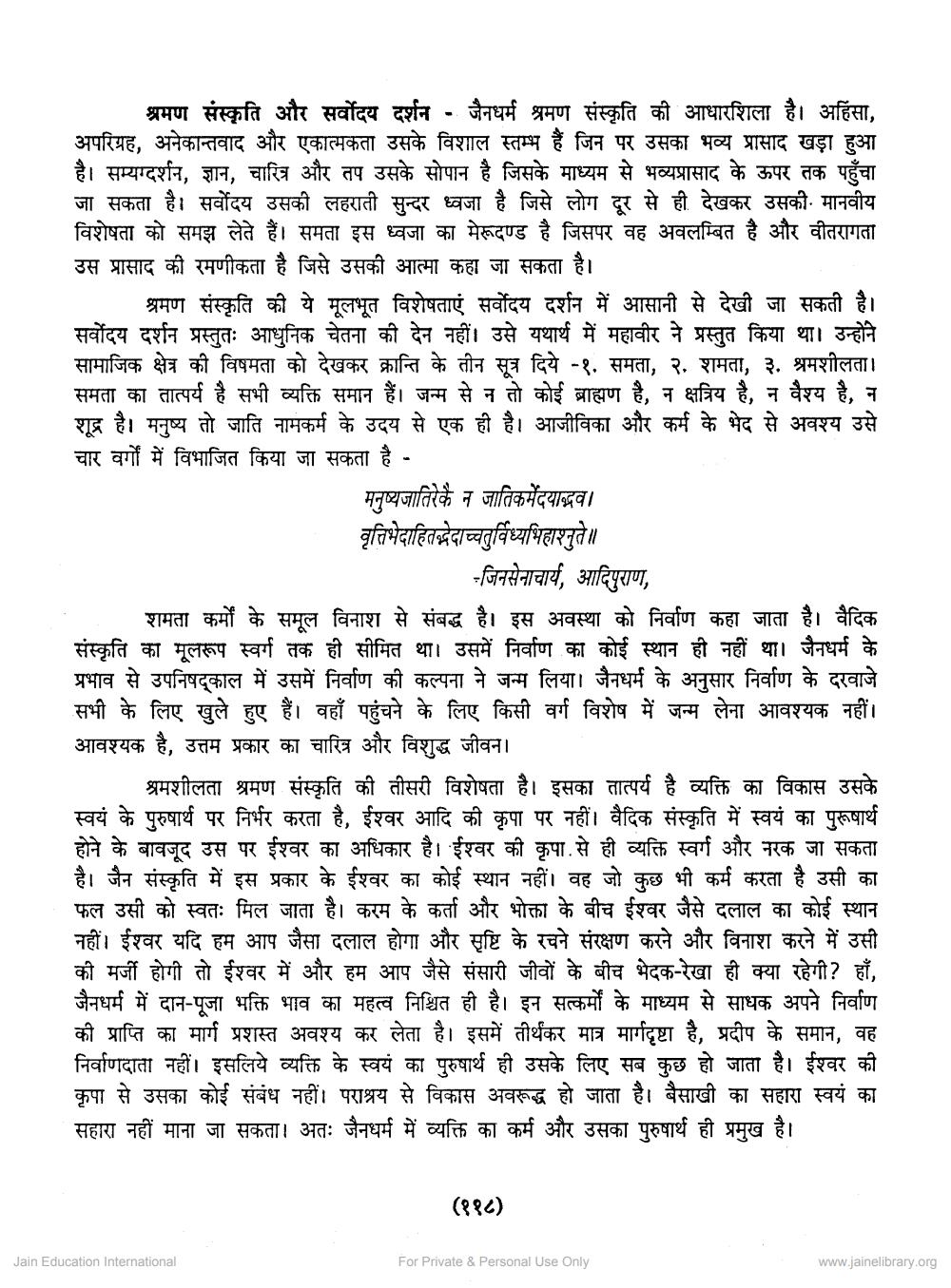Book Title: Jain Dharm Sarvodaya tirth Hai Author(s): Bhagchandra Jain Publisher: Z_Mahasati_Dway_Smruti_Granth_012025.pdf View full book textPage 2
________________ श्रमण संस्कृति और सर्वोदय दर्शन जैनधर्म श्रमण संस्कृति की आधारशिला है। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकान्तवाद और एकात्मकता उसके विशाल स्तम्भ हैं जिन पर उसका भव्य प्रासाद खड़ा हुआ है । सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप उसके सोपान है जिसके माध्यम से भव्यप्रासाद के ऊपर तक पहुँचा जा सकता है । सर्वोदय उसकी लहराती सुन्दर ध्वजा है जिसे लोग दूर से ही देखकर उसकी मानवीय विशेषता को समझ लेते हैं । समता इस ध्वजा का मेरूदण्ड है जिसपर वह अवलम्बित है और वीतरागता उस प्रासाद की रमणीकता है जिसे उसकी आत्मा कहा जा सकता है। श्रमण संस्कृति की ये मूलभूत विशेषताएं सर्वोदय दर्शन में आसानी से देखी जा सकती है। सर्वोदय दर्शन प्रस्तुतः आधुनिक चेतना की देन नहीं । उसे यथार्थ में महावीर ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र की विषमता को देखकर क्रान्ति के तीन सूत्र दिये - १. समता, २. शमता, ३. श्रमशीलता । समता का तात्पर्य है सभी व्यक्ति समान हैं। जन्म से न तो कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। मनुष्य तो जाति नामकर्म के उदय से एक ही है । आजीविका और कर्म के भेद से अवश्य उसे चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है - मनुष्यजातिरेकै न जातिकर्मेंदयाद्भव। वृत्तिभेदाहितद्भेदाच्चतुर्विध्यभिहाश्नुते ॥ -जिनसेनाचार्य, आदिपुराण, शमता कर्मों के समूल विनाश से संबद्ध है। इस अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। वैदिक संस्कृति का मूलरूप स्वर्ग तक ही सीमित था । उसमें निर्वाण का कोई स्थान ही नहीं था । जैनधर्म के प्रभाव से उपनिषद्काल में उसमें निर्वाण की कल्पना ने जन्म लिया। जैनधर्म के अनुसार निर्वाण के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। वहाँ पहुंचने के लिए किसी वर्ग विशेष में जन्म लेना आवश्यक नहीं । आवश्यक है, उत्तम प्रकार का चारित्र और विशुद्ध जीवन । श्रमशीलता श्रमण संस्कृति की तीसरी विशेषता है। इसका तात्पर्य है व्यक्ति का विकास उसके स्वयं के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, ईश्वर आदि की कृपा पर नहीं । वैदिक संस्कृति में स्वयं का पुरूषार्थ होने के बावजूद उस पर ईश्वर का अधिकार है। ईश्वर की कृपा से ही व्यक्ति स्वर्ग और नरक जा सकता है। जैन संस्कृति में इस प्रकार के ईश्वर का कोई स्थान नहीं । वह जो कुछ भी कर्म करता है उसी का बीच ईश्वर जैसे दलाल का कोई स्थान संरक्षण करने और विनाश करने में उसी फल उसी को स्वतः मिल जाता है। करम के कर्ता और भोक्ता के नहीं । ईश्वर यदि हम आप जैसा दलाल होगा और सृष्टि के रचने की मर्जी होगी तो ईश्वर में और हम आप जैसे संसारी जीवों के बीच भेदक- रेखा ही क्या रहेगी? हाँ, जैनधर्म में दान-पूजा भक्ति भाव का महत्व निश्चित ही है। इन सत्कर्मों के माध्यम से साधक अपने निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त अवश्य कर लेता है। इसमें तीर्थंकर मात्र मार्गदृष्टा है, प्रदीप के समान, वह निर्वाणदाता नहीं। इसलिये व्यक्ति के स्वयं का पुरुषार्थ ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। ईश्वर की कृपा से उसका कोई संबंध नहीं। पराश्रय से विकास अवरूद्ध हो जाता है । बैसाखी का सहारा स्वयं का सहारा नहीं माना जा सकता । अतः जैनधर्म में व्यक्ति का कर्म और उसका पुरुषार्थ ही प्रमुख है। Jain Education International (११८) For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10