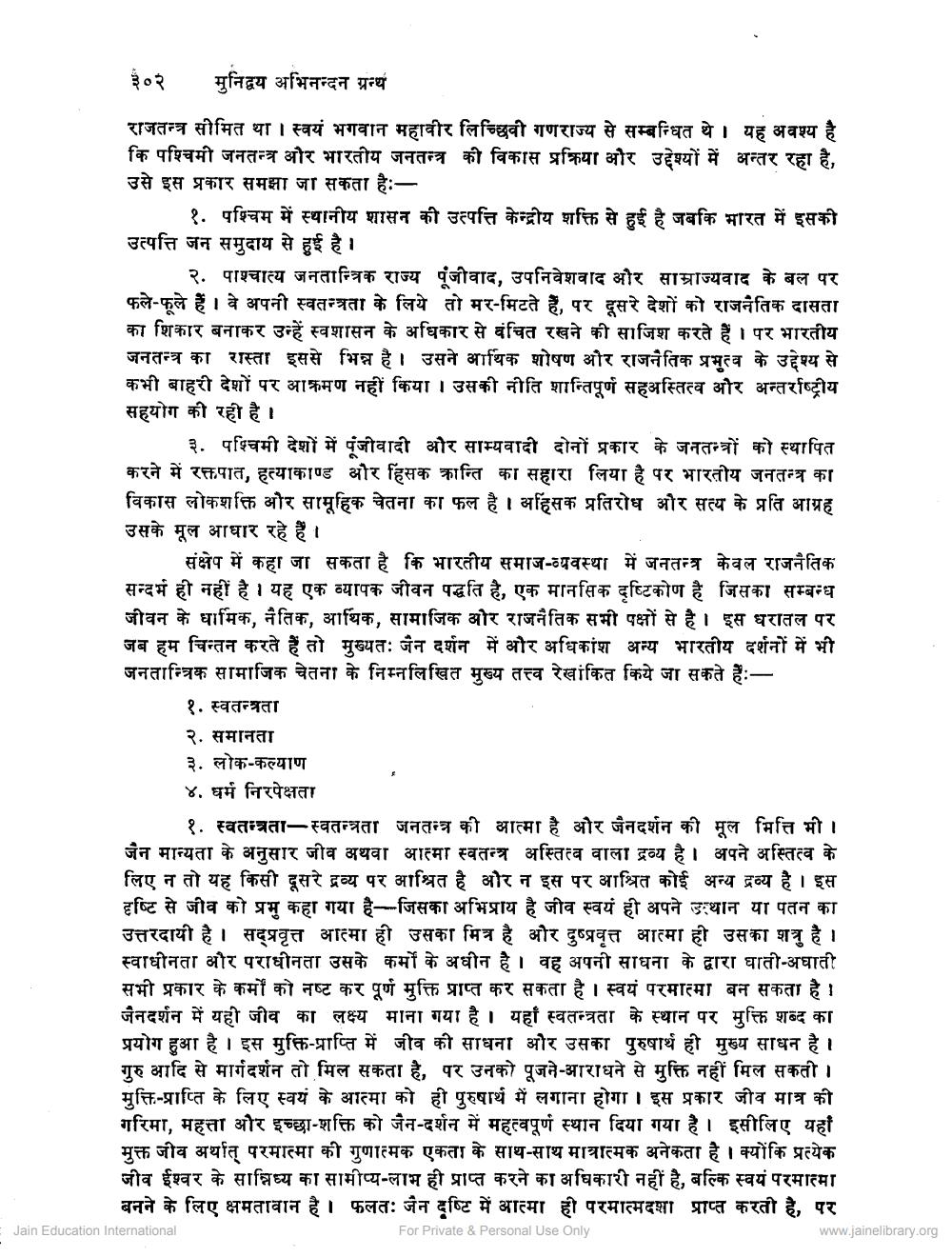Book Title: Jain Darshan me Jan tantrik Samajik Chetna ke Tattva Author(s): Narendra Bhanavat Publisher: Z_Munidway_Abhinandan_Granth_012006.pdf View full book textPage 2
________________ ३०२ मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रन्थ राजतन्त्र सीमित था। स्वयं भगवान महावीर लिच्छिवी गणराज्य से सम्बन्धित थे। यह अवश्य है कि पश्चिमी जनतन्त्र और भारतीय जनतन्त्र की विकास प्रक्रिया और उद्देश्यों में अन्तर रहा है, उसे इस प्रकार समझा जा सकता है: १. पश्चिम में स्थानीय शासन की उत्पत्ति केन्द्रीय शक्ति से हई है जबकि भारत में इसकी उत्पत्ति जन समुदाय से हुई है। २. पाश्चात्य जनतान्त्रिक राज्य पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बल पर फले-फूले हैं। वे अपनी स्वतन्त्रता के लिये तो मर-मिटते हैं, पर दूसरे देशों को राजनैतिक दासता का शिकार बनाकर उन्हें स्वशासन के अधिकार से वंचित रखने की साजिश करते हैं। पर भारतीय जनतन्त्र का रास्ता इससे भिन्न है। उसने आर्थिक शोषण और राजनैतिक प्रभुत्व के उद्देश्य से कभी बाहरी देशों पर आक्रमण नहीं किया। उसकी नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की रही है। ३. पश्चिमी देशों में पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों प्रकार के जनतन्त्रों को स्थापित करने में रक्तपात, हत्याकाण्ड और हिंसक क्रान्ति का सहारा लिया है पर भारतीय जनतन्त्र का विकास लोकशक्ति और सामूहिक चेतना का फल है। अहिंसक प्रतिरोध और सत्य के प्रति आग्रह उसके मूल आधार रहे हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय समाज-व्यवस्था में जनतन्त्र केवल राजनैतिक सन्दर्भ ही नहीं है। यह एक व्यापक जीवन पद्धति है, एक मानसिक दृष्टिकोण है जिसका सम्बन्ध जीवन के धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी पक्षों से है। इस धरातल पर जब हम चिन्तन करते हैं तो मुख्यतः जैन दर्शन में और अधिकांश अन्य भारतीय दर्शनों में भी जनतान्त्रिक सामाजिक चेतना के निम्नलिखित मुख्य तत्त्व रेखांकित किये जा सकते हैं: १. स्वतन्त्रता २. समानता ३. लोक-कल्याण ४. धर्म निरपेक्षता १. स्वतन्त्रता-स्वतन्त्रता जनतन्त्र की आत्मा है और जैनदर्शन की मूल भित्ति भी। जैन मान्यता के अनुसार जीव अथवा आत्मा स्वतन्त्र अस्तित्व वाला द्रव्य है। अपने अस्तित्व के लिए न तो यह किसी दूसरे द्रव्य पर आश्रित है और न इस पर आश्रित कोई अन्य द्रव्य है। इस दृष्टि से जीव को प्रभु कहा गया है जिसका अभिप्राय है जीव स्वयं ही अपने उत्थान या पतन का उत्तरदायी है। सद्प्रवृत्त आत्मा ही उसका मित्र है और दुष्प्रवृत्त आत्मा ही उसका शत्रु है । स्वाधीनता और पराधीनता उसके कर्मों के अधीन है। वह अपनी साधना के द्वारा घाती-अघाती सभी प्रकार के कर्मों को नष्ट कर पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकता है। स्वयं परमात्मा बन सकता है। जैनदर्शन में यही जीव का लक्ष्य माना गया है। यहाँ स्वतन्त्रता के स्थान पर मुक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। इस मुक्ति-प्राप्ति में जीव की साधना और उसका पुरुषार्थ ही मुख्य साधन है। गुरु आदि से मार्गदर्शन तो मिल सकता है, पर उनको पूजने-आराधने से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति-प्राप्ति के लिए स्वयं के आत्मा को ही पुरुषार्थ में लगाना होगा। इस प्रकार जीव मात्र की गरिमा, महत्ता और इच्छा-शक्ति को जैन-दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसीलिए यहां मुक्त जीव अर्थात् परमात्मा की गुणात्मक एकता के साथ-साथ मात्रात्मक अनेकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव ईश्वर के सान्निध्य का सामीप्य-लाभ ही प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा बनने के लिए क्षमतावान है। फलतः जैन दृष्टि में आत्मा ही परमात्मदशा प्राप्त करती है, पर Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7