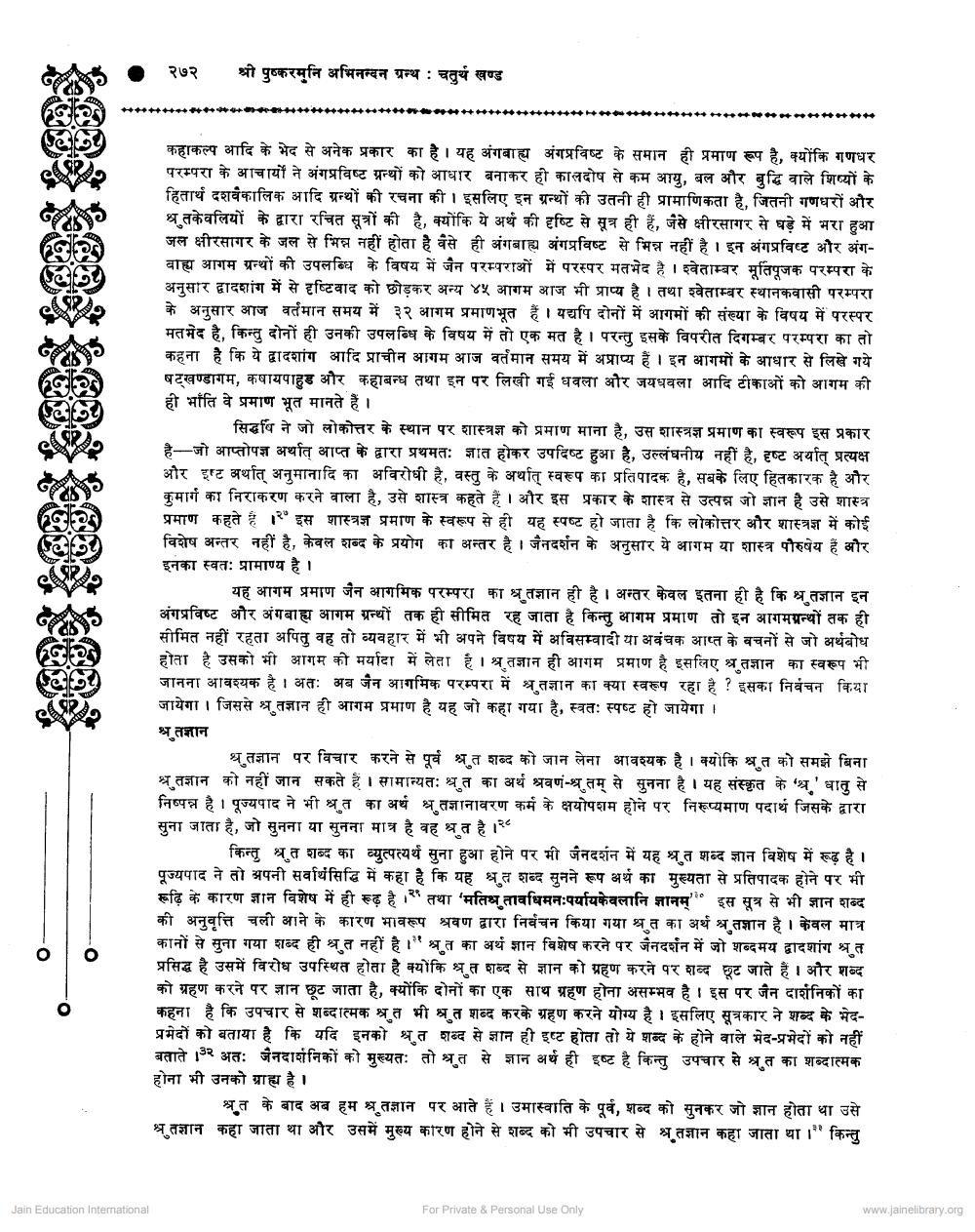Book Title: Jain Darshan me Agam Praman Author(s): Harindrabhushan Jain Publisher: Z_Pushkarmuni_Abhinandan_Granth_012012.pdf View full book textPage 4
________________ -O ७. ० Jain Education International २७२ श्री पुष्करमूनि अभिनन्दन ग्रन्थ चतुर्थखण्ड कहाकल्प आदि के भेद से अनेक प्रकार का है । यह अंगबाह्य अंगप्रविष्ट के समान ही प्रमाण रूप है, क्योंकि गणधर परम्परा के आचार्यों ने अंगप्रविष्ट ग्रन्थों को आधार बनाकर ही कालदोष से कम आयु, बल और बुद्धि वाले शिष्यों के हितार्थं दशवेकालिक आदि ग्रन्थों की रचना की । इसलिए इन ग्रन्थों की उतनी ही प्रामाणिकता है, जितनी गणधरों और अतकेवलियों के द्वारा रचित सूत्रों की है, क्योंकि ये अर्थ की दृष्टि से मूत्र ही हैं, जैसे क्षीरसागर से पड़े में मरा हुआ जल क्षीरसागर के जल से भिन्न नहीं होता है वैसे ही अंगबाह्य अंगप्रविष्ट से भिन्न नहीं है। इन अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य आगम ग्रन्थों की उपलब्धि के विषय में जैन परम्पराओं में परस्पर मतभेद है । श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा के अनुसार द्वादशांग में से दृष्टिवाद को छोड़कर अन्य ४५ आगम आज भी प्राप्य है । तथा श्वेताम्बर स्थानकवासी परम्परा के अनुसार आज वर्तमान समय में ३२ आगम प्रमाणभूत हैं । यद्यपि दोनों में आगमों की संख्या के विषय में परस्पर मतभेद है, किन्तु दोनों ही उनकी उपलब्धि के विषय में तो एक मत है । परन्तु इसके विपरीत दिगम्बर परम्परा का तो कहना है कि ये द्वादशांग आदि प्राचीन आगम आज वर्तमान समय में अप्राप्य हैं। इन आगमों के आधार से लिखे गये षट्खण्डागम, कषायपाहुड और कहाबन्ध तथा इन पर लिखी गई धवला और जयधवला आदि टीकाओं को आगम की ही भाँति वे प्रमाण भूत मानते हैं । सिद्धर्षि ने जो लोकोत्तर के स्थान पर शास्त्रज्ञ को प्रमाण माना है, उस शास्त्रज्ञ प्रमाण का स्वरूप इस प्रकार है - जो आप्तोपज्ञ अर्थात् आप्त के द्वारा प्रथमतः ज्ञात होकर उपदिष्ट हुआ है, उल्लंघनीय नहीं है, दृष्ट अर्थात् प्रत्यक्ष और इष्ट अर्थात् अनुमानादि का अविरोधी है, वस्तु के अर्थात् स्वरूप का प्रतिपादक है, सबके लिए हितकारक है और कुमार्ग का निराकरण करने वाला है, उसे शास्त्र कहते हैं। और इस प्रकार के शास्त्र से उत्पन्न जो ज्ञान है उसे शास्त्र प्रमाण कहते हैं । २° इस शास्त्रज्ञ प्रमाण के स्वरूप से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकोत्तर और शास्त्रज्ञ में कोई विशेष अन्तर नहीं है, केवल शब्द के प्रयोग का अन्तर है। जैनदर्शन के अनुसार ये आगम या शास्त्र पौरुषेय हैं और इनका स्वतः प्रामाण्य है । यह आगम प्रमाण जैन आगमिक परम्परा का श्रुतज्ञान ही है । अन्तर केवल इतना ही है कि श्रुतज्ञान इन अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य आगम ग्रन्थों तक ही सीमित रह जाता है किन्तु आगम प्रमाण तो इन आगमग्रन्थों तक ही सीमित नहीं रहता अपितु वह तो व्यवहार में भी अपने विषय में अविसम्वादी या अवंचक आप्त के वचनों से जो अर्थबोध होता है उसको भी आगम की मर्यादा में लेता है। श्रुतज्ञान ही आगम प्रमाण है इसलिए श्रुतज्ञान का स्वरूप भी जानना आवश्यक है। अतः अब जैन आगमिक परम्परा में श्रुतज्ञान का क्या स्वरूप रहा है ? इसका निर्वाचन किया जायेगा । जिससे श्रुतज्ञान ही आगम प्रमाण है यह जो कहा गया है, स्वतः स्पष्ट हो जायेगा । [तज्ञान श्रुतज्ञान पर विचार करने से पूर्व श्रुत शब्द को जान लेना आवश्यक है । क्योकि श्रुत को समझे बिना श्रुतज्ञान को नहीं जान सकते हैं। सामान्यतः श्रुत का अर्थ श्रवणं श्रुतम् से सुनना है । यह संस्कृत के 'श्र' धातु से निष्पन्न है । पूज्यपाद ने भी श्रुत का अर्थ श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर निरूप्यमाण पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनना या सुनना मात्र है वह श्रुत है ।२८ किन्तु श्रुत शब्द का व्युत्पत्यर्थं सुना हुआ होने पर भी जनदर्शन में यह श्रुत शब्द ज्ञान विशेष में रूढ़ है । पूज्यपाद ने तो अपनी सर्वार्थसिद्धि में कहा है कि यह श्रुत शब्द सुनने रूप अर्थ का मुख्यता से प्रतिपादक होने पर भी रूढ़ि के कारण ज्ञान विशेष में ही रूढ़ है ।" तथा 'मति तावधिमनः पर्यायकेवलानि ज्ञानम् २० इस सूत्र से भी ज्ञान शब्द की अनुवृत्ति चली आने के कारण भावरूप श्रवण द्वारा निर्वचन किया गया श्रुत का अर्थ श्रुतज्ञान है । केवल मात्र कानों से सुना गया शब्द ही श्रुत नहीं है ।" श्रुत का अर्थ ज्ञान विशेष करने पर जैनदर्शन में जो शब्दमय द्वादशांग श्रत प्रसिद्ध है उसमें विरोध उपस्थित होता है क्योंकि श्रुत शब्द से ज्ञान को ग्रहण करने पर शब्द छूट जाते हैं । और शब्द को ग्रहण करने पर ज्ञान छूट जाता है, क्योंकि दोनों का एक साथ ग्रहण होना असम्भव है। इस पर जैन दार्शनिकों का कहना है कि उपचार से शब्दात्मक श्रुत भी श्रुत शब्द करके ग्रहण करने योग्य है । इसलिए सूत्रकार ने शब्द के भेदप्रमेदों को बताया है कि यदि इनको श्रुत शब्द से ज्ञान ही इष्ट होता तो ये शब्द के होने वाले भेद-प्रभेदों को नहीं बताते 132 अतः जैनदार्शनिकों को मुख्यतः तो श्रुत से ज्ञान अर्थ ही इष्ट है किन्तु उपचार से श्रुत का शब्दात्मक होना भी उनको ग्राह्य है । श्रुत के बाद अब हम श्रुतज्ञान श्रुतज्ञान कहा जाता था और उसमें मुख्य पर आते हैं । उमास्वाति के पूर्व शब्द को सुनकर जो ज्ञान होता था उसे कारण होने से शब्द को भी उपचार से श्रुतज्ञान कहा जाता था ।" किन्तु For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9